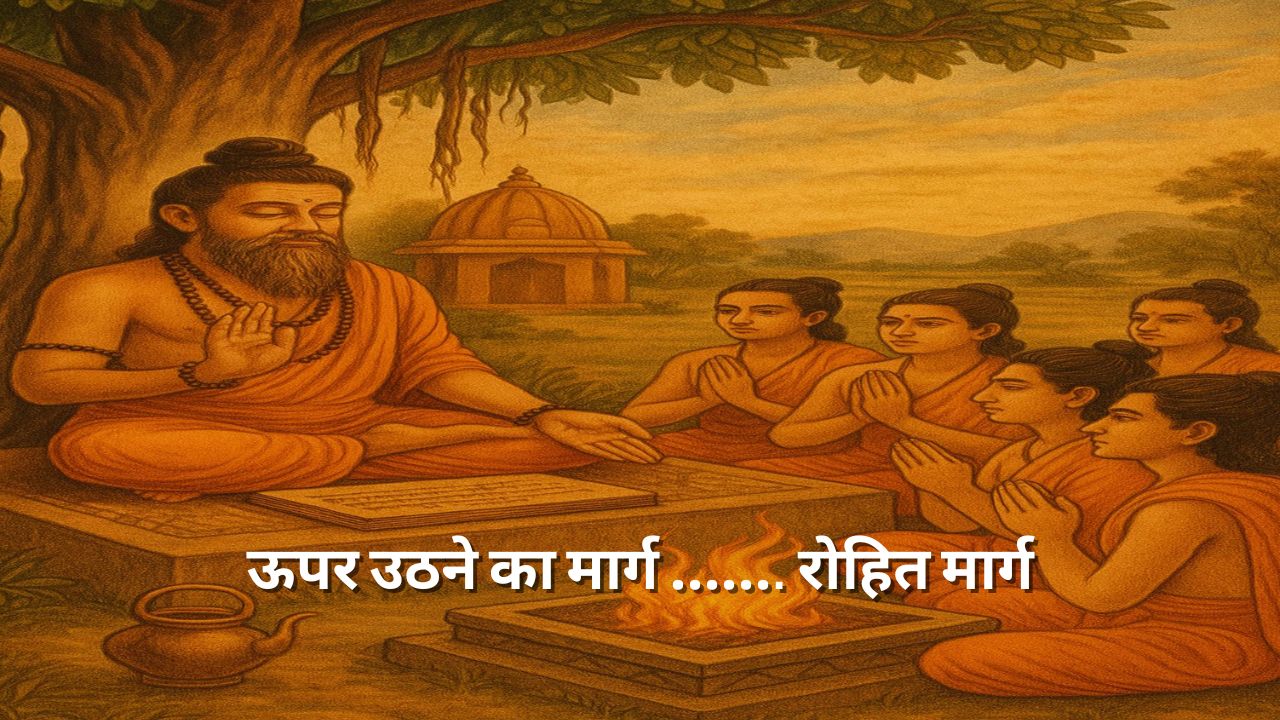- मिस्टिक ज्ञान
- |
- 31 October 2024
- |
- 0 Comments
अरुण कुमार उपाध्याय (धर्मज्ञ)
(१) रोहित कथा- सूर्यवंश के राजा इक्ष्वाकु (८५७६ ईपू में अभिषेक) की ३१ पीढ़ी बाद सत्यव्रत के पुत्र हरिश्चन्द्र हुए। उनसे ११ पीढ़ी पूर्व मान्धाता के राज्य में हर समय कहीं सूर्य का उदय, कहीं अस्त होता था। इस कथा को ब्रिटिश राज्य ने अपने लिए प्रसिद्ध किया। मान्धाता १५वें त्रेता (८१४२-७७८२ ई.पू) में थे। उनकी १८ पीढ़ी बाद राजा बाहु यवन आक्रमण में मारा गया। यह आक्रमण डायोनिसस या बाक्कस ने किया था जिसकी तिथि भारतीय लेखों के आधार पर मेगास्थनीज ने ६७७७ ईपू अप्रैल में दी है। बाहु से ७ पीढ़ी पूर्व अर्थात् प्रायः७३०० ईपू. में हरिश्चन्द्र हुए।
ब्रह्म पुराण, के द्वितीय खण्ड गौतमी माहात्म्य, अध्याय ३४ में कथा है कि राजा हरिश्चन्द्र के पुत्र नहीं हो रहा था तो उन्होंने गौतमी तट पर वरुण की पूजा की। वरुण ने कहा कि यदि पुत्र द्वारा वरुण का यज्ञ करें तो तीनों लोकों में विभूषित पुत्र दूंगा। इसके बाद उनको रोहित नामक पुत्र हुआ। पुत्र होते ही वरुण ने यज्ञ के लिए कहा। राजा ने कहा दांत निकलने पर यज्ञ करूंगा। दांत निकलने पर कहा कि सभी दांत निकलें तब करूंगा। ६ वर्ष के बाद कहा कि ये दांत टूट कर पुनः जमेंगें तब यज्ञ करूंगा। उसके बाद कहा कि क्षत्रिय धर्म से धनुर्वेद की शिक्षा लेने के बाद यज्ञ करूंगा। विद्वान् होने के बाद युवराज हो गया तो पुनः वरुण ने यज्ञ के लिए कहा।
तब रोहित ने कहा कि वरुण को ही यज्ञ पशु बना कर विष्णु का यज्ञ करूंगा। इस पर वरुण क्रुद्ध हो गये तथा हरिश्चन्द्र को जलोदर का रोगी बना दिया। रोहित घर से चला गया। पिता के रोग की बात सुन कर वह लौटने लगा तो बार बार इन्द्र उसे समझा कर रोक देते थे। इस प्रकार ६ वर्ष में ६ बार रोका। सातवें वर्ष में रोहित ने अजीगर्त मुनि के मध्यम पुत्र शुनःशेप को खरीदा तथा उसे यज्ञ पशु रूप में लाया। उसे लेकर हरिश्चन्द्र वसिष्ठ विश्वामित्र, वामदेव आदि ऋषियों के साथ गौतमी तट पर पहुंचे। हरिश्चन्द्र इसके लिए तैयार नहीं थे क्योंकि राजा प्रजा का रक्षक होता है। पर ऋषियों की सलाह पर वे गौतमी तट पर गये। विश्वामित्र की प्रार्थना पर बिना बलि के ही यज्ञ सम्पूर्ण हुआ तथा विश्वामित्र ने शुनःशेप को अपना ज्येष्ठ पुत्र स्वीकार किया। जिन पुत्रों ने शुनःशेप को बड़ा भाई नहीं माना उनको घर से निकाल दिया।
प्रायः यही कथा भागवत पुराण, स्कन्ध ९, अध्याय ७, तथा ऐतरेय ब्राह्मण, अध्याय ३१में है। ऋग्वेद (१/२४) में शुनःशेप ऋषि के मन्त्र हैं।
(२) जलोदर चिकित्सा-इस कथा में एक विरोधाभास है कि वरुण ने आशीर्वाद दिया था कि उनके आशीर्वाद से जो पुत्र होगा वह तीनों लोकों में अपने गुण के कारण विख्यात होगा। यदि जन्म लेते ही उसकी बलि लेते तो वह विख्यात कैसे होता तथा इस पुत्र जन्म के आशीर्वाद का कोई अर्थ नहीं है। यहां रोहित की बलि का अर्थ है जलोदर रोग की चिकित्सा के लिए रोहितक का प्रयोग होता है जो यकृत की बीमारी दूर करता है।
इसे गुजरात में रक्त या रगट रोहिड (रोहेड़ा, Tecomella undulata, Tecoma) कहते हैं। कुछ अन्य वनस्पतियों को भी रक्त रोहिड कहते हैं जो जलोदर की चिकित्सा में विकल्प रूप से व्यवहार होती हैं-Polygonum glabrum, Myristica attenuta, Knema attenuata। अधिकांश आयुर्वेद ग्रन्थों में जलोदर चिकित्सा के लिए रोहितक छाल के क्वाथ या रोहितक घृत के प्रयोग का वर्णन है। वेद में इसे अप्वा कहा गया है।
अथर्व वेद के अनुसार असत्य भाषण एवं दुराचार से जलोदर (अप्वा) होता है। हरिश्चन्द्र को भी असत्य भाषण के बाद यह रोग हुआ था।
अप्वा (जलोदर)- अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्गानि अप्वे परेहि।
अभि प्रेहि निर्दह हत्सु शोकैरन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम् (ऋक्, १०/१०३/१२)
अमीषां चित्तानि प्रतिमोहयन्ती गृहाणाङ्गानि अप्वे परेहि।
अभि प्रेहि निर्दह हृत्सु शोकैर्ग्राह्यामित्रां स्तमसा विध्य शत्रून्॥ (अथर्व, ३/२५)
हरिमाणं ते अङ्गेभ्यो अप्वां अन्तरोदरात्।
यक्ष्मोधामनरात्मनो बहिर्निर्मन्त्रयामहे॥
(अथर्व, ९/१३/९-या ९/६, पर्याय ६/९) चरक संहिता, चिकित्सा स्थान, अध्याय १३-
स्नेहपित्तस्य मन्दाग्नेः क्षीणस्यातिकृशस्य वा।
अत्यम्बुपानान्नष्ट्ऽग्नौ मारुतः क्लोम्नि संस्थितः॥४५॥
स्रोतःसु रुद्धमार्गेषु कफश्चोदकमूच्छितः।
वर्धयेता यदेवाम्बु स्वस्थानादुदराय तौ॥४६॥
तस्य रूपाणि-अनन्नकाङ्क्षा-पिपासा-गुदस्राव-शूल-श्वास-कास-दौर्बल्यान्यपि चोदरं नाना वर्ण राजि सिरा सन्ततमुदक पूर्ण दृति क्षोभ संस्पर्श भवति, एतदुदकोदरं विद्यात्॥४७॥
चिकित्सा-रोहीतकलतानां तु काण्डकामभयाजले।
मूत्रे वा सुनुयात्तच्च सप्तरात्रिस्थित पिबेत्॥८१॥
कामला गुल्ममेहार्शः प्लीहसर्वोदरक्रिमीन्।
तद्धन्याज्जाङ्गलरसैर्जीर्णे स्याच्चात्र भोजनम्॥८२॥
रोहितक घृत-रोहीतकत्वचः कृत्वा पलानां पञ्चविंशतिम्।
कोलद्विप्रस्थसंयुक्तं कषायमुपकल्पयेत्॥८३॥
पालिकैः पञ्चकौलैस्तु तैः सर्वैश्चापि तुल्यया।
रोहीतकत्वचा पिष्टैर्घृतप्रस्थं विपाचयेत्॥८४॥
(३) अब्राहम कथा-दक्षिण ईराक के उर नगर में अब्राहम रहते थे। (यहूदी तोरा, बाइबिल के जेनेसिस के अध्याय ११, १५, १६, १७, २१, २५)। उन्को भी सन्तान नही हो रही थी तथा उनकी पत्नी सारा की आयु ७५ वर्ष हो गयी थी। भगवान् की पूजा से मिस्र की दासी हगर से उनको इस्माइल नामक पुत्र हुआ जिसके बारे में कहा कि वह महान् राजा होगा तथा उसके १२ पुत्र होंगे। इसके बाद सारा उस पर अत्याचार करने लगी तो वह भाग कर इजरायल चली गयी। अब्राहम भी उसके साथ बीर शेबा में रहने लगे।
भगवान् ने इस्माइल की बलि देने के लिए कहा। बलि के लिए उसे खूंटे से बान्धा गया, तब देवदूत ने कहा कि इसके बदले भेड़ की बलि दो। यहां भी बलि देने का आदेश भगवान् के आशीर्वाद का उलटा है। यदि महान् पुत्र तथा उससे बहुत सन्तान होने के बारे में कहा था, तो वह बलि देने से कैसे पूरा होगा?
शुनःशेप सूक्त में भी उल्लेख है कि राजा वरुण ने उरु (ऊर) नगर बनाया था-
उरुं हि राजा वरुण श्चकार (ऋग्वेद, १/२४/८)।
शिल्प शास्त्र के अनुसार विष्णु ने उरु डिजाइन का नगर बनाया था-शं नो विष्णुरुरुक्रमः (ऋग्वेद, १/९०/१) दक्षिण भारत के अधिकांश नगर उरु या उर हैं-बंगलूर, मंगलूर, तंजाउर, नेल्लूर, चित्तूर। यह गोलाकार नगर है, जिसमें बीच का भाग सबसे ऊंचा होगा।
इसमाइल के १२ पुत्रों से अरब की १२ जातियां हुयीं जिनको ईसा की १२ भेड़ (अनुयायी) भी कहते हैं। इस्लाम में कुछ लोगों का मत है कि पैगम्बर मुहम्मद ही पूर्व जन्म में इस्माइल थे। इस बलि को ही बकरीद कहते हैं।
(४) बकरीद-पूजा के लिए भगवान् को सांकेतिक अर्पण बकरीद है। ईद = पूजा, संस्कृत का ईळे (ऋग्वेद प्रथम मन्त्र-अग्निमीळे पुरोहितम्)। पूजा के लिए कुछ देना पड़ता है। यह सांकेतिक रूप से देते हैं, क्योंकि हर वस्तु भगवान् की ही है। बकर के २ अर्थ हैं। भगवान् अर्थ में बकरीद का अर्थ भगवान् की पूजा है। तुर्की में बकर का अर्थ गौ है। वहां के लिए बकरीद का अर्थ होगा गौ की पूजा (कुरान, अल बकरा, सूरा १३१)।
अरब में बकर का अर्थ भेड़ या अन्य चौपाया है। भारत में इसका अर्थ अज या बकरा हो गया। संस्कृत में भी अज के २ अर्थ हैं-अजन्मा ब्रह्म या बकरा। ब्रह्म निर्माण के लिए अज (पुरुष) तथा अजा (३ गुणों की प्रकृति) रूप में विभाजित होता है। क्रिया रूपी नर के रूप में इसे वैश्वानर कहते हैं जो मनुष्य के भीतर अन्नों को पचाता है। वैश्वानर का अर्थ बकरा भी है जो सदा खाता रहता है।
अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः।
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते, जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः॥५॥
(श्वेताश्वतर उपनिषद्, ४/५, ऋग्वेद, १/१६४/२०, अथर्व, ९/१४/२०) = ३ गुणों की प्रकृति (३ रंगों की अजा) से बहुत सी प्रजा हुई। अज (पुरुष, ब्रह्म) भोगों तथा कर्मों को छोड़ देता है। इसी मन्त्र से वाचस्पति मिश्र ने सांख्य दर्शन की व्याख्या आरम्भ की है।
अज-अजा को व्यक्ति स्तर पर आत्मा जीव या बाइबिल में आदम-ईव कहा है, जिनसे सृष्टि होती है। यहां जहाति का अर्थ मारना है। द्रष्टा रूप पुरुष कर्म में वासना को मारता है। जहाति का यही अर्थ अरबी में भी है। पर वहां उसका अर्थ करते हैं, अपने सम्प्रदाय को नहीं मानने वालों की हत्या। जीवों के भीतर वैश्वानर या अज भोजन को पचाता है-
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्॥ (गीता, १५/१४)
(५) नरमेध-यज्ञ में बलि का अर्थ हत्या या sacrifice करते हैं। यज्ञ का अर्थ विनाश नहीं, निर्माण है। सभ्यता के आरम्भ में ही प्रजापति ने कहा था कि यज्ञ द्वारा अपनी जरूरी चीजों का उत्पादन करो। निर्माण के लिए उतना ही भाग लगेगा जितना जरूरी है। निर्माण के साधन की हत्या नहीं करनी है। यज्ञ चक्र चलता रहेगा तभी जरूरी चीजें मिलेंगी तथा मनुष्य सभ्यता चलती रहेगी। उससे बचा हुआ भाग ही खाना है। यज्ञ चलते रहने से वह सदा मिलता रहेगा, अतः इसे अमृत कहा गया है।
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरो वाच प्रजापतिः ।
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥१०॥ (गीता, अध्याय ३)
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ॥१३॥
एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः ।
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥१६॥
यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्।
(गीता, ४/३१) संसार का निर्मित रूप विश्व है, क्रिया या गति रूप जगत् है, चक्रीय क्रम में निर्माण जगत्यां जगत् है। उससे बचा हुआ ही उपभोग करना चाहिये जिससे यज्ञ चलता रहे। यह यज्ञों के सारांश रूप में यजुर्वेद के अन्तिम अध्याय में कहा है-
ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। (ईशावायोपनिषद्, १)
किसी की भी बलि का अर्थ है, उसके उत्पाद को ग्रहण किया जाय जितना वह लगातार दे सकता है। गो का दूध घी आदि उत्पाद लेते हैं, उसे मारने से स्रोत ही नष्ट हो जायेगा। बैल से खेती होती है। अनादि काल से गो पर ही सभ्यता टिकी हुई है, अतः उसे यज्ञ का पर्याय माना गया है जिसे मारना निषिद्ध है।
यजुर्वेद के प्रथम मन्त्र में ही गो को अघ्न्या कहा गया है। नरमेध का भी यही अर्थ है कि मनुष्य को सक्षम किया जाय जिससे वह अपने को तथा समाज को कुछ दे सके। इसी अर्थ में वरुण ने रोहित की बलि के लिए कहा था। व्यक्ति शिक्षा के लिए अपने को समर्पित करेगा तभी गुणी बन सकता है, जैसा वरुण ने पुत्र जन्म के आशीर्वाद के समय कहा था।
गुरु के पास शिक्षा के लिए कोई जाता है, तो गुरु उसका आलभन करते है। इस क्रिया को सभी पशुओं की शमिता (शान्त करना) कहते हैं। आलभन का अर्थ किया जाता है कि पशु या मनुष्य को छूकर देखते हैं कि कहां से उसे काटा जाय कि वह शान्त या मृत हो जाय। मरने के बाद न कोई शिक्षा हो सकती है, न पशु का लगातार उपयोग।
आन्तरिक यज्ञ है कि हृदय से निकली १०० नाड़ियों को छोड़ कर केवल सुषुम्ना मार्ग से जायें तब मुक्ति होती है। इसे शतौदना गौ का दान कहा गया है। शत्ं चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसृतैका।
तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति, विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्ति॥ (कठोपनिषद्, २/३/१६)
हिरण्यं ज्योतिषं कृत्वा यो ददाति शतौदनाम्।
यो ते देवि शमितारः पक्तारो ये च ते जनाः॥ (अथर्व, १०/९/७)
देव, माता-पिता आदि को शमिता कहा गया है। निश्चित रूप से वे अपने बच्चों को नहीं मारेंगे।
दैव्याः शमितार उत मनुष्या आरभध्वम्।
उपनयत् मेध्या दुरः।
अन्वेनं माता मनयताम्। अनुं पिता। … उदीचीनां अस्य पदो निधत्तात्। … अध्तिगो शमीध्वं शमीध्वमध्रिगो। अध्रिगुश्चापापश्च उभौ शमितारौ॥ (तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३/६/६/४)
कृषि के लिए बीज डालते हैं, इसी प्रकार किसी भी यज्ञ में निर्माण के लिए जो बीज डालते हैं, उसे अज कहा गया है, उसके लिए छाग की बलि नहीं दी जाती है-
बीजैर्यज्ञेषु यष्टव्यमिति वै वैदिकी श्रुतिः। अज संज्ञानि बीजानि च्छागं नो हन्तुमर्हथ॥ (महाभारत, शान्ति पर्व, ३३७/४) (५)
रोहित मार्ग-इसका मूल है-रुह् बीज जन्मनि प्रादुर्भावे च (धातुपाठ, १/५९८)-बीज का उगना, उससे वृक्ष का जन्म, उत्पन्न होना, प्रकट होना। इसमें उपसर्ग से ४ प्रकार के अर्थ हैं-अधिरोह-ऊपर चढ़ना, आरोहण। अवरोह-नीचे उतरना। आरोह-ऊपर चढ़ना या बैठना। प्ररोह-उगना, अङ्कुर उत्पन्न होना। पुरुष सूक्त में ब्रह्म से सृष्टि का उत्पन्न होना मूल से विश्व निर्माण के स्तर हैं।
स्थूल विश्व से सूक्ष्म का अनुमान अतिरोहण है-यदन्नेनातिरोहति (पुरुष सूक्त, २) नीचे से उठने की सभी क्रियायें रोहित हैं-भूमि में बीज से धान्य आदि का अंकुरण, सूर्य स्रोत से द्युलोक तथा पृथ्वी का निर्माण, पार्थिव पदार्थों से पशु, मनुष्य की उत्पत्ति।
रोहिता इव वै ब्रीहयो रोहित इवायं (पृथिवी) लोको, रोहित इवासौ (द्यु लोकः)-काठक ब्राह्मण (१२/४)
एतद् वा आसां (गवाम्) बीजं यद् रोहितं रूपम् (मैत्रायणी ब्राह्मण, ४/२/१४)
रोहित वह क्रम या छन्द है, जिससे इन्द्र ७ स्वर्ग लोकों तक क्रमशः ऊपर उठते हैं।
रोहितं वै नामैतच्छन्दो यत् पारुच्छेपमेतेन वा इन्द्रः सप्त स्वर्गाल्लोकानरोहत्। (ऐतरेय ब्राह्मण, ५/१०)
हर छन्द या माप के बाद कुछ रुकना है, उसके बाद अगला छन्द आरम्भ होगा। यह विभाजन काण्ड है। बांस के स्तम्भ में कई गांठ होती है। मनुष्यों का क्रम भी काण्डों के अनुसार बढ़ता है, पिता से पुत्र, तब पौत्र आदि। अतः दोनों को वंश या कुल कहते हैं (ओड़िशा में बांस से बने सूप को कूला कहते हैं)।
मनुष्य के मेरुदण्ड में भी ३३ गांठ है, सुषुम्ना के चक्रों के अनुसार ७ गांठ है। यह आकाश के ७ लोकों की प्रतिमा है। इन्द्र रूपी तेज भूलोक में सबसे कम है। अगले लोकों में जैसे जैसे पदार्थ का घनत्वकम होता है, इन्द्र तेज का अनुपात बढ़ता जाता है। यह ७ स्वर्गों का आरोहण है। मनुष्य जीवन भी काण्डों से विभक्त है।
कक्षा १ के बाद २ में, उसके बाद ३, ४, ५ आदि में। उसके बाद विवाह, व्यवसाय, स्थान परिवर्तन आदि कई प्रकार के काण्ड या गांठ हैं। हमारा उद्देश्य है कि हर काण्ड से आगे बढ़ते रहें। इसके लिये प्रतीक है बांस। किन्तु उतनी बड़ी वस्तु का अर्पण नही होता है, अतः उसके छोटे रूप दूर्वा का अर्पण करते हैं। इसकी कोई गांठ जहां भी जमीन से लगती है, वहां से नयी दूर्वा आरम्भ हो जाती है। अतः अपनी उन्नति कामना के लिए दूर्वा देते हैं तथा मन्त्र पढ़ते हैं कि जैसे दूर्वा हर काण्ड से बढ़ती है, वैसे ही हमारी हर काण्ड से उन्नति हो।
काण्डात् काण्डात् प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि।
एवा नो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च। (वाज.सं. १३/२०, तैत्तिरीयसं. ४/२/९/२, काण्व सं. १६/१६, मैत्रायणी संहिता, २४/१९, शतपथ ब्राह्मण, ७/४/२/१४) इसका तथा पुरुष सूक्त (२) का आध्यात्मिक अर्थ है कि हम सुषुम्ना मार्ग पर मूलाधार से क्रमशः ऊपर उठते हुए ७वें सहस्रार चक्र में परमात्मा से साक्षात्कार करें।
महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहम्, स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि।
मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथम्, सहस्रारे पद्मे सह रहसि पत्या विहरसि (विहरसे)-सौन्दर्य-लहरी,
९ ७ चक्र शरीर के ७ कोषों के केन्द्र हैं-
अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय, चित्तमय, आत्मामय। तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा। (योग सूत्र, २/२७) महोपनिषद्, अध्याय ५-
अज्ञान भूः सप्त पदाज्ञभूः सप्त पदैव हि॥१॥
प्रश्नोपनिषद् में यह ६ प्रश्नों के उत्तर रूप में समझाया गया है। भागवत माहात्म्य में शरीर के ७ चक्रों के प्रतीक रूप में ७ गांठ का बांस रखा गया था। मनुष्य का गुरु या परमात्मा से सम्बन्ध विन्दु चक्र से है। इसे मिला कर अथर्व वेद में ८ चक्र तथा शरीर के ९ छिद्रों को ९ द्वार कहा है। अष्टा चक्रा नव द्वारा देवानां पूरयोध्या (अथर्व, १०/२/२१) (६)
त्याग मार्ग-जो हमारी जरूरत से अधिक है उसी का त्याग करते हैं। गौ, वृक्ष आदि जिसका लगातार उत्पादन करते हैं, वही दे सकते हैं। इसी प्रकार हर व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार परिवार के लिए कुछ देता है। परिवार से बचा कर कुछ समाज को दिया जाता है। समाज से बचा कर देश को देते हैं। हर देश विश्व सभ्यता बचाने के लिए अन्य देशों को कुछ दे रहा है तथा अपनी जरूरत की चीजें ले रहा है। यह ४ स्तर का दान है। आध्यात्मिक रूप से मोक्ष के लिए विषयों का इन्द्रिय में, इन्द्रियों का मन में, मन का आत्मा तथा आत्मा का परमात्मा में लय होता है। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते॥ (गीता २/२७)
Related Posts
0 Comments
Comments are not available.