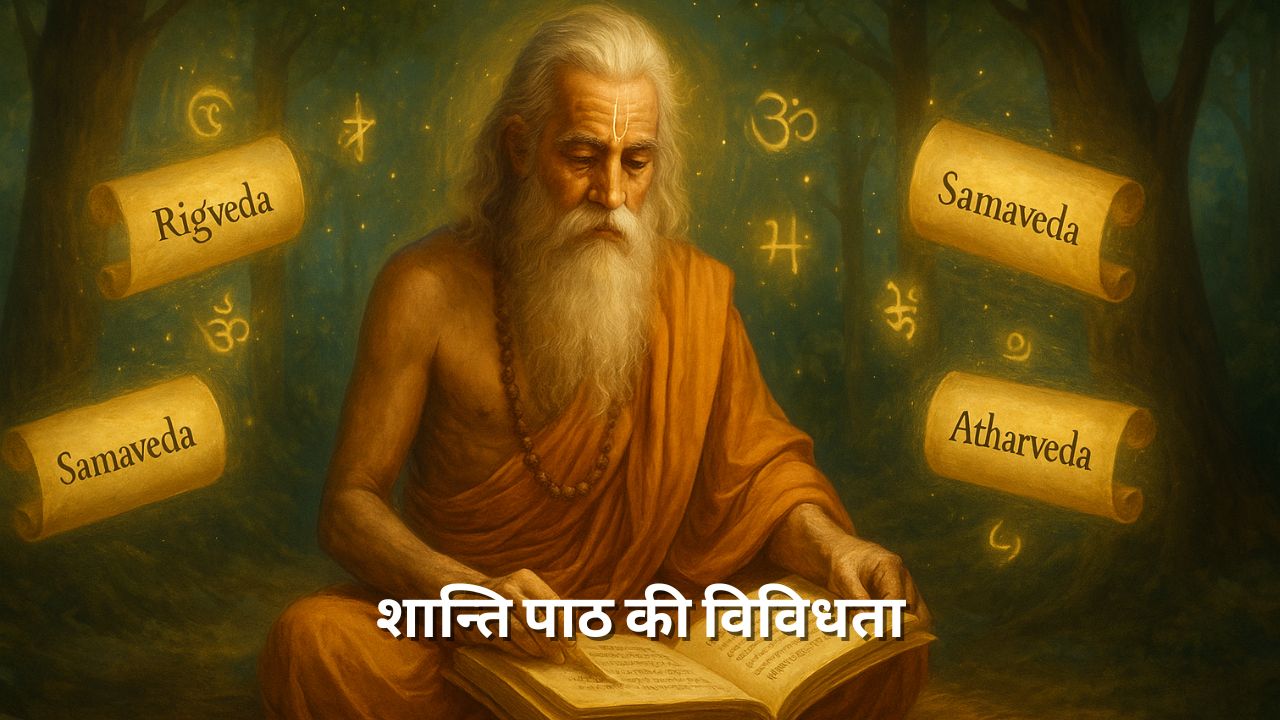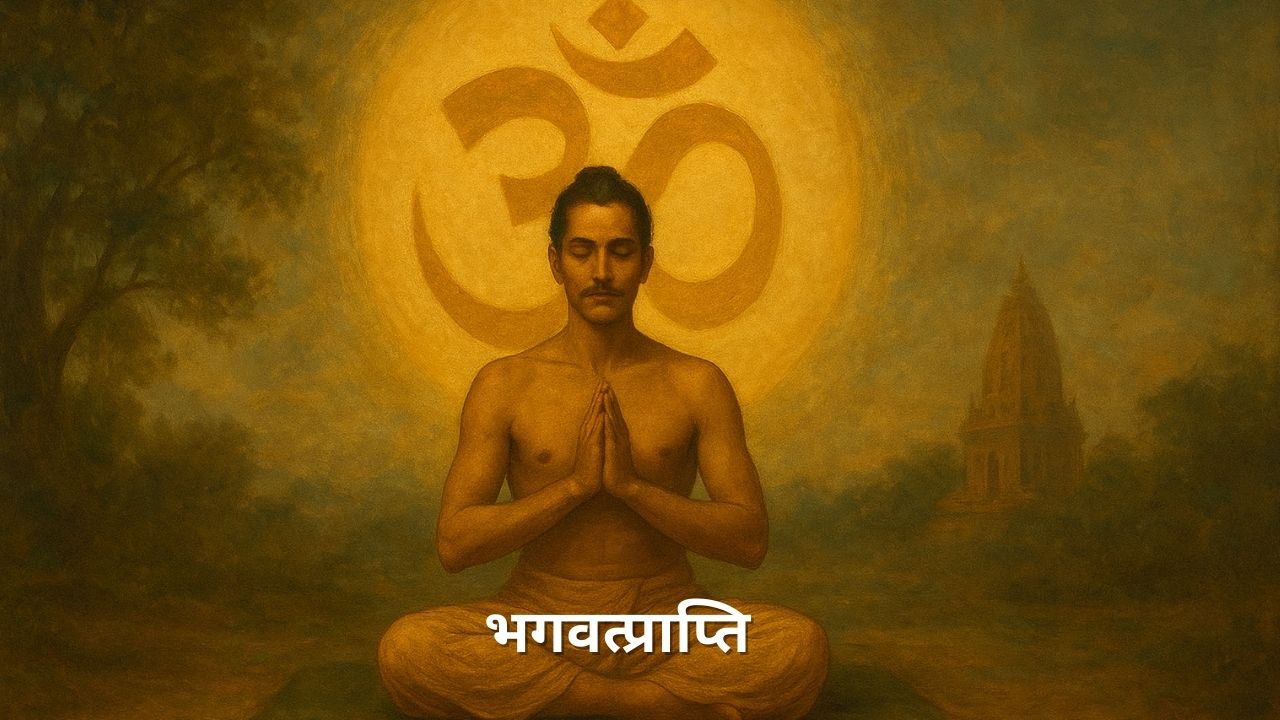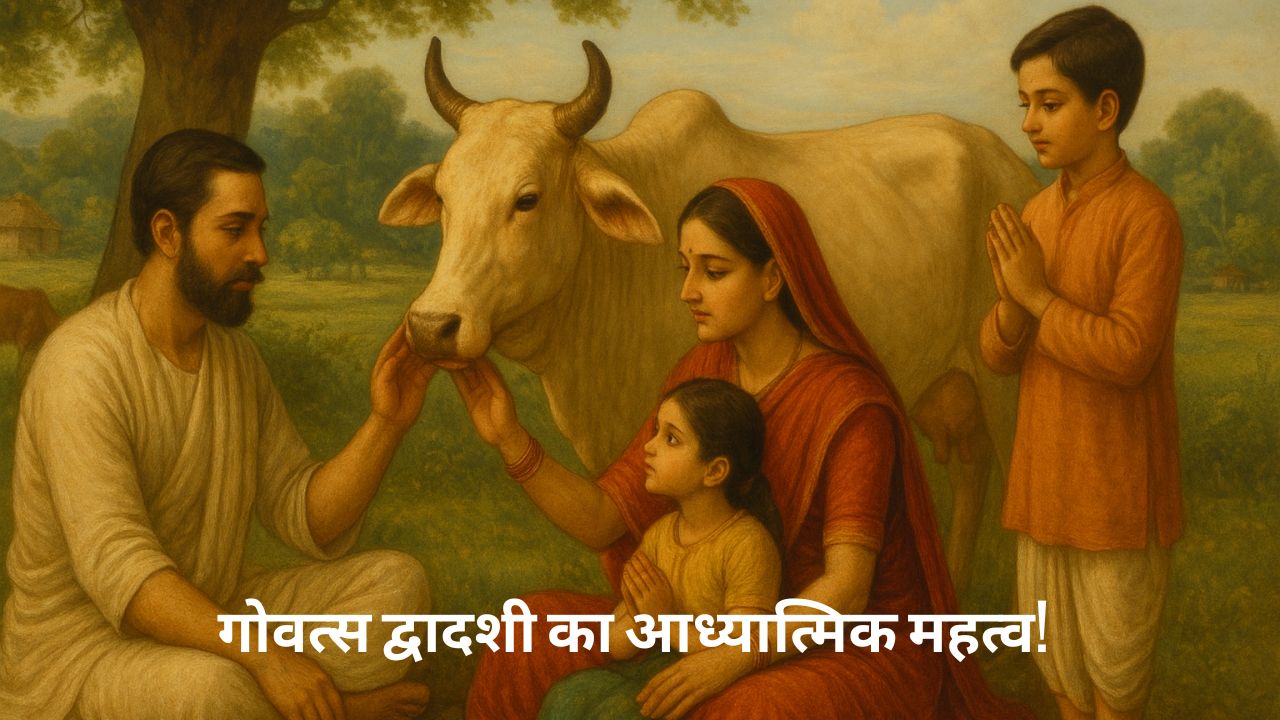- धर्म-पथ
- |
- 23 June 2025
- |
- 1 Comments
श्री अरुण कुमार उपाध्याय (धर्मज्ञ )-
इसे समझने के लिये वाद या सिलेबस के बन्धन से मुक्त हो कर २ विचार आवश्यक हैं-
(१) वेद वर्गीकरण का आधार, (२) उपनिषद् को अपने वेद का आवश्यक अङ्ग मानना।
वेद के त्रयी विभाजन के अनुसार ४ वेद हैं-मूल के ३ विभाजन के बाद मूल भी बचा रह गया, अतः त्रयी = १ + ३ = ४ वेद। इसका प्रतीक पलास दण्ड है जिसका यज्ञोपवीत के समय वेदारम्भ संस्कार में प्रयोग होता है। इसकी शाखा से ३ पत्ते निकलने पर शाखा भी बची रहती है। बिल्व (बेल) पत्र भी प्रतीक हो सकता है। आश्वलायन गृह्य-सूत्र, (१/१९/१३; १/२०/१) के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए क्रम से पलाश, उदुम्बर एवं बिल्व का दण्ड होना चाहिए, या कोई भी वर्ण उनमें से किसी एक का दण्ड बना सकता है। आपस्तम्ब गृह्य-सूत्र, (११/१५-१६) के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए क्रम से पलाश न्यग्रोध की शाखा (जिसका निचला भाग दण्ड का ऊपरी भाग माना जाय) एवं बदर या उदुम्बर का दण्ड होना चाहिए। वट वृक्ष शिव का या उनसे आरम्भ गुरु शिष्य परम्परा का प्रतीक है। उसकी शाखा नीचे जमीन से लग कर वैसा ही वृक्ष बनाती है; इसी प्रकार गुरु शिष्य को ज्ञान दे कर अपने जैसा बनाता है। उदुम्बर (गूलर) विश्व का प्रतीक है, उसके आवरण में अनेक बीज हैं, इसी प्रकार ब्रह्माण्ड में १०० अरब सूर्य हैं।
मूल वेद अथर्व था, जिससे ३ शाखा ऋक्, यजु, साम निकली।
ब्रह्मा देवानां प्रथमं सम्बभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता।
स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह॥१॥
अथर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्मा ऽथर्वा तां पुरोवाचाङ्गिरे ब्रह्म-विद्याम्।
स भरद्वाजाय सत्यवहाय प्राह भरद्वाजो ऽङ्गिरसे परावराम्॥२॥ (मुण्डकोपनिषद्, १/१/१,२ )।
द्वे विद्ये वेदितव्ये- ... परा चैव, अपरा च।
तत्र अपरा ऋग्वेदो, यजुर्वेदः, सामवेदो ऽथर्ववेदः, शिक्षा, कल्पो, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दो, ज्योतिषमिति। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते। (मुण्डकोपनिषद्, १/१/४,५)
विभाजन के बाद अविभाज्य अंश ब्रह्म रूप अथर्ववेद में रह गया-
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्। (गीता, १३/१६)
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। (गीता, १८/२०)
ब्रह्म वै पलाशः। (शतपथ ब्राह्मण, १/३/३/१९, ५/२/४/१८, ६/६/३/७)
ब्रह्म वै पलाशस्य पलाशम् (पर्णम्) (शतपथ ब्राह्मण, २/६/२/८)
तेजो वै ब्रह्मवर्चसं वनस्पतीनां पलाशः। (ऐतरेय ब्राह्मण, २/१)
यस्मिन् वृक्षे सुपलाशे देवैः सम्पिबते यमः। अत्रा नो विश्यतिः पिता पुराणां अनुवेनति॥ (ऋक्, १०/१३५/१)
ब्राह्मणो बैल्व-पालाशौ क्षत्रियो वाट-खादिरौ। पैलवौदुम्बरौ वैश्यो दण्डानर्हति धर्मतः॥ (मनु स्मृति, २/४५)
त्रयी विभाजन का आधार है, ऋक् = मूर्ति, यजु = गति, साम = महिमा या प्रभाव, अथर्व = अविभक्त ब्रह्म। इसी को मनु स्मृति आदि में अग्नि (सघन ताप या पदार्थ), वायु (गति) तथा रवि (तेज) भी कहा गया है।
ऋग्भ्यो जातां सर्वशो मूर्त्तिमाहुः, सर्वा गतिर्याजुषी हैव शश्वत्।
सर्वं तेजं सामरूप्यं ह शश्वत्, सर्वं हेदं ब्रह्मणा हैव सृष्टम्॥ (तैत्तिरीय ब्राह्मण,३/१२/८/१)
अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्।
दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थमृग्यजुः साम लक्षणम्॥ (मनु स्मृति,१/२३)
गति २ प्रकार की है- शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल गति प्रकाश युक्त अर्थात् दीखती है। कृष्ण गति अन्धकार युक्त अर्थात् भीतर छिपी हुयी है।
शुक्ल गति ३ प्रकार की है- निकट आना, दूर जाना, सम दूरी पर रहना (वृत्ताकार कक्षा)। वस्तु का आन्तरिक प्रसारण या संकोच मिला कर ५ गति कही गयी है।
अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्। --- धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्। (गीता, ८/२४-२५)
उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकुञ्चनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि। (वैशेषिक सूत्र,१/१/७)
शरीर या किसी पिण्ड के भीतर की गति दीखता नहीं है। वह कृष्ण गति १७ प्रकार की है, इस अर्थ में प्रजापति या पुरुष को १७ प्रकार का कहा गया है। समाज (विट् = समाज, वैश्य) भी १७ प्रकार है। विट् सप्तदशः। (ताण्ड्य महाब्राह्मण १८/१०/९) विशः सप्तदशः (ऐतरेय ब्राह्मण, ८/४)
सप्तदशो वै पुरुषो दश प्राणाश्चत्वार्यङ्गान्यात्मा पञ्चदशो ग्रीवाः षोडश्च्यः शिरः सप्तदशम्। (शतपथ ब्राह्मण, ६/२/२/९)
राष्ट्रं सप्तदशः। (तैत्तिरीय ब्राह्मण, १/८/८/५)
सर्व्वः सप्तदशो भवति। (ताण्ड्य महाब्राह्मण, १७/९/४)
सप्तदश एव स्तोमो भवति प्रतिष्ठायै प्रजात्यै। (ताण्ड्य महाब्राह्मण, १२/६/१३)
तस्माऽएतस्मै सप्तदशाय प्रजापतये। एतत् सप्तदशमन्नं समस्कुर्वन्य एष सौम्योध्वरो ऽथ या अस्य ताः षोडश कला एते ते षोडशर्त्विजः (शतपथ ब्राह्मण, १०/४/१/१९)
अर्थात्, व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के अंगों का आन्तरिक समन्वय १७ प्रकार से है जो दीखता नहीं है। वह कृष्ण गति है। एक समतल को किसी चिह्न (टप्पा) द्वारा १७ प्रकार से भरा जा सकता है। इसे आधुनिक बीजगणित में समतल स्फटिक सिद्धान्त कहते हैं। (Modern algebra by Michael Artin, Prentice-Hall, page 172-174) ५ महाभूतों की शुक्ल गति ५ x ३ = १५ प्रकार की होगी आन्तरिक गति १७ x ५ = ८५ प्रकार की है। अतः शुक्ल यजुर्वेद की१५ शाखा तथा कृष्ण यजुर्वेद की ८६ शाखा (१ अगति या यथा स्थिति मिलाकर) हैं। समतल चादर की तरह मेघ भी पृथ्वी सतह को ढंक कर रखता है, अतः ज्योतिष में १७ के लिये मेघ, घन आदि शब्दों का प्रयोग होता है।
Related Posts
1 Comments