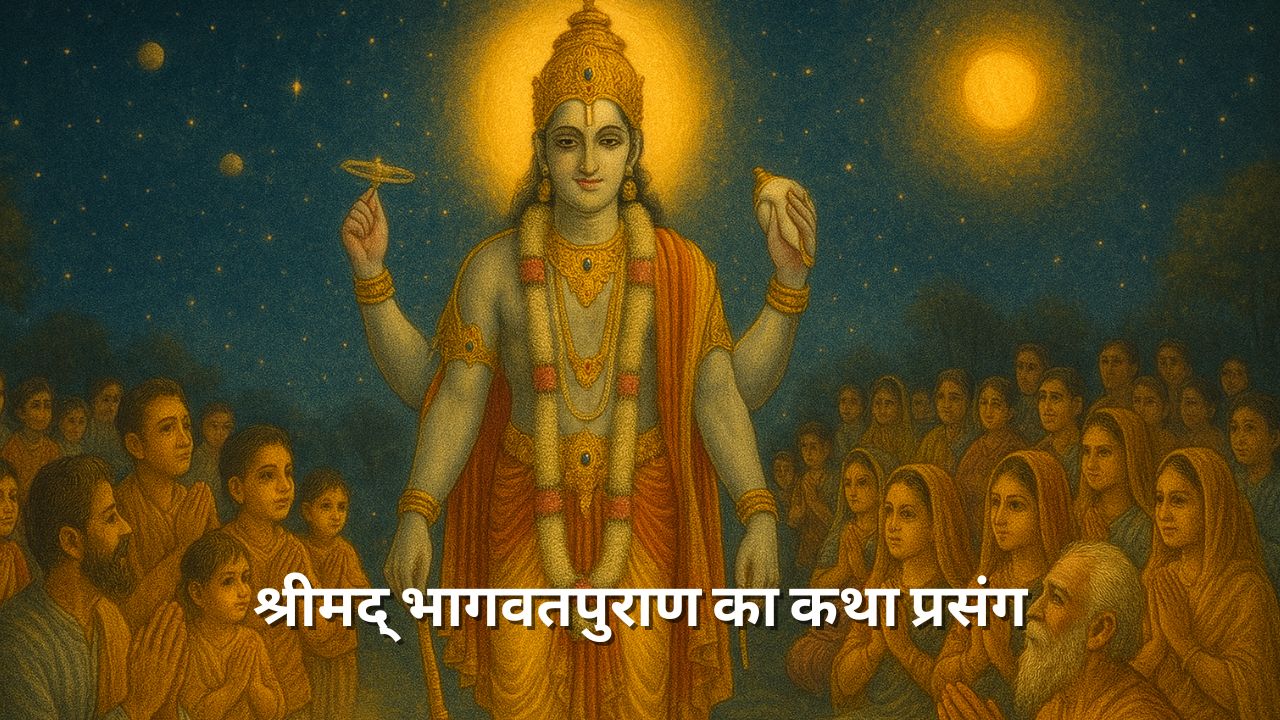- मिस्टिक ज्ञान
- |
- 31 October 2024
- |
- 0 Comments
डॉ. दीनदयाल मणि त्रिपाठी (प्रबंध संपादक)-
इस प्रकार वेदवाणी इस जगत में ‘बोध’ एवं ‘प्रतिबोध’ नाम के ‘दो ऋषि’ होना अर्थात् ज्ञान प्राप्ति के दो आधार होना वर्णन करती है, इन्हें लोक-जीवन की रक्षा करने वाला कथन करती है, जिन्हें उपनिषदवाणी में श्रुति द्वारा ‘अपरा विद्या’ और ‘परा विद्या’ कहा जाकर ‘अविद्या’ एवं ‘विद्या’ कहा गया है तथा इन दोनों को एक साथ जान लेना और लोक जीवन में अपनाना आवश्यक बतलाया गया है ।-
*विद्यां चाविद्यां च यस्तद् वेदोभयं सह ।*
*अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥ (ईशा. 11)* अर्थात् – “जो मनुष्य विद्या (परा विद्या) और अविद्या (अपरा विद्या) उन दोनों को यथार्थ रूप में साथ-साथ (एकसाथ) जान लेता है, वह अविद्या (अपरा विद्या) द्वारा मृत्यु सागर को पार करके अर्थात् जीवनयात्रा को पूर्ण करत हुआ, विद्या (परा विद्या) के अनुपालन (अनुष्ठान) द्वारा अमृतत्व को भोगता है । अर्थात् वह अविनाशी आनन्दमय परब्रह्म परमात्मा को इस जीवन में प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है ।
” इस प्रकार श्रुति बोध एवं प्रतिबोध आधारित इन दोनों ही विद्याओं – ‘अपरा विद्या’ और ‘परा विद्या’ को, मनुष्य जीवन को संतुष्ट करने वाला कहती है; इन्हें सुख-दुःख प्राप्ति का कारण तथा प्राणों की रक्षा करने वाला एवं दीर्घायु का कारण होना वर्णन करती है तथा अपेक्षा करती है कि ये दोनों अवस्थाएँ अपने बोध प्रदानकर्ता ऋषिरूप में रात में और दिन में भी जागते रहें, अर्थात् सृष्टिचक्र के अहोरात्र में सतत् बोध प्राप्ति का आधार बने रहें ।
इसके साथ ही केनोपनिषद् में श्रुति कथन आया है कि ‘इस लोक में मनुष्य आत्मा के द्वारा बल तथा ज्ञान के द्वारा ही अमृतत्त्व को प्राप्त करता है-
*प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि विन्दते*।
*आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दतेऽमृतम् । । (केन.उप. २.४)* अर्थात् – “प्रतीक या संकेत के माध्यम से उत्पन्न / प्राप्त ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, निश्चय ही इसके द्वारा मनुष्य अपने ‘अमृत स्वरूप’ आत्मा (अन्तर्यामी परमात्मा) को प्रात करता है ।
अपने आत्मा को जानकर वह बल, पराक्रम, शौर्य, ओज, पौरुष आदि को प्राप्त करता है तथा विद्या (ज्ञान) द्वारा अमृतरुप परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है ।
” अतः योगेश्वर श्रीकृष्ण की बाललीलाओं का वर्णन करने वाली ये सब बालकथाएँ अपनी ‘बोध’ एवं ‘प्रतिबोध’ अवस्था आधार पर ‘अपरा विद्या’ में पारङ्गित पुरुषों के लिये, जो केवल ‘शाब्दिक अर्थ’ को महत्व प्रदान करते हैं, उनके लिये तो मनोरंजन का कार्य करने वाली हो गयी हैं; किंतु ‘प्रतिबोध’ आधारित ‘परा विद्या’ रूप में ‘ज्ञान के आलोक में’ ये सब आत्म-साधना के मार्ग को प्रकट करने वाली तथा जीवनपथ की अबूझ बातों को अपने ‘सांकेतिक अर्थ’ द्वारा उजागर करने वाली होना जानी गयी हैं । तथा बालक्रीड़ा आधारित बालकथा रूप में ये अनवरतरूप से चलने वाले सृष्टिचक्र में सदैव के लिये ‘शिक्षाप्राप्ति’ का आधार हो गयी हैं ।
ये तो “पौराणिक आख्यान” रूप में दिवसकाल हेतु निम्न ‘संस्कृत सुभाषित’ अनुसार ‘बालमन’ के लिये (अर्थात् ‘अपरा विद्या’ में पारंगत व्यक्तिके लिये) ‘शिक्षा प्राप्ति’ का आधार और साधन तथा लोक-जीवन में सदैव के लिये उपयोगी हो गयी हैं । :-
*यन्न्वे भाजने लग्नः संस्कारो नान्य था भवेत्।*
*कथाच्छलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते ॥ (हितोपदेश, मित्रलाभ 8)*
अर्थात् – “मिट्टी के पात्र में किया गया कलात्मक संस्कार या रेखांकन आदि जिस प्रकार उसके पकाये जाने पर मिट नहीं सकता, इसी प्रकार बालकों को कथा साहित्य या कहानियों के माध्यम (बहाने) से नीतिशास्त्र की महत्वपूर्ण बातों का उपदेश दिया जाता है ।
” योगेश्वर श्रीकृष्ण की बाललीला से जुडी हुई ऐसी ही एक बहुचर्चित पौराणीक कथा है –
‘श्रीकृष्ण द्वारा गोपिकाओं का चीरहरण’ । ‘अपरा विद्या’ में पारङ्गत आधुनिक व्याख्याकारों द्वारा ‘चीरहरण’ के इस आख्यान को बड़ा ही विवादित माना गया है ।
इस कथा/ आख्यान के आधार पर उनके द्वारा श्रीकृष्ण के चरित्र-चित्रण में अश्लीलता का आरोप भी लगाया जाता है । किंतु उनका यह कथन ठीक होना पाया नहीं जाता । यह तो कठोपनिषद् में आये श्रुति कथनानुसार ‘बालबुद्धि का कार्य’ होना या ‘मूर्खता को अपना लेना’ ही प्रकट होता है । जिसे निम्न विवेचन आधार पर भलीभांति जाना जा सकता है ।
इस आख्यान का बोधपरक रूप तो योग-मार्ग की सम्पूर्ण शिक्षा देने वाला है । अपने यथार्थ रूप में यह आख्यान ‘योग-क्रिया’ आधारित ‘साधना मार्ग’ को प्रकट करता है । वस्तुतः यह तो प्राणायाम की प्रक्रिया पर आधारित योग-यात्रा के उस अकथनीय मार्ग को जान लेने में सहायता करता है, जिससे प्रत्येक साधक को अनिवार्यतः गुजरना होता है ।
यह आख्यान तो इस “मानवदेह के वस्त्ररूप” और ‘साधना मार्ग’ में प्राप्त होने वाली “देह-गेह-आत्मविस्मृति” की व्याख्या तथा बोध प्राप्ति की अवस्था से जुडा हुआ है, जिसे ‘समाधी अवस्था’ रूप में जाना गया है तथा जिसे इस जीवात्मा के स्वामी ‘प्रकाशरूप परमेश्वरर’ से मिलन का साधन माना गया है ।
अतः इस आलेख में अब हम इस ललित आख्यान से मिलने वाले ‘कथा-सन्देश’ को किंचित् विस्तार से किंतु अति संक्षेप में ही ‘आधारभूत’ रूपमें जानते और प्रकट करने का प्रयत्नस करते हैं ताकि यह विवरण ‘ज्ञान के आलोक’ में सबके लिये उपयोगी हो जावे ।
सृष्टिचक्र के दिवसकाल में सब के लिये योग-यात्रा का साधन हो जावे । अस्तु-
Related Posts
0 Comments
Comments are not available.