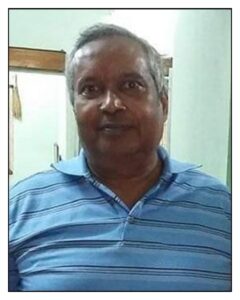- धर्म-पथ
- |
-
31 October 2024
- |
- 0 Comments
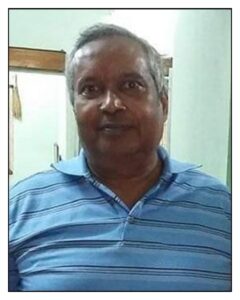
अरुण कुमार उपाध्याय (धर्मज्ञ)-
अद्वैत के बिना सृष्टि नहीं चल सकती। इसके कई अर्थ हैं।
(१) स
भी देश काल पात्र के लिए एक नियम– भगवान् को भी सृष्टि के नियमों का पालन करना पड़ता है। इसलिए हर बार वैसी ही सृष्टि करनी पड़ती है-
सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् (ऋक्, १०/१९०/३)
= जैसा सूर्य चन्द्र पहले बनाया था, वैसा ही इस बार भी बनाया।
(२) ज्ञान का आधार-
यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव-अनुपश्यति।
सर्व भूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते॥६॥
यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एव अभूद् विजानतः।
तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वं अनु-पश्यतः॥७॥
(ईशावास्योपनिषद्, वाज. यजु, अध्याय, ४०)
= जो सभी प्राणियों को आत्मा (परमात्मा) में ही सदा देखता है तथा सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है, वह किसी से घृणा नहीं करता। जो सभी प्राणियों को आत्मा (अपने) समान पूरी तरह समझता है, वह सभी में एकत्व का अनुभव करता है।
यहां २ बार अनु-पश्यतः कहा है। सामान्य पश्य का अर्थ रूप देखना है। अनुपश्यतः से उसे पहचानते हैं। जैसे एक बार आम का वृक्ष देखा तथा बताया गया कि यह आम है। दूसरी बार अन्य वृक्ष देखा जो इससे भिन्न था किन्तु अन्य प्रकार के वृक्षों की तुलना में पहले देखे गये आम से अधिक मिलता था। अतः इसे भी आम ही मान लिया। हर वृक्ष के सभी पत्ते अलग-अलग हैं, किन्तु उनमें आपस में कुछ समानता है। यह विजानता = विज्ञान बुद्धि या पद्धति है। इसी प्रकार कोई मनुष्य एक ही समय लेख लिखता है तो एक ही अक्षर हर ५० बार अलग-अलग प्रकार से लिखेगा। आयु के साथ भी लेखन शैली बदलती रहती है। तथापि हस्त रेखा का वैज्ञानिक उनमें कुछ समानतायें खोज लेता है-आज के ५० रूपों तथा भविष्य के सहस्रों रूपों में। इनके द्वारा वह १० अरब अन्य व्यक्तियों के लेखन से अन्तर भी खोज लेता है। मनुष्य का चेहरा बोलते समय बदलता रहता है, फोटो में अलग अलग दीखेगा। उसका स्वर भी बदलता है। किन्तु १ दिन का बच्चा भी अपनी मां का चेहरा तथा ध्वनि हर रूप में पहचान लेता है। एक रूप देखना जानना है, करोड़ों रूपों में एकत्व देखना तथा अन्य पदार्थों के एकत्व से भिन्नता देखना-विजानन है।
अनुपश्यतः का अन्य अर्थ है कि पहले हर वस्तु भिन्न भिन्न दीखती है। बाद में चिन्तन द्वारा एकता दीखती है। चिन्तन के बाद मानसिक दर्शन अनु-पश्यति है।
यही एकत्व सभी विज्ञान का आधार है जिसे कई प्रकार से कहा गया है-
सर्वं खल्विदं ब्रह्म (छान्दोग्य उप., ३/१४/१ आदि)
एको वशी सर्व भूतान्तरात्मा (कठोपनिषद्, ५/१२ आदि)
एको देवः सर्व भूतेषु गूढ़ः (श्वेताश्वतर उप, ६/११)
या इलाह इल्-इल्लाह (कुरान का कलमा) = जो कुछ है, वह अल्लाह है, उसके सिवा कुछ नहीं है। माहेश्वर सूत्र के अल् प्रत्याहार में सभी अक्षर आ जाते हैं। अतः अलम् = पर्याप्त, सब कुछ। इसस्र् अंग्रेजी में all तथा अरबी में अल्लाह हुआ है। मळयालम में अन्तिम अक्षर ळ है जिसका उच्चारण ज़ जैसा है। अतः उसमें अ से ळ (ज़) तक सभी वर्ण हैं। इसका अनुकरण अंग्रेजी में है-A to Z।
एकत्व के अन्य अर्थ-
(१) विज्ञान के नियम-संसार में विज्ञान के नियम सभी स्थान तथा सभी समय एक ही हैं। बिना इस धारणा के कोई विज्ञान नहीं हो सकता। अतः यह कहना गलत है कि धर्म तथा विज्ञान का कोई सम्बन्ध नहीं है। धर्म में ब्रह्म के एकत्व पर ही विज्ञान आधारित है। आज हमने देखाकि जल के एक अणु में हाइड्रोजन के २ तथा ऑक्सीजन का १ अणु है। उसके बाद हम मान लेते हैं कि करोड़ों वर्ष पूर्व भी जल का अणु वैसा ही था तथा वह केवल भारत में नहीं अमेरिका या ब्रह्माण्ड के दूसरे छोर पर भी वही होगा। यदि विज्ञान के नियम हर समय स्थान पर बदलते जायेंगे, तो कुछ समझा नहीं जा सकता है। यही वर्ण व्यवस्था भी है। यदि यह कर्म के अनुसार हर क्षण बदलता है, तो इसे कहने का कोई अर्थ ही नहीं है।
(२) भाषा का एकत्व-सभी भाषाओं में शब्दों का समान अर्थ होता है। यदि लोगों के लिए इसका मनमाना अर्थ होने लगे, तो कोई किसी से बात नहीं कर पायेगा।
अपना कहा जब आप ही समझे तो क्या समझे।
मजा कहने का तब है, जब कि एक कहे और दूसरा समझे।
(अकबर इलाहाबादी)
(३) व्यक्तियों का एकत्व-सभी व्यक्ति मूलतः एक ही प्रकार के हैं। सभी की शारीरिक तथा मानसिक वृत्तियां समान हैं। इसी आधार पर चिकित्सा शास्त्र बना है। रसोई भी वैसे ही बनती है। यदि एक व्यक्ति को मिर्च तीखी लगती है, तो अन्य को मीठी नहीं लगेगी।
(४) लिपि का एकत्व-सभी व्यक्तियों के लिये लिपि में एक ही चिह्न होंगे तभी एक का लिखा दूसरा समझेगा तथा भविष्य के लिए भी ज्ञानसुरक्षित रहेगा। यह एकत्व सर्वोच्च अधिकारी द्वारा ही निर्धारित हो सकता है, जैसे ब्रह्मा, आदम या चीन में फान ने किया था। नहीं तो हर व्यक्ति कहेगा कि उसके चिह्न ही ठीक हैं या अपनी संस्कृति के अनुसार हैं और कोई किसी की बात नहीं मानेगा।
(५) व्यवस्था का एकत्व-विश्व में कई प्रकार की क्रियायें चल रही हैं। सबके बीच सूक्ष्म सम्पर्क है किन्तु इतना नहीं कि वह दूसरे की क्रिया बन्द कर दे। वेद में विश्व के ३ स्तरों को परस्पर सम्बन्धित माना गया है- आकाश में आधिदैविक, पृथ्वी पर आधिभौतिक, शरीर के भीतर आध्यात्मिक। यह स्पष्ट है क्योंकि आकाश के सृष्टि क्रम में पृथ्वी बनी, उसमें मनुष्य का जीवन चल रहा है। मनुष्य भी पृथ्वी को प्रभावित कर सकता है-जलवायु को अशुद्ध कर या सुरक्षित रख कर। अभी मंगल तथा चन्द्र पर यान जा कर उनको प्रभावित कर रहे हैं। किन्तु परस्पर प्रभाव इतना नहीं है कि हर व्यक्ति अपना काम नहीं कर सके। बल्कि आकाशीय पिण्डों का सूक्ष्म प्रभाव मापना कठिन है। इनका किरण गति से प्रभाव होता है जिनका विशद् वर्णन वाज. यजुर्वेद (१५/१५-१९, १७/५८, १८/४०), ऋक् (१०/३७, १०/९६, १०/१३१ सूक्त), अथर्व (२०/३० सूक्त), मैत्रायणी सं (२/८/२२, २/१०/४८), तैत्तिरीय सं (४/६/३/३, ५/४/६/३), शतपथ ब्राह्मण (९/२/३/१२), बॄहदारण्यक उप. (४/४/८/९), छान्दोग्य उप. (८/६), कूर्म पुराण (भाग १, ४३/२-८), मत्स्य पुराण (१२८/२९-३३), वायु पुराण (५३/४४-५०), लिङ्ग पुराण (१/६०/२३), ब्रह्माण्ड पुराण (१/२/२४/६५-७२) आदि में है।
(६) यज्ञ का एकत्व-हर यज्ञ या उत्पादन भी परस्पर आश्रित होने के कारण एक ही व्यवस्था हैं। कृषि उत्पाद से जीवन चलता है अतः यज्ञ परिभाषा में कृषि सम्बन्धित शब्द ही हैं-
अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न-सम्भवः।
यज्ञाद् भवति पर्जन्यः, यज्ञः कर्म समुद्भवः॥। (गीता, ३/१४)
यज्ञों के समन्वय या एक व्यवस्था से ही साध्य उन्नति के शिखर पर पहुंचे और देव कहलाये-
यज्ञेन यज्ञं अयजन्त देवाः, तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्।
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः॥
(पुरुष सूक्त, १६, ऋक्, १/१६४/५०, १०/९०/१६, वाज. यजु, ३१/१६, तैत्तिरीय सं., ३/५/११/५, मैत्रायणी सं, ४/१०/३, काण्व सं, १५/१२ आदि)
(७) ब्रह्म का एकत्व-ब्रह्म एक होने के कारण एक व्यक्ति का भगवान् दूसरे से अलग नहीं है। अतः धर्म परिवर्तन धर्म के मूल आधार के विरुद्ध है।
(८) ज्ञान का एकत्व-हमारे ज्ञान का आधार है सभी शास्त्रों का समन्वय। ब्रह्म सूत्र के प्रथम ४ सूत्र हैं-अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जनाद्यस्य यतः (इस विश्व का जिससे जन्म आदि हुआ, वह ब्रह्म है)। शास्त्रयोनित्वात्। तत् तु समन्वयात्।
सभी शास्त्र परस्पर आश्रित हैं। भौतिक विज्ञान का छात्र रसायन विज्ञान, गणित, या भाषाओं का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि यह शास्त्र उन सब पर आधारित है।
(९) भिन्न वर्णनों का एकत्व-हर शास्त्र अपनी परिभाषा या मान्यता के अनुसार लिखा जाता है। एक शास्त्र की मान्यता के अनुसार अन्य शास्त्र की आलोचना नहीं हो सकती। शंकराचार्य ने सत्य तथा मिथ्या के अनेक स्तर माने हैं, कम सत्य को मूल सत्य की तुलना में मिथ्या कहा है। जगत् मिथ्या कहने का यह अर्थ नहीं है कि संसार का अस्तित्व नहीं है, बल्कि वह मूल स्रोत ब्रह्म की तुलना में अस्थिर या अन्य प्रकार से कम सत्य है। बादरायण व्यास ने ब्रह्म के विभिन्न वर्णनों की एकता दिखाने के लिए ब्रह्म सूत्र लिखा। पर उसकी भी ८ प्रकार की व्याख्यायें हो गयीं।
(१०) निर्विशेष तथा विशिष्ट अद्वैत-विश्व का मूल स्रोत समरूप था, अतः उसे रस कहा गया (रसो वै सः-तैत्तिरीय उपनिषद्, २/७/२)। उसमें भेद नहीं होने के कारण वर्णन नहीं हो सकता। अतः उसकी २ प्रकार से व्याख्या होती है-उसके प्रभाव या वस्तुओं में एकत्व का अनुभव-जैसे रस के अनुभव से आनन्द होता है (रसं लब्ध्वा आनन्दी भवति-तैत्तिरीय उप, २/७/२)। उसका बाहरी या प्रभाव का वर्णन को उपवर्णन कहते हैं-
एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं (गजेन्द्र मोक्ष में स्तुति के बाद शुकदेव जी का मन्तव्य)।
अन्य विधि है कि कोई भी आभास या अनुभव पूर्ण नहीं है, अतः इसे नेति (न इति = इतना ही नहीं है) कहते हैं-
निगम नेति शिव अन्त न पावा। ताहि धरहिं जननी हठि धावा॥
(रामचरितमानस, १/२०२/८)
गजेन्द्र मोक्ष में भी कुछ नेति उदाहरण हैं-
स वै न देवासुर-मर्त्य तिर्यङ्, न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तुः।
नायं गुणं कर्म न सन्न चासन्, निषेधशेषो जयतादशेषः॥
(भागवत पुराण, ८/३/२४)
यहां शण्ढ का अर्थ नपुंसक है- न स्त्री, न पुरुष। आज कल सांढ का अर्थ पुरुष गौ है। पहले वृषभ या ऋषभ सम्मान की वस्तु थी, जैसे अर्जुन को गीता में कई बार पुरुषर्षभ (पुरुष-ऋषभ) कहा है। आजकल वृषभ या बैल का अर्थ नपुंसक है।
विशिष्ट अद्वैत विशिष्ट वस्तुओं में अद्वैत है। विशेष तत्त्व क्या है? जैसे मिट्टी एक ही तरह की है। उसकी ईंटों की चिति (चिनाई) से कई प्रकार के घर बनते हैं। यह मिट्टी का चिति के कारण विशेष रूप है, जो पहले नहीं था। इसे इष्टका-चिति कहा गया है, जिसके कई यज्ञ रूप हैं। स्वर्ण तथा उससे बने विभिन्न प्रकार के आभूषणों का भी उदाहरण दिया जाता है। वैशेषिक दर्शन में ६ पदार्थ कहे गये हैं, उनकी विभिन्न प्रकार की चिति के कारण जो नया गुण उत्पन्न होता है, वह विशेष है। इसकी व्याख्या के कारण यह वैशेषिक दर्शन है।
आकाश में मूल रस से ७ लोक बने, अर्थात् ६ठी चिति के बाद। अतः पुरुष तथा विविध रूपों को षष्ठी चिति कहा गया है। हर चिति का निर्माण काल १ अहः (दिन) है (गीता, ८/१८)।
देवक्षेत्रं वै षष्टमहः (गोपथ ब्रा. उत्तर, ६/१०, ऐतरेय ब्रा, ५/९)
पुरुष एव षष्टमहः (कौषीतकि ब्रा, २३/४)
सर्वरूपं वै षष्टमहः (कौषीतकि ब्रा, २३/६, ८, २९/५)
अन्तः षष्टमहः (कौषीतकि ब्रा, २३/७, २६/८)
शिर एव षष्ठी चितिः (शतपथ ब्राह्मण, ८/७/४/१७)
वैज्ञानिक भाषा में विचार करें तो मनुष्य (या कोई भी वस्तु) कलिल (सेल) से बना है, कलिल अणु से, अणु परमाणु से, परमाणु कणों से, कण पितर से, पितर ऋषि से बने हैं।
इन विशिष्ट पदार्थॊ में ६ चिति पूर्व की एकता दिखाने के लिए विशिष्ट-अद्वैत सिद्धान्त रामानुजाचार्य का है। इसके लिए उनको ४ व्यूह आदि का उपयोग करना पड़ा जो शंकराचार्य के लिए आवश्यक नहीं था।
मध्वाचार्य के द्वैत सिद्धान्त का भी यह अर्थ नहीं है कि वे ब्रह्म को २ मानते थे। ब्रह्म १ ही है किन्तु उसके रूपों की व्याख्या करने के लिए आधिभौतिक और आधिदैविक अलग अलग शास्त्र बनते हैं। भक्ति मार्ग में भी साधक अपने को ब्रह्म से भिन्न मानता है और योग द्वारा एकत्व की चेष्टा करता है। स्वयं शंकराचार्य ने परकाया प्रवेश किया था तो उनकी चेतना २ स्थानों में एक साथ थी।