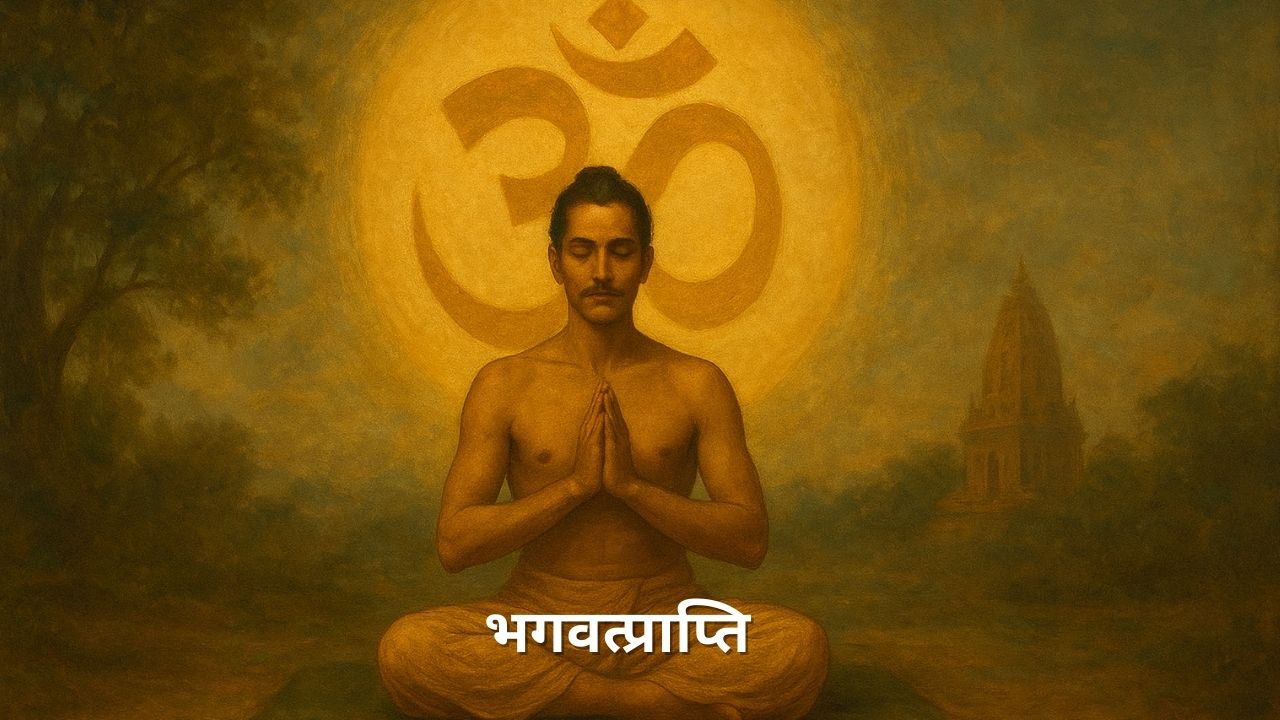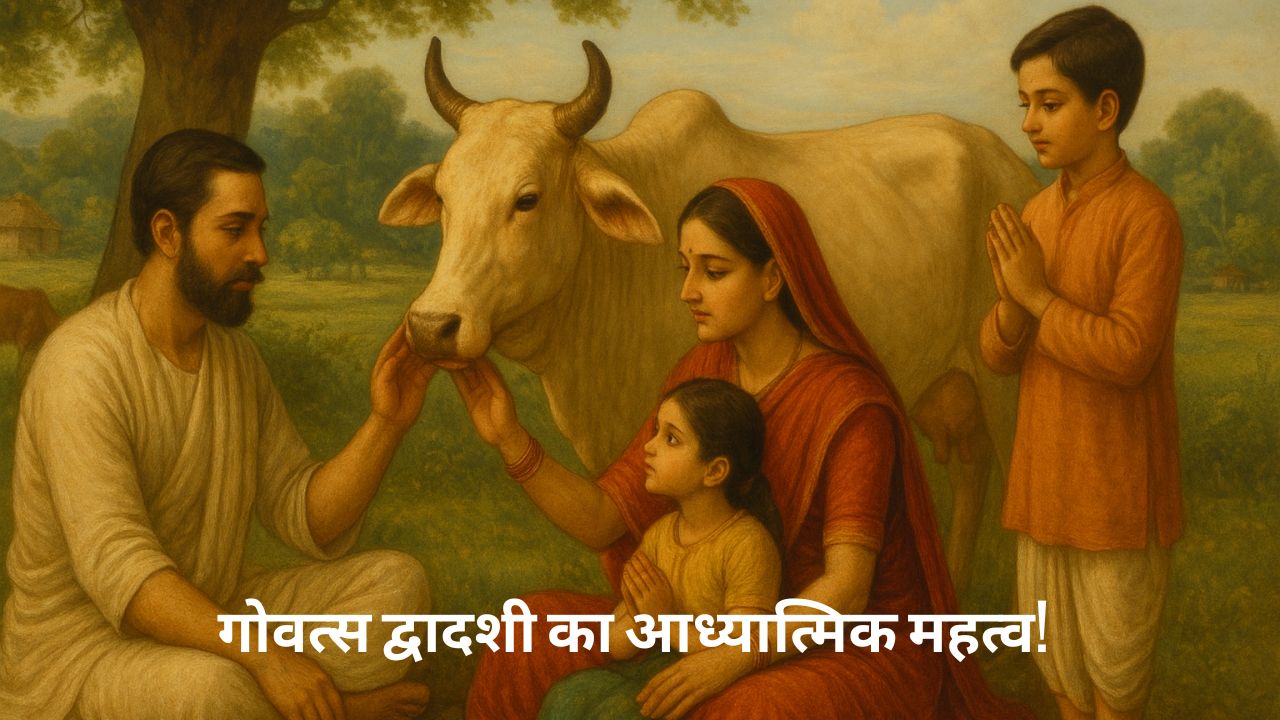- धर्म-पथ
- |
- 31 October 2024
- |
- 0 Comments
मनोहर विधालंकर- (४२) सरस्वतीमनुमति भगं यन्तो हवामहे । परवाचं जुष्टां मधुमतीमवादिषं देवानां देवहूतिषु ॥ -अथर्व ५-७-४ (४३) यं याचाम्यहं वाचा सरस्वत्या मनोयुजा। श्रद्धा तमद्य विन्दतु दत्ता सोमेन बभ्रुणा ॥ -अथर्व ५-७-५ ऋषि:- अथर्वा । देवता-सरस्वती । छन्द:-अनुष्टुप् ।। शब्दार्थ-(देवानाम्) सन्तों, विद्वानों और वैज्ञानिकों की (देवहूतिष ) विद्वत् गोष्ठियों में (जुष्टां) सभ्यों द्वारा सेवनीय और प्रीतिपूर्ण (मधुमतीम्) मधुरतायुक्त (वाचं) वाणी का (अवादिषम्) प्रयोग करता हूँ। इस प्रकार हम सभी सभ्य (भगं यन्तः) ऐश्वर्य युक्त भाग घेय को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए (अनुमतिम्) परमेश्वर या गुरु की मति के अनुकूल मति बनाने वाली (सरस्वतीं) वेदमाता को (हवामहे) पुकारते हैंप्रयोग करते हैं तथा तदनुकूल आचरण करते हैं। उपरोक्त साधना के द्वारा स्थिर तथा शान्त चित्त होकर (अहं) मैं—याचक (मनोयुजा) पूर्ण मनोयोग युक्त (सरस्वत्या) अपनी संस्कृति या वेदवाणी द्वारा अनुमोदित (वाचा) वाणी से (यं याचामि) जिस देव से जो कुछ माँगता हूँ; (बभ्रणा) भरण-पोषण में समर्थ (सोमेन) वीर्यप्रद सोम द्वारा (दत्ता) प्रतिपादित (श्रद्धा) मेरी श्रद्धा-सत्य में प्रीति तथा दृढ़ धारणा (तम्) उस देव को प्राप्त होकर, उससे मुझे अभिवाञ्छित दिव्य गुण-कर्म-पदार्थ (विन्दतु) प्राप्त करावे। विशेष—इस मन्त्र का ऋषि अथर्वा=संशय रहित स्थिर गतिवाला है, और वह संकेत करता है कि यदि किसी भी पदार्थ को प्राप्त करना हो तो उसे संशय रहित पूर्ण श्रद्धा के साथ प्राप्त करने का सतत प्रयत्न करना चाहिए। निष्कर्ष-हम किसी भी समाज या गोष्ठी में सम्मिलित हों, मधुर तथा प्रीति पूर्ण वाणी का प्रयोग करना चाहिए। सम्म यदि हमारा व्यवहार सभ्यतापूर्ण तथा हमारी आकांक्षा श्रद्धा से समन्वित होगी तो अवश्य सफल होगी। (४४) अपानाय व्यानाय प्राणाय भूरि धायसे । सरस्वत्या उरुव्यचे विधेम हविषा वयम् ॥ -अथर्व ६-४१-२ ऋषिः – ब्रह्मा। छन्द:-अनुष्टप् । शब्दार्थ– (अपानाय) रोगों, दोषों, दरितों को बाहर निकालने वाले (प्राणाय) जीवन, स्वास्थ्य तथा सुवितों को अन्दर लाने वाले (व्यानाय) सारे शरीर में व्याप्त हो कर जीवनी शक्ति को कायम रखने वाले, इस प्रकार (भूरि धायसे) नाना प्रकार से जीवन धारण करने वाले तथा (उरुव्यचे) बहुत प्रकार की शक्तियों का विकास करने वाले प्राण के लिए (वयम्) हम सब (सरस्वत्या) ज्ञान की अधिठात्री देवी द्वारा अनुमोदित (हविषा) भोग सामग्री द्वारा (विधेम) परिचर्या करते हैं। निष्कर्ष-ज्ञान पूर्वक भोग करने से प्राण की परिचर्या होती है, हानि नहीं होती। प्राण, अपान और व्यान को संयत करके मनुष्य ज्ञानी, योगी तथा मनीषी बन सकता है। भोग भोग्य है, त्याज्य नहीं। किन्तु उन्हें सीमा में सरस्वती की अनुमति से ही भोगना चाहिए। तभी वे भग (ऐश्वर्य) प्रदान करते हैं । जीवन यज्ञ को सुखपूर्वक बिताने के लिए ब्रह्मा का पथ प्रदर्शन आवश्यक है। १०० यज्ञों को सुचारु रूप से चलाने वाला ब्रह्मा-परमात्मा है। उसका सब से सौम्य, स्नेहमय तथा धी-प्रेरक रूप सरस्वती का है। सरस्वती मातृ रूपा है। इसलिए वह न कभी अकल्याण चाहती और न करती है। शरीर रूपी यज्ञ के ब्रह्मा (मन) पर सरस्वती देवी की कृपा हो तभी श्रद्धा उत्पन्न होती है और आवश्यक भोगों को प्राप्त कराती है। (४५) सं वो मनांसि सं व्रता समाकूतीर्नमामसि। अमी ये विव्रता स्थन तान्वः संनमयामसि ॥ -अथर्व ६-६४-१ (४६) अहं गृभ्णामि मनसा मनांसि मम चित्तमनुचित्तेभिरेत । मम वशेषु हृदयानि वः कृणोमि मम यातमनुवनि एत ॥ – अथर्व ६-६४-२ ऋषि:- अथर्वाङ्गिराः । छन्दः-अनुष्टुप् । विराट् जगती। शब्दार्थ-प्रजापति अर्थात् राष्ट्र में राजा, घर में गृहपति और मानव देह में आत्मा है । और राष्ट्र की प्रजा, घर के सदस्य तथा शरीर की इन्द्रियाँ प्रजाएँ हैं। (वः) पाप प्रजाओं के (मनांसि) मनों या उनकी वृत्तियों को (व्रता) कर्मों तथा (आकृती:) संकल्पों को (सं नमामसि) अपने अनुकूल बनाते हैं और (वः) आप में से (ये अमी) जो ये (विव्रता) विरुद्ध कर्मों वाले (स्थन) हैं (तान्) उनको (संनमयामसि) अच्छे कर्मों की ओर झुकाते हैं। मेरा अपने अनुकूल बनाने का प्रकार जोर जबर्दस्ती का नहीं है। अपितु (अहं) मैं (मनसा) अपने शान्त तथा हित कामना वाले मन से (मनांसि) आप के मनों को (गृभ्णामि) ग्रहण करता हूँ-अपने अनुकूल बनाता हूँ। इसलिए आप लोग (चित्तेभिः) अपने चेतनापूर्ण मनो द्वारा अर्थात् सोच-विचार कर, किसी भय या लोभ से नहीं (मम चित्तमन्) मेरी चेतना के अनुकूल बनकर (एत) मेरी ओर प्राओं मेरी आज्ञाओं तथा इच्छाओं का अनुसरण करो। (वः हृदयानि) आप के हृदयों को (मम वशेष कृणोमि) अपनी इच्छा के अनुसार अपने वश में करता हूँ, ताकि (मम यातमनु) मेरे चलन के अनुकूल (वनिः) आचरण करते हुए (एत) जीवन भर चलते रहो। निष्कर्ष-सब क्षेत्रों में मुखिया का कर्तव्य है कि वह अपने अधीनस्थ जनों के मनों व चितों को प्रेम से, रक्षा से, सुविधाएँ प्रदान करके अपने अनुकूल बनाए। यदि कभी विरोध हो भी जाए तो प्रेम पूर्वक उनकी आवश्यकतामों तथा इच्छाओं को जानकर तदनुकूल व्यवहार द्वारा उनके हृदयों को अपने वश में करने का प्रयत्न करे। अपने आतंक द्वारा उन्हें दबाकर सच्चे अर्थों में अपना अनुगामी या राष्ट्र का हितैषी नहीं बनाया जा सकता। इसी प्रकार अधीनस्थ जनों का कर्तव्य है कि विरोध हो जाने पर वे प्रजापति की इच्छानों का आदर करते हुए, सोच विचार कर उसके अनुकूल बनने का प्रयत्न करें, जिससे राष्ट्र, गृह या शरीर में विरोध न दिखाई दे। विशेष—मन, संकल्प, व्रत, चित, हृदय इत्यादि सरस्वती की कृपा और सहायता से ही एकमत होकर समान मार्ग पर चलते हैं। (४७) यस्ते पृथः स्तनयित्नुर्य ऋष्वो देवः केतुविश्वमाभूषतीदम् । मा नो वधीविद्युता देवसस्य मोत वधी रश्मिभिः सूर्यस्य । -अथर्व ७-११-१ ऋषिः-शौनकः । देवता-सरस्वती । छन्द:-त्रिष्टुप् । शब्दार्थ-हे सरस्वति देवि ! (ते) तेरा (यः) जो (पृथः) विस्तृत (स्तनयित्नः) स्तन या मेघ के समान पोषण तथा शान्ति देने वाला (ऋष्वः) दर्शनीय तथा महान् (दैवः केतुः) दिव्य ज्ञान (इदं विश्वम्) इस सारे विश्व को (आभूषति) प्राभूषण की तरह स्पृहणीय तथा आकर्षक बनाता है। हमारे लिए हितकर उस (देवसस्यम्) देवताओं के भोजन रूप ज्ञान को (विद्युता) विद्युत् के समान चपल चमक से (मा वधी:) समाप्त मत कर और (सूर्यस्य रश्मिभिः) ज्ञान सूर्य की प्रखर किरणों की चकाचोंध से (मा वधी:) मत समाप्त कर। निष्कर्ष-सरस्वती की साधना द्वारा सुषुम्ना में प्रवाहित कुण्डलिनी शक्ति के जागरण से प्राप्त ज्ञान ही देवताओं का भोजन है । देवकामी जन इसी भोजन पर जीवित रहते हैं, और यह भोजन उन्हें आकर्षक, शान्त और अनुकरणीय बनाता है। चकाचौंध उत्पन्न करने वाला राजस (वैज्ञानिक) ज्ञान तथा सूर्य की रश्मियों के समान शुभ्र सात्विक (दार्शनिक) ज्ञान भी देवकोटि में पहुंचने वाले मनुष्य के लिए बन्धन कारक है। इसलिए इन दोनों से रक्षा की प्रार्थना की गई है। विशेष—इस मन्त्र का ऋषि शौनक अपने नाम द्वारा निर्देश करता है कि यदि मनष्य ज्ञान वृद्धि या किसी भी प्रकार की समद्धि प्राप्त करके सुखी बनना चाहता है तो उसे सरस्वती की साधना करके शभ्र बने रहना चाहिये। किसी प्रकार की प्रासक्ति में नहीं पड़ना चाहिए। (४८) यदाशसा वदतो मे विचक्षभे यद्याचमानस्य चरतो जनॉ अनु। यदात्मनि तन्वो मे विरिष्टं सरस्वती तदापणद् घृतेन ॥ -अथर्व ७-५७-१ ऋषिः–वामदेवः । देवता-सरस्वती । छन्दः-जगती। शब्दार्थ-(यद्) यदि (प्राशसा वदतः) किसी इच्छा को व्यक्त करते हुए और उसे पूरा करने के लिए (जनॉ अनु चरतः) मनष्यों के पीछे-पीछे चलकर (याचमानस्य) याचना करते हुए (मे) मेरा मन (विचक्षुभे) क्षब्ध हुआ है (यद्) अथवा (मे तन्वः आत्मनि) स्थल, सूक्ष्म या कारण शरीर के अन्तरात्मा में (विरिष्टं) हिंसा रोग या न्यूनता आ गई है तो (सरस्वती) मातृ रूपा संस्कृति या सरस्वती देवी (तद्) उस न्यूनता को (धृतेन) घृत सदृश स्निग्धता या दीप्ति से (अापणत्) पूरित कर दे। निष्कर्ष—-इच्छा उत्पन्न होने पर, उसे पूरा करने के प्रयत्न में अथवा उसके पूरा न होने से मन क्षुब्ध होता है। इसलिए मन को शान्त रखने के लिए इच्छाओं को त्यागने का प्रयत्न करना चाहिए। शरीर की हिंसा होने पर घाव में या क्षीणता होने पर घृत उपचार का काम देता है। और मन के विक्षोभ में ज्ञान की दीप्ति से शान्ति मिलती है। विशेष-इच्छा को त्यागने से पूर्व सुन्दर तथा दिव्य विचारों को अपनाना चाहिए। दिव्य विचारों को अपनाने का अर्थ है, स्वार्थ, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध आदि दुर्भावनाओं की पूरी तरह से मुक्ति। इस क्रम को अपनाए बिना सहसा इच्छाओं को त्यागना संभव नहीं है। (४६) सप्त क्षरन्ति शिशवे मरुत्वते पित्रे पुत्रासो अप्यवीवृतन्नतानि उभे इदस्योभे अस्य राजत उभे यतेते उभे अस्य पुष्यतः॥ -अथर्व ७-५७-२ ऋषिः–वामदेवः । देवता-सरस्वती। छन्दः-जगती। शब्दार्थ-(मरुत्वते) प्राण साधना में लगे हुए (शिशवे) शिशु तुल्य सरल चित्त वाले (पित्रे) अपने मन और शरीर की रक्षा में लगे साधक के लिए (पुत्रासः सप्त) सर्पण शील सातों ऋषि (५ ज्ञानेन्द्रियाँ+मन+बुद्धि) (ऋतानि-क्षरन्ति) अपने ज्ञाच रूपी जल को क्षरित करते रहते हैं। (अपि) यदि साधक इन ऋतों को (अवीवतन्) अपने जीवन में प्रवृत्त कर ले तो (अस्य) इस साधक के (उभे) दोनों शरीर और मन (यतेते) साधना का प्रयत्न करते रहते हैं (उभे अस्य पुष्यतः) दोनों पुष्ट और सक्षम हो जाते हैं और (उभे अस्य राजतः) दोनों ही दीप्त होकर विराजते हैं। निष्कर्ष-साधक का चित्त शिशु की तरह सरल तथा दुरितों से अनजान होना चाहिए। उसे अपने शरीर और इन्द्रियों की पुत्र के समान रक्षा करनी चाहिए। ये इन्द्रियाँ हेय नहीं, ऋषि तुल्य हैं और शरीर की रक्षा सदा प्रमाद रहित होकर करती है। इन्द्रियाँ-शरीर, शरीर-मन, मन-प्रात्मा के युगल इस मन्त्र में उभे शब्द से ग्रहण किए जा सकते हैं। विशेष—मनुष्य को पशु कोटि में न जाकर देवकोटि में जाने का प्रयत्न करना चाहिए। देव बनने के बाद उसे वामदेव और महादेव बनना चाहिए। महादेव ही पूर्ण योगी अथवा प्राण साधना के आदर्श हैं (५०) सरस्वति व्रतेषु ते दिव्येषु देवि धामसु। जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि ररास्व नः ॥ -अथर्व ७-६८-१ (५१) इदं ते हव्यं घृतवत्सरस्वति-इदं पितृणां हविरास्यं यत् । इमानि त उदिता शंतमानि तेभिर्वयं मधुमन्तः स्याम ॥ -अथर्व ७-६८-२ (५२) शिवा नः शंतमा भव सुमडीका सरस्वति। मा ते युयोम संदृशः॥ -अथर्व ७-६८-३ ऋषिः-शन्तातिः । देवता-सरस्वती । छन्दः-अनुष्टुप्-त्रिष्टुप्-गायत्री। ब्रह्मचर्याश्रम में रहकर विद्या प्राप्त करने के बाद, जब मनुष्य गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर लेता है। तब शान्ति की इच्छा से इस सूक्त का पाठ करता है । इसलिए यह भी माना जा सकता है कि गृहस्थी अपनी पत्नी की सरस्वती के रूप में इस सूक्त द्वारा स्तुति करता है, और उससे गृहस्थ को मधुरता, शान्ति तथा सुख प्रदान करने की प्रार्थना करता है। शब्दार्थ-(देवि सरस्वति) हृदय में रस को प्रवाहित करने वाली हे देवि (ते दिव्येषु व्रतेषु) तेरे साथ किए हुए दिव्य व्रतों को पूरा करते हुए और (दिव्येषु धामसु) दिव्य पवित्र धामों में विहार करते हुए (आहुतं हव्यं) तेरे निमित्त लाये हुए भोग्य पदार्थों को (जुषस्व) प्रीतिपूर्वक सेवन कर, सुखपूर्वक रह और (देवि) हे देवि, यथा समय (न:) हमारे कुल के लिए (प्रजां ररास्व) सन्तान प्राप्त करा। (सरस्वति) हे देवि (ते) तेरे लिए (इदं धृतवत् हव्यम्) ये स्निग्ध मधुर भोज्य पदार्थ तथा (पितृणाम् ) पितृ परम्परा से प्राप्त (आस्यं हविः) स्वाद के लिए मुख में डालने योग्य भोज्य वस्तुएँ उपस्थित हैं। इस प्रकार हमारे घर में (ते) तेरे लिए (इमानि शंतमनि उदिता) सब प्रकार से शान्त परिस्थितियाँ प्राप्त हैं। इसलिए (तेभिः) उन भोज्य पदार्थों और परिस्थितियों के कारण तू ऐसा व्यबहार चला कि (वयं) हम घर के सभी सदस्य (मधुमन्तः स्याम) परस्पर मधुर व्यवहार करने वाले बने रहें। (सरस्वति) हे सरस हृदये! तू (न:) हमारे कुल के लिए (शिवा) कल्याणकारिणी (शंतमा) शान्ति स्थापिका तथा (सुमृडीका) अच्छी प्रकार सुख कारिणी (भव) हो। हम कभी (ते संदृशः) तेरी दृष्टि से (मा युयोम) ओझल न हो जावें । तू हममें से किसी की उपेक्षा मत करना । सबका ध्यान रख । निष्कर्ष-पत्नी की इच्छा के बिना और पत्नी को सन्तुष्ट किए बिना उत्तम सन्तान नहीं प्राप्त हो सकती। यद्यपि भोजन की अपनी कुल परम्परा होती है, फिर भी नववधू के स्वाद का ध्यान रखना चाहिए। उसे सन्तुष्ट रखे बिना घर में शान्ति और मधुरता प्रवाहित नहीं हो सकती। यदि पत्नी चाहे तो घर को कल्याण, शान्ति और सुख का धाम बना सकती है। और तब कोई भी सदस्य उसकी दृष्टि से वियुक्त नहीं होना चाहता है। (५३) प्रतितिष्ठ विराडसि विष्णरिवेह सरस्वति । सिनीवालि प्रजायतां भगस्य समतावसत् ॥ -अथर्व १४-२-१५ ऋषिः-सूर्या सावित्री। देवता-सरस्वती। छन्दः-भुरिक् त्रिष्टुप् । शब्दार्थ-(सरस्वति)हे सरस हृदये, मातकामे, देवि (विराट् असि) तू अपने प्रेम और मातत्व के कारण विशिष्ट दीप्ति से सम्पन्न है। इसलिए (विष्णुरिव) सर्वत्र व्याप्त होने वाले सूर्य के समान (प्रतितिष्ठ) सबके हृदयों में प्रतिष्ठा पूर्वक विराजमान हो । हे (सिनीवालि) अन्न प्रदायिनि और अतएव सबको प्रेम द्वारा बाँधने वाली देवि ! तू ऐसी कृपा कर कि हमारे कुल में सदा (भगस्य प्रजायताम् ) सौभाग्य की उत्पत्ति होती रहे। इस कुल का प्रत्येक सदस्य सदा (भगस्य) ऐश्वर्य प्रदाता देव की (सुमतौ असत्) अच्छी सम्मति (कृपा) का पात्र बना रहे — निष्कर्ष-१. जहाँ सुमति तहाँ सम्पति नाना। २. प्रेमपूर्वक अन्नदान का बन्धन बड़ा दृढ़ होता है। इस बन्धन से दृष्टिकोण संकचित न होकर विस्तृत होता है । दृष्टिकोण के विस्तार के साथ-साथ प्रतिष्ठा और घनिष्ठता भी बढ़ती जाती है। ३. ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः। ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षष्णां भग इतीरणा ।। विशेष—इस मन्त्र की ऋषिका सावित्री-उत्पादन की है। वह सन्तान पान करती है। और घर के लिए उपयोगी पदार्थों के उत्पादन में व्यस्त रहती हई ऐश्वर्य को बढ़ाती रहती है। परिणामतः अपने कुल में और समाज में प्रेरणा का स्रोत (सूर्या) बन जाती है। सावित्री की तरह सती स्त्री सदा सूर्या के समान विश्व में चमकेगी और सबको प्रकाश देगी।
Related Posts
0 Comments
Comments are not available.