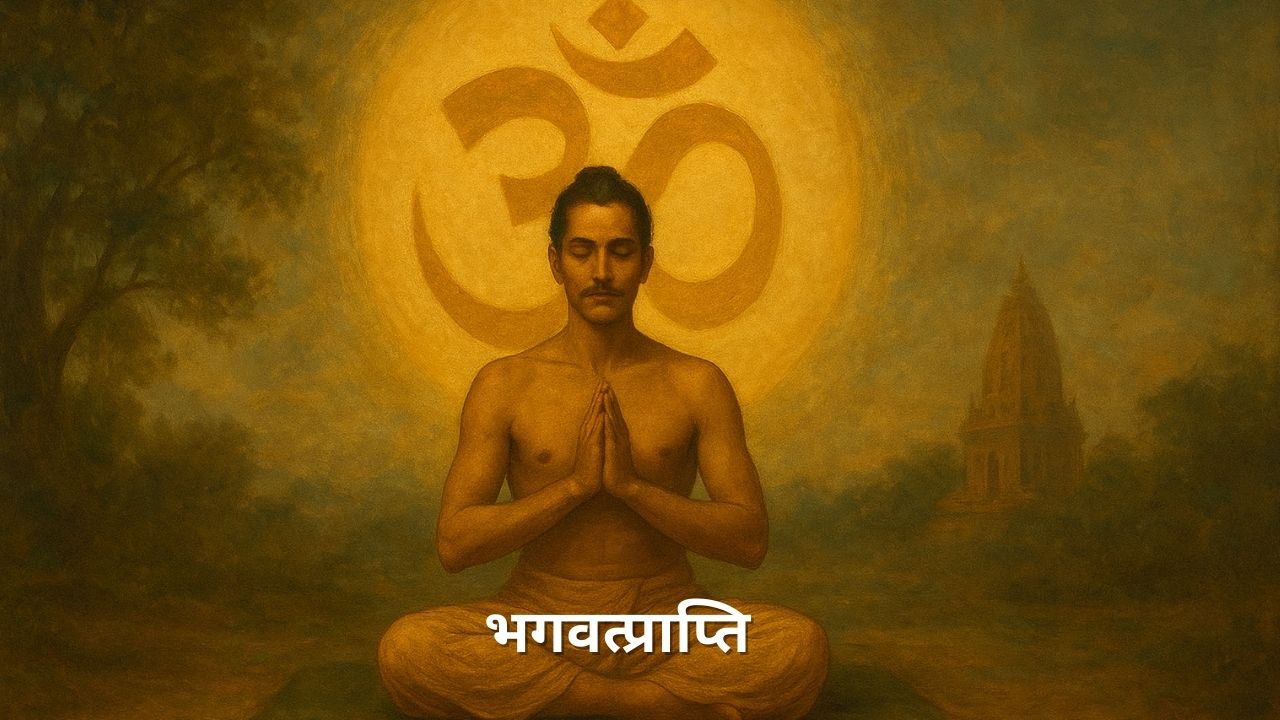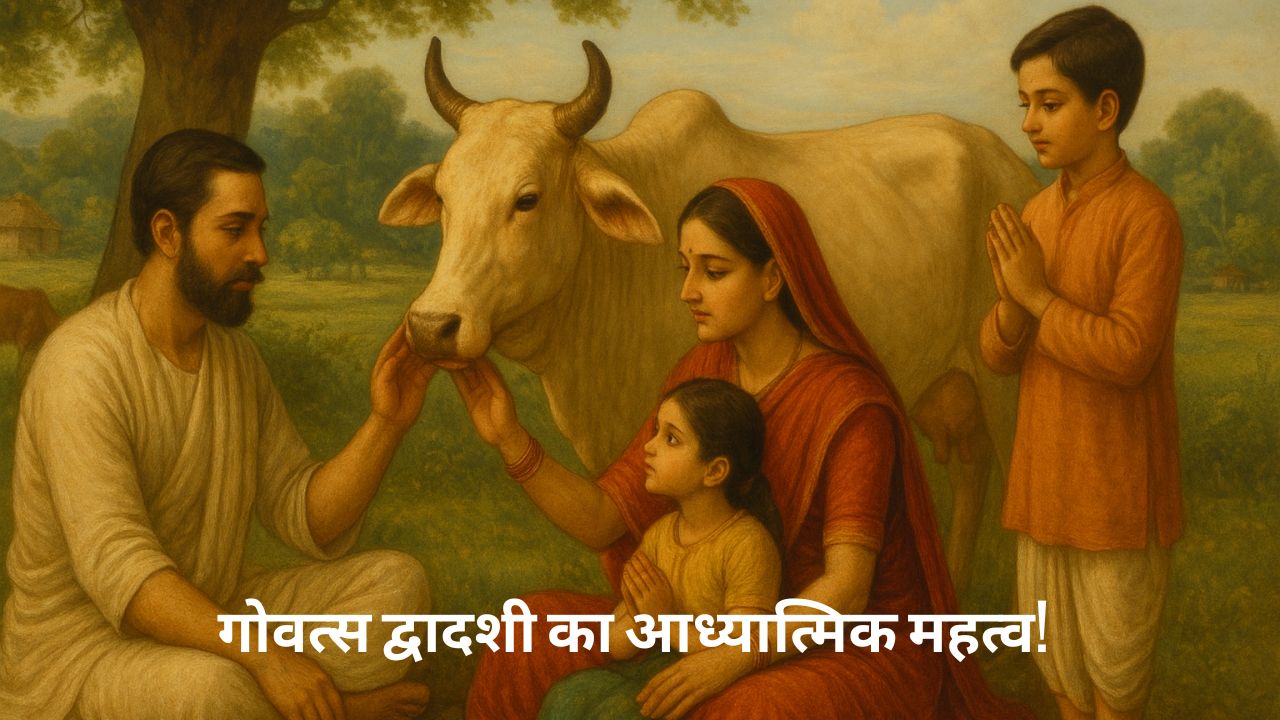- धर्म-पथ
- |
- 31 October 2024
- |
- 0 Comments
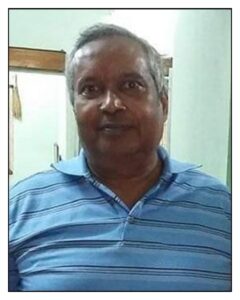 अरुण कुमार उपाध्याय (धर्मज्ञ)-
गीता, अध्याय ३ में अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण से कहा कि कभी आप कहते हैं कि ज्ञान अच्छा है, कभी कहते हैं कि कर्म करो। मिश्रित वाक्यों से मुझे भ्रमित कर रहे हैं। निश्चित कर कहिये कि दोनों में कौन अच्छा है। भगवान् ने कहा कि पहले मैंने लोक में २ प्रकार की निष्ठा कही है-सांख्य मार्ग वालों की ज्ञान योग तथा योगियों की कर्मयोग से। बिना कर्म आरम्भ किये मनुष्य कोई भोग नहीं कर सकता है, केवल संन्यास से ही कोई सिद्धि नहीं मिलती।
अर्जुन उवाच-ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन।
तत्किं कर्मणी घोरे मां नियोजयसि केशव॥१॥
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे।
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्॥२॥
श्रीभगवानुवाच-लोकेऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ।
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्॥३॥
न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुषोश्नुते।
न च संन्यस्नादेव सिद्धिं समधिगच्छति॥४॥ (गीता, ३/१-४)
यहां पहले या प्राचीन काल से तात्पर्य भगवान् के पूर्व अवतार से है, जिसकी चर्चा अगले चतुर्थ अध्याय में है-पहले मैंने विवस्वान् को यह योग बताया था, उनसे क्रमशः वैवस्वत मनु और इक्ष्वाकु को मिला तब से परम्परा द्वारा राजर्षियों को मिला। बहुत काल बीतने पर यह परम्परा नष्ट हो अयी जिसे वे पुनः प्रारम्भ कर रहे हैं।
श्रीभगवानुवाच-इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्।
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिष्वाकवेऽब्रवीत्॥१॥
एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः।
स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप॥२॥ (गीता, ४/१-२)
यही अगस्त्य ने सुतीक्ष्ण को कहा था-
सुतीक्ष्ण उवाच-मोक्षस्य कारणं कर्म ज्ञानं वा मोक्षसाधनम्।
उभयं वा विनिश्चित्य एकं कथय कारणम्॥६॥
अगस्तिः उवाच-उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः।
तथैव ज्ञानकर्मभ्यां जायते परमं पदम्॥७॥
(योगवासिष्ठ रामायण, १/१/६-७)
जैसे पक्षी दोनों पंखों से ही उड़ सकते हैं, उसी प्रकार मनुष्य ज्ञान के साथ कर्म द्वारा ही परम पद पा सकता है।
गीता के अन्तिम अध्याय में अधिक सूक्ष्म वर्णन है-
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना।
करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः॥१८॥
ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः।
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि॥१९॥
कर्म द्वारा ही ज्ञान मिल सकता है वह भी पूरा नहीं-ज्ञान अनन्त है, उसमें वही वस्तु ज्ञेय है जिसका साम (महिमा, प्रभाव) हम तक पहुंचता है। ज्ञेय का भी कुछ ही अंश जान सकते हैं, वह भी स्पष्ट नहीं, केवल परिज्ञान-कई अनुमानों का समन्वय। इसके कई कारण दर्शन तथा विज्ञान में कहे हैं-हमारे अनुभव या यन्त्र की क्षमता, दर्शन क्रिया द्वारा वस्तु में परिवर्तन (आधुनिक भौतिक विज्ञान में मैक तथा आइंस्टीन का सापेक्षवाद, क्वाण्टम मेकानिक्स), विचार या शब्द द्वारा पूर्ण वर्णन की असमर्थता। अव्यक्त ज्ञान को प्रकट करने के लिए शब्द नहीं मिलते-उनका अनुमान कई शब्दों से घेर कर होता है, जिसे ईशावास्योपनिषद् में पर्यगात् तथा द्रष्टा को परिभू कहा है-
स पर्यगात् शुक्रं अकायं अव्रणं अस्नाविरं शुद्धं अपापविद्धं, कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूः याथातथ्यतो अर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः।
कर्म के ३ अंग हैं-करण (उपकरण, साधन), कर्म, कर्ता। सांख्य में चेतन पुरुष तत्त्व कर्ता है, साधन या भौतिक पदार्थ प्रकृति के रूप हैं। कर्ता को विधि का ज्ञान होने पर ही कर्म कर सकता है। यह ज्ञान तत्त्व सांख्य दर्शन में नहीं है।
अहंकार के कारण मनुष्य द्वैत को स्वीकार नहीं करता। अपने विचार के अतिरिक्त अन्य विचार का विरोध करते हैं। किसी भी भाषा के शब्दकोष में हर शब्द के कई वैकल्पिक अर्थ होते हैं। इसी प्रकार वेद मन्त्रों के कई प्रकार के आधिदैविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक अर्थ हैं। कई बार परस्पर विरोधी अर्थ एक साथ ठीक होते हैं। भौतिक विज्ञान में इसे मानसिक रूप से स्वीकार करने में कठिनाई होती है कि इलेक्ट्रोन या अन्य कण कण हैं या तरंग। या मात्रा की शुद्ध माप करने पर ऊर्जा की अशुद्धि बढ़ जाती है। इस प्रकार का द्वैत अभिनवगुप्त के तन्त्रालोक में है। यदि ध्यान द्वारा किसी घटना को देखते हैं, तो उसके काल निर्णय में अशुद्धि होती है (३ दिन, ३ मास, ३ पक्ष या ३ वर्ष का अनुमान होता है)।
माधवीय शंकर दिग्विजय, अध्याय ८ में ३ विरोधी तत्त्वों पर शास्त्रार्थ की चर्चा है जो मण्डन मिश्र के घर के सुग्गे भी रटते थे-
फलप्रदं कर्म फाल्प्रदोऽजः कीराङ्गनाः यत्र गिरं गिरन्ति।
द्वारस्थ नीडान्तर सन्निरुद्धा जानीहि तन्मण्डनपण्डितौकः॥
जगद् ध्रुवं स्यात्, जगदध्रुवं स्यात्, कीराङ्गनाः —॥
स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं, कीराङ्गनाः —॥
तीनों विपरीत युग्म एक साथ ठीक हैं इस कारण सभी की चर्चा होती है। कर्म से ही फल मिल सकता है, किन्तु सफलता बाह्य परिस्थिति पर भी निर्भर है। जगत् में ध्रुव और अध्रुव (क्षर-अक्षर विभाग) दोनों हैं। वेद स्वतः प्रमाण है, किन्तु उसका अर्थ मीमांसा, वेदान्त, निरुक्त, ज्योतिष आदि सिद्धान्तों पर निर्भर है।
कई लोगों की धारणा है कि प्राचीन काल के ऋषि मुनि केवल ध्यान द्वारा सृष्टि रहस्य जान लेते थे। कुछ कहते हैं कि यज्ञ में हवन कर या पशुबलि दे कर गणना करते थे। २००५ में प्रख्यात वैज्ञानिक श्री जयन्त नार्लीकर ने भारत में ज्योतिष का अज्ञान सिद्ध करने के लिए ५ प्रश्न पूछे थे तथा उत्तर देने वाले के साथ चर्चा का प्रस्ताव रखा था। विश्व की माप तथा ग्रहण गणना आदि से सम्बन्धित प्रश्न थे। मैंने भारतीय ज्योतिष की माप के १५ उदाहरण दिये जो उनकी पुस्तक Cosmology, Cambridge University Press, में नहीं थी या अशुद्ध थी। उनकी शिकायत थी कि ग्रहण का उल्लेख नहीं होने के कारण काल निर्धारण नहीं हो पाता है। मैंने १७ ईमेल द्वारा ३०० ग्रहण उल्लेख के उदाहरण केवल ओड़िशा के प्रकाशित दानपत्रों के अनुसार दिये तथा उनका काल निर्धारण करने का आग्रह किया।
भारत के राजा प्रायः सूर्यग्रहण के समय दान देते थे। मन्त्र साधना भी उसी समय होती थी। इसके लिए आवश्यक है कि सूर्यग्रहण के समय और स्थान की सटीक गणना हो। इस पर नारलीकर जी ने कहा कि वे गणना करने में असमर्थ हैं और मुझे कहा कि संस्कृत पण्डित श्री सुब्बारायप्पा से सम्पर्क करें। ग्रहण से दीर्घकालिक समय निर्धारण मूर्खतापूर्ण कल्पना है, क्योंकि ग्रहण का चक्र १८ वर्ष १० दिन का होता है। इसके अर्ध चक्र में भी ग्रहण पुनः उसी प्रकार होते हैं-३३३९ चान्द्र तिथि में जिसका उल्लेख ऋग्वेद (३/९/९) में है। १९८५ के अन्तर-राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण में रूस के वैज्ञानिक अम्बरसौम्यन (आकाश का ज्ञाता) कहा था कि भारत के लोग १०,००० वर्ष पूर्व भी ग्रहण की गणना कर लेते थे, पर सम्मेलन में उपस्थित विश्व के २०० श्रेष्ठ वैज्ञानिक ऐसा करने में असमर्थ हैं। नारलीकर के आग्रह से आयोजित सेमिनार में वह स्वयं अनुपस्थित हो गये। उनके प्रतिनिधि तथा भारतीय ज्योतिष इतिहास के सहलेखक आये तथा कहा कि भारत में विज्ञान की परम्परा नहीं थी और पुरोहित लोग बकरे की बलि दे कर ग्रहण गणना करते थे। मैंने आग्रह किया कि आप बकरे की बलि दे कर कम से कम छत की उंचाई बता दें, सूर्य चन्द्र तो बहुत दूर हैं। विज्ञान का अर्थ नहीं समझने के बारे में कुछ नहीं कहा, मुझे गाली दी कि उनका अपमान हो रहा है। यज्ञ का अर्थ पशुबलि (Sacrifice) तथा ऋषि का अर्थ पुरोहित (priest) कर ऐसा भ्रम फलाया गया है। कुछ अन्य लोगों ने कहा कि ध्यान द्वारा गणना की जाती थी। सूर्य सिद्धान्त या वेद-पुराण में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। उनसे मैंने आग्रह किया कि खीर बनाने के लिये चीनी जा रही थी-ध्यान द्वारा उसकी मात्रा बतायें तथा चीनी है या गुड़-यह कहें। ध्यान का उपयोग मन को शान्त कर विधि समझने के लिए है। किन्तु माप दो बाह्य चीजों की तुलना है-जैसे लम्बाई माप के लिए मीटर तथा इच्छित दूरी की तुलना माप कर या गणित द्वारा करते हैं।
इसी प्रकार केवल ध्यान द्वारा शारीरिक शक्ति नहीं मिल सकती। उसके लिए व्यायाम, सात्विक भोजन, नियमित जीवन भी चाहिये। ध्यान इसमें सहायक हो सकता है, पर वह पर्याप्त नहीं है।
अरुण कुमार उपाध्याय (धर्मज्ञ)-
गीता, अध्याय ३ में अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण से कहा कि कभी आप कहते हैं कि ज्ञान अच्छा है, कभी कहते हैं कि कर्म करो। मिश्रित वाक्यों से मुझे भ्रमित कर रहे हैं। निश्चित कर कहिये कि दोनों में कौन अच्छा है। भगवान् ने कहा कि पहले मैंने लोक में २ प्रकार की निष्ठा कही है-सांख्य मार्ग वालों की ज्ञान योग तथा योगियों की कर्मयोग से। बिना कर्म आरम्भ किये मनुष्य कोई भोग नहीं कर सकता है, केवल संन्यास से ही कोई सिद्धि नहीं मिलती।
अर्जुन उवाच-ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन।
तत्किं कर्मणी घोरे मां नियोजयसि केशव॥१॥
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे।
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्॥२॥
श्रीभगवानुवाच-लोकेऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ।
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्॥३॥
न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुषोश्नुते।
न च संन्यस्नादेव सिद्धिं समधिगच्छति॥४॥ (गीता, ३/१-४)
यहां पहले या प्राचीन काल से तात्पर्य भगवान् के पूर्व अवतार से है, जिसकी चर्चा अगले चतुर्थ अध्याय में है-पहले मैंने विवस्वान् को यह योग बताया था, उनसे क्रमशः वैवस्वत मनु और इक्ष्वाकु को मिला तब से परम्परा द्वारा राजर्षियों को मिला। बहुत काल बीतने पर यह परम्परा नष्ट हो अयी जिसे वे पुनः प्रारम्भ कर रहे हैं।
श्रीभगवानुवाच-इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्।
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिष्वाकवेऽब्रवीत्॥१॥
एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः।
स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप॥२॥ (गीता, ४/१-२)
यही अगस्त्य ने सुतीक्ष्ण को कहा था-
सुतीक्ष्ण उवाच-मोक्षस्य कारणं कर्म ज्ञानं वा मोक्षसाधनम्।
उभयं वा विनिश्चित्य एकं कथय कारणम्॥६॥
अगस्तिः उवाच-उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः।
तथैव ज्ञानकर्मभ्यां जायते परमं पदम्॥७॥
(योगवासिष्ठ रामायण, १/१/६-७)
जैसे पक्षी दोनों पंखों से ही उड़ सकते हैं, उसी प्रकार मनुष्य ज्ञान के साथ कर्म द्वारा ही परम पद पा सकता है।
गीता के अन्तिम अध्याय में अधिक सूक्ष्म वर्णन है-
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना।
करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः॥१८॥
ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः।
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि॥१९॥
कर्म द्वारा ही ज्ञान मिल सकता है वह भी पूरा नहीं-ज्ञान अनन्त है, उसमें वही वस्तु ज्ञेय है जिसका साम (महिमा, प्रभाव) हम तक पहुंचता है। ज्ञेय का भी कुछ ही अंश जान सकते हैं, वह भी स्पष्ट नहीं, केवल परिज्ञान-कई अनुमानों का समन्वय। इसके कई कारण दर्शन तथा विज्ञान में कहे हैं-हमारे अनुभव या यन्त्र की क्षमता, दर्शन क्रिया द्वारा वस्तु में परिवर्तन (आधुनिक भौतिक विज्ञान में मैक तथा आइंस्टीन का सापेक्षवाद, क्वाण्टम मेकानिक्स), विचार या शब्द द्वारा पूर्ण वर्णन की असमर्थता। अव्यक्त ज्ञान को प्रकट करने के लिए शब्द नहीं मिलते-उनका अनुमान कई शब्दों से घेर कर होता है, जिसे ईशावास्योपनिषद् में पर्यगात् तथा द्रष्टा को परिभू कहा है-
स पर्यगात् शुक्रं अकायं अव्रणं अस्नाविरं शुद्धं अपापविद्धं, कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूः याथातथ्यतो अर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः।
कर्म के ३ अंग हैं-करण (उपकरण, साधन), कर्म, कर्ता। सांख्य में चेतन पुरुष तत्त्व कर्ता है, साधन या भौतिक पदार्थ प्रकृति के रूप हैं। कर्ता को विधि का ज्ञान होने पर ही कर्म कर सकता है। यह ज्ञान तत्त्व सांख्य दर्शन में नहीं है।
अहंकार के कारण मनुष्य द्वैत को स्वीकार नहीं करता। अपने विचार के अतिरिक्त अन्य विचार का विरोध करते हैं। किसी भी भाषा के शब्दकोष में हर शब्द के कई वैकल्पिक अर्थ होते हैं। इसी प्रकार वेद मन्त्रों के कई प्रकार के आधिदैविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक अर्थ हैं। कई बार परस्पर विरोधी अर्थ एक साथ ठीक होते हैं। भौतिक विज्ञान में इसे मानसिक रूप से स्वीकार करने में कठिनाई होती है कि इलेक्ट्रोन या अन्य कण कण हैं या तरंग। या मात्रा की शुद्ध माप करने पर ऊर्जा की अशुद्धि बढ़ जाती है। इस प्रकार का द्वैत अभिनवगुप्त के तन्त्रालोक में है। यदि ध्यान द्वारा किसी घटना को देखते हैं, तो उसके काल निर्णय में अशुद्धि होती है (३ दिन, ३ मास, ३ पक्ष या ३ वर्ष का अनुमान होता है)।
माधवीय शंकर दिग्विजय, अध्याय ८ में ३ विरोधी तत्त्वों पर शास्त्रार्थ की चर्चा है जो मण्डन मिश्र के घर के सुग्गे भी रटते थे-
फलप्रदं कर्म फाल्प्रदोऽजः कीराङ्गनाः यत्र गिरं गिरन्ति।
द्वारस्थ नीडान्तर सन्निरुद्धा जानीहि तन्मण्डनपण्डितौकः॥
जगद् ध्रुवं स्यात्, जगदध्रुवं स्यात्, कीराङ्गनाः —॥
स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं, कीराङ्गनाः —॥
तीनों विपरीत युग्म एक साथ ठीक हैं इस कारण सभी की चर्चा होती है। कर्म से ही फल मिल सकता है, किन्तु सफलता बाह्य परिस्थिति पर भी निर्भर है। जगत् में ध्रुव और अध्रुव (क्षर-अक्षर विभाग) दोनों हैं। वेद स्वतः प्रमाण है, किन्तु उसका अर्थ मीमांसा, वेदान्त, निरुक्त, ज्योतिष आदि सिद्धान्तों पर निर्भर है।
कई लोगों की धारणा है कि प्राचीन काल के ऋषि मुनि केवल ध्यान द्वारा सृष्टि रहस्य जान लेते थे। कुछ कहते हैं कि यज्ञ में हवन कर या पशुबलि दे कर गणना करते थे। २००५ में प्रख्यात वैज्ञानिक श्री जयन्त नार्लीकर ने भारत में ज्योतिष का अज्ञान सिद्ध करने के लिए ५ प्रश्न पूछे थे तथा उत्तर देने वाले के साथ चर्चा का प्रस्ताव रखा था। विश्व की माप तथा ग्रहण गणना आदि से सम्बन्धित प्रश्न थे। मैंने भारतीय ज्योतिष की माप के १५ उदाहरण दिये जो उनकी पुस्तक Cosmology, Cambridge University Press, में नहीं थी या अशुद्ध थी। उनकी शिकायत थी कि ग्रहण का उल्लेख नहीं होने के कारण काल निर्धारण नहीं हो पाता है। मैंने १७ ईमेल द्वारा ३०० ग्रहण उल्लेख के उदाहरण केवल ओड़िशा के प्रकाशित दानपत्रों के अनुसार दिये तथा उनका काल निर्धारण करने का आग्रह किया।
भारत के राजा प्रायः सूर्यग्रहण के समय दान देते थे। मन्त्र साधना भी उसी समय होती थी। इसके लिए आवश्यक है कि सूर्यग्रहण के समय और स्थान की सटीक गणना हो। इस पर नारलीकर जी ने कहा कि वे गणना करने में असमर्थ हैं और मुझे कहा कि संस्कृत पण्डित श्री सुब्बारायप्पा से सम्पर्क करें। ग्रहण से दीर्घकालिक समय निर्धारण मूर्खतापूर्ण कल्पना है, क्योंकि ग्रहण का चक्र १८ वर्ष १० दिन का होता है। इसके अर्ध चक्र में भी ग्रहण पुनः उसी प्रकार होते हैं-३३३९ चान्द्र तिथि में जिसका उल्लेख ऋग्वेद (३/९/९) में है। १९८५ के अन्तर-राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण में रूस के वैज्ञानिक अम्बरसौम्यन (आकाश का ज्ञाता) कहा था कि भारत के लोग १०,००० वर्ष पूर्व भी ग्रहण की गणना कर लेते थे, पर सम्मेलन में उपस्थित विश्व के २०० श्रेष्ठ वैज्ञानिक ऐसा करने में असमर्थ हैं। नारलीकर के आग्रह से आयोजित सेमिनार में वह स्वयं अनुपस्थित हो गये। उनके प्रतिनिधि तथा भारतीय ज्योतिष इतिहास के सहलेखक आये तथा कहा कि भारत में विज्ञान की परम्परा नहीं थी और पुरोहित लोग बकरे की बलि दे कर ग्रहण गणना करते थे। मैंने आग्रह किया कि आप बकरे की बलि दे कर कम से कम छत की उंचाई बता दें, सूर्य चन्द्र तो बहुत दूर हैं। विज्ञान का अर्थ नहीं समझने के बारे में कुछ नहीं कहा, मुझे गाली दी कि उनका अपमान हो रहा है। यज्ञ का अर्थ पशुबलि (Sacrifice) तथा ऋषि का अर्थ पुरोहित (priest) कर ऐसा भ्रम फलाया गया है। कुछ अन्य लोगों ने कहा कि ध्यान द्वारा गणना की जाती थी। सूर्य सिद्धान्त या वेद-पुराण में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। उनसे मैंने आग्रह किया कि खीर बनाने के लिये चीनी जा रही थी-ध्यान द्वारा उसकी मात्रा बतायें तथा चीनी है या गुड़-यह कहें। ध्यान का उपयोग मन को शान्त कर विधि समझने के लिए है। किन्तु माप दो बाह्य चीजों की तुलना है-जैसे लम्बाई माप के लिए मीटर तथा इच्छित दूरी की तुलना माप कर या गणित द्वारा करते हैं।
इसी प्रकार केवल ध्यान द्वारा शारीरिक शक्ति नहीं मिल सकती। उसके लिए व्यायाम, सात्विक भोजन, नियमित जीवन भी चाहिये। ध्यान इसमें सहायक हो सकता है, पर वह पर्याप्त नहीं है।
Related Posts
0 Comments
Comments are not available.