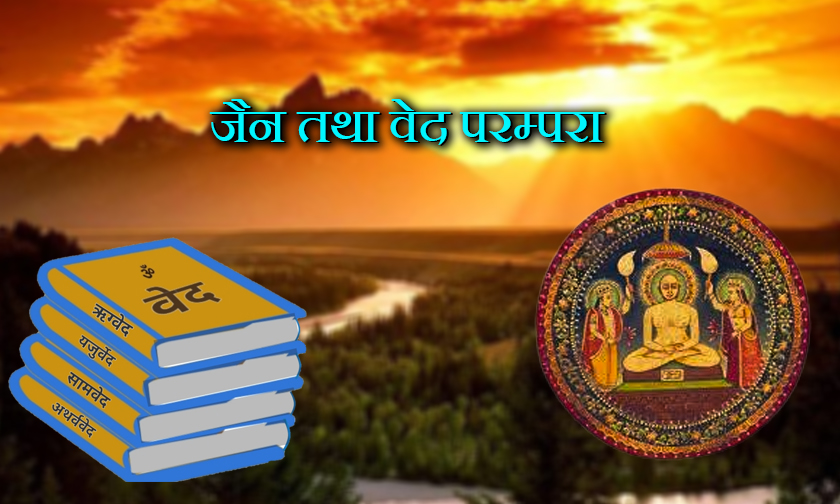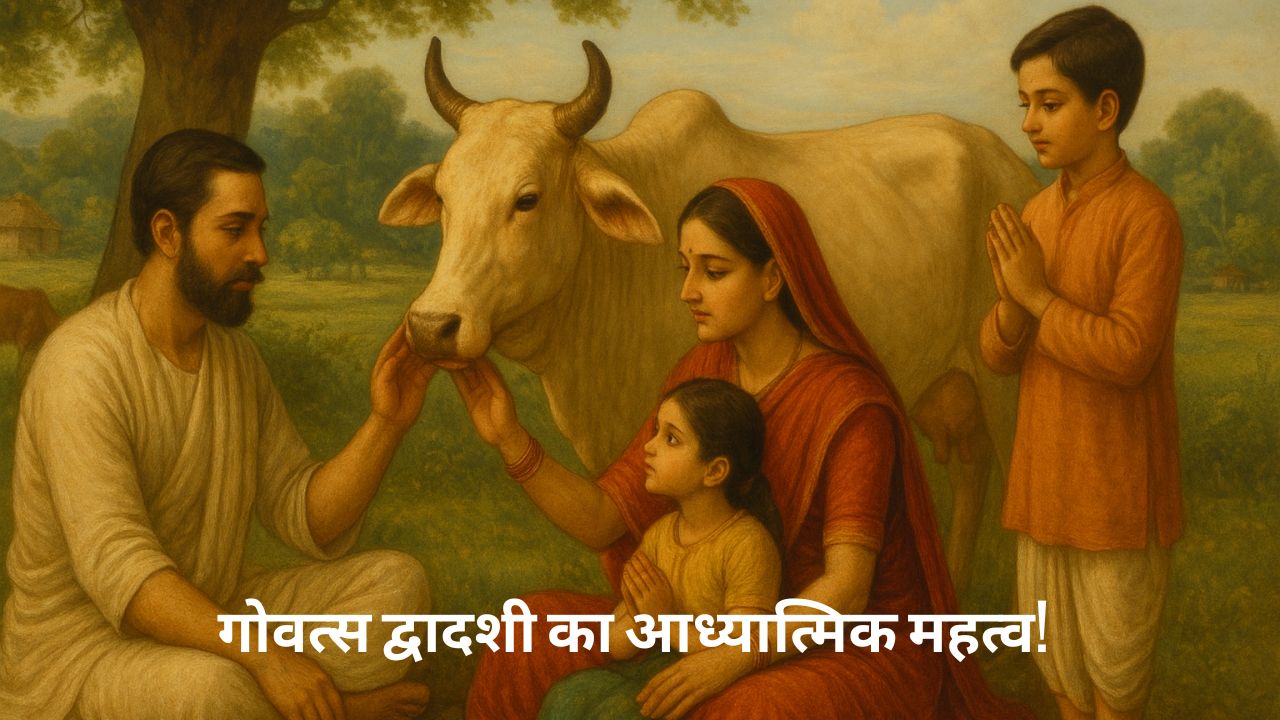- धर्म-पथ
- |
- 31 October 2024
- |
- 0 Comments
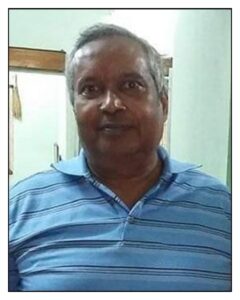 श्री अरुण कुमार उपाध्याय (धर्मज्ञ)
mysticpower- १. जैन तथा वैदिक मत-जैन और बौद्ध मतों को प्रायः नास्तिक या वेद विरोधी मानते हैं। पर वेद में सभी प्रकार के मतों का समन्वय है। शाब्दिक अर्थ के तर्क के रूप में बौद्ध मत भी है जो गौतम के न्याय दर्शन का ही थोड़ा दूसरे शब्दों में वर्णन है। वेद में जैन तर्क भी कई स्थानों पर हैं। जैन तर्क में अस्ति-नास्ति-स्यात् (शायद) को मिलाकर ७ प्रकार के शाब्दिक विकल्प हैं। ३ तथा ७ प्रकार के सत्यों का वर्णन भागवत पुराण में ब्रह्मा द्वारा भगवान् कृष्ण की स्तुति में भी है-
सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। सत्यस्य सत्यम् ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः॥ (भागवत पुराण, १०/२/२६)
श्री अरुण कुमार उपाध्याय (धर्मज्ञ)
mysticpower- १. जैन तथा वैदिक मत-जैन और बौद्ध मतों को प्रायः नास्तिक या वेद विरोधी मानते हैं। पर वेद में सभी प्रकार के मतों का समन्वय है। शाब्दिक अर्थ के तर्क के रूप में बौद्ध मत भी है जो गौतम के न्याय दर्शन का ही थोड़ा दूसरे शब्दों में वर्णन है। वेद में जैन तर्क भी कई स्थानों पर हैं। जैन तर्क में अस्ति-नास्ति-स्यात् (शायद) को मिलाकर ७ प्रकार के शाब्दिक विकल्प हैं। ३ तथा ७ प्रकार के सत्यों का वर्णन भागवत पुराण में ब्रह्मा द्वारा भगवान् कृष्ण की स्तुति में भी है-
सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। सत्यस्य सत्यम् ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः॥ (भागवत पुराण, १०/२/२६)
 https://www.mycloudparticles.com/
वेद में भी ३ प्रकार के ७ विकल्पों का कई स्थानों पर वर्णन है-
ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः। वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे॥१॥ (अथर्व, शौनक संहिता, १/१/१)
सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः। देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुम्। (पुरुष सूक्त, यजुर्वेद, ३१/१५)
https://www.mycloudparticles.com/
वेद में भी ३ प्रकार के ७ विकल्पों का कई स्थानों पर वर्णन है-
ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः। वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे॥१॥ (अथर्व, शौनक संहिता, १/१/१)
सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः। देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुम्। (पुरुष सूक्त, यजुर्वेद, ३१/१५)
 https://www.pixincreativemedia.com/
शब्द रूप में ३ या ७ ही विकल्प होते हैं। गणित के अनुसार अनन्त विकल्प होंगे। इसमें संशय होता है। अतः जैन मत को अनेकान्त या स्याद्वाद भी कहते हैं। वेद में ३ प्रकार के अनन्तों का वर्णन है, जिनको विष्णु सहस्रनाम में अनन्त, असंख्येय, अप्रमेय कहा है। नासदीय सूक्त (ऋग्वेद, १०/१२९) में भी संशयवाद है जिसकी पण्डित मधुसूदन ओझा ने दशवाद रहस्य में व्याख्या की है-
तम आसीत् तमसा गूळ्हमग्रेऽ प्रकेतं सलिलं सर्व मा इदम्।
तुच्छ्येनाभ्व पिहितं यदासीत् तपसस्तन्महिनाजायतैकम्॥३॥
को अद्धा वेद क इह प्र वोचत् कुत अजाता कुत इयं विसृष्टिः।
अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाऽथ को वेद यत आबभूव॥६॥
आरम्भ में सब तरफ अन्धकार था उसमें कोई सीमा या पदार्थ का पता नहीं चलता था। वह स्वयं अपनी महिमा में तप रहा था। निश्चय पूर्वक कोई नहीं कह सकता कि यह सृष्टि कहां से हुई और कैसे इसके बहुत से भेद हो गये। (विसृष्टि = पुराण का प्रतिसर्ग)। देव भी तो सृष्टि के बाद ही हुये, वे कैसे जान सकते हैं कि यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ?
वेद सनातन शास्त्र हैं, उनकी वैज्ञानिक व्याख्या के लिए हर काल में शास्त्र बने थे जो जैन शास्त्र हैं। पार्थिव विश्व को आकाश की प्रतिमा कहा गया है, पर विज्ञान माध्यम से उसे समझने के लिए अलग अलग व्याख्या होगी। अतः वेद के ६ अंग और ६ उपांगों के बदले जैन शास्त्रों में १२ अंग और १२ उपांग थे जिनमें कोई भी उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार मध्वाचार्य का द्वैतवाद है, ब्रह्म अपनी निर्मित सृष्टि में भी है (तत् सृष्ट्वा, तदेव अनुप्राविशत्-तैत्तिरीय उपनिषद्, २/६/४)। किन्तु व्याख्या के लिए अव्यक्त ब्रह्म और भौतिक जगत् को अलग मानना पड़ता है।
२. ऋषि और मुनि- ऋषि शब्द के ७ अर्थ हैं-(१) रस्सी-सृष्टि का मूल १०-३५ मी. के तन्तु। सृष्टि का मूल असत् (अदृश्य) प्राण था जो रस्सी की तरह श्रम और तप से खींचते थे (शतपथ ब्राह्मण, ६/१/१/१) ।
इन ऋषियों से पितर, फिर देव-दानव, देवों से जगत् (चर, स्थाणु, अनुपूर्व-३ प्रकार के कण) हुए-
ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितॄभ्यो देव दानवाः। देवेभ्यश्च जगत्सर्वं चरं स्थाण्वनुपूर्वशः॥ (मनुस्मृति, ३/२०१)
(२) तारा -जैसे सप्तर्षि, (३) मन्त्र द्रष्टा-जो आधिदैविक (आकाश), आधिभौतिक (पृथ्वी) तथा आध्यात्मिक (शरीर के भीतर) विश्वों का सम्बन्ध (इनको जोड़ने वाली रस्सी, या ब्रह्म और सामान्य मनुष्य के बीच की रस्सी), (४) गुरु-शिष्य परम्परा आरम्भ करने वाले (उनके बीच की रस्सी), (५) गोत्र प्रवर्तक (६) आनुवंशिक सम्बन्ध -२१ पीढ़ी तक (७ पीढ़ी तक पिण्ड, १४ पीढ़ी तक उदक, उसके बाद २१ पीढ़ी तक ऋषि), (७) आकाश के १० आयाम (दश, दशा, दिशा, आशा) में ७ वां जो दो कणों के बीच आकर्षण द्वारा सम्बन्ध हैं।
मुनि उसे कहते हैं जो राग, भय, क्रोध से मुक्त हो कर अपने मन और शरीर पर नियन्त्रण रखता है और स्थिर बुद्धि का है-
दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः। वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते॥ (गीता, २/५६)
जो मुनि है, वही ऋषि हो सकता है। ऋषि परम्परा वेद है, मुनि परम्परा लौकिक शास्त्र हैं, जिनसे वेद समझा जा सकता है।
ऋषि सत्य का दर्शन कर सकता है, पर वह तभी स्वीकृत हो सकता है जब सत्ता द्वारा भी समर्थन हो। राजा का भी लोग तभी अनुकरण करते हैं जब वह सच्चरित्र हो। अतः वही लोग जैन तीर्थंकर हुये, जो राजा बनने के बाद सन्यासी बने। राजा के रूप में राज्य चलाने का अनुभव हो, उसके बाद निरपेक्ष और निस्पृह हो। इसी लिये आरुणि उद्दालक को शिक्षा पूरी करने के लिये राजा अश्वपति के पास भेजा गया (छान्दोग्य उपनिषद्, अध्याय ५)। ऐसा ही व्यक्ति लौकिक और पारलौकिक रूप से संसार से पार करा सकता है, अतः उसे तीर्थंकर (नदी या समुद्र पार करने के लिये तट) कहते हैं।
ऋषि या गुरु-शिष्य क्रम तीर्थंकरों में भी है। स्रोत को ऋषभ तथा अन्तिम को महावीर (महः = सीमा) कहा गया है। बीच के सभी नाथ (बान्धने वाले) हैं।
३. वर्तमान युग के तीर्थंकर-पुराणों में अभी ब्रह्माब्द का तीसरा दिन चल रहा है। हर ब्रह्माब्द २४,००० वर्ष का है जिसके २ भाग हैं। प्रथम अवसर्पिणी १२,००० वर्ष का है जिसमें क्रम से सत्य. त्रेता, द्वापर, कलि आते हैं जिनका अनुपात ४,३,२,१ है। उसके बाद १२,००० वर्ष के उत्सर्पिणी में विपरीत क्रम से उतने ही मान के युग आते हैं-कलि, द्वापर, त्रेता, सत्य। वैवस्वत मनु से तीसरा ब्रह्माब्द आरम्भ हुआ है-जिसमें सत्य, त्रेता, द्वापर की समाप्ति महाभारत के ३६ वर्ष बाद ३१०२ ई.पू. में हुई। उसके बाद १२०० वर्षों का कलि १९०२ ई.पू. तक था जिसके बाद उत्सर्पिणी का कलि ७०२ ई.पू. तक, द्वापर १६९९ ई. तक रहा। उसके बाद अभी त्रेता चल रहा है जो ५२९९ ई. तक रहेगा। इस अवसर्पिणी में ऋषभ देव से महावीर तक जैन मत के २४ तीर्थङ्कर हुए। ऋषभ का अर्थ है सभ्यता, ज्ञान, कर्म का आरम्भ, वृषा = वर्षा करने वाला। इसी से वृषभ हुआ है जो कृषि का मूल आधार है जिस पर सभ्यता निर्भर है।
प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि।
स्वलक्षणा प्रादुरभूत्किलास्यतः स मे ऋषीणामृषभः प्रसीदताम्॥ (भागवत पुराण, २/४/२२)
अवसर्पिणी का अन्त १९०२ ई.पू. में हुआ। उससे ३ वर्ष पूर्व भगवान् महावीर का जन्म ११-३-१९०५ ई.पू. चैत्र शुक्ल १३ को हुआ। उनके १३०० वर्ष बाद ५९९ ई.पू. में उज्जैन में जैन मुनि कालकाचार्य का जन्म हुआ जिन्होंने जैन शात्रों का उद्धार किया अतः उनको वीर (महावीर नहीं) कहते हैं और उनके निधन से ५२७ ई.पू. से वीर सम्वत् आरम्भ होता है। वीर का अर्थ सीमा होता है -रामायण अयोध्या काण्ड (७१/५) में मत्स्य की सीमा को वीरमत्स्य कहा है(वर्तमान पंजाब में होशियारपुर जिले का दसूया)। व्रती अर्थ में भी वीर होता है (भागवत, १०/८७/४५) वीर का अर्थ पुत्र भी है- अघा स वीरैर्दशभिर्वि यूया (ऋक् ७/१०४/१५) । इन अर्थों में अन्तिम तीर्थंकर महावीर थे अर्थात् ऋषभ महिमा की सीमा पर। ऋषभ देव ही वृषभ वाहन महादेव के मूर्त रूप हैं और उनके अवतार को भी महावीर (हनुमान्) कहते हैं। बीच के २२ तीर्थंकर पहले और बाद के तीर्थंकरों के बीच के सूत्र थे अतः उनको नाथ कहा गया है (नध = बान्धना)
कूर्म पुराण (५२/-१०) वायु पुराण (२३/१८९) के अनुसार २८ व्यासों में ऋषभ देव ११वें थे। भागवत पुराण स्कन्ध ५ के अध्याय ४ में तथा विष्णु पुराण अध्याय (२/१) में ऋषभ देव जी की महिमा का वर्णन है। व्यास परम्परा ३१०२ ई.पू. से २६,००० वर्ष पूर्व स्वायम्भुव मनु द्वारा आरम्भ हुयी जिनको मनुष्य रूप में ब्रह्मा कहते हैं। महाभारत, शान्ति पर्व अध्याय ३४८ के अनुसार ७ मनुष्य ब्रह्मा थे जिनको जैन तीर्थंकरों के रूप में परमेष्ठी (ब्रह्मा का पर्यायवाची) कहा गया है। वैवस्वत मनु के पिता विवस्वान् भी ५वें व्यास थे तथा उसके बाद ६ठे व्यास यम के बाद जल प्रलय हुआ था। प्रायः १०,००० ई.पू. के जल प्रलय के बाद प्रायः ९५०० ई.पू. में ऋषभ देव हुए। जल प्रलय के बाद पिछले प्रलय (३१००० ई.पू.) के बाद जैसे ब्रह्मा ने सभ्यता शुरु की उसी तरह इस बार ऋषभदेव जी ने भी किया। इस अर्थ में उनको स्वायम्भुव मनु का वंशज कहा गया है।
पुराणों में जो वर्णन है उसके अनुसार जैन शास्त्रों में ऋषभ देव को असि (तलवार), मसि (स्याही), कृषि का प्रेरक तथा शत्रु संहारक रूप में अरिहन्त कहा है। अरिहन्त का छोटा रूप अर्हत् (योग्य) है। अः +(ह) अम् = अर्हम्, अः + म् = ॐ। ऋग्वेद (१०/१६६) सूक्त के ऋषि ऋषभ हैं। देवता सपत्ननाशन (अरिहन्त) हैं।
ऋषभं मा समानानां सपत्नानां विषासहिम्। हन्तारं शत्रूणां कृधि विराजं गोपतिं गवाम्॥१॥
अहमस्मि सपत्नहेन्द्र इवारिष्टो अक्षतः। अधः सपत्ना मे पदोरिमे सर्वे अभिष्ठिताः॥२॥
अत्रैव वोऽपि नह्याम्युभे आत्नीव ज्यया। वाचस्पते नि षेधेमान्यथा मदधरं वदान्॥३॥
अभिभूरहमागमं विश्वकर्मेण धाम्ना। आ वश्चित्तमा वोऽहं समितिं ददे॥४॥
योगक्षेमं व आदायाहं भूयासमुत्तम आ वो मूर्धानमक्रमीम्।
अधस्पदान्म् उद्वदत मण्डूका इवोदकान् मण्डूका उदकादिव॥५॥
यहां गोपतिं गवाम् का अर्थ है गो-वृषभ आधारित कृषि। ऋक् (१०/७१) के अनुसार ने ब्रह्मा ने बृहस्पति द्वारा हर वस्तु के नाम रखे और दृश्य वाक् (लिपि) बनायी। ऋषभ जी ने भी वाचस्पति द्वारा संशोधित लिपि बनाई जिसे जैन शास्त्रों में ब्राह्मी कहा गया है। समिति (सभा, संस्था) बनायी तथा विश्वकर्मा रूप में विश्व व्यवस्था बनायी जैन शास्त्रों के अनुसार कर्म विभाजन के लिये ४ वर्ण बनाये थे तथा उनकी पहचान के लिये ३ प्रकार के यज्ञोपवीत निर्धारित किया (३ प्रकार की गांठ)।
४. पूर्व कल्प के तीर्थंकर-वेन ऋषभ जी के पूर्व के हैं जिनको पद्मपुराण में जैन कहा गया है। वह ७ ब्रह्मा या परमेष्ठी में नहीं थे, पर तीर्थंकर हो सकते हैं क्योंकि उनको विष्णु लोक की प्राप्ति हुयी थी। उनके सूक्त हैं-ऋग्वेद (१०/१२३), अथर्व वेद (२/१, ४/१,२)। उनके पुत्र पृथु का समय प्रायः १७,००० ई.पू. है और ये प्रह्लाद कार्त्तिकेय (१५८०० ई.पू.) के पूर्व के तथा कश्यप (१७५०० ई.पू.) के बाद के थे। वेन को भी बहुत प्रतापी तथा योग्य कहा गया है। वेन का शाब्दिक अर्थ तेजस्वी है और शुक्र को भी वेनः (Venus) कहा है।
पद्म पुराण,भूमि खण्ड २, अध्याय (३३-३७) के अनुसार वेन बहुत ही प्रतापी और धार्मिक राजा था। उसके राजा बनते ही चोर-डाकू छिप गये थे। बाद में प्रभुत्व पाने पर वह अहंकारी हो गया और विष्णु के स्थान पर अपनी पूजा कराने लगा। अध्याय (२/३७) के अनुसार एक नग्न मुण्डित साधु आया और कहा कि मैं जिन रूप हूं तथा अर्हत् देव का उपासक हूं। अर्थात् वह दिगम्बर जैन था और ऋषभ देव के पूर्व का था।
पुरुषः कश्चिदायातः छद्मलिंगधरस्तदा। नग्नरूपो महाकायः शिरोमुण्डो महाप्रभः॥५॥
मार्जनीं शिखिपत्राणां कक्षायां स हि धारयन्।गृहीतं पानपात्रं तु नारिकेल मयं करे॥६॥
पठमानोह्यसच्छास्त्रं वेद धर्म विदूषकम्। यत्र वेनो महाराजस्तत्रायातस्त्वरान्वितः॥७॥
पातक उवाच-अहं धर्स्य सर्वस्वमहं पूज्यतमो सुरैः। अहं ज्ञानमहं सत्यमहं धाता सनातनः॥१३॥
अहं धर्ममहं मोक्षः सर्वदेवमयोह्यहम्। ब्रह्म देहात् समुद्भूतः सत्यसन्धोऽस्मिनान्यथा॥१४॥
जिनरूपं विजानीहि सत्य धर्म कलेवरम्। मामेव हि प्रधावन्ति योगिनो ज्ञान तत्पराः॥१५॥
अर्हन्तो देवता यत्र निर्ग्रन्थो दृश्यते गुरुः। दया चैव परो धर्मस्तत्र मोक्षः प्रदृश्यते॥१७॥
पितॄणां तर्पणं नास्ति नातिथिर्वैश्वदेविकम्। क्षपणस्यवरा पूजा अर्हतो ध्यानमुत्तमम्॥२०॥
अयं धर्म समाचारो जैन मारे प्रदृश्यते। एतत्ते सर्व माख्यातं निज धर्मस्य लक्षणम्॥२१॥
भागवत पुराण (४/१४) के अनुसार ऋषियों के शाप से दग्ध हो गया। पर वेन के मरते ही चोर-डाकुओं का उपद्रव आरम्भ हो गया। अतः वेन के शरीर के मन्थन से राजा पृथु का जन्म हुआ जो पृथ्वी के दोहन (खनिज तथा कृषि) के लिये विख्यात हैं। किन्तु पद्म पुराण (२/३९) अध्याय के अनुसार शरीर से पाप के निष्क्रमण के बाद वेन ने तप किया और विष्णु की स्तुति की। अध्याय (२/१००, १२३, १२५) के अनुसार यज्ञ के कारण वेन को विष्णु लोक की प्राप्ति हुई।
५. परमेष्ठी तीर्थंकर- पूर्व कल्प के तीर्थंकरों को जैन शास्त्रों में परमेष्ठी कहा गया है। परमेष्ठी ब्रह्मा को कहते हैं। महाभारत शान्ति पर्व अध्याय ३४८-३४९ के अनुसार ७ मनुष्य ब्रह्मा थे। ब्रह्मा को परमेष्ठी तथा पितामह भी कहा जाता है। जैन शास्त्रों में ऋषभदेव के पूर्व के तीर्थंकरों को परमेष्ठी कहा गया है। इनके नाम हैं-
(१) मुख्य-नारायण के मुख से-उनसे वैखानस (भूगर्भ से धातु खनन करने वाले) ने वेद सीखा।
(२) आंख से-उनको सोम ने वेद पढ़ाया तथा उनसे बालखिल्यों ने सीखा।
(३) वाणी से-महाभारत, शान्तिपर्व (३४९/३९) में उनको वाणी (तथा हिरण्यगर्भ) का पुत्र अपान्तरतमा कहा गया है। उन्होंने त्रिसुपर्ण ऋषि को वेद पढ़ाया। अपान्तरतमा पुराणों के अनुसार गौतमी (गोदावरी) तट पर रहते थे।
इस ब्रह्मा की ६४ अक्षरों की ब्राह्मी लिपि आज भी कन्नड़ तथा तेलुगू रूप में चल रही है। आदि शंकराचार्य को इस अपान्तरतमा का अवतार कहा गया है। जैन शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मी लिपि का आरम्भ ऋषभ देव से हुआ, उनके समय अक्षरों का नया रूप हो सकता है।
(४) आदि कृतयुग (३७९०२-३३१०२ ई.पू.) में नारायण के कर्ण से ब्रह्मा हुए। इन्होंने आरण्यक, रहस्य और संग्रह सहित स्वारोचिष मनु, शंखपाल और दिक्पाल सुवर्णाभ को वेद पढ़ाया।
(५) आदि कृतयुग में ही नारायण की नाक से ब्रह्मा हुये जिन्होंने वीरण, रैभ्य मुनि तथा कुक्षि (दिक्पाल) को पढ़ाया।
(६) अण्डज ब्रह्मा ने बर्हिषद् मुनि, ज्येष्ठ सामव्रती तथा राजा अविकम्पन को पढ़ाया।
(७) पद्मनाभ ब्रह्मा ने दक्ष, विवस्वान् तथा इक्ष्वाकु को पढ़ाया। यह परम्परा है, कोई एक ही व्यक्ति १४००० ई.पू. के विवस्वान् तथा ८५७६ ई.पू. के इक्ष्वाकु को नहीं पढ़ा सकता है। यह सम्भवतः मणिपुर के थे, शरीर में नाभि पद्म में मणिपूर चक्र है। भारत का प्राचीन नाम अजनाभ वर्ष था, इसका नाभि-कमल (पद्मनाभ) मणिपुर है, जिससे इस ब्रह्मा का जन्म हुआ। इसके बाद का क्षेत्र ब्रह्म देश (अब महा-अमर = म्याम्मार) है।
६. अन्य तीर्थंकर-ऋषभ देव के पुत्र भरत भी सन्यासी हुए थे पर वे योग भ्रष्ट हो गये अतः तीर्थंकर नहीं बने। उसके बाद कई अन्य राजा भी विश्व विख्यात थे तथा सन्यासी बने। पर कठिनाई है कि जैन ग्रन्थों में केवल सन्यास का नाम दिया है अतः पता नहीं चलता कि यह किस पौराणिक राजा का सन्यास नाम है। अन्य सम्भावित जैन तीर्थंकरों के सन्यास पूर्व नाम हैं-इक्ष्वाकु (८५७६ ई.पू), पुरुरवा (८४५० ई.पू.), ययाति (८२०० ई.पू.), मान्धाता (७६०० ई.पू.), सगर (६७६२ ई.पू.), दुष्यन्त पुत्र भरत (५००० ई.पू.), संवरण (४१५९-४०७१ ई.पू.), कुरु (४०७१-३९९९ ई.पू.), उपरिचर वसु (३७५१-३७०९ ई.पू.)। निम्नलिखित व्यास भी तीर्थंकर हो सकते हैं-सुरक्षण (८१०० ई.पू.), त्र्यारुण (७७०० ई.पू.), धनञ्जय (७४०० ई.पू.), कृतञ्जय (७००० ई.पू.), ऋतञ्जय (६६५० ई.पू.), वाचस्पति (निर्यन्तर ५६०० ई.पू.), सुकल्याण (५२०० ई.पू.), तृणविन्दु (४८५० ई.पू.)। महान् राजाओं में नहुष (८२५० ई.पू.) भी थे जो कुछ समय इन्द्र पद पर भी रहे, बाद में शाप से सर्प हो गये (मेक्सिको की नहुआ जाति)। श्रीराम (४४३३-४३६३ ई.पू.) महानतम राजा थे, पर वे राजा रहते ही परलोक गये और सन्यासी नहीं बने। उस समय उनके पुत्र लव-कुश केवल २१ वर्ष के थे और वयस्क नहीं हुए थे। अतः नहुष और श्रीराम तीर्थंकर नहीं हैं।
तीर्थंकर युधिष्ठिर-२२ वें तीर्थंकर नेमिनाथ के बारे में कई कल्पनायें हैं। कुछ लोग उनको छान्दोग्य उपनिषद् का ऋषि अरिष्टनेमि मानते हैं (नेमि शब्द के कारण) पर ये राजा नहीं थे जो बाद में सन्यासी हुए। नेमिनाथ जी भगवान् कृष्ण के भाई थे। उनके भाइयों में केवल २ ही राजा हुए थे-दुर्योधन राजा बना था पर धृतराष्ट्र के प्रतिनिधि रूप में; उसका अभिषेक नहीं हुआ था। युधिष्ठिर का महाभारत युद्ध के बाद १७-१२-३१३९ ई.पू. को अभिषेक हुआ था तथा २८-८-३१०२ ई.पू. तक शासन किया। उसके बाद वे सन्यासी बने तथा २५ वर्ष बाद ३०७६ ई.पू. में उनके देहान्त से कश्मीर में लौकिक सम्वत् आरम्भ हुआ। उन्हीं के लिये धर्मराज तथा लोकोत्तर (उनका रथ भूमि से ६ इंच ऊपर चलता था) शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये दोनों ही तीर्थंकर के विशेषण हैं।
आगामी तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जो युधिष्ठिर की ८ पीढ़ी बाद काशी के राजपरिवार में हुए थे। उनका मूल नाम युधिष्ठिर हो सकता है क्योंकि उनके सन्यास से जैन युधिष्ठिर सम्वत् (२६३४ ई.पू.) मे आरम्भ होता है। युधिष्ठिर की ७ पीढ़ी बाद सरस्वती नदी सूख गयी तथा गंगा की अप्रत्याशित बाढ़ में हस्तिनापुर बह गया और पाण्डव राजा निचक्षु कौसाम्बी आ गये। इस महान् विपर्यय में एक शक्तिशाली राजा के सन्यासी होने की जरूरत थी जो देश में धर्म और शान्ति रख सके। उस समय वाराणसी राज्य ही इसमें सक्षम था।
७. ऋषभदेव जी की आयु-पुराणों में बड़ी बड़ी संख्यायें दी गयी हैं तथा हम अपनी प्रशंसा के लिये उनको और बड़ा करते जाते हैं। पर इससे वे अविश्वसनीय बन जाते हैं तथा भक्त भी उनकी ऐतिहासिक सत्यता पर विश्वास नहीं करते।
ऋषभदेव जी की आयु १०० कोड़ा कोड़ी अर्थात् १०० करोड़ का पुनः करोड़ गुणा; या १ पर १६ शून्य वर्ष। यह ब्रह्माण्ड की आयु (८६४ करोड वर्ष का ब्रह्मा का दिनरात) से ११ लाख गुणा बड़ा है। अपनी प्रशंसा में इतनी बड़ी संख्या कैसे निकली? ऋषभ देव जी विष्णु के २४ अवतारों में से एक हैं। पूरा विश्व विष्णु की श्वास (सृष्टि-प्रलय का चक्र = ८६४ कोटि वर्ष) है। यह सृष्टि वेद है जिसके बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है-जाकी श्वास सहज श्रुति चारी (रामचरितमानस, बालकाण्ड, २०३/३)
यही बृहदारण्यक उपनिषद् में कहा है-
एवं वा अरेऽस्य महतोभूतस्य निःश्वसितमेतद्यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ऽथर्वाङ्गिरस इतिहास पुराण विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि अस्यैवैतानि निःश्वसितानि। (बृहदारण्यक उपनिषद्, २/४/१०)
ज्योतिष में श्वास चक्र को असु कहा गया है जो ४ सेकण्ड का होता है। ४ सेकण्ड को ८६४ करोड़ वर्ष मानने पर १०० कोड़ा-कोड़ी वर्ष का अर्थ ५३ वर्ष होगा। भगवती सूत्र में ऋषभ देव जी का राज्यकाल ५३ पूर्वा कहा गया है, जहां पूर्वा का अर्थ इस गणना के अनुसार वर्ष होगा।
इसी प्रकार रामायण, युद्ध काण्ड, सर्ग (२८/३८-४०) में भी राम की सेना १० घात ६२ कही गयी है, जो सौरमण्डल के इलेक्ट्रान संख्या का १०० गुणा है। यदि प्रति सैनिक का भार शस्त्र सहित १०० किलोग्राम माना आय तो राम सेना के सैनिकों का कुल भार १० घात ६४ होगा। पूरे विश्व का कुल अनुमानित भार १० घात ५३ है, जिसका १०० अरब गुणा राम की सेना का भार होगा। ऐसे मूर्खतापूर्ण वर्णन के कारण रावण ने अपने दूतों शुक और सारण को पागल मान कर भगा दिया था। रामचरितमानस में भी उनके सेनापतियों की संख्या १८ पद्म कही गयी है जो विश्व की वर्तमान जनसंख्या का २० लाख गुणा अधिक है। वस्तुतः १८ क्षेत्रों (पद्म) में रावण के साथ युद्ध हुआ था और हर क्षेत्र के लिये १-१ सेनापति थे जिनको पद्म कहा है (युद्ध काण्ड, अध्याय २६-२७)। उत्तरकाण्ड (२५/३३) के अनुसार रावण ने इन्द्र पर ४ (४ सहस्र = प्रायः ४) अक्षौहिणी सेना के साथ आक्रमण किया था। उसके बाद उसकी सेना ५ अक्षौहिणी से कुछ अधिक हुई होगी। इसके हिसाब से राम ने ६ अक्षौहिणी सेना जुटाई। नीलकण्ठ टीका के अनुसार राम के पास ६२ इकाई (६.२ अक्षौहिणी) तथा रावण के पास ७० इकाई (७ अक्षौहिणी) सेना थी। महाभारत उद्योग पर्ब (१५५/२४) में अक्षौहिणी को १० भाग में बांटा है। आदि पर्व (२/१९-२५) के अनुसार १ अक्षौहिणी में २,१८,५०० युद्ध करने वाले सैनिक होते हैं। अर्थात् राम सेना १३.५ लाख तथा रावण सेना १५.२ लाख थी।
https://www.pixincreativemedia.com/
शब्द रूप में ३ या ७ ही विकल्प होते हैं। गणित के अनुसार अनन्त विकल्प होंगे। इसमें संशय होता है। अतः जैन मत को अनेकान्त या स्याद्वाद भी कहते हैं। वेद में ३ प्रकार के अनन्तों का वर्णन है, जिनको विष्णु सहस्रनाम में अनन्त, असंख्येय, अप्रमेय कहा है। नासदीय सूक्त (ऋग्वेद, १०/१२९) में भी संशयवाद है जिसकी पण्डित मधुसूदन ओझा ने दशवाद रहस्य में व्याख्या की है-
तम आसीत् तमसा गूळ्हमग्रेऽ प्रकेतं सलिलं सर्व मा इदम्।
तुच्छ्येनाभ्व पिहितं यदासीत् तपसस्तन्महिनाजायतैकम्॥३॥
को अद्धा वेद क इह प्र वोचत् कुत अजाता कुत इयं विसृष्टिः।
अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाऽथ को वेद यत आबभूव॥६॥
आरम्भ में सब तरफ अन्धकार था उसमें कोई सीमा या पदार्थ का पता नहीं चलता था। वह स्वयं अपनी महिमा में तप रहा था। निश्चय पूर्वक कोई नहीं कह सकता कि यह सृष्टि कहां से हुई और कैसे इसके बहुत से भेद हो गये। (विसृष्टि = पुराण का प्रतिसर्ग)। देव भी तो सृष्टि के बाद ही हुये, वे कैसे जान सकते हैं कि यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ?
वेद सनातन शास्त्र हैं, उनकी वैज्ञानिक व्याख्या के लिए हर काल में शास्त्र बने थे जो जैन शास्त्र हैं। पार्थिव विश्व को आकाश की प्रतिमा कहा गया है, पर विज्ञान माध्यम से उसे समझने के लिए अलग अलग व्याख्या होगी। अतः वेद के ६ अंग और ६ उपांगों के बदले जैन शास्त्रों में १२ अंग और १२ उपांग थे जिनमें कोई भी उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार मध्वाचार्य का द्वैतवाद है, ब्रह्म अपनी निर्मित सृष्टि में भी है (तत् सृष्ट्वा, तदेव अनुप्राविशत्-तैत्तिरीय उपनिषद्, २/६/४)। किन्तु व्याख्या के लिए अव्यक्त ब्रह्म और भौतिक जगत् को अलग मानना पड़ता है।
२. ऋषि और मुनि- ऋषि शब्द के ७ अर्थ हैं-(१) रस्सी-सृष्टि का मूल १०-३५ मी. के तन्तु। सृष्टि का मूल असत् (अदृश्य) प्राण था जो रस्सी की तरह श्रम और तप से खींचते थे (शतपथ ब्राह्मण, ६/१/१/१) ।
इन ऋषियों से पितर, फिर देव-दानव, देवों से जगत् (चर, स्थाणु, अनुपूर्व-३ प्रकार के कण) हुए-
ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितॄभ्यो देव दानवाः। देवेभ्यश्च जगत्सर्वं चरं स्थाण्वनुपूर्वशः॥ (मनुस्मृति, ३/२०१)
(२) तारा -जैसे सप्तर्षि, (३) मन्त्र द्रष्टा-जो आधिदैविक (आकाश), आधिभौतिक (पृथ्वी) तथा आध्यात्मिक (शरीर के भीतर) विश्वों का सम्बन्ध (इनको जोड़ने वाली रस्सी, या ब्रह्म और सामान्य मनुष्य के बीच की रस्सी), (४) गुरु-शिष्य परम्परा आरम्भ करने वाले (उनके बीच की रस्सी), (५) गोत्र प्रवर्तक (६) आनुवंशिक सम्बन्ध -२१ पीढ़ी तक (७ पीढ़ी तक पिण्ड, १४ पीढ़ी तक उदक, उसके बाद २१ पीढ़ी तक ऋषि), (७) आकाश के १० आयाम (दश, दशा, दिशा, आशा) में ७ वां जो दो कणों के बीच आकर्षण द्वारा सम्बन्ध हैं।
मुनि उसे कहते हैं जो राग, भय, क्रोध से मुक्त हो कर अपने मन और शरीर पर नियन्त्रण रखता है और स्थिर बुद्धि का है-
दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः। वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते॥ (गीता, २/५६)
जो मुनि है, वही ऋषि हो सकता है। ऋषि परम्परा वेद है, मुनि परम्परा लौकिक शास्त्र हैं, जिनसे वेद समझा जा सकता है।
ऋषि सत्य का दर्शन कर सकता है, पर वह तभी स्वीकृत हो सकता है जब सत्ता द्वारा भी समर्थन हो। राजा का भी लोग तभी अनुकरण करते हैं जब वह सच्चरित्र हो। अतः वही लोग जैन तीर्थंकर हुये, जो राजा बनने के बाद सन्यासी बने। राजा के रूप में राज्य चलाने का अनुभव हो, उसके बाद निरपेक्ष और निस्पृह हो। इसी लिये आरुणि उद्दालक को शिक्षा पूरी करने के लिये राजा अश्वपति के पास भेजा गया (छान्दोग्य उपनिषद्, अध्याय ५)। ऐसा ही व्यक्ति लौकिक और पारलौकिक रूप से संसार से पार करा सकता है, अतः उसे तीर्थंकर (नदी या समुद्र पार करने के लिये तट) कहते हैं।
ऋषि या गुरु-शिष्य क्रम तीर्थंकरों में भी है। स्रोत को ऋषभ तथा अन्तिम को महावीर (महः = सीमा) कहा गया है। बीच के सभी नाथ (बान्धने वाले) हैं।
३. वर्तमान युग के तीर्थंकर-पुराणों में अभी ब्रह्माब्द का तीसरा दिन चल रहा है। हर ब्रह्माब्द २४,००० वर्ष का है जिसके २ भाग हैं। प्रथम अवसर्पिणी १२,००० वर्ष का है जिसमें क्रम से सत्य. त्रेता, द्वापर, कलि आते हैं जिनका अनुपात ४,३,२,१ है। उसके बाद १२,००० वर्ष के उत्सर्पिणी में विपरीत क्रम से उतने ही मान के युग आते हैं-कलि, द्वापर, त्रेता, सत्य। वैवस्वत मनु से तीसरा ब्रह्माब्द आरम्भ हुआ है-जिसमें सत्य, त्रेता, द्वापर की समाप्ति महाभारत के ३६ वर्ष बाद ३१०२ ई.पू. में हुई। उसके बाद १२०० वर्षों का कलि १९०२ ई.पू. तक था जिसके बाद उत्सर्पिणी का कलि ७०२ ई.पू. तक, द्वापर १६९९ ई. तक रहा। उसके बाद अभी त्रेता चल रहा है जो ५२९९ ई. तक रहेगा। इस अवसर्पिणी में ऋषभ देव से महावीर तक जैन मत के २४ तीर्थङ्कर हुए। ऋषभ का अर्थ है सभ्यता, ज्ञान, कर्म का आरम्भ, वृषा = वर्षा करने वाला। इसी से वृषभ हुआ है जो कृषि का मूल आधार है जिस पर सभ्यता निर्भर है।
प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि।
स्वलक्षणा प्रादुरभूत्किलास्यतः स मे ऋषीणामृषभः प्रसीदताम्॥ (भागवत पुराण, २/४/२२)
अवसर्पिणी का अन्त १९०२ ई.पू. में हुआ। उससे ३ वर्ष पूर्व भगवान् महावीर का जन्म ११-३-१९०५ ई.पू. चैत्र शुक्ल १३ को हुआ। उनके १३०० वर्ष बाद ५९९ ई.पू. में उज्जैन में जैन मुनि कालकाचार्य का जन्म हुआ जिन्होंने जैन शात्रों का उद्धार किया अतः उनको वीर (महावीर नहीं) कहते हैं और उनके निधन से ५२७ ई.पू. से वीर सम्वत् आरम्भ होता है। वीर का अर्थ सीमा होता है -रामायण अयोध्या काण्ड (७१/५) में मत्स्य की सीमा को वीरमत्स्य कहा है(वर्तमान पंजाब में होशियारपुर जिले का दसूया)। व्रती अर्थ में भी वीर होता है (भागवत, १०/८७/४५) वीर का अर्थ पुत्र भी है- अघा स वीरैर्दशभिर्वि यूया (ऋक् ७/१०४/१५) । इन अर्थों में अन्तिम तीर्थंकर महावीर थे अर्थात् ऋषभ महिमा की सीमा पर। ऋषभ देव ही वृषभ वाहन महादेव के मूर्त रूप हैं और उनके अवतार को भी महावीर (हनुमान्) कहते हैं। बीच के २२ तीर्थंकर पहले और बाद के तीर्थंकरों के बीच के सूत्र थे अतः उनको नाथ कहा गया है (नध = बान्धना)
कूर्म पुराण (५२/-१०) वायु पुराण (२३/१८९) के अनुसार २८ व्यासों में ऋषभ देव ११वें थे। भागवत पुराण स्कन्ध ५ के अध्याय ४ में तथा विष्णु पुराण अध्याय (२/१) में ऋषभ देव जी की महिमा का वर्णन है। व्यास परम्परा ३१०२ ई.पू. से २६,००० वर्ष पूर्व स्वायम्भुव मनु द्वारा आरम्भ हुयी जिनको मनुष्य रूप में ब्रह्मा कहते हैं। महाभारत, शान्ति पर्व अध्याय ३४८ के अनुसार ७ मनुष्य ब्रह्मा थे जिनको जैन तीर्थंकरों के रूप में परमेष्ठी (ब्रह्मा का पर्यायवाची) कहा गया है। वैवस्वत मनु के पिता विवस्वान् भी ५वें व्यास थे तथा उसके बाद ६ठे व्यास यम के बाद जल प्रलय हुआ था। प्रायः १०,००० ई.पू. के जल प्रलय के बाद प्रायः ९५०० ई.पू. में ऋषभ देव हुए। जल प्रलय के बाद पिछले प्रलय (३१००० ई.पू.) के बाद जैसे ब्रह्मा ने सभ्यता शुरु की उसी तरह इस बार ऋषभदेव जी ने भी किया। इस अर्थ में उनको स्वायम्भुव मनु का वंशज कहा गया है।
पुराणों में जो वर्णन है उसके अनुसार जैन शास्त्रों में ऋषभ देव को असि (तलवार), मसि (स्याही), कृषि का प्रेरक तथा शत्रु संहारक रूप में अरिहन्त कहा है। अरिहन्त का छोटा रूप अर्हत् (योग्य) है। अः +(ह) अम् = अर्हम्, अः + म् = ॐ। ऋग्वेद (१०/१६६) सूक्त के ऋषि ऋषभ हैं। देवता सपत्ननाशन (अरिहन्त) हैं।
ऋषभं मा समानानां सपत्नानां विषासहिम्। हन्तारं शत्रूणां कृधि विराजं गोपतिं गवाम्॥१॥
अहमस्मि सपत्नहेन्द्र इवारिष्टो अक्षतः। अधः सपत्ना मे पदोरिमे सर्वे अभिष्ठिताः॥२॥
अत्रैव वोऽपि नह्याम्युभे आत्नीव ज्यया। वाचस्पते नि षेधेमान्यथा मदधरं वदान्॥३॥
अभिभूरहमागमं विश्वकर्मेण धाम्ना। आ वश्चित्तमा वोऽहं समितिं ददे॥४॥
योगक्षेमं व आदायाहं भूयासमुत्तम आ वो मूर्धानमक्रमीम्।
अधस्पदान्म् उद्वदत मण्डूका इवोदकान् मण्डूका उदकादिव॥५॥
यहां गोपतिं गवाम् का अर्थ है गो-वृषभ आधारित कृषि। ऋक् (१०/७१) के अनुसार ने ब्रह्मा ने बृहस्पति द्वारा हर वस्तु के नाम रखे और दृश्य वाक् (लिपि) बनायी। ऋषभ जी ने भी वाचस्पति द्वारा संशोधित लिपि बनाई जिसे जैन शास्त्रों में ब्राह्मी कहा गया है। समिति (सभा, संस्था) बनायी तथा विश्वकर्मा रूप में विश्व व्यवस्था बनायी जैन शास्त्रों के अनुसार कर्म विभाजन के लिये ४ वर्ण बनाये थे तथा उनकी पहचान के लिये ३ प्रकार के यज्ञोपवीत निर्धारित किया (३ प्रकार की गांठ)।
४. पूर्व कल्प के तीर्थंकर-वेन ऋषभ जी के पूर्व के हैं जिनको पद्मपुराण में जैन कहा गया है। वह ७ ब्रह्मा या परमेष्ठी में नहीं थे, पर तीर्थंकर हो सकते हैं क्योंकि उनको विष्णु लोक की प्राप्ति हुयी थी। उनके सूक्त हैं-ऋग्वेद (१०/१२३), अथर्व वेद (२/१, ४/१,२)। उनके पुत्र पृथु का समय प्रायः १७,००० ई.पू. है और ये प्रह्लाद कार्त्तिकेय (१५८०० ई.पू.) के पूर्व के तथा कश्यप (१७५०० ई.पू.) के बाद के थे। वेन को भी बहुत प्रतापी तथा योग्य कहा गया है। वेन का शाब्दिक अर्थ तेजस्वी है और शुक्र को भी वेनः (Venus) कहा है।
पद्म पुराण,भूमि खण्ड २, अध्याय (३३-३७) के अनुसार वेन बहुत ही प्रतापी और धार्मिक राजा था। उसके राजा बनते ही चोर-डाकू छिप गये थे। बाद में प्रभुत्व पाने पर वह अहंकारी हो गया और विष्णु के स्थान पर अपनी पूजा कराने लगा। अध्याय (२/३७) के अनुसार एक नग्न मुण्डित साधु आया और कहा कि मैं जिन रूप हूं तथा अर्हत् देव का उपासक हूं। अर्थात् वह दिगम्बर जैन था और ऋषभ देव के पूर्व का था।
पुरुषः कश्चिदायातः छद्मलिंगधरस्तदा। नग्नरूपो महाकायः शिरोमुण्डो महाप्रभः॥५॥
मार्जनीं शिखिपत्राणां कक्षायां स हि धारयन्।गृहीतं पानपात्रं तु नारिकेल मयं करे॥६॥
पठमानोह्यसच्छास्त्रं वेद धर्म विदूषकम्। यत्र वेनो महाराजस्तत्रायातस्त्वरान्वितः॥७॥
पातक उवाच-अहं धर्स्य सर्वस्वमहं पूज्यतमो सुरैः। अहं ज्ञानमहं सत्यमहं धाता सनातनः॥१३॥
अहं धर्ममहं मोक्षः सर्वदेवमयोह्यहम्। ब्रह्म देहात् समुद्भूतः सत्यसन्धोऽस्मिनान्यथा॥१४॥
जिनरूपं विजानीहि सत्य धर्म कलेवरम्। मामेव हि प्रधावन्ति योगिनो ज्ञान तत्पराः॥१५॥
अर्हन्तो देवता यत्र निर्ग्रन्थो दृश्यते गुरुः। दया चैव परो धर्मस्तत्र मोक्षः प्रदृश्यते॥१७॥
पितॄणां तर्पणं नास्ति नातिथिर्वैश्वदेविकम्। क्षपणस्यवरा पूजा अर्हतो ध्यानमुत्तमम्॥२०॥
अयं धर्म समाचारो जैन मारे प्रदृश्यते। एतत्ते सर्व माख्यातं निज धर्मस्य लक्षणम्॥२१॥
भागवत पुराण (४/१४) के अनुसार ऋषियों के शाप से दग्ध हो गया। पर वेन के मरते ही चोर-डाकुओं का उपद्रव आरम्भ हो गया। अतः वेन के शरीर के मन्थन से राजा पृथु का जन्म हुआ जो पृथ्वी के दोहन (खनिज तथा कृषि) के लिये विख्यात हैं। किन्तु पद्म पुराण (२/३९) अध्याय के अनुसार शरीर से पाप के निष्क्रमण के बाद वेन ने तप किया और विष्णु की स्तुति की। अध्याय (२/१००, १२३, १२५) के अनुसार यज्ञ के कारण वेन को विष्णु लोक की प्राप्ति हुई।
५. परमेष्ठी तीर्थंकर- पूर्व कल्प के तीर्थंकरों को जैन शास्त्रों में परमेष्ठी कहा गया है। परमेष्ठी ब्रह्मा को कहते हैं। महाभारत शान्ति पर्व अध्याय ३४८-३४९ के अनुसार ७ मनुष्य ब्रह्मा थे। ब्रह्मा को परमेष्ठी तथा पितामह भी कहा जाता है। जैन शास्त्रों में ऋषभदेव के पूर्व के तीर्थंकरों को परमेष्ठी कहा गया है। इनके नाम हैं-
(१) मुख्य-नारायण के मुख से-उनसे वैखानस (भूगर्भ से धातु खनन करने वाले) ने वेद सीखा।
(२) आंख से-उनको सोम ने वेद पढ़ाया तथा उनसे बालखिल्यों ने सीखा।
(३) वाणी से-महाभारत, शान्तिपर्व (३४९/३९) में उनको वाणी (तथा हिरण्यगर्भ) का पुत्र अपान्तरतमा कहा गया है। उन्होंने त्रिसुपर्ण ऋषि को वेद पढ़ाया। अपान्तरतमा पुराणों के अनुसार गौतमी (गोदावरी) तट पर रहते थे।
इस ब्रह्मा की ६४ अक्षरों की ब्राह्मी लिपि आज भी कन्नड़ तथा तेलुगू रूप में चल रही है। आदि शंकराचार्य को इस अपान्तरतमा का अवतार कहा गया है। जैन शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मी लिपि का आरम्भ ऋषभ देव से हुआ, उनके समय अक्षरों का नया रूप हो सकता है।
(४) आदि कृतयुग (३७९०२-३३१०२ ई.पू.) में नारायण के कर्ण से ब्रह्मा हुए। इन्होंने आरण्यक, रहस्य और संग्रह सहित स्वारोचिष मनु, शंखपाल और दिक्पाल सुवर्णाभ को वेद पढ़ाया।
(५) आदि कृतयुग में ही नारायण की नाक से ब्रह्मा हुये जिन्होंने वीरण, रैभ्य मुनि तथा कुक्षि (दिक्पाल) को पढ़ाया।
(६) अण्डज ब्रह्मा ने बर्हिषद् मुनि, ज्येष्ठ सामव्रती तथा राजा अविकम्पन को पढ़ाया।
(७) पद्मनाभ ब्रह्मा ने दक्ष, विवस्वान् तथा इक्ष्वाकु को पढ़ाया। यह परम्परा है, कोई एक ही व्यक्ति १४००० ई.पू. के विवस्वान् तथा ८५७६ ई.पू. के इक्ष्वाकु को नहीं पढ़ा सकता है। यह सम्भवतः मणिपुर के थे, शरीर में नाभि पद्म में मणिपूर चक्र है। भारत का प्राचीन नाम अजनाभ वर्ष था, इसका नाभि-कमल (पद्मनाभ) मणिपुर है, जिससे इस ब्रह्मा का जन्म हुआ। इसके बाद का क्षेत्र ब्रह्म देश (अब महा-अमर = म्याम्मार) है।
६. अन्य तीर्थंकर-ऋषभ देव के पुत्र भरत भी सन्यासी हुए थे पर वे योग भ्रष्ट हो गये अतः तीर्थंकर नहीं बने। उसके बाद कई अन्य राजा भी विश्व विख्यात थे तथा सन्यासी बने। पर कठिनाई है कि जैन ग्रन्थों में केवल सन्यास का नाम दिया है अतः पता नहीं चलता कि यह किस पौराणिक राजा का सन्यास नाम है। अन्य सम्भावित जैन तीर्थंकरों के सन्यास पूर्व नाम हैं-इक्ष्वाकु (८५७६ ई.पू), पुरुरवा (८४५० ई.पू.), ययाति (८२०० ई.पू.), मान्धाता (७६०० ई.पू.), सगर (६७६२ ई.पू.), दुष्यन्त पुत्र भरत (५००० ई.पू.), संवरण (४१५९-४०७१ ई.पू.), कुरु (४०७१-३९९९ ई.पू.), उपरिचर वसु (३७५१-३७०९ ई.पू.)। निम्नलिखित व्यास भी तीर्थंकर हो सकते हैं-सुरक्षण (८१०० ई.पू.), त्र्यारुण (७७०० ई.पू.), धनञ्जय (७४०० ई.पू.), कृतञ्जय (७००० ई.पू.), ऋतञ्जय (६६५० ई.पू.), वाचस्पति (निर्यन्तर ५६०० ई.पू.), सुकल्याण (५२०० ई.पू.), तृणविन्दु (४८५० ई.पू.)। महान् राजाओं में नहुष (८२५० ई.पू.) भी थे जो कुछ समय इन्द्र पद पर भी रहे, बाद में शाप से सर्प हो गये (मेक्सिको की नहुआ जाति)। श्रीराम (४४३३-४३६३ ई.पू.) महानतम राजा थे, पर वे राजा रहते ही परलोक गये और सन्यासी नहीं बने। उस समय उनके पुत्र लव-कुश केवल २१ वर्ष के थे और वयस्क नहीं हुए थे। अतः नहुष और श्रीराम तीर्थंकर नहीं हैं।
तीर्थंकर युधिष्ठिर-२२ वें तीर्थंकर नेमिनाथ के बारे में कई कल्पनायें हैं। कुछ लोग उनको छान्दोग्य उपनिषद् का ऋषि अरिष्टनेमि मानते हैं (नेमि शब्द के कारण) पर ये राजा नहीं थे जो बाद में सन्यासी हुए। नेमिनाथ जी भगवान् कृष्ण के भाई थे। उनके भाइयों में केवल २ ही राजा हुए थे-दुर्योधन राजा बना था पर धृतराष्ट्र के प्रतिनिधि रूप में; उसका अभिषेक नहीं हुआ था। युधिष्ठिर का महाभारत युद्ध के बाद १७-१२-३१३९ ई.पू. को अभिषेक हुआ था तथा २८-८-३१०२ ई.पू. तक शासन किया। उसके बाद वे सन्यासी बने तथा २५ वर्ष बाद ३०७६ ई.पू. में उनके देहान्त से कश्मीर में लौकिक सम्वत् आरम्भ हुआ। उन्हीं के लिये धर्मराज तथा लोकोत्तर (उनका रथ भूमि से ६ इंच ऊपर चलता था) शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये दोनों ही तीर्थंकर के विशेषण हैं।
आगामी तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जो युधिष्ठिर की ८ पीढ़ी बाद काशी के राजपरिवार में हुए थे। उनका मूल नाम युधिष्ठिर हो सकता है क्योंकि उनके सन्यास से जैन युधिष्ठिर सम्वत् (२६३४ ई.पू.) मे आरम्भ होता है। युधिष्ठिर की ७ पीढ़ी बाद सरस्वती नदी सूख गयी तथा गंगा की अप्रत्याशित बाढ़ में हस्तिनापुर बह गया और पाण्डव राजा निचक्षु कौसाम्बी आ गये। इस महान् विपर्यय में एक शक्तिशाली राजा के सन्यासी होने की जरूरत थी जो देश में धर्म और शान्ति रख सके। उस समय वाराणसी राज्य ही इसमें सक्षम था।
७. ऋषभदेव जी की आयु-पुराणों में बड़ी बड़ी संख्यायें दी गयी हैं तथा हम अपनी प्रशंसा के लिये उनको और बड़ा करते जाते हैं। पर इससे वे अविश्वसनीय बन जाते हैं तथा भक्त भी उनकी ऐतिहासिक सत्यता पर विश्वास नहीं करते।
ऋषभदेव जी की आयु १०० कोड़ा कोड़ी अर्थात् १०० करोड़ का पुनः करोड़ गुणा; या १ पर १६ शून्य वर्ष। यह ब्रह्माण्ड की आयु (८६४ करोड वर्ष का ब्रह्मा का दिनरात) से ११ लाख गुणा बड़ा है। अपनी प्रशंसा में इतनी बड़ी संख्या कैसे निकली? ऋषभ देव जी विष्णु के २४ अवतारों में से एक हैं। पूरा विश्व विष्णु की श्वास (सृष्टि-प्रलय का चक्र = ८६४ कोटि वर्ष) है। यह सृष्टि वेद है जिसके बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है-जाकी श्वास सहज श्रुति चारी (रामचरितमानस, बालकाण्ड, २०३/३)
यही बृहदारण्यक उपनिषद् में कहा है-
एवं वा अरेऽस्य महतोभूतस्य निःश्वसितमेतद्यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ऽथर्वाङ्गिरस इतिहास पुराण विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि अस्यैवैतानि निःश्वसितानि। (बृहदारण्यक उपनिषद्, २/४/१०)
ज्योतिष में श्वास चक्र को असु कहा गया है जो ४ सेकण्ड का होता है। ४ सेकण्ड को ८६४ करोड़ वर्ष मानने पर १०० कोड़ा-कोड़ी वर्ष का अर्थ ५३ वर्ष होगा। भगवती सूत्र में ऋषभ देव जी का राज्यकाल ५३ पूर्वा कहा गया है, जहां पूर्वा का अर्थ इस गणना के अनुसार वर्ष होगा।
इसी प्रकार रामायण, युद्ध काण्ड, सर्ग (२८/३८-४०) में भी राम की सेना १० घात ६२ कही गयी है, जो सौरमण्डल के इलेक्ट्रान संख्या का १०० गुणा है। यदि प्रति सैनिक का भार शस्त्र सहित १०० किलोग्राम माना आय तो राम सेना के सैनिकों का कुल भार १० घात ६४ होगा। पूरे विश्व का कुल अनुमानित भार १० घात ५३ है, जिसका १०० अरब गुणा राम की सेना का भार होगा। ऐसे मूर्खतापूर्ण वर्णन के कारण रावण ने अपने दूतों शुक और सारण को पागल मान कर भगा दिया था। रामचरितमानस में भी उनके सेनापतियों की संख्या १८ पद्म कही गयी है जो विश्व की वर्तमान जनसंख्या का २० लाख गुणा अधिक है। वस्तुतः १८ क्षेत्रों (पद्म) में रावण के साथ युद्ध हुआ था और हर क्षेत्र के लिये १-१ सेनापति थे जिनको पद्म कहा है (युद्ध काण्ड, अध्याय २६-२७)। उत्तरकाण्ड (२५/३३) के अनुसार रावण ने इन्द्र पर ४ (४ सहस्र = प्रायः ४) अक्षौहिणी सेना के साथ आक्रमण किया था। उसके बाद उसकी सेना ५ अक्षौहिणी से कुछ अधिक हुई होगी। इसके हिसाब से राम ने ६ अक्षौहिणी सेना जुटाई। नीलकण्ठ टीका के अनुसार राम के पास ६२ इकाई (६.२ अक्षौहिणी) तथा रावण के पास ७० इकाई (७ अक्षौहिणी) सेना थी। महाभारत उद्योग पर्ब (१५५/२४) में अक्षौहिणी को १० भाग में बांटा है। आदि पर्व (२/१९-२५) के अनुसार १ अक्षौहिणी में २,१८,५०० युद्ध करने वाले सैनिक होते हैं। अर्थात् राम सेना १३.५ लाख तथा रावण सेना १५.२ लाख थी।
Related Posts
0 Comments
Comments are not available.