- मिस्टिक ज्ञान
- |
- 31 October 2024
- |
- 0 Comments
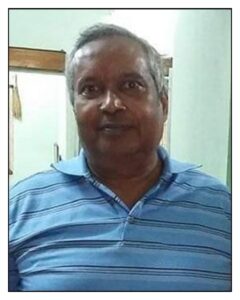 श्री अरुण कुमार उपाध्याय (धर्मज्ञ )-
Mystic Power- १. निर्गुण-सगुण-निर्गुण अव्यक्त ब्रह्म ही सगुण रूप धारण करता है। निर्गुण तथा निर्विशेष में कोई भेद नहीं है, अतः इसका वर्णन नहीं हो सकता है। वेद (निगम), तन्त्र (आगम) या पुराण में जो कुछ वर्णन है, वह सगुण का ही है। निर्गुण का वर्णन नकार रूप में है-कि यह वैसा कुछ नहीं है, जो दीख रहा है। इसे नेति-नेति कहा है-
निगम नेति शिव अन्त न पावा। ताहि धरहिं जननि हठि धावा॥
(रामचरितमानस, बालकाण्ड, २०२/८)
या-निगम नेति शिव ध्यान न पावा।
(रामचरितमानस, अरण्य काण्ड, २६/११)
श्री अरुण कुमार उपाध्याय (धर्मज्ञ )-
Mystic Power- १. निर्गुण-सगुण-निर्गुण अव्यक्त ब्रह्म ही सगुण रूप धारण करता है। निर्गुण तथा निर्विशेष में कोई भेद नहीं है, अतः इसका वर्णन नहीं हो सकता है। वेद (निगम), तन्त्र (आगम) या पुराण में जो कुछ वर्णन है, वह सगुण का ही है। निर्गुण का वर्णन नकार रूप में है-कि यह वैसा कुछ नहीं है, जो दीख रहा है। इसे नेति-नेति कहा है-
निगम नेति शिव अन्त न पावा। ताहि धरहिं जननि हठि धावा॥
(रामचरितमानस, बालकाण्ड, २०२/८)
या-निगम नेति शिव ध्यान न पावा।
(रामचरितमानस, अरण्य काण्ड, २६/११)
 नेति रूप में वर्णन गजेन्द्र मोक्ष में है-
स वै न देवासुर मर्त्य तिर्यङ्, न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तुः।
नायं गुणं कर्म न सन्न चासन्, निषेध शेषो जयतादशेषः॥
(भागवत पुराण, ८/३/२४)
निर्विशेष का वर्णन नहीं हो सकता, अतः उसका उपवर्णन होता है, अपूर्ण उपमाओं से तुलना कर कहते हैं कि केवल यही नहीं है।
एवं गजेन्द्रं उपवर्णित निर्विशेषम् (भागवत पुराण, ८/३/३०)
अनुमान से उसके निकट के वर्णन को वेद में ’पर्यगात्’ कहा है-
स पर्यगात्-शुक्रं, अकायं, अव्रणं, शुद्धं, अपापविद्धं-
कविः मनीषीः परिभूः स्वयम्भूः
याथातथ्यतो अर्थान् व्यदधात्, शाश्वतीभ्यः समाभ्यः॥
(ईशावास्योपनिषद्, वाज. यजु, ४०/८)
नेति रूप में वर्णन गजेन्द्र मोक्ष में है-
स वै न देवासुर मर्त्य तिर्यङ्, न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तुः।
नायं गुणं कर्म न सन्न चासन्, निषेध शेषो जयतादशेषः॥
(भागवत पुराण, ८/३/२४)
निर्विशेष का वर्णन नहीं हो सकता, अतः उसका उपवर्णन होता है, अपूर्ण उपमाओं से तुलना कर कहते हैं कि केवल यही नहीं है।
एवं गजेन्द्रं उपवर्णित निर्विशेषम् (भागवत पुराण, ८/३/३०)
अनुमान से उसके निकट के वर्णन को वेद में ’पर्यगात्’ कहा है-
स पर्यगात्-शुक्रं, अकायं, अव्रणं, शुद्धं, अपापविद्धं-
कविः मनीषीः परिभूः स्वयम्भूः
याथातथ्यतो अर्थान् व्यदधात्, शाश्वतीभ्यः समाभ्यः॥
(ईशावास्योपनिषद्, वाज. यजु, ४०/८)
 यह वाक् और अर्थ (शब्द, विश्व) दोनों के लिए है-
अव्यक्त विश्व या वाक् व्यक्त विश्व व्यक्त वाक्
(१). शुक्र तम तम
(२). अकाय पिण्ड शब्द आदि
(३). अव्रण छिद्र, दोष अपूर्णता, लुप्त शब्द।
(४). अस्नाविरम् ऋषि (रस्सी) कारक आदि से सम्बन्ध
(५). शुद्ध मिश्रण अपूर्ण रूप
(६). अपापविद्ध माया के आवरण शब्द, पद, वाक्य का पार्थक्य
अव्यक्त या निर्गुण का सगुण रूप में वर्णन ही शाश्वत काव्य है। वाक्य तात्कालिक घटना है, इसका व्यापक वर्णन काव्य है (वर्ण विपर्यय)।
२. उपमा- अव्यक्त विश्व के वर्णन के लिए व्यक्त पदार्थों से उनकी तुलना करते हैं। मूल शब्द भौतिक विश्व के लिए थे। अध्यात्म (शरीर के भीतर) तथा अधिदैव में उनके अर्थों का विस्तार या वृद्धि होती है। यह सादृश्य ही उपमा है।
(१) माता पिता-आकाश में पृथ्वी के सभी स्तरों को माता कहते हैं, उनके आकाश को पिता।
तिस्रो मातॄस्त्रीन्पितॄन्बिभ्रदेक ऊर्ध्वतस्थौ नेमवग्लापयन्ति ।
मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे विश्वमिदं वाचमविश्वमिन्वाम् ॥ (ऋग्वेद, १/१६४/१०)
इनकी परिभाषा है कि सूर्य चन्द्र से प्रकाशित भाग पृथ्वी है। दोनों से प्रकाशित पृथ्वी ग्रह है। सूर्य का प्रकाशित क्षेत्र सौर पृथ्वी है, जिसके ताप, तेज, प्रकाश ३ पद हैं। सूर्य प्रकाश की सीमा ब्रह्माण्ड है, जो सूर्य रूपी विष्णु का परम पद कहा है। बड़ी पृथ्वी में भी पृथ्वी ग्रह जैसे ही द्वीप, समुद्र, नदियों के नाम हैं-जैसे सौर मण्डल में ग्रह कक्षा से बने वलयाकार क्षेत्र पृथ्वी के द्वीपों के नाम पर हैं, तथा उनके बीच के भाग समुद्र। ब्रह्माण्ड का केन्द्रीय चक्र आकाशगंगा है।
रवि चन्द्रमसोर्यावन्मयूखैरवभास्यते। स समुद्र सरिच्छैला पृथिवी तावती स्मृता॥
(विष्णु पुराण, २/७/३)
इदं विष्णुर्विचक्रमे, त्रेधा निदधे पदम् (ऋक्, १/२२/१७)
सौरमण्डल के ३ विक्रम-भूरिति वा अग्निः। भुव इति वायुः। सुवः इति आदित्यः (तैत्तिरीय उपनिषद्, १/५/२)
तद् विष्णोः परमं पदम्, सदा पश्यन्ति सूरयः (ऋक्, १/२२/२०)
(२) पति-पत्नी-सांख्य दर्शन के अनुसार चेतन तत्त्व पुरुष है, जड़ पदार्थ स्त्री है, जो पुरुष द्वारा नियन्त्रित होते हैं। घनता के क्रम में पदार्थ के ५ स्तर हैं-आकाश, वायु, अग्नि, अप् (जल), पृथ्वी।
तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः (आत्मा, चेतन द्वारा) आकाशः सम्भूतः। आकाशाद् वायुः। वायोः अग्निः। अग्नेः आपः। अद्भ्यः पृथिवी। (तैत्तिरीय उपनिषद्, २/१/३)
चेतन तत्त्व द्वारा अचेतन स्तरों का नियन्त्रण अन्यत्र भी कहा है-
गगन समीर अनल जल धरनी। इन्ह कइ नाथ सहज जड़ करनी॥२॥
ढोल गवाँर सूद्र पसु नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी॥६॥
(रामचरितमानस, सुन्दर काण्ड, ५९)
आकाश खाली स्थान है, उसका शब्द गुण है-दोनों गुण ढोल में होने से उसकी उपमा ढोल से है (ढोल के भीतर पोल, उससे शब्द)।
दुन्दुभेः तु ग्रहणेन दुन्दुभ्य आघातस्य शब्दो गृहीतः (बृहदारण्यक उपनिषद्, २/४/७)
जड़ चेष्टा वाले को ग्राम्य (गंवार) कहा है-
ग्राम्यासु जड चेष्टासु सततं विचिकित्सते (अक्ष्युपनिषद्, ८)
शूद्र का अर्थ है-आशु + द्रवति, जो शीघ्रता से काम करता है, तकनीक में दक्ष है। किन्तु जितने का आदेश होता है तथा पैसा मिलता है, उतना ही काम करता है। शूद्राः किमु-स्व क्रियया विहीनः (भव सन्तरणोपनिषद्, २/६४)
जो ८ प्रकार के सांसारिक पाशों से बन्धा है, वह पशु है-पशुपतिः अहङ्कार आविष्टः संसारी जीवः स एव पशुः (जाबालि उपनिषद्, २)
पाशबद्धः स्मृतो जीवः पासमुक्तः सनातनः। (नारायण उत्तरतापिनी उपनिषद्, १/७)
घृणा लज्जा भयं शंका ,जुगुप्सा चेति पञ्चमी।
कुलं शीलं तथा जातिरष्टो पाशः प्रकीर्तिताः॥
पाशबद्धो भवेत् जीवः, पाशमुक्तो सदाशिवः। (कुलार्णव तन्त्र)
पशु निर्माण या यज्ञ का साधन मात्र है, चेतनाहीन पुरुष भी पशु है।
(अग्निः) एतान् पञ्च पशून् अपश्यत्। पुरुषं अश्वं गां, अविं, अजं-यद् अपश्यत्, तस्मात् एते पशवः। (शतपथ ब्राह्मण, ६/२/१/२)
देवा यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुम्॥१५॥
भूमि धारण करने का स्थान है जैसे स्त्री मनुष्य को गर्भ में धारण करती है।
भूमिरापो ऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च (गीता, ७/४)
भूमिः धेनुः धरणी लोकधारिणी (महानारायण उपनिषद्, ४/५)
धरुणो मातरं धयन् इति अग्निं एव एतत् पृथिवीं धयन्तं आह। (शतपथ ब्राह्मण, ४/६/९/९)
(३) पुरुष स्त्री-यह २ प्रकार का विभाजन है। विकिरण या वर्षा करने वाला वृषा है, उसे ग्रहण करने वाला योषा (युक्त होने वाला)।
एष वै वृषा हरिः, य एष(सूर्यः) तपति (शतपथ ब्राह्मण, १४/३/१/२६)
योषा वेदिः (ग्रहण करने का स्थान), वृषा अग्निः (शतपथ ब्राह्मण, १/४/१/३३)
वृषा द्वारा पहले की तरह सृष्टि करने वाला वृषाकपि है-
तद् यत् कम्पायमानो रेतो वर्षति, तस्माद् वृषाकपिः (गोपथ ब्राह्मण, उत्तर, ६/१२)
कण या पिण्ड रूप पुरुष है, क्षेत्र रूप स्त्री है। सघन पिण्ड या ऊर्जा अग्नि है, फैला हुआ विरल पदार्थ सोम है। अग्नि पुरुष है, सोम श्री या स्त्री है।
इयं पृथिवी अग्निः (शतपथ ब्राह्मण, ६/१/२/१४, १४/९/१/१४)
श्रीर्वै सोमः (शतपथ ब्राह्मण, ४/१/३/९)
३. लोक गीत-निर्गुण गीत सामान्यतः कबीर के कहे जाते हैं। किन्तु आगम-निगम-पुराण में अव्यक्त तत्त्व के सभी वर्णन निर्गुण ही हैं। तुलसीदास ने दोनों को एक ही तत्त्व के २ रूप कहे हैं-
सगुनहि अगुनहि नहिं कछु भेदा। गावहिं मुनि पुरान बुध बेदा॥१॥
अगुन अरुप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई॥२॥
जो गुन रहित सगुन सोइ कैसें। जलु हिम उपल बिलग नहिं जैसें॥३॥
(रामचरितमानस, बालकाण्ड, ११५)
कबीरदास ने अपने को निरक्षर कहा है। उनके शिष्यों ने उनका उपदेश लिखा, जो बीजक कहा जाता है। किन्तु कोई भी प्रचलित निर्गुण गीत कबीर के बीजक या ग्रन्थों में नहीं है। यह कबीर के कई सौ वर्षों बाद उनके भक्तों ने लिखे हैं और अभी भी लिख रहे हैं।
४. विद्यापति-शरीर का सञ्चालक सूक्ष्म या वामन आत्मा (बालक रूप स्वामी)- पिआ मोर बालक हम तरुणी गे
कोन तप चुकलहुँ भेलहुँ जननी गे।
पहिरि लेल सखि सब दछिनक चीर
पिआ के देखैत मोर दगध सरीर। पिआ मोर बालक....
पिआ लेलि गोद कि चललि बजार
हटिआ के लोक पुछए के लागु तोहार। पिआ मोर बालक...
नहि मोरा दिओर कि नहि छोट भाइ
पुरब लिखल छल बालुम गे दाइ। पिआ मोर बालक....
बाट रे बटोहिआ कि तोहुँ मोरा भाइ
हमरो समाद नैहर नेने जाइ। पिआ मोर बालक...
कहिअनु बाबा के किनय धेनु गाइ
दुधबा पिआय के पोसता जमाइ। पिआ मोर बालक....
भनहिं 'विद्यापति' सुनु ब्रजनारी, धैरज धए रहू मिलत मुरारि।
बालक पिया या सूक्ष्म वामन आत्मा-शरीर रथ है, इसका सञ्चालक आत्मा रथी है-
आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरं रथमेव तु। बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च॥३॥
इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्। आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः॥४॥
(कठोपनिषद्, १/३)
आत्मा रूप वामन की उपासना कर उत्थान होता है-
ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति। मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते॥।३॥
(कठोपनिषद्, २/२/३)
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः
(कठोपनिषद्, ६/१७, श्वेताश्वतर उपनिषद्, ३/१३)
यही स्कन्द पुराण उत्कल खण्ड में रथ यात्रा प्रसंग में लिखा है-
दोलायमानं गोविन्दं, मञ्चस्थं मधुसूदनम्।
रथस्थं वामनं दृष्ट्वा, पुनर्जन्म न विद्यते॥
यह १८९० तक स्कन्द पुराण में था जिसे वाचस्पत्यम् तथा शब्द कल्पद्रुम कोष ने उद्धृत किया है।
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। (गीता, ८/१६)
५. महामृत्युञ्जय मन्त्र-त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्॥
(ऋक्, ७/५९/१२, वाज. ३/६०, तैत्तिरीय सं, १/८/६/२, मैत्रायणी सं, १/१०/४, २०, काण्व सं, ९/७, ३६१४, शतपथ ब्राह्मण, २/६/२/१२, १४, तैत्तिरीय ब्राह्मण, १/६/१०/५)
= तीन अम्बक वाले (सूर्य, चन्द्र, अग्नि नेत्र वाले, या जिसकी अम्बिका स्त्री हैं) की पूजा करते हैं, जो सुगन्ध या दिव्य गन्ध युक्त है तथा पुष्टि साधनों की वृद्धि करता है। जैसे ककड़ी का फल पकने पर स्वयं टूट जाता है, उसी प्रकार मृत्यु द्वारा शरीर से मुक्त हो जायेंगे, पर अमृत से हमारा सम्बन्ध नहीं छूटता।
शरीर से आत्मा निकल कर परमात्मा से मिलती है, उसी प्रकार कन्या विवाह के बाद पिता के घर से निकल कर पति के घर जाती है। परमात्मा को ही पति कहा जाता है। कन्या विवाह सम्बन्धित मन्त्र वाजसनेयि संहिता मन्त्र के अगले भाग में है।
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम्।
उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामुतः (वाज, ३/६०-भाग २)
= (कुमारियों के अर्थ में) पति की प्राप्ति करानेवाला, सुगन्धयुक्त, त्रिनेत्र की हम पूजा करती हैं। ककड़ी का फल जैसे अपने डण्ठल से छूट जाता है, उसी प्रकार हम कुमारियां माता, पिता, भाई आदि मातृगृह के बन्धुजनों से, उस कुल से, उस घर से दूर जायेंगी। किन्तु त्र्यम्बक के प्रसाद से हम पति से दूर न जांय, अर्थात् पति गोत्र में ही बनी रहें।
यजुर्वेद के इन दोनों मन्त्रों के समान अर्थ वाले हजारों निर्गुण गीत हैं, जिनमें मनुष्य को पत्नी, ब्रह्म को पति कहा गया है तथा शरीर से आत्मा निकलने को कन्या के ससुराल जाने जैसा कहा है। माया के बन्धन को ननद कहा गया है। इसे संस्कृत में ननान्दृ कहते हैं, अर्थात् जो प्रसन्न नहीं हो। पति अपनी बहन के अतिरिक्त पत्नी से भी प्रेम करने लगता है, जिससे ननद का अधिकार कुछ कम हो जाता है। इस भाव का एक प्रसिद्ध निर्गुण गीत साहिर लुधियानवी ने लिखा तथा मन्ना डे ने गाया था।
लागा चुनरी में दाग, छुपाऊँ कैसे,
चुनरी में दाग, छुपाऊँ कैसे, घर जाऊँ कैसे
लागा चुनरी में दाग...
हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया
जाके बाबुल से नज़रें मिलाऊँ कैसे, घर जाऊँ कैसे
भूल गई सब बचन बिदा के, खो गई मैं ससुराल में आके
जाके बाबुल से नज़रे मिलाऊँ कैसे, घर जाऊँ कैसे
कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल
वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल
जाके बाबुल से नज़रे मिलाऊँ कैसे, घर जाऊँ कैसे
कबीर से आरम्भ कर महेन्द्र मिश्र तक के इस अर्थ के बहुत से भोजपुरी गीत हैं।
इसी आशय का महेन्द्र मिश्र का प्रसिद्ध गीत है-
खेलइत रहलीं हम सुपुली मउनियाँ
ए ननदिया मोरी है, आई गइलें डोलिया कहाँर।
बाबा मोरा रहितें रामा, भइया मोरा रहितें
ए ननदिया मोरी हे, फेरि दीहतें डोलिया कहाँर।
काँच-काँच बाँसवा के डोलिया बनवलें,
ए ननदिया मोरी है, लागी गइलें चारि गो कहाँर।
नाहीं मोरा लूर ढंग एको न रहनवाँ
न ननदिया मोरी लेई के चलेलें ससुरार।
कहत महेन्दर मोरा लागे नाही मनवाँ
ए ननदिया मोरी हे छूटि गइलें बाबा के दुआर।
यह वाक् और अर्थ (शब्द, विश्व) दोनों के लिए है-
अव्यक्त विश्व या वाक् व्यक्त विश्व व्यक्त वाक्
(१). शुक्र तम तम
(२). अकाय पिण्ड शब्द आदि
(३). अव्रण छिद्र, दोष अपूर्णता, लुप्त शब्द।
(४). अस्नाविरम् ऋषि (रस्सी) कारक आदि से सम्बन्ध
(५). शुद्ध मिश्रण अपूर्ण रूप
(६). अपापविद्ध माया के आवरण शब्द, पद, वाक्य का पार्थक्य
अव्यक्त या निर्गुण का सगुण रूप में वर्णन ही शाश्वत काव्य है। वाक्य तात्कालिक घटना है, इसका व्यापक वर्णन काव्य है (वर्ण विपर्यय)।
२. उपमा- अव्यक्त विश्व के वर्णन के लिए व्यक्त पदार्थों से उनकी तुलना करते हैं। मूल शब्द भौतिक विश्व के लिए थे। अध्यात्म (शरीर के भीतर) तथा अधिदैव में उनके अर्थों का विस्तार या वृद्धि होती है। यह सादृश्य ही उपमा है।
(१) माता पिता-आकाश में पृथ्वी के सभी स्तरों को माता कहते हैं, उनके आकाश को पिता।
तिस्रो मातॄस्त्रीन्पितॄन्बिभ्रदेक ऊर्ध्वतस्थौ नेमवग्लापयन्ति ।
मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे विश्वमिदं वाचमविश्वमिन्वाम् ॥ (ऋग्वेद, १/१६४/१०)
इनकी परिभाषा है कि सूर्य चन्द्र से प्रकाशित भाग पृथ्वी है। दोनों से प्रकाशित पृथ्वी ग्रह है। सूर्य का प्रकाशित क्षेत्र सौर पृथ्वी है, जिसके ताप, तेज, प्रकाश ३ पद हैं। सूर्य प्रकाश की सीमा ब्रह्माण्ड है, जो सूर्य रूपी विष्णु का परम पद कहा है। बड़ी पृथ्वी में भी पृथ्वी ग्रह जैसे ही द्वीप, समुद्र, नदियों के नाम हैं-जैसे सौर मण्डल में ग्रह कक्षा से बने वलयाकार क्षेत्र पृथ्वी के द्वीपों के नाम पर हैं, तथा उनके बीच के भाग समुद्र। ब्रह्माण्ड का केन्द्रीय चक्र आकाशगंगा है।
रवि चन्द्रमसोर्यावन्मयूखैरवभास्यते। स समुद्र सरिच्छैला पृथिवी तावती स्मृता॥
(विष्णु पुराण, २/७/३)
इदं विष्णुर्विचक्रमे, त्रेधा निदधे पदम् (ऋक्, १/२२/१७)
सौरमण्डल के ३ विक्रम-भूरिति वा अग्निः। भुव इति वायुः। सुवः इति आदित्यः (तैत्तिरीय उपनिषद्, १/५/२)
तद् विष्णोः परमं पदम्, सदा पश्यन्ति सूरयः (ऋक्, १/२२/२०)
(२) पति-पत्नी-सांख्य दर्शन के अनुसार चेतन तत्त्व पुरुष है, जड़ पदार्थ स्त्री है, जो पुरुष द्वारा नियन्त्रित होते हैं। घनता के क्रम में पदार्थ के ५ स्तर हैं-आकाश, वायु, अग्नि, अप् (जल), पृथ्वी।
तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः (आत्मा, चेतन द्वारा) आकाशः सम्भूतः। आकाशाद् वायुः। वायोः अग्निः। अग्नेः आपः। अद्भ्यः पृथिवी। (तैत्तिरीय उपनिषद्, २/१/३)
चेतन तत्त्व द्वारा अचेतन स्तरों का नियन्त्रण अन्यत्र भी कहा है-
गगन समीर अनल जल धरनी। इन्ह कइ नाथ सहज जड़ करनी॥२॥
ढोल गवाँर सूद्र पसु नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी॥६॥
(रामचरितमानस, सुन्दर काण्ड, ५९)
आकाश खाली स्थान है, उसका शब्द गुण है-दोनों गुण ढोल में होने से उसकी उपमा ढोल से है (ढोल के भीतर पोल, उससे शब्द)।
दुन्दुभेः तु ग्रहणेन दुन्दुभ्य आघातस्य शब्दो गृहीतः (बृहदारण्यक उपनिषद्, २/४/७)
जड़ चेष्टा वाले को ग्राम्य (गंवार) कहा है-
ग्राम्यासु जड चेष्टासु सततं विचिकित्सते (अक्ष्युपनिषद्, ८)
शूद्र का अर्थ है-आशु + द्रवति, जो शीघ्रता से काम करता है, तकनीक में दक्ष है। किन्तु जितने का आदेश होता है तथा पैसा मिलता है, उतना ही काम करता है। शूद्राः किमु-स्व क्रियया विहीनः (भव सन्तरणोपनिषद्, २/६४)
जो ८ प्रकार के सांसारिक पाशों से बन्धा है, वह पशु है-पशुपतिः अहङ्कार आविष्टः संसारी जीवः स एव पशुः (जाबालि उपनिषद्, २)
पाशबद्धः स्मृतो जीवः पासमुक्तः सनातनः। (नारायण उत्तरतापिनी उपनिषद्, १/७)
घृणा लज्जा भयं शंका ,जुगुप्सा चेति पञ्चमी।
कुलं शीलं तथा जातिरष्टो पाशः प्रकीर्तिताः॥
पाशबद्धो भवेत् जीवः, पाशमुक्तो सदाशिवः। (कुलार्णव तन्त्र)
पशु निर्माण या यज्ञ का साधन मात्र है, चेतनाहीन पुरुष भी पशु है।
(अग्निः) एतान् पञ्च पशून् अपश्यत्। पुरुषं अश्वं गां, अविं, अजं-यद् अपश्यत्, तस्मात् एते पशवः। (शतपथ ब्राह्मण, ६/२/१/२)
देवा यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुम्॥१५॥
भूमि धारण करने का स्थान है जैसे स्त्री मनुष्य को गर्भ में धारण करती है।
भूमिरापो ऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च (गीता, ७/४)
भूमिः धेनुः धरणी लोकधारिणी (महानारायण उपनिषद्, ४/५)
धरुणो मातरं धयन् इति अग्निं एव एतत् पृथिवीं धयन्तं आह। (शतपथ ब्राह्मण, ४/६/९/९)
(३) पुरुष स्त्री-यह २ प्रकार का विभाजन है। विकिरण या वर्षा करने वाला वृषा है, उसे ग्रहण करने वाला योषा (युक्त होने वाला)।
एष वै वृषा हरिः, य एष(सूर्यः) तपति (शतपथ ब्राह्मण, १४/३/१/२६)
योषा वेदिः (ग्रहण करने का स्थान), वृषा अग्निः (शतपथ ब्राह्मण, १/४/१/३३)
वृषा द्वारा पहले की तरह सृष्टि करने वाला वृषाकपि है-
तद् यत् कम्पायमानो रेतो वर्षति, तस्माद् वृषाकपिः (गोपथ ब्राह्मण, उत्तर, ६/१२)
कण या पिण्ड रूप पुरुष है, क्षेत्र रूप स्त्री है। सघन पिण्ड या ऊर्जा अग्नि है, फैला हुआ विरल पदार्थ सोम है। अग्नि पुरुष है, सोम श्री या स्त्री है।
इयं पृथिवी अग्निः (शतपथ ब्राह्मण, ६/१/२/१४, १४/९/१/१४)
श्रीर्वै सोमः (शतपथ ब्राह्मण, ४/१/३/९)
३. लोक गीत-निर्गुण गीत सामान्यतः कबीर के कहे जाते हैं। किन्तु आगम-निगम-पुराण में अव्यक्त तत्त्व के सभी वर्णन निर्गुण ही हैं। तुलसीदास ने दोनों को एक ही तत्त्व के २ रूप कहे हैं-
सगुनहि अगुनहि नहिं कछु भेदा। गावहिं मुनि पुरान बुध बेदा॥१॥
अगुन अरुप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई॥२॥
जो गुन रहित सगुन सोइ कैसें। जलु हिम उपल बिलग नहिं जैसें॥३॥
(रामचरितमानस, बालकाण्ड, ११५)
कबीरदास ने अपने को निरक्षर कहा है। उनके शिष्यों ने उनका उपदेश लिखा, जो बीजक कहा जाता है। किन्तु कोई भी प्रचलित निर्गुण गीत कबीर के बीजक या ग्रन्थों में नहीं है। यह कबीर के कई सौ वर्षों बाद उनके भक्तों ने लिखे हैं और अभी भी लिख रहे हैं।
४. विद्यापति-शरीर का सञ्चालक सूक्ष्म या वामन आत्मा (बालक रूप स्वामी)- पिआ मोर बालक हम तरुणी गे
कोन तप चुकलहुँ भेलहुँ जननी गे।
पहिरि लेल सखि सब दछिनक चीर
पिआ के देखैत मोर दगध सरीर। पिआ मोर बालक....
पिआ लेलि गोद कि चललि बजार
हटिआ के लोक पुछए के लागु तोहार। पिआ मोर बालक...
नहि मोरा दिओर कि नहि छोट भाइ
पुरब लिखल छल बालुम गे दाइ। पिआ मोर बालक....
बाट रे बटोहिआ कि तोहुँ मोरा भाइ
हमरो समाद नैहर नेने जाइ। पिआ मोर बालक...
कहिअनु बाबा के किनय धेनु गाइ
दुधबा पिआय के पोसता जमाइ। पिआ मोर बालक....
भनहिं 'विद्यापति' सुनु ब्रजनारी, धैरज धए रहू मिलत मुरारि।
बालक पिया या सूक्ष्म वामन आत्मा-शरीर रथ है, इसका सञ्चालक आत्मा रथी है-
आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरं रथमेव तु। बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च॥३॥
इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्। आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः॥४॥
(कठोपनिषद्, १/३)
आत्मा रूप वामन की उपासना कर उत्थान होता है-
ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति। मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते॥।३॥
(कठोपनिषद्, २/२/३)
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः
(कठोपनिषद्, ६/१७, श्वेताश्वतर उपनिषद्, ३/१३)
यही स्कन्द पुराण उत्कल खण्ड में रथ यात्रा प्रसंग में लिखा है-
दोलायमानं गोविन्दं, मञ्चस्थं मधुसूदनम्।
रथस्थं वामनं दृष्ट्वा, पुनर्जन्म न विद्यते॥
यह १८९० तक स्कन्द पुराण में था जिसे वाचस्पत्यम् तथा शब्द कल्पद्रुम कोष ने उद्धृत किया है।
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। (गीता, ८/१६)
५. महामृत्युञ्जय मन्त्र-त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्॥
(ऋक्, ७/५९/१२, वाज. ३/६०, तैत्तिरीय सं, १/८/६/२, मैत्रायणी सं, १/१०/४, २०, काण्व सं, ९/७, ३६१४, शतपथ ब्राह्मण, २/६/२/१२, १४, तैत्तिरीय ब्राह्मण, १/६/१०/५)
= तीन अम्बक वाले (सूर्य, चन्द्र, अग्नि नेत्र वाले, या जिसकी अम्बिका स्त्री हैं) की पूजा करते हैं, जो सुगन्ध या दिव्य गन्ध युक्त है तथा पुष्टि साधनों की वृद्धि करता है। जैसे ककड़ी का फल पकने पर स्वयं टूट जाता है, उसी प्रकार मृत्यु द्वारा शरीर से मुक्त हो जायेंगे, पर अमृत से हमारा सम्बन्ध नहीं छूटता।
शरीर से आत्मा निकल कर परमात्मा से मिलती है, उसी प्रकार कन्या विवाह के बाद पिता के घर से निकल कर पति के घर जाती है। परमात्मा को ही पति कहा जाता है। कन्या विवाह सम्बन्धित मन्त्र वाजसनेयि संहिता मन्त्र के अगले भाग में है।
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम्।
उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामुतः (वाज, ३/६०-भाग २)
= (कुमारियों के अर्थ में) पति की प्राप्ति करानेवाला, सुगन्धयुक्त, त्रिनेत्र की हम पूजा करती हैं। ककड़ी का फल जैसे अपने डण्ठल से छूट जाता है, उसी प्रकार हम कुमारियां माता, पिता, भाई आदि मातृगृह के बन्धुजनों से, उस कुल से, उस घर से दूर जायेंगी। किन्तु त्र्यम्बक के प्रसाद से हम पति से दूर न जांय, अर्थात् पति गोत्र में ही बनी रहें।
यजुर्वेद के इन दोनों मन्त्रों के समान अर्थ वाले हजारों निर्गुण गीत हैं, जिनमें मनुष्य को पत्नी, ब्रह्म को पति कहा गया है तथा शरीर से आत्मा निकलने को कन्या के ससुराल जाने जैसा कहा है। माया के बन्धन को ननद कहा गया है। इसे संस्कृत में ननान्दृ कहते हैं, अर्थात् जो प्रसन्न नहीं हो। पति अपनी बहन के अतिरिक्त पत्नी से भी प्रेम करने लगता है, जिससे ननद का अधिकार कुछ कम हो जाता है। इस भाव का एक प्रसिद्ध निर्गुण गीत साहिर लुधियानवी ने लिखा तथा मन्ना डे ने गाया था।
लागा चुनरी में दाग, छुपाऊँ कैसे,
चुनरी में दाग, छुपाऊँ कैसे, घर जाऊँ कैसे
लागा चुनरी में दाग...
हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया
जाके बाबुल से नज़रें मिलाऊँ कैसे, घर जाऊँ कैसे
भूल गई सब बचन बिदा के, खो गई मैं ससुराल में आके
जाके बाबुल से नज़रे मिलाऊँ कैसे, घर जाऊँ कैसे
कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल
वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल
जाके बाबुल से नज़रे मिलाऊँ कैसे, घर जाऊँ कैसे
कबीर से आरम्भ कर महेन्द्र मिश्र तक के इस अर्थ के बहुत से भोजपुरी गीत हैं।
इसी आशय का महेन्द्र मिश्र का प्रसिद्ध गीत है-
खेलइत रहलीं हम सुपुली मउनियाँ
ए ननदिया मोरी है, आई गइलें डोलिया कहाँर।
बाबा मोरा रहितें रामा, भइया मोरा रहितें
ए ननदिया मोरी हे, फेरि दीहतें डोलिया कहाँर।
काँच-काँच बाँसवा के डोलिया बनवलें,
ए ननदिया मोरी है, लागी गइलें चारि गो कहाँर।
नाहीं मोरा लूर ढंग एको न रहनवाँ
न ननदिया मोरी लेई के चलेलें ससुरार।
कहत महेन्दर मोरा लागे नाही मनवाँ
ए ननदिया मोरी हे छूटि गइलें बाबा के दुआर।
Related Posts
0 Comments
Comments are not available.






