- मिस्टिक ज्ञान
- |
- 31 October 2024
- |
- 0 Comments
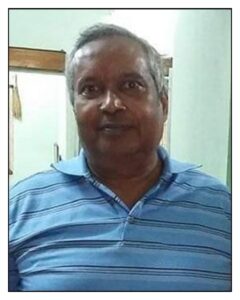 श्री अरुण कुमार उपाध्याय (धर्मज्ञ)
वेद, पुराण तथा इतिहास ग्रन्थों में रेवती के कई अर्थ हैं, जिनके कारण भ्रम होता है।
(१) रेवती नक्षत्र-यह चन्द्र कक्षा के २७ नक्षत्रों में अन्तिम है। नक्षत्रों की २ प्रकार से गणना है। स्थिर तारा के अनुसार मेष राशि तथा अश्विनी नक्षत्र के आरम्भ से गणना होती है। ऋतु चक्र या वर्ष की गणना जब सूर्य विषुव रेखा पर लम्ब होता है, उस समय से वर्ष तथा वसन्त ऋतु की गणना होती है। इस विन्दु पर विषुव वृत्त तथा क्रान्तिवृत्त (पृथ्वी कक्षा या पृथ्वी से देखने पर सूर्य कक्षा) का मिलन विदु है। इस विन्दु से दोनों वृत्त कैंची की तरह अलग होते हैं, अतः उसे कृत्तिका कहते हैं ।कृत्तिका के विपरीत १८०अंश की दूरी पर दोनों शाखायें मिलती हैं, अतः उसे द्वि-शाखा या विशाखा नक्षत कहते हैं। कृत्तिका से आरम्भ कर १३ नक्षत्रों में सूर्य उत्तर गोल में रहता है, अतः इनको देव नक्षत्र कहा गया है। उसके बाद के १४ नक्षत्रों में सूर्य दक्षिण गोल में रहेगा, उनको असुर नक्षत्र कहा है।
श्री अरुण कुमार उपाध्याय (धर्मज्ञ)
वेद, पुराण तथा इतिहास ग्रन्थों में रेवती के कई अर्थ हैं, जिनके कारण भ्रम होता है।
(१) रेवती नक्षत्र-यह चन्द्र कक्षा के २७ नक्षत्रों में अन्तिम है। नक्षत्रों की २ प्रकार से गणना है। स्थिर तारा के अनुसार मेष राशि तथा अश्विनी नक्षत्र के आरम्भ से गणना होती है। ऋतु चक्र या वर्ष की गणना जब सूर्य विषुव रेखा पर लम्ब होता है, उस समय से वर्ष तथा वसन्त ऋतु की गणना होती है। इस विन्दु पर विषुव वृत्त तथा क्रान्तिवृत्त (पृथ्वी कक्षा या पृथ्वी से देखने पर सूर्य कक्षा) का मिलन विदु है। इस विन्दु से दोनों वृत्त कैंची की तरह अलग होते हैं, अतः उसे कृत्तिका कहते हैं ।कृत्तिका के विपरीत १८०अंश की दूरी पर दोनों शाखायें मिलती हैं, अतः उसे द्वि-शाखा या विशाखा नक्षत कहते हैं। कृत्तिका से आरम्भ कर १३ नक्षत्रों में सूर्य उत्तर गोल में रहता है, अतः इनको देव नक्षत्र कहा गया है। उसके बाद के १४ नक्षत्रों में सूर्य दक्षिण गोल में रहेगा, उनको असुर नक्षत्र कहा है।
 https://www.mycloudparticles.com/
मुखं वा एतद् ऋतूनां यद् वसन्तः। (तैत्तिरीय ब्राह्मण, १/१/२/६)
सा तत ऊर्ध्व आरोहत्। सारोहिण्यभवत्। तद् रोहिण्यै रोहिणित्वम्। (तैत्तिरीय ब्राह्मण, १/१/१०/६)
कृत्तिकातः गणना-
मुखं वा एतत् नक्षत्राणा यत् कृत्तिकाः। एतद्वा अग्नेः नक्षत्रं यत् कृत्तिकाः। (तैत्तिरीय ब्राह्मण, १/१/२/१)
= अग्नि का अर्थ अग्रि या अग्रणी भी है। प्रथम होने के कारण कृत्तिका अग्नि नक्षत्र है। या, संवत्सर की अग्नि इस नक्षत्र में (सूर्य आने पर) पूरी तरह प्रज्वलित हो जाती है।
कृत्तिका प्रथमं। विशाखे उत्तमं। तानि देव नक्षत्राणि। यानि देवनक्षत्राणि तानि दक्षिणेन परियन्ति। अनुराधाः प्रथमम्। अपभरणीरुत्तमम्। तानि यम नक्षत्राणि। यानि यम नक्षत्राणि तानि उत्तरेण (परियन्ति) (तैत्तिरीय ब्राह्मण, १/५/२/७)
संवत्सरोऽसि नक्षत्रेषु स्थितः। ऋतूनां प्रतिष्ठा। (तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३/११/१/१३)
https://www.mycloudparticles.com/
मुखं वा एतद् ऋतूनां यद् वसन्तः। (तैत्तिरीय ब्राह्मण, १/१/२/६)
सा तत ऊर्ध्व आरोहत्। सारोहिण्यभवत्। तद् रोहिण्यै रोहिणित्वम्। (तैत्तिरीय ब्राह्मण, १/१/१०/६)
कृत्तिकातः गणना-
मुखं वा एतत् नक्षत्राणा यत् कृत्तिकाः। एतद्वा अग्नेः नक्षत्रं यत् कृत्तिकाः। (तैत्तिरीय ब्राह्मण, १/१/२/१)
= अग्नि का अर्थ अग्रि या अग्रणी भी है। प्रथम होने के कारण कृत्तिका अग्नि नक्षत्र है। या, संवत्सर की अग्नि इस नक्षत्र में (सूर्य आने पर) पूरी तरह प्रज्वलित हो जाती है।
कृत्तिका प्रथमं। विशाखे उत्तमं। तानि देव नक्षत्राणि। यानि देवनक्षत्राणि तानि दक्षिणेन परियन्ति। अनुराधाः प्रथमम्। अपभरणीरुत्तमम्। तानि यम नक्षत्राणि। यानि यम नक्षत्राणि तानि उत्तरेण (परियन्ति) (तैत्तिरीय ब्राह्मण, १/५/२/७)
संवत्सरोऽसि नक्षत्रेषु स्थितः। ऋतूनां प्रतिष्ठा। (तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३/११/१/१३)
 https://pixincreativemedia.com/
(२) रैवत साम-प्रभाव क्षेत्र को साम कहते हैं। पृथ्वी के ३ साम हैं-रथन्तर, वैरूप, शक्वर। सूर्य के बृहत्, वैराज, रैवत हैं।
यद्वै रथन्तरं तद् वैरूपं, यद् बृहत् तद् वैराजम्। यद्रथन्तरं तच्छाक्वरम्। यद् बृहत् तद् रैवतम्। (ऐतरेय ब्राह्मण १७/७/१३)।
इसके अतिरिक्त ऐतरेय ब्राह्मण (१९/६/१८), तैत्तिरीय ब्राह्मण (१/४/६) भी देखें।
रथन्तर साम के स्तोम (क्षेत्र) हैं-९, १५, १७, २१ (अहर्गण)। पृथ्वी के भीतर ३ धाम हैं। उसके बाद प्रत्येक धाम क्रमशः २-२ गुणा बड़े हैं (बृहदारण्यक उपनिषद्, ३/३/२)। अतः ’क’ धाम की त्रिज्या = पृथ्वी त्रिज्या x २ घात (क-३)। वैरूप साम देवलोक या सूर्य प्रकाश क्षेत्र है-३३ अहर्गण तक। देवा वै तृतीयेन अह्ना स्वर्गं लोकं आयन् तान् असुरा रक्षांसि अन्ववारयन्त ते विरूपा भवत---तद् वैरूपं साम अभवत् (ऐतरेय ब्राह्मण, ५/१) शक्वरी छन्द में ५६ अक्षर हैं, ५६ धाम ब्रह्माण्ड सीमा के पार का अन्धकार क्षेत्र है। अतः शक्वरी का अर्थ रात्रि है।
सूर्य का प्रभाव क्षेत्र बृहत् साम है। सौर मण्डल ३३ अहर्गण तक है, उसके बाद प्रजापति क्षेत्र ३४ अहर्गण से आरम्भ होता है। ३६ अक्षर का बृहती छन्द है, उसका क्षेत्र ३४-३८ अहर्गण तक है। उसके बाद विराट् (१० x ४ = ४० अक्षर) का वैराज साम है। इस साम की सीमा (४२ अहर्गण) महर्लोक है, जो सूर्य के चारों तरफ ब्रह्माण्ड की सर्पाकार भुजा की मोटाई का गोल है। सूर्य का प्रकाश जहां तक दीखता है, उसे विष्णु का परम पद या ब्रह्माण्ड की सीमा कहा गया है। यह रैवत साम है जिसके बाद रात्रि या अन्धकार क्षेत्र आरम्भ होता है।
रेवती से नक्षत्र मण्डल की समाप्ति होती है, या उस साम क्षेत्र में ब्रह्माण्ड का निर्माण होता है। ब्रह्माण्ड काश्यपी पृथ्वी है, यह पश्यक (द्रष्टा) या पशु का विपरीत है। अतः रेवती को पशु कहा है। रेवती क्षेत्र में निर्माण होने से वह माता है। यह वर्ष चक्र से या ब्रह्माण्ड सीमा के भीतर पुष्ट करता है, अतः इसका देवता पूषा है, जो विश्ववेदा या उसे जानने वाला है। ऋषि रूप में यह एकर्षि है जो सूर्य (स्रोत) तथा यम (अन्त) के बीच का क्रम है। ब्रह्माण्ड की माप रूप में यह गायत्री जैसा है। गायत्री छन्द के २४ अक्षर हैं। २ घात २४ = प्रायः १ कोटि। मनुष्य से आरम्भ कर पृथ्वी, सौर मण्डल, ब्रह्माण्ड, पूर्ण विश्व क्रमशः १-१ कोटि गुणा बड़े हैं (विष्णु पुराण, २/७/३-४)। रेवती से वर्ष का अन्त होता है तथा नया निर्माण (कृषि चक्र आदि) आरम्भ होता है। अतः कहा है कि मघा (या अघा) में गौ मारते हैं, रेवती में पुनः उत्पन्न होते हैं। मघा को वेद में अघा भी कहा गया है जिसमें गोदान किया जाता है-
अघासु हन्यते गावः अर्जुन्योः पर्युह्यते (ऋक्, १०/८५/१३)
अर्जुन का अर्थ फाल्गुनी नक्षत्र है। इसके पूर्व-उत्तर २ भाग हैं, अतः द्विवचन प्रयोग है। उसमें या रेवती नक्षत्र में पुनः न्र्माण होता है।
स (प्रजापतिः) रेवतीरसृजत तद् गवां घोषो अन्वसृज्यत(ताण्ड्य महाब्राह्मण, ७/८/१३)
रेवतीर्नः सधमादे (ऋक्, १/३०/१३)
ज्योती रेवती साम्नाम् (ताण्ड्य महाब्राह्मण, १३/७/२) -ज्योति सीमा तक रेवती।
गायत्री वै रेवती (ताण्ड्य महाब्राह्मण, १६/५/१९)-लोकों की माप।
रेवत्यो मातरः (ताण्ड्य महाब्राह्मण,१३/९/१७)
आपो वै रेवतीः (तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३/२/८/२, ताण्ड्य महाब्राह्मण, ७/९/२०, १३/९/१६)
ब्रह्माण्ड क्षेत्र रेवती या अप् में माता जैसा विश्व का जन्म हो रहा है।
पशवो वै रेवत्यः (ताण्ड्य महाब्राह्मण, १३/१०/११, १३/७/३ आदि)
रेवत्यः सर्वा देवताः (ऐतरेय ब्राह्मण, २/१६)
पूष्णो रेवती। गावः परस्ताद् वत्सा अवस्तात् (तैत्तिरीय ब्राह्मण, १/५/१/५)
(पौष मास में गौ या वर्ष की अग्नि समाप्त होती है, फाल्गुन में खाली होने के बाद चैत्र में पुनः निर्माण होता है।
निर्माण का स्रोत पूषा एकर्षि है तथा विश्व-वेदा है-
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा (ऋक्, १/८९/६, वाज.यजु, २५/१९)
पूषन् एकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मीन् समूह (ईशावास्योपनिषद्, वाज. यजु, ४०/१६)
रेवती नक्षत्र के ३२ तारा मनुष्य दन्तों की तरह २ पंक्ति में हैं, जिनको पूषा का दांत कहा गया है।
तस्य (पूष्णः) दन्तान् परोयाप तस्माद् आहुः अदन्तकः (कौषीतकि ब्राह्मण, ६/१३)
तस्माद् आहुः अदन्तकः पूषा पिष्टभाजन इति (गोपथ ब्राह्मण, उत्तर, १/२)
मनुष्य आयु पूर्ण होने के समय वैसा ही हो जाता है।
(३) रैवत मन्वन्तर-कलि आरम्भ तक स्वायम्भुव मनु से २६,००० वर्ष बीते थे जिस काल को मन्वन्तर (ऐतिहासिक) कहा गया है। इनका काल आदि त्रेता कहा है, जो उनसे ४०० वर्ष पूर्व समाप्त हो गया था।
षड्विंशति सहस्राणि वर्षाणि मानुषाणि तु।
वर्षाणां युगं ज्ञेयं दिव्यो ह्येष विधिः स्मृतः॥ (ब्रह्माण्ड पुराण, १/२/२९/१९)
स वै स्वायम्भुवः पूर्वं पुरुषो मनुरुच्यते।
तस्यैकसप्तति युगं मन्वन्तरमिहोच्यते॥ (ब्रह्माण्ड पुराण, १/ २/९/३६,३७)
तस्मादादौ तु कल्पस्य त्रेता युगमुखे तदा (वायु पुराण, ९/४६)
त्रेता युगमुखे पूर्वमासन् स्वायम्भुवेऽन्तरे। (वायु पुराण, ३१/३)
स्वायम्भुवेऽन्तरे पूर्वमाद्ये त्रेता युगे तदा। (वायु पुराण, ३३/५)
इतिहास के लिए १२,००० वर्षों का युग लिया गया है तथा इस चक्र में ही आगम अनुसार बीज संस्कार लिखा है। (भास्कराचार्य-२, सिद्धान्त शिरोमणि, भू-परिधि, ७-८)।
अवसर्पिणी में युगों का क्रम है-सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि-जिनके मान हैं-४८००, ३६००, २४००, १२०० वर्ष। इसके बाद विपरीत क्रम से युग होते हैं-कलि, द्वापर, त्रेता, सत्य। दोनों मिला कर २४,००० वर्ष का अयनाब्द युग है। २६,००० वर्ष के बदले २४,००० वर्ष का युग चक्र लेते हैं, जो अयन तथा मन्दोच्च गति (३१२,००० वर्ष) चक्रों का समन्वय है। जल प्रलय या हिमयुग इसी चक्र में हैं। अयन चक्र से समन्वय के लिए बीज संशोधन करना पड़ता है।
वैवस्वत मनु का काल १३,९०२ ईपू से आरम्भ हुआ, जो इक्ष्वाकु (८५७६ ईपू) तक चला। २९१०२ ईपू में स्वायम्भुव मनु काल समाप्त हुआ जो ४००० वर्षों का था (त्रेता ३६०० + ४००)। इसके बीच सभी मनु तथा सावर्णि मनु हुए, जो उन्हीं के सम्बन्धी थे। उनके काल हैं-
मनु - सावर्णि मनु - काल (ईपू)
स्वायम्भुव - इन्द्र ३३१०२-२९१०२
स्वारोचिष- देव २९१०२-२६०६२
उत्तम -रुद्र -२६०६२-२३०२२
तामस- धर्म- २३०२२-१९९८२
रैवत- ब्रह्म -१९९८२-१६९४२
चाक्षुष- दक्ष-१६९४२-१३९०२
वैवस्वत-मेरु- १३९०२-८५७६
रैवत मनु या ब्रह्म-सावर्णि (कश्यप) का काल था -१९९८२-१६९४२ ईपू। इसके आरम्भ मे रैवत हुए जब तामस के पतन के बाद पुनः विकास हुआ। अन्तिम भाग में कश्यप हुए जिनका काल १७५०० ईपू है। उस समय अदिति नक्षत्र पुनर्वसु से वर्ष आरम्भ या विषुव संक्रान्ति होती थी।-अदितिर्जातम्, अदितिर्जनित्वम् (शान्ति पाठ, ऋक्, १/८९/१०, वाज.यजु, २५/२३) उससे ७ नक्षत्र पूर्व रेवती नक्षत्र से दिव्य वर्ष या उत्तरायण का आरम्भ होता था। रेवती के पतन का अर्थ है, रेवती के बदले अन्य नक्षत्र से वर्ष का आरम्भ (मार्कण्डेय पुराण, अध्याय ७५, स्कन्द पुराण, ७/२/१७/१४५, देवी भागवत माहात्म्य, अध्याय ४)।
(४) रेवती का अशुभत्व-४ राशि = ९ नक्षत्र = १२० अंश। अतः मेष-अश्विनी, सिंह-मघा, धनु-मूल का आरम्भ एक साथ होता है। इन सन्धि विन्दुओं के निकट का भाग गण्ड मूल कहलाता है, जिसमें जन्म होना अशुभ मानते हैं।
मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाला अपने मूल या परिवार को नष्ट कर देता है (मूल को झाड़ू या बर्हणि, बढ़नी, की तरह साफ करता है। इसे विचृति भी कहा गया है-
विचृतोर्यमस्य मूलबर्हणात् परि पाह्येनम्।
अत्येनं नेषद् दुरितानि विश्वा दीरायुत्वाय शतशारदाय।
(अथर्व सं, ६/११०/२)
निर्ऋत्यै मूलबर्हणी। प्रतिभञ्जन्तः परस्तात्। प्रतिशृणन्तो ऽवस्तात्। (तैत्तिरीय ब्राह्मण, १/५/१/१७)
रेवती के अशुभ का सम्बन्ध सौराष्ट्र, आनर्त से कहा गया है, जिसका कारण स्पष्ट नहीं है-
रेवती पूर्वेणोपसृष्टा पशून् उपहन्ति दक्षिणेन आनर्त्तान्। पश्चिमेन बाह्लीक-सिन्धु-सौवीर-कीर-पह्लवान्। उत्तरेण आपः सर्वतः सुराष्ट्र-वैदेह-हिरण्यपाद-क्षुद्रक-मालव-मलयज-वृजिन-हैमवत -बाहुदा-कुम्भि- भोजानाम्। हिरण्यपादानां च श्रेष्ठम्। यच्च पार्श्वेषूक्तम्। (बल्लाल सेन का अद्भुत् सागर, ऋक्षाद्यद्भुतावर्त्तः)
रैवतक पर्वत कभी रैवत मनु का स्थान था। उस वंश या क्षेत्र की कन्या रेवती थी, जिसका बलराम से विवाह हुआ था। उसकी कहानी रहस्यात्मक है कि वह ब्रह्मा जी से योग्य वर पूछने गये थे तब तक पृथ्वी में कई युग बीत गये थे (देवीभागवत पुराण, ७/७/४६, विष्णु पुराण, ४/१/६६ आदि)। यह आइंस्टीन के सापेक्षवाद के अनुसार काल की गति कम होने का वर्णन है। इस प्रकार की अन्य कथा योगवासिष्ठ रामायण के मण्डप उपाख्यान में भी है।
https://pixincreativemedia.com/
(२) रैवत साम-प्रभाव क्षेत्र को साम कहते हैं। पृथ्वी के ३ साम हैं-रथन्तर, वैरूप, शक्वर। सूर्य के बृहत्, वैराज, रैवत हैं।
यद्वै रथन्तरं तद् वैरूपं, यद् बृहत् तद् वैराजम्। यद्रथन्तरं तच्छाक्वरम्। यद् बृहत् तद् रैवतम्। (ऐतरेय ब्राह्मण १७/७/१३)।
इसके अतिरिक्त ऐतरेय ब्राह्मण (१९/६/१८), तैत्तिरीय ब्राह्मण (१/४/६) भी देखें।
रथन्तर साम के स्तोम (क्षेत्र) हैं-९, १५, १७, २१ (अहर्गण)। पृथ्वी के भीतर ३ धाम हैं। उसके बाद प्रत्येक धाम क्रमशः २-२ गुणा बड़े हैं (बृहदारण्यक उपनिषद्, ३/३/२)। अतः ’क’ धाम की त्रिज्या = पृथ्वी त्रिज्या x २ घात (क-३)। वैरूप साम देवलोक या सूर्य प्रकाश क्षेत्र है-३३ अहर्गण तक। देवा वै तृतीयेन अह्ना स्वर्गं लोकं आयन् तान् असुरा रक्षांसि अन्ववारयन्त ते विरूपा भवत---तद् वैरूपं साम अभवत् (ऐतरेय ब्राह्मण, ५/१) शक्वरी छन्द में ५६ अक्षर हैं, ५६ धाम ब्रह्माण्ड सीमा के पार का अन्धकार क्षेत्र है। अतः शक्वरी का अर्थ रात्रि है।
सूर्य का प्रभाव क्षेत्र बृहत् साम है। सौर मण्डल ३३ अहर्गण तक है, उसके बाद प्रजापति क्षेत्र ३४ अहर्गण से आरम्भ होता है। ३६ अक्षर का बृहती छन्द है, उसका क्षेत्र ३४-३८ अहर्गण तक है। उसके बाद विराट् (१० x ४ = ४० अक्षर) का वैराज साम है। इस साम की सीमा (४२ अहर्गण) महर्लोक है, जो सूर्य के चारों तरफ ब्रह्माण्ड की सर्पाकार भुजा की मोटाई का गोल है। सूर्य का प्रकाश जहां तक दीखता है, उसे विष्णु का परम पद या ब्रह्माण्ड की सीमा कहा गया है। यह रैवत साम है जिसके बाद रात्रि या अन्धकार क्षेत्र आरम्भ होता है।
रेवती से नक्षत्र मण्डल की समाप्ति होती है, या उस साम क्षेत्र में ब्रह्माण्ड का निर्माण होता है। ब्रह्माण्ड काश्यपी पृथ्वी है, यह पश्यक (द्रष्टा) या पशु का विपरीत है। अतः रेवती को पशु कहा है। रेवती क्षेत्र में निर्माण होने से वह माता है। यह वर्ष चक्र से या ब्रह्माण्ड सीमा के भीतर पुष्ट करता है, अतः इसका देवता पूषा है, जो विश्ववेदा या उसे जानने वाला है। ऋषि रूप में यह एकर्षि है जो सूर्य (स्रोत) तथा यम (अन्त) के बीच का क्रम है। ब्रह्माण्ड की माप रूप में यह गायत्री जैसा है। गायत्री छन्द के २४ अक्षर हैं। २ घात २४ = प्रायः १ कोटि। मनुष्य से आरम्भ कर पृथ्वी, सौर मण्डल, ब्रह्माण्ड, पूर्ण विश्व क्रमशः १-१ कोटि गुणा बड़े हैं (विष्णु पुराण, २/७/३-४)। रेवती से वर्ष का अन्त होता है तथा नया निर्माण (कृषि चक्र आदि) आरम्भ होता है। अतः कहा है कि मघा (या अघा) में गौ मारते हैं, रेवती में पुनः उत्पन्न होते हैं। मघा को वेद में अघा भी कहा गया है जिसमें गोदान किया जाता है-
अघासु हन्यते गावः अर्जुन्योः पर्युह्यते (ऋक्, १०/८५/१३)
अर्जुन का अर्थ फाल्गुनी नक्षत्र है। इसके पूर्व-उत्तर २ भाग हैं, अतः द्विवचन प्रयोग है। उसमें या रेवती नक्षत्र में पुनः न्र्माण होता है।
स (प्रजापतिः) रेवतीरसृजत तद् गवां घोषो अन्वसृज्यत(ताण्ड्य महाब्राह्मण, ७/८/१३)
रेवतीर्नः सधमादे (ऋक्, १/३०/१३)
ज्योती रेवती साम्नाम् (ताण्ड्य महाब्राह्मण, १३/७/२) -ज्योति सीमा तक रेवती।
गायत्री वै रेवती (ताण्ड्य महाब्राह्मण, १६/५/१९)-लोकों की माप।
रेवत्यो मातरः (ताण्ड्य महाब्राह्मण,१३/९/१७)
आपो वै रेवतीः (तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३/२/८/२, ताण्ड्य महाब्राह्मण, ७/९/२०, १३/९/१६)
ब्रह्माण्ड क्षेत्र रेवती या अप् में माता जैसा विश्व का जन्म हो रहा है।
पशवो वै रेवत्यः (ताण्ड्य महाब्राह्मण, १३/१०/११, १३/७/३ आदि)
रेवत्यः सर्वा देवताः (ऐतरेय ब्राह्मण, २/१६)
पूष्णो रेवती। गावः परस्ताद् वत्सा अवस्तात् (तैत्तिरीय ब्राह्मण, १/५/१/५)
(पौष मास में गौ या वर्ष की अग्नि समाप्त होती है, फाल्गुन में खाली होने के बाद चैत्र में पुनः निर्माण होता है।
निर्माण का स्रोत पूषा एकर्षि है तथा विश्व-वेदा है-
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा (ऋक्, १/८९/६, वाज.यजु, २५/१९)
पूषन् एकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मीन् समूह (ईशावास्योपनिषद्, वाज. यजु, ४०/१६)
रेवती नक्षत्र के ३२ तारा मनुष्य दन्तों की तरह २ पंक्ति में हैं, जिनको पूषा का दांत कहा गया है।
तस्य (पूष्णः) दन्तान् परोयाप तस्माद् आहुः अदन्तकः (कौषीतकि ब्राह्मण, ६/१३)
तस्माद् आहुः अदन्तकः पूषा पिष्टभाजन इति (गोपथ ब्राह्मण, उत्तर, १/२)
मनुष्य आयु पूर्ण होने के समय वैसा ही हो जाता है।
(३) रैवत मन्वन्तर-कलि आरम्भ तक स्वायम्भुव मनु से २६,००० वर्ष बीते थे जिस काल को मन्वन्तर (ऐतिहासिक) कहा गया है। इनका काल आदि त्रेता कहा है, जो उनसे ४०० वर्ष पूर्व समाप्त हो गया था।
षड्विंशति सहस्राणि वर्षाणि मानुषाणि तु।
वर्षाणां युगं ज्ञेयं दिव्यो ह्येष विधिः स्मृतः॥ (ब्रह्माण्ड पुराण, १/२/२९/१९)
स वै स्वायम्भुवः पूर्वं पुरुषो मनुरुच्यते।
तस्यैकसप्तति युगं मन्वन्तरमिहोच्यते॥ (ब्रह्माण्ड पुराण, १/ २/९/३६,३७)
तस्मादादौ तु कल्पस्य त्रेता युगमुखे तदा (वायु पुराण, ९/४६)
त्रेता युगमुखे पूर्वमासन् स्वायम्भुवेऽन्तरे। (वायु पुराण, ३१/३)
स्वायम्भुवेऽन्तरे पूर्वमाद्ये त्रेता युगे तदा। (वायु पुराण, ३३/५)
इतिहास के लिए १२,००० वर्षों का युग लिया गया है तथा इस चक्र में ही आगम अनुसार बीज संस्कार लिखा है। (भास्कराचार्य-२, सिद्धान्त शिरोमणि, भू-परिधि, ७-८)।
अवसर्पिणी में युगों का क्रम है-सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि-जिनके मान हैं-४८००, ३६००, २४००, १२०० वर्ष। इसके बाद विपरीत क्रम से युग होते हैं-कलि, द्वापर, त्रेता, सत्य। दोनों मिला कर २४,००० वर्ष का अयनाब्द युग है। २६,००० वर्ष के बदले २४,००० वर्ष का युग चक्र लेते हैं, जो अयन तथा मन्दोच्च गति (३१२,००० वर्ष) चक्रों का समन्वय है। जल प्रलय या हिमयुग इसी चक्र में हैं। अयन चक्र से समन्वय के लिए बीज संशोधन करना पड़ता है।
वैवस्वत मनु का काल १३,९०२ ईपू से आरम्भ हुआ, जो इक्ष्वाकु (८५७६ ईपू) तक चला। २९१०२ ईपू में स्वायम्भुव मनु काल समाप्त हुआ जो ४००० वर्षों का था (त्रेता ३६०० + ४००)। इसके बीच सभी मनु तथा सावर्णि मनु हुए, जो उन्हीं के सम्बन्धी थे। उनके काल हैं-
मनु - सावर्णि मनु - काल (ईपू)
स्वायम्भुव - इन्द्र ३३१०२-२९१०२
स्वारोचिष- देव २९१०२-२६०६२
उत्तम -रुद्र -२६०६२-२३०२२
तामस- धर्म- २३०२२-१९९८२
रैवत- ब्रह्म -१९९८२-१६९४२
चाक्षुष- दक्ष-१६९४२-१३९०२
वैवस्वत-मेरु- १३९०२-८५७६
रैवत मनु या ब्रह्म-सावर्णि (कश्यप) का काल था -१९९८२-१६९४२ ईपू। इसके आरम्भ मे रैवत हुए जब तामस के पतन के बाद पुनः विकास हुआ। अन्तिम भाग में कश्यप हुए जिनका काल १७५०० ईपू है। उस समय अदिति नक्षत्र पुनर्वसु से वर्ष आरम्भ या विषुव संक्रान्ति होती थी।-अदितिर्जातम्, अदितिर्जनित्वम् (शान्ति पाठ, ऋक्, १/८९/१०, वाज.यजु, २५/२३) उससे ७ नक्षत्र पूर्व रेवती नक्षत्र से दिव्य वर्ष या उत्तरायण का आरम्भ होता था। रेवती के पतन का अर्थ है, रेवती के बदले अन्य नक्षत्र से वर्ष का आरम्भ (मार्कण्डेय पुराण, अध्याय ७५, स्कन्द पुराण, ७/२/१७/१४५, देवी भागवत माहात्म्य, अध्याय ४)।
(४) रेवती का अशुभत्व-४ राशि = ९ नक्षत्र = १२० अंश। अतः मेष-अश्विनी, सिंह-मघा, धनु-मूल का आरम्भ एक साथ होता है। इन सन्धि विन्दुओं के निकट का भाग गण्ड मूल कहलाता है, जिसमें जन्म होना अशुभ मानते हैं।
मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाला अपने मूल या परिवार को नष्ट कर देता है (मूल को झाड़ू या बर्हणि, बढ़नी, की तरह साफ करता है। इसे विचृति भी कहा गया है-
विचृतोर्यमस्य मूलबर्हणात् परि पाह्येनम्।
अत्येनं नेषद् दुरितानि विश्वा दीरायुत्वाय शतशारदाय।
(अथर्व सं, ६/११०/२)
निर्ऋत्यै मूलबर्हणी। प्रतिभञ्जन्तः परस्तात्। प्रतिशृणन्तो ऽवस्तात्। (तैत्तिरीय ब्राह्मण, १/५/१/१७)
रेवती के अशुभ का सम्बन्ध सौराष्ट्र, आनर्त से कहा गया है, जिसका कारण स्पष्ट नहीं है-
रेवती पूर्वेणोपसृष्टा पशून् उपहन्ति दक्षिणेन आनर्त्तान्। पश्चिमेन बाह्लीक-सिन्धु-सौवीर-कीर-पह्लवान्। उत्तरेण आपः सर्वतः सुराष्ट्र-वैदेह-हिरण्यपाद-क्षुद्रक-मालव-मलयज-वृजिन-हैमवत -बाहुदा-कुम्भि- भोजानाम्। हिरण्यपादानां च श्रेष्ठम्। यच्च पार्श्वेषूक्तम्। (बल्लाल सेन का अद्भुत् सागर, ऋक्षाद्यद्भुतावर्त्तः)
रैवतक पर्वत कभी रैवत मनु का स्थान था। उस वंश या क्षेत्र की कन्या रेवती थी, जिसका बलराम से विवाह हुआ था। उसकी कहानी रहस्यात्मक है कि वह ब्रह्मा जी से योग्य वर पूछने गये थे तब तक पृथ्वी में कई युग बीत गये थे (देवीभागवत पुराण, ७/७/४६, विष्णु पुराण, ४/१/६६ आदि)। यह आइंस्टीन के सापेक्षवाद के अनुसार काल की गति कम होने का वर्णन है। इस प्रकार की अन्य कथा योगवासिष्ठ रामायण के मण्डप उपाख्यान में भी है।
Related Posts
0 Comments
Comments are not available.






