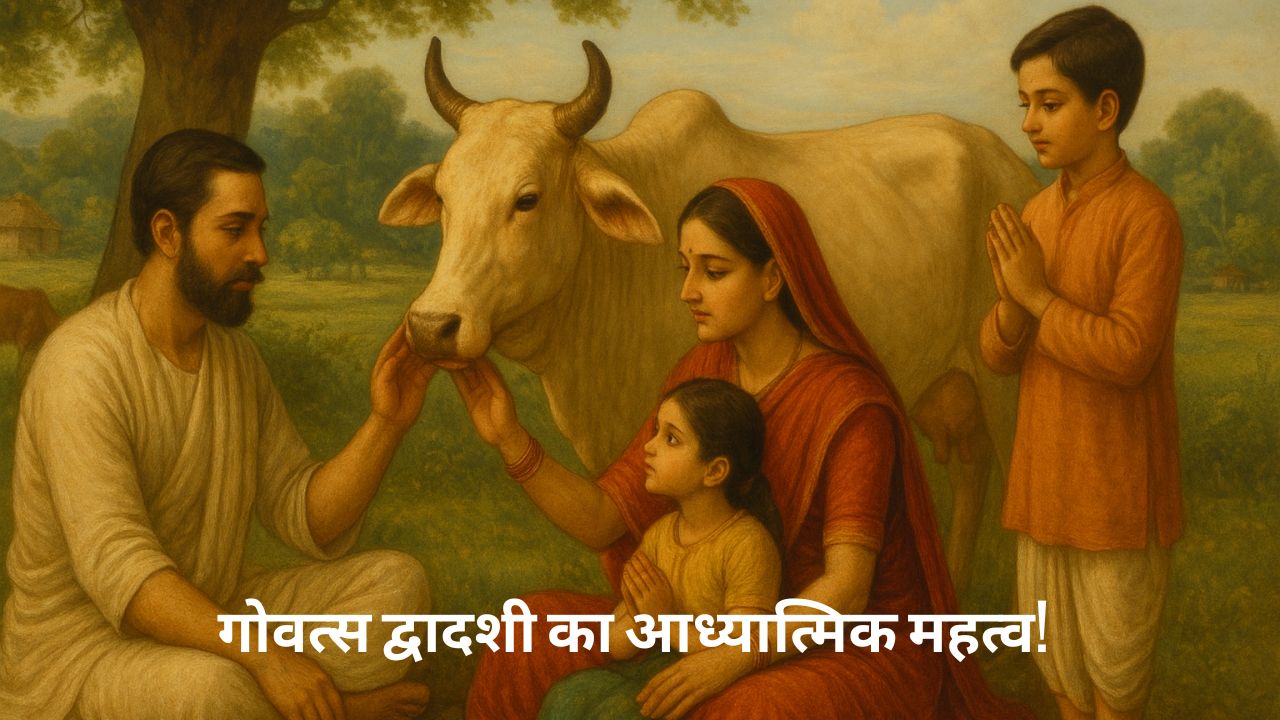- धर्म-पथ
- |
-
31 October 2024
- |
- 0 Comments
श्री पं. गड्गगाप्रसाद जी एम. ए.
चीफ जस्टिस, टिहरी गढ़वाल राज्य तथा डिप्टी कलक्टर युक्त प्रान्त,
भूतपूर्व प्रोफेसर मेरठ कालेज तथा प्रधान, आर्य सार्वदेशिक सभा, देहली
वेदों पर प्रायः ये दोष लगाया जाता है कि वे बहुदेवोपासना, तत्व पूजा और प्रकृति पूजा आदि की शिक्षा देते हैं। यह दोषारोपण सर्वथा न्याय विरूद्ध है। इस मूल का कारण अमिनि, इन्द्र, मित्र, वरूण आदि वैदिक शब्दों के दो भिन्न अर्थों का मिश्रित करना है। वैदिक निर्वचन का यह प्राचीन और सुनिश्चित सिद्धान्त है, जिसका महत्त्व जितना ही अधिक समझा जाय उतना ही अच्छा है कि वैदिक शब्दों के यौगिक अर्थ लिये जाने चाहिये। इस प्रकार वेदों में जो शब्द व्यवहृतत हुए हैं उनके दो अर्थ होते हैं और कभी-कभी दो से भी अधिक। उदाहरणार्थ “इन्द्र” शब्द जो इदि ऐश्वर्य धातु से निकाला है कम से कम तीन अर्थों में प्रयुक्त होता है। कभी उसके अर्थ सूर्य के होते हैं क्योंकि उसका प्रकाश, ऐश्वर्य वा तेज युक्त होता है, कभी उसके अर्थ राजा के होते हैं जिसके अधिकार में संसारिक ऐश्वर्य होता है और कभी-कभी उसके अर्थ ईश्वर के होते हैं जिसका अनुपम ऐश्वर्य है। स्वामी दयानन्द कृत सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में इस विषय की पूर्ण व्याख्या की गई है। उसमें ग्रन्थकार ने ऐसे बहुत से शब्दों के यौगिक अर्थ देकर भली भाँति सिद्ध किया है कि जब वे शब्द उपासना के विषय में प्रयुक्त होते हैं तो उन सबसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ही बोध होता है। इन शब्दों में से कुछेक को उनके अनेक अर्थों सहित नीचे उद्धृत करते है: -
।. इन्द्र (दि, ऐश्वर्य धातु से)
(]) सूर्य (2) राजा (3) परमेश्वरा
- मित्र, (मिद, स्नेहने धातु से)
(]) सूर्य (2) सखा (3) सबका मित्र परमेश्वर3. वरूण, (वृ-वरणे, ईर्ष्यायाम् धातु से )
(3) आकाश (2) परमेश्वर जो महान् और सर्वोत्तम है।
- अग्नि, (अंचु गति पूजनयो धातु से )
(1) अम्नि या उष्णता जो शीघ्रता पूर्वक गमन करती है, (2) सर्वव्यापक औः
उपासनीय परमेश्वरा
- वायु (वा गति गंधनयो धातु से)
(]) हवा (2) परमेश्वर जो सब से अधिक बलवान है।
- चन्द्र (चिदि, आह्वादे धातु से)
(]) चन्द्रमा जिसे देख सब आनन्दित होते हैं
(2) सर्वसुखों का दाता परमेश्वरा
- यम (यम उपरमे धातु से)
(1) राजा (2) सबका शासका
- काल, (कल संख्याने धातु से)
(1) समय (2) परमेश्वर जो सबकी गणना करता है।
9. यज्ञ, (यज देव पूजा सड़ूगतिकरण दानेषु धातु से )
(1) उपासना या आहुति देने की प्रक्रिया, (2) परमेश्वर जो पूजा के योग्य है।
10.रूद्र, (रूदिर अश्र विमोचने धातु से)
(1) राजा जो दुसरे का दमन करता है, (2) ईश्वर जो दुष्टों को दण्ड देता है।
और भी शब्द हैं जो वेदों में साधारणतया ईश्वर के लिये प्रयुक्त होते हैं, परन्तु पाश्चात्य विद्वान अपने हृदयों पर पुराणों की कथा, वर्त्तमान समय के हिन्दूओं के मिथ्या भ्रम और मूर्ति पूजा का कुप्रभाव पड़ने के कारण बहुधा उन्हें विविध देवताओं के अर्थ में लेते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव प्रसिद्ध शब्द इसी प्रकार के हैं जो हिन्दूओं के देवालय में तीन प्रधान देवताओं के लिये आते हैं। सुविज्ञ पाठकों को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे विचार वेदों से सर्वथा बाहर हैं। स्वामी दयानन्द सरस्वती उपर्युक्त नामों कीनिम्न प्रकार व्युत्पत्ति और व्याख्या करते है:-
ब्रह्मा- (वृहि वृद्धौ धातु से ) परमात्मा जो बड़ा है।
विष्णु- विष् (विष्लृ व्याप्ती धातु से ) ईश्वर जो समस्त वस्तुओं में व्यापक हैं।
शिव- (शिव कल्याणे धातु से) ईश्वर जो सब भलाईयों का कारण है।
शंकर- का शब्दार्थ “वह जो कल्याण करता है।?
महादेव- का शब्दार्थ 'देवों में बड़ा? है।
गणेश- का शब्दार्थ “गणों का स्वामी' है।
ये समस्त शब्द एक ईश्वर का ही बोध कराते हैं। इस बात की पुष्टि देवों की आन्तरिक साक्षी से होती है। हम यहाँ ऋग्वेद का मन्त्र उद्धृत करते हैं।
इन्द्रं मित्र वरूणमग्निमाहुरथो दिव्य: स सुपर्णों गुरूत्मान्|
एक॑ सद्रिप्रा: बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहु: ॥
ऋग्वेद मं. स. 94 मंत्र 49 ॥
उस एक अविनाशी ब्रह्म को जो दिव्य स्वरूप, उत्तम गुणों से युक्त परमात्मा है विद्वान लोग बहुत से नामों से पुकारते हैं, जैसे इन्द्र (ऐश्वर्य युक्त) मित्र (सब का सखा) वरूण (सर्वोत्तम), अग्नि (सब का उपास्य) यम (सब का राजा) मातरिश्वा (सब से बलवान) ।
उसी वेद के दूसरे स्थान में हम पाते है: -
सुपर्ण विप्रा कवयो वचोभिरेक॑ सन्त बहुधा कल्पयन्ति।
ऋग्वेद मं. 0 सू. 4 मं.5॥
विद्वान् और बुद्धिमान पुरूष अनेक गुण युक्त एक परमेश्वर की सत्ता को अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं।
यजुर्वेद में फिर हम पढ़ते है: -
तदेवाम्निस्तदादित्यस्तद् वायु स्तदु चन्द्रमा :।
तदेव शुक्र तद् ब्रह्म] ताआप: स प्रजापति: ॥
यजुर्वेद अध्याय 32 मं.]॥
“वह अग्नि(उपासनीय) है, वह आदित्य (नाश-रहित) है, वह वायु (अनन्त बलयुक्त) है, वह चन्द्रमा (हर्ष का देने वाला) है, वह शुक्र (उत्पादक) है, वह ब्रह्म (महान) है, वह आप: (सर्वव्यापक) है, वह प्रजापति (सब प्राणियों का स्वामी) है।”
उपर्युक्त विचार की पुष्टि नीचे लिखी बाह्य साक्षी से भी होती है: -
कैवल्योपनिषद् में लिखा है: -
स ब्रह्मा स विष्णु: स रूद्र: स शिव: सो 5क्षर: स परम: स्वराट्।
स इन्द्र: स कालाग्नि: स चन्द्रमा: ॥
कैवेल्योपनिषद्
वह ब्रह्म( महान्) है वह विष्णु (सर्वव्यापक) है, वह रूद्र (दण्ड देने वाला) है, वह शिव (सब आनन्द और भलाईयों का मूल) है। वह अक्षर (अविनाशी) है, वह सब से अधिक उच्च और सब से अधिक दीक्तिमान् है, वह इन्द्र (ऐश्वर्यमान) है, वह कालाग्नि (पूजनीय और सब की गणना करने वाला) है, वह चन्द्रमा (आनन्द का देने वाला) है।
फिर मनुस्मृति में लिखा है: -
प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि।
रूक्माम॑ स्वप्नधीगम्यं विद्यात्त पुरूष परम॥
एतमम्निं वदन्त्येके मनुमन्ये प्रजापतिम
इन्द्रमेकेडपरे प्राणमपरे ब्रह्मशाश्वतम्॥
मनु 2-22-23
मनुष्य को चाहिये कि परमेश्वर को जाने, जो सब का शासक, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म प्रकाशयुक्त और केवल ध्यान द्वारा जानने योग्य है। कोई उसे अग्नि (पूजा के योग्य) कोई मनु (मनस्वी) कोई प्रजापति (सब प्रजा का स्वामी) कहता है, कोई उसे इन्द्र (ऐश्वर्यवान्) कोई प्राण (जीवन-मूल) और कोई उसे सनातन ब्रह्म कहता है।
इस विषय में भ्रम फैलाने का सब से अधिक प्रभावपूर्ण कारण “या* उससे निकले हुए देवता शब्द का अशुद्ध अर्थ है। स्वामी दयानन्द सरस्वती के “देव” शब्द के शुद्ध अर्थ और विद्वता पूर्ण व्याख्या करके सर्व साधारण को हलचल में डालने से पूर्व, यूरोप में संस्कृत के विद्वानों का यह ढंग था कि वे देवता शब्द का अर्थ सदैव “ईश्वर” किया करते थे। वेदों में बहुत सी वस्तुओं को देव या देवता के नाम से विशेषित किया है। इसलिये यह सहज ही में कल्पना कर ली गई कि वेद अनेक ईश्वरों में विश्वास रखने की शिक्षा देते हैं। समस्त संस्कृत साहित्य में अन्य किसी एक शब्द के अनुवाद ने इस सनातन और महानू् धर्म्म के किसी महत्त्वपूर्ण विषय पर इतना भ्रम नहीं फैलाया जितना कि उपर्युक्त शब्द के अनुवाद ने।
देव शब्द दिव प्रकाशने धातु से निकला है अतएव उसका अक्षरार्थ चमकीली या प्रकाश युक्त वस्तु है और इसी कारण उसका गौण व रूढ़ि अर्थ वह वस्तु है जो दिव्य गुण रखती है। इस लिये सूर्य्य, चन्द्र और सृष्टि की अन्य शक्तियाँ अर्थात् अग्नि, वायु आदि के लिये देवता शब्द का प्रयोग किया गया है। हम यजुर्वेद में पढ़ते है: -
अमिनिर्देवता बातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता बसबो देवता रूद्रा
देवतादित्या देवता मरूतो देवता विश्वे देवा बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देबता बरूणो
देबता।
यजु. 4-20
इस विषय में स्वामी दयानन्द सरस्वती के लेखों ने समस्त विचारों की काया पलट दी है। प्रो. मैक्समूलर अपने एक सब से पिछले ग्रन्थ में अर्थात् 08: छा ०क्का ॥
॥2७०॥ ५५? में जिसमें स्वामी दयानन्द के विचारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से झलक रहा है।
स्वीकार करते हैं। “कोष हमें बतलाते हैं कि देव के अर्थ ईश्वर और देवताओं के हैंनिस्सन्देह ऐसा है भी- परन्तु यदि हम वेदों के मन्त्रों में देव शब्द का उल्था सदैव (600) परमेश्वर करें तो वह भाषान्तर न होकर वैदिक कवि के विचारों का रूपान्तर करना होगा। प्रारम्भ में देव के अर्थ “प्रकाशयुक्त' के थे। अतएव वह निरन्तर आकाश, नक्षत्र, सूर्य, उषा, दिन, वसन्त ऋतु, नदी और पृथ्वी के लिया प्रयुक्त होता था और जब
कोई कवि सब वस्तुओं को एक शब्द में जिसे हम सामान्य संज्ञा कहते हैं वर्णन करना चाहता था तो वह उन सब को देव कहता था। ”
वे फिर लिखते हैं- “हमें कभी नहीं भूलना चाहिये कि प्राचीन धार्मिक गाथाओं में जिन्हें हम देवता कहते हैं, वे वास्तविक और जीवित व्यक्ति न थे जिनके विषय में हम कह सकें कि वे ऐसे या वैसे थे। देव जिसका अनुवाद कि हमने ईश्वर किया है केवल गुण वाचक संज्ञा है। वह ऐसे गुणों को प्रकट करता है जो अन्तरिक्ष और पृथ्वी में, सूर्य और नक्षत्रों में उघा और समुद्र में समान हैं अर्थात् प्रकाश। ”
इसलिये हम प्राचीन ऋषियों को केवल इस कारण कि वे ऊपर लिखे भौतिक पदार्तों को देवता के नाम से विशेषित करते हैं बहु ईश्चवववादी अथवा प्रकृतिपूजक नहीं कह सकते। यदि हम ऐसा कहें तो उस मनुष्य को भी ऐसा ही कहना होगा जो सूर्य् और चन्द्रमा को प्रकास युक्त कहता है अथवा प्रकाशयुक्त आकास या चमकती हुई विजय आदि का वर्णन करता है।
यास्कमुनि जिनकी प्रमाणिकता वेद विषय पर सब से अधिक मानी जाती है और जो वैदिक कोष (निघण्टु) और वैदिक निर्वचन शास्त्र (निरूक्त) के सुप्रसिद्ध कर्त्ता हुये हैं। देव शब्द की व्याख्या और भी अधिक विस्तृत अर्थों में करते हैं।
वे देव शब्द की इस प्रकार निरूक्ति करते है:-
देबो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो वा भवति। निरूक्त 7. 5॥
जो हमें किसी प्रकार का लाभ पहुँचाता है, जो वस्तुओं को प्रकाशित कर सकता है या उन पर प्रकाश डाल सकता है और जो प्रकाश का मूल खोत (वा स्थान) है वह “देव? है।
अतएव देव शब्द अनेक और वस्तुओं के लिये प्रयुक्त होता है। हम यहाँ उसके कुछ विशेष अर्थों का उल्लेख करते है:-
(।) वह माता पिता के लिये व्यवह्तत होता है क्योंकि वे हमको असीम लाभ पहुँचाते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद् में माता, पिता, आचार्य देव कहे गये है:-
मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य्य देवो भव तैत्तिरीय उपनि. अनु. ॥
(2) वह विद्वान के लिये भी आता है क्योंकि अनेक आत्मा प्रकाश युक्त होते हैं, और वे अनेक बातों पर प्रकाश डालते हैं। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है
“विद्वां सोहि देवा:”- विद्वान् पुरूष देवता है।
(3) उसका इन्द्रियों के लिये भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उनके द्वारा हमें भौतिक (दृश्यमान) जगत का ज्ञान होता है। उदाहरणार्थ यजुर्वेद में लिखा है।
अनेजदेकं मनसो जबीयो नैनद् देवा आप्नुवन् पूर्व मर्षत्।यजु, अ. 4 मं. 4॥
परमेश्वर एक है वह गतिशील नहीं तथापि उसकी गति मन से भी अधिक है। यद्यपि वह पूर्व से ही इन्द्रियों में है तथापि इन्द्रियाँ (देव) उस तक नहीं पहुँच सकतीं। फिर
मुण्डकोपनिषद् में पढ़ते है: -
न च॒क्षुपा गृह्मते नापि वाता नान्यर्देवस्तपसा कर्मणा वा। ज्ञानप्रसादेन विशुद्ध
सत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमान:॥मुण्डक 2। 8॥परमेश्वर नेत्र या वाणी अथवा अन्य इन्द्रियों (देवों) के द्वारा नहीं जाना जाता और न तप वा कर्मों से प्राप्त होता है। प्रत्युत जो मनुष्य विशुद्ध भाव से उसका ध्यान करता है वह ज्ञान की शान्त ज्योति से उसका दर्शन करता है।
(4) हमारे पाठकों में से बहुत से इस बात को जानते होंगे कि प्रत्येक वैदिक मन्त्र का देवता होता है। यूरोपीय विद्वान् इससे उस देवता विशेष का अर्थ लेते हैं जिसे उस मंत्र में सम्बोधित किया गया है। विविध मन्त्रों के विविध देवता होने के कारण यह कल्पना कर ली गई है कि वैदिक ऋषि बहुत से देवताओं को पूजने और सम्बोधन करने वाले थे परन्तु यह बहुत बड़ी भूल है। यास्कमुनि कहते हैः
अथातो दैवतं तद्यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां
'तद्दैवतमित्याचक्षते। सैषा देवतोपपरीक्षा यत्काम ऋषिर्यस्यां देवतायामर्थ
पत्यमिच्छन् स्तुतिम् प्रयुक्ते तद्ैवत: स मन्त्रो भवति॥। निरूक्त 7। ॥
इसका यह भावार्थ है कि मंत्र के देवता से उस विषय का ग्रहण करना चाहिये जिसकी उसमें व्याख्या की गई है।
(5) देव शब्द परमेश्वर के लिये भी आता है, जो सब वस्तुओं का प्रकाशक, समस्त प्रकाश और ज्ञान का मूल स्रोत और उन सब वस्तुओं का प्रदाता है
जिनका हम संसार में उपभोग करते हैं, परन्तु उसका अर्थ सदैव ईश्वर ही नहीं होता। वस्तुतः जैसा कि प्रोफेसर मोक्षमूलर मानते हैं देव शब्द वस्तु वाचकनहीं प्रत्युत गुणवाचक है। अतएव इसका प्रयोग उन समस्त वस्तुओं के लिए हो सकता है जिसमें उसके निर्वाचित गुण पाये जाते हैं जैसे प्रकाश, लाभ पहुँचाना, चमकाना, अथवा किसी वस्तु पर प्रकास डालना आदि।
अब पाठक गण देख सकेंगे कि यदि पुराने आर्य्य लोग सूर्य, चन्द्र, आकाश, समुद्र, पृथ्वी, अन्तरिक्ष को देवता कहते थे तो इससे यह न समझना चाहिये कि वे उन्हें ईश्वर मानते थे अथवा उनकी पूजा करते थे। ये सब तथा बहुत सी और भी वस्तुएं ईश्वर के समान देवता के अर्थों के अन्तर्गत आ जाती हैं, परन्तु इन सब में से केवल एक ईश्वर ही 'पूजने के योग्य है। यजुर्वेद स्पष्ट रीति से कहता है:-
बेदाहमेतं पुरूष महांतमादित्यवर्ण तमस: परस्तात्| तमेव विदित्वाति मृत्युमेति
नान्य: पन््था विद्यतेब्यनाय॥ यजुर्वेद 3। | 8 ॥
हम उस परमात्मा को जाने जो पूर्ण प्रकाश स्वरूप और अन्धकार से परे है। केवल उसी का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त मुक्ति का दूसरा मार्ग नहीं है।
'शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट और जोरदार शब्दों में बतलाया गया है:-
यो्न्यां देवतामुपासते न स बेद यया पशुरेव सदेवाम॥
शतपथ ब्राह्मण का. 4 अ. 4
जो किसी कूमरे देवता की पूजा करता है वह नहीं जानता , वह विद्वानों के मध्य पशुव॒त् है।
हम यहाँ ऋग्वेद से कुछ मन्त्र उद्धृत करते हैं जिनसे प्रकट होगा कि वेद में कितनी स्पष्ट और युक्त संगत रीति से विशुद्ध और पूर्ण ईश्वर वाद की शिक्षा दी गई है:- हिरण्यगर्भ: समवर्त्तताग्रे भूतस्य जात: पतिरिक आसीत|
स दाधार पृथ्वी द्यामुतेमां कस्मैदेबाय हविषा विधेम।। ॥
य आत्मादा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवा: ।
अस्यच्छायामृतं यस्य मृत्यु: कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 2 ॥
यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूवा
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पद: कस्मै देवाय हविषा विधेम।। 3 ॥
अस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्र रसयां सहाहु: ।
अस्थेमा: प्रदिशो यस्य बाहु कस्मैदेवाय हविषा विधेम ॥ 4॥
येन छौरूग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्व: स्तभितं येन नाक:।
योषन्तरिक्षे रजसो विमान: कस्मैदेवाय हविषा विधेम॥। 5 ॥
य॑ क्रन्दसी अवसातस्पभाने अभ्यैक्षेतां मनसारेजमाने ।
यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥। 6 ॥
आपोह यद् वृहतीविश्वमायन् गर्भ दधाना: जनयन्तीरग्निमा
ततो देबानां समवर्त्ततासुरेक: कस्मैदेवाथ हविषा विधेम।। 7 ॥
यश्विदाषों महिनापर्य पश्यद् दक्षं दधाना: जनयन्तीर्यज्ञमा
यो देवानामधिदेव एक आसीत् कस्मैदेबाय हविषा विधेम॥ 8॥
मानोंहिंसीज्जनिता य: पृथिव्या यो वा दिवम् सत्यधर्माजजान।
यश्वापश्चन्द्रा वृहतीर्जजान कस्मैदेवाय हविषा विधेम॥। 9 ॥प्रजापते न स्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव।
यत्कामास्ते जुहुमस्तननो अस्तु बयं स्थाम पतयोरयीणाम् ॥ 0॥
क्र. वे. मं. 0 सू. 2 मं. -0॥
आरम्भ काल में ईश्वर था जो प्रकाश का मूल है। अखिल विश्व का वही एक स्वामी था। उसी ने पृथ्वी और आकाश को स्थिर कर रक््खा था। वही है जिसकी हमें प्रार्थना करनी चाहिये। जो आत्मिकज्ञान और बल का देने वाला है, संसार जिसकी पूजा करता है,जिसकी आज्ञा का पालन सब विद्वान् लोग करते हैं, जिसकी शरण अमरत्व है, जिसकी छाया मृत्यु है उसी देव की हम उपासना करें। 2।
'जो अपनी महत्ता के कारण इस चराचर जगत् का एक मात्र राजा है, जो दुपाये और चौपाओं का उत्पादक और स्वामी है उसी देव की हम उपासना करें।
हिमवान पर्वत और जल से भरे समुद्र जिसके महत्व की घोषणा करते हैं, ये दिशाएं, जिसकी भुजा हैं उसी देव की हम उपासना करें। जिसने इतने बड़े आकाश को धारण किया हुआ है, और पृथ्वी को अचल कर रक्खा है, जिसके द्वारा स्वर्ग और मोक्ष स्थित हैं जो समस्त अन्तरिक्ष में अपने आत्मबल से व्याप्त हैं, उसी देव की हम उपासना करें। जिसकी ओर पृथ्वी और अन्तरिक्ष देखते हैं क्योंकि वे उसी की रक्षा में स्थित और उसी की इच्छा से परिचालित होते हैं जिसमें सूर्य उदय होता और चमकता है उसी देव की हम उपासना करें।जिस समय इस विस्तृत प्रकृति वा उपादान कारण ने जो अग्नि दशा में था तथा जो विश्व को अपने गर्भ में धारण किये था- अपने आप को प्रकट किया उस समय वही समस्त प्रकाशवान् पदोर्थों (देवों) का जीवन था उसी देव की हम उपासना करें।
जिससे अपनी महत्ता से उस फैले हुये उपादान कारण को जिसमें उष्णता और शक्ति धारण की हुई थी और जिससे यह सृष्टि प्रादुर्भूत हो रही थी , जो समस्त प्रकाश युक्त पदार्थों (देवों) का एक मात्र “अधिदेव” है उसी देव की हम उपासना करें।
जो पृथ्वी का उत्पादक है और जिस सत्य नियम वाले ने आकाश को भी पैदा किया है और जिसने विस्तृत और प्रकाश युक्त उपादान का प्रादुर्भाव किया है, वह हमें दुख न पहुंचावे , उसी देव की हम उपासना करें।
हे विश्व के स्वामी! तेरे अतिरिक्त इन उत्पन्न हुए पदार्थों को वश में रख कर शासित करने वाला कोई दूसरा नहीं है जिन वस्तुओं की कामना में हम तेरी उपासना करते हैं यह हमारी हों और हम संसार के समस्त उत्तम पदार्थों के स्वामी हों।
इन दस मन्त्रों में “एक” शब्द चार बार से कम व्यवह्वत हुआ। यदि पाठक गण ईश्वर के अद्वितीय होने में इससे अधिक स्पष्ट, असंदिग्ध, सुन्दर और प्रौढ़ वर्णन की खोज करे धर्म ग्रन्थों में करेंगे तो खोज निष्फल होगी।
जब कभी वेदों या उपनिषदों के एक या दो वाक्य जिन में ईश्वर एकत्व का वर्णन होता है, पाश्चात्य विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं तो वे झट कह उठते हैं कि ये
*अद्वैतवाद' की शिक्षा देतें हैं, एक ईश्वरवाद की नहीं और इनका अर्थ यह है कि केवल एक ईश्वर है दूसरी कोई वस्तु नहीं , यह नहीं है कि परमेश्वर एक है दूसरा परमेश्वर नहीं अर्थात् ऐसे वाक्यों का अभिप्राय अद्वैतवाद एक है। परक ईश्वरवाद परक नहीं। हमें खेद है कि ग्रन्थ के प्रकृत विषय से हम अधिक दूर नहीं जा सकते। हम इस बात का निर्णय पाठकों के ऊपर छोड़ते हैं कि इन मन्त्रों को जिनमें परमेश्वर को विश्व का विधाता और स्थिर रखने वाला, समस्त विश्व का एक मात्र राजा स्वर्ग को व्यवस्थित रखने वाला, अमरत्व का प्रदान करने वाला और हमारी पूजा के योग्य वर्णन किया गया है। किसी प्रकार भी अद्वैतवाद की शिक्षा देने वाला समझा जा सकता है? अब हम अथर्ववेद के कुछेक मन्त्रों को प्रो. मैक्समुलर के भाष्य सहित नीचे उद्धृत करते है:
बृहन्नेषामधिष्ठाता अन्तिकादिव पश्यति।
अस्तायन् मन्यते चरन् सर्व देवा डे बिदु :॥ । ॥
यस्तिष्ठति चरति यश्व बज्चति योनिलायम् चरति य: प्रतडकम]
द्वौ संनिषद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्वेद बरूणस्तृतीय: ॥ 2 ॥
उतेय॑ भूमिर्वरूणस्य राज्ञ उतासौ झौर्वृहती दूरे अन्ता।
उतो समुद्रो वरूणस्य कुक्षी उत्तास्मन्नल्प उदके निलीन:॥ 3 ॥
उत यो द्यामतिसर्पति परस्तान्न समुच्यातै वरूणस्य राज्ञ:।
दिवस्पर्श: प्रचरन्ति दमस्य सहस्राक्षा अति पश्यन्ति भूमिम्॥ 4॥
सर्व तद्राजा बरूणो विचष्ट यदन्तरा रोदसी यत् परस्तात]
संख्याता अस्य निमिषो जनाना मक्षानिवस्वनध्नी निमिनोति तानि॥ 5 ॥
येते पाशा वरूण सप्त सप्त त्रेधा तिष्ठन्ति विपितारू शन्त:।
छिनन्तु सर्वे अनृतम् बदन्त: य: सत्य बाद्यति त॑ सृजन्तु ॥ 6 ॥
अथर्व, का. 4 सू. 6॥
इन सब का अधिष्ठाता वरूण ऐसे देख रहा है, मानो वह समीप है, यदि कोई मनुष्य खड़ा होता है, चलता है, छिपता है, या लेटने को जाता है, वा उठता है या दो मनुष्यपरस्पर कानाफूसी या मन्त्रणा करते हैं तो राजा वरूण उसे जानता है, वह तीसरा वहाँ उपस्थित है। -2
यह पृथ्वी तथा विस्तृत आकाश जिसके सिरे बहुत दू हैं राजा वरूण के अधिकार में है। दोनों समुद्र (आकाश और समुद्र) वरूण की कुक्षी हैं और वह पानी के इन छोटे से बिन्दू में भी व्याप्त है।
यदि कोई पुरूण आकाश से भी बहुत परे भाग जाय तो भी वह राजा वरूण से नहीं बच सकता। 3।
उस के गुप्तचर आकाश से संसार की ओर आते हैं और सहसोो नेत्रों से इस पृथ्वी पर दृष्टिपात करते हैं। 4।
राजा वरूण उन सब को देखता है जो आकास और पृथिवी के मध्य में है। आकाश इनसे भी परे है। उसने मनुष्यों के नेत्रों के पलक मारने की भी गणना कर ली है। खिलाड़ी के पांसा फैंकने के समान उसने समस्त वस्तुओं को अखण्ड रूप से स्थित कर रखा है। 5।
हे वरूण! तेरे भयानक पाश जो सात सात और तीन-तीन करके फैले हुए हैं मिथ्यावादियों को फांस लें और सत्य बोलने वालों को छोड़ देते हैं। 6 ॥
अब यह स्पष्ट हो गया कि वेद विशुद्द और पूर्ण एक ईश्वर्वाद की शिक्षा देते हैं जो अद्वैतवाद के सिद्धान्त से उतनी ही भिन्न है जितनी वह ईश्वर के मानने वाले ढूसरे धर्मों
(विशेषत: सैमीटिक $०॥४8० अर्थात् यहूदी, ईसाई और मुहम्मदी मतों) के ईश्वरवाद से।