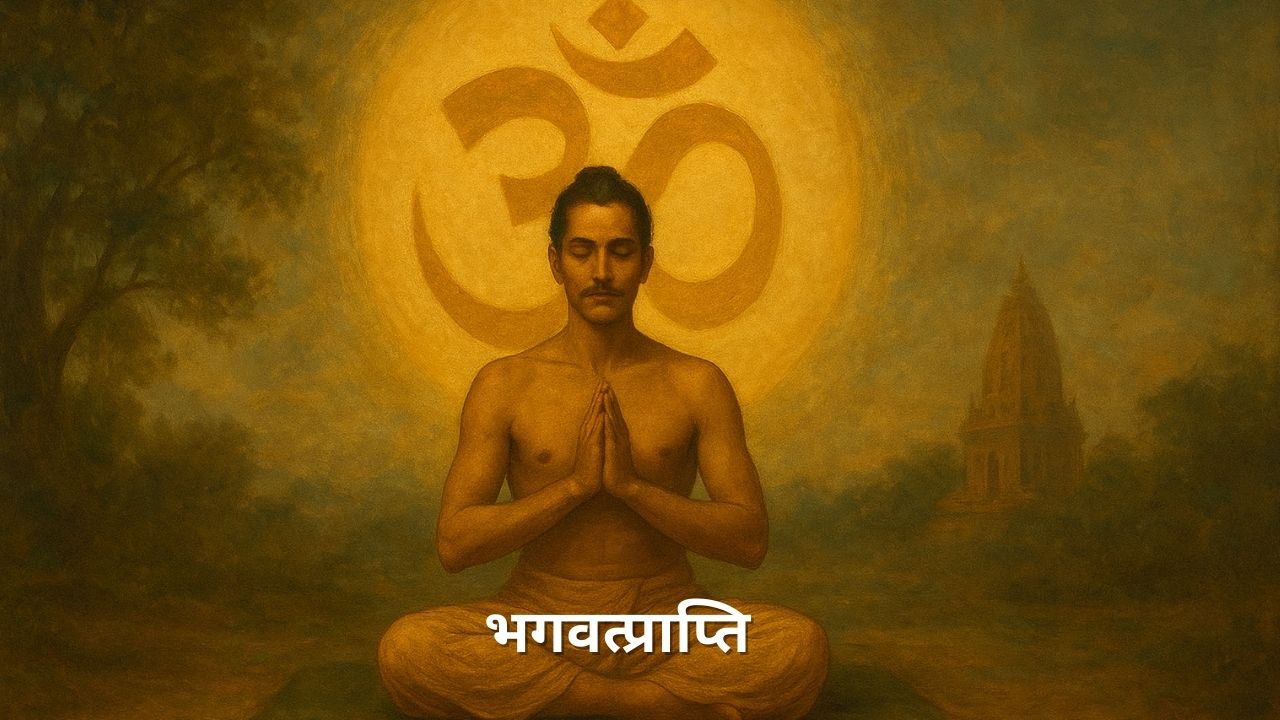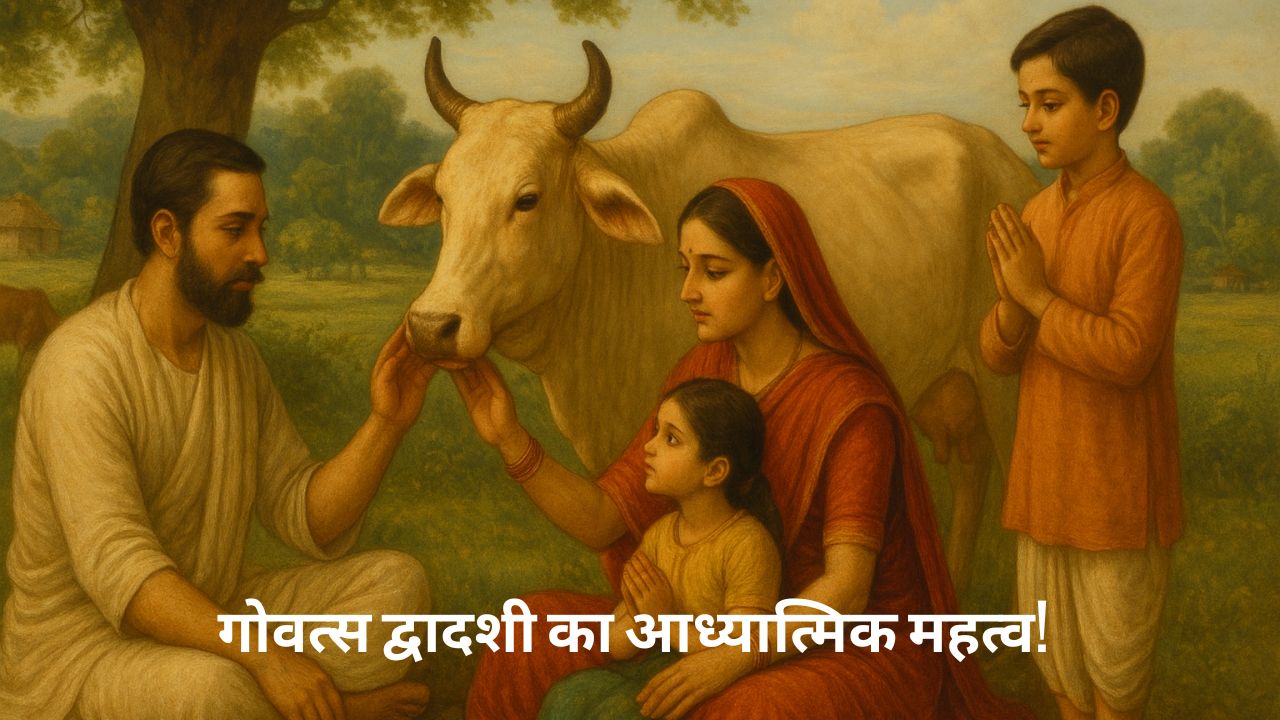- धर्म-पथ
- |
- 31 October 2024
- |
- 0 Comments
 डा. दीनदयाल मणि त्रिपाठी
“यजुस” के नाम पर ही वेद का नाम यजुस+वेद(=यजुर्वेद) शब्दों की संधि से बना है।
“यजुस्” का अर्थ समर्पण से होता है । इसका मुख्य अर्थ हैः-
(1.) “यजुर्यजतेः ” (निरुक्तः-7.12) अर्थात् यज्ञ से सम्बद्ध मन्त्रों को “यजुष्” कहते हैं ।
(2.) “इज्यतेनेनेति यजुः ।” अर्थात् जिन मन्त्रों से यज्ञ किया जाता है, उन्हें यजुष् कहते हैं । पदार्थ (जैसे ईंधन, घी, आदि), कर्म (सेवा, तर्पण ),योग, इंद्रिय निग्रह इत्यादि के हवन को यजन यानि समर्पण की क्रिया कहा गया है ।
यजुर्वेद का यज्ञ के कर्मकाण्ड से साक्षात् सम्बन्ध है, अतः इसे “अध्वर्युवेद” भी कहा जाता है । यज्ञ में अध्वर्यु नामक ऋत्विज् यजुर्वेद का प्रतिनिधित्व करता है और वही यज्ञ का नेतृत्व करता है । इसीलिए सायण ने कहा है कि वह यज्ञ के स्वरूप का निष्पादक है ।
(3.) अनियताक्षरावसानो यजुः । अर्थात् जिन मन्त्रों में पद्यों के तुल्य अक्षर-संख्या निर्धारित नहीं होती है, वे यजुष् हैं ।
(4.) शेषे यजुःशब्दः । (पूर्वमीमांसा—2.1.37) अर्थात् पद्यबन्ध और गीति से रहित मन्त्रात्मक रचना को यजुष् कहते हैं । इसका अभिप्राय यह है कि सभी गद्यात्मक मन्त्र-रचना यजुः की कोटि में आती है ।
(5.) एकप्रयोजनं साकांक्षं पदजातमेकं यजुः । अर्थात् एक उद्देश्य से कहे हुए साकांक्ष एक पज-समूह को एक यजुः कहेंगे । इसका अभिप्राय यह है कि एक सार्थक वाक्य को यजुः की एक इकाई माना जाता है ।
मुख्यवेद-यजुर्वेद
तैत्तिरीय-संहिता के भाष्य की भूमिका में सायण ने यजुर्वेद का महत्त्व बताते हुए कहा है कि यजुर्वेद भित्ति (दीवार) है और अन्य ऋग्वेद एवं सामवेद चित्र है । इसलिए यजुर्वेद सबसे मुख्य है । यज्ञ को आधार बनाकर ही ऋचाओं का पाठ और सामगान होता है ।
“भित्तिस्थानीयो यजुर्वेदः, चित्रस्थानावितरौ । तस्मात् कर्मसु यजुर्वेदस्यैव प्राधान्यम् ।” (तै.सं. भू.)
यजुर्वेद का दार्शनिक रूपः-
ब्राह्मण-ग्रन्थों में यजुर्वेद का दार्शनिक रूप प्रस्तुत किया गया है । यजुर्वेद विष्णु का स्वरूप है,
अर्थात् इसमें विष्णु (परमात्मा) के स्वरूप का वर्णन है ।
“यजूंषि विष्णुः।” शतपथ-ब्राह्मण—4.6.7.3) )
यजुर्वेद प्राणतत्त्व और मनस्तत्त्व का वर्णन करता है , अतः वह प्राण है, मन हैः—“प्राणो वै यजुः।” (शतपथ-ब्राह्मण–14.8.14.2) । “मनो यजुः।” (शतपथ-ब्राह्मण—14.4.3.12)
यजुर्वेद में वायु और अन्तरिक्ष का वर्णन है, अतः वह अन्तरिक्ष का प्रतिनिधि है ।
“अन्तरिक्षलोको यजुर्वेदः ।” (षड्विंश-ब्राह्मण–1.5 )
यजुर्वेद तेजस्विता का उपदेश देता है ,
अतः वह महः (तेज) है । “यजुर्वेदः एव महः ।” (गोपथ-ब्राह्मण–5.15) ।
यजुर्वेद क्षात्रधर्म और कर्मठता की शिक्षा देता है. अतः वह क्षत्रियों का वेद है ।
“यजुर्वेदं क्षत्रियस्याहुर्योनिम् ।” (तैत्तिरीय-ब्राह्मण–3.12.9.2) इस वेद में अधिकांशतः यज्ञों और हवनों के नियम और विधान हैं, अतःयह ग्रन्थ कर्मकाण्ड प्रधान है।
यजुर्वेद की संहिताएं लगभग अंतिम रची गई संहिताएं थीं, जो ईसा पूर्व द्वितीय सहस्राब्दि से प्रथम सहस्राब्दी के आरंभिक सदियों में लिखी गईं थी। इस ग्रन्थ से आर्यों के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है।
यजुर्वेद संहिता में वैदिक काल के धर्म के कर्मकाण्ड आयोजन हेतु यज्ञ करने के लिये मंत्रों का संग्रह है।
इनमे कर्मकाण्ड के कई यज्ञों का विवरण हैः-
अग्निहोत्र अश्वमेध वाजपेय सोमयज्ञ राजसूय अग्निचयन ऋग्वेद के लगभग ६६३ मंत्र यथावत् यजुर्वेद में मिलते हैं। यजुर्वेद वेद का एक ऐसा प्रभाग है, जो आज भी जन-जीवन में अपना स्थान किसी न किसी रूप में बनाये हुऐ है संस्कारों एवं यज्ञीय कर्मकाण्डों के अधिकांश मन्त्र यजुर्वेद के ही हैं।
डा. दीनदयाल मणि त्रिपाठी
“यजुस” के नाम पर ही वेद का नाम यजुस+वेद(=यजुर्वेद) शब्दों की संधि से बना है।
“यजुस्” का अर्थ समर्पण से होता है । इसका मुख्य अर्थ हैः-
(1.) “यजुर्यजतेः ” (निरुक्तः-7.12) अर्थात् यज्ञ से सम्बद्ध मन्त्रों को “यजुष्” कहते हैं ।
(2.) “इज्यतेनेनेति यजुः ।” अर्थात् जिन मन्त्रों से यज्ञ किया जाता है, उन्हें यजुष् कहते हैं । पदार्थ (जैसे ईंधन, घी, आदि), कर्म (सेवा, तर्पण ),योग, इंद्रिय निग्रह इत्यादि के हवन को यजन यानि समर्पण की क्रिया कहा गया है ।
यजुर्वेद का यज्ञ के कर्मकाण्ड से साक्षात् सम्बन्ध है, अतः इसे “अध्वर्युवेद” भी कहा जाता है । यज्ञ में अध्वर्यु नामक ऋत्विज् यजुर्वेद का प्रतिनिधित्व करता है और वही यज्ञ का नेतृत्व करता है । इसीलिए सायण ने कहा है कि वह यज्ञ के स्वरूप का निष्पादक है ।
(3.) अनियताक्षरावसानो यजुः । अर्थात् जिन मन्त्रों में पद्यों के तुल्य अक्षर-संख्या निर्धारित नहीं होती है, वे यजुष् हैं ।
(4.) शेषे यजुःशब्दः । (पूर्वमीमांसा—2.1.37) अर्थात् पद्यबन्ध और गीति से रहित मन्त्रात्मक रचना को यजुष् कहते हैं । इसका अभिप्राय यह है कि सभी गद्यात्मक मन्त्र-रचना यजुः की कोटि में आती है ।
(5.) एकप्रयोजनं साकांक्षं पदजातमेकं यजुः । अर्थात् एक उद्देश्य से कहे हुए साकांक्ष एक पज-समूह को एक यजुः कहेंगे । इसका अभिप्राय यह है कि एक सार्थक वाक्य को यजुः की एक इकाई माना जाता है ।
मुख्यवेद-यजुर्वेद
तैत्तिरीय-संहिता के भाष्य की भूमिका में सायण ने यजुर्वेद का महत्त्व बताते हुए कहा है कि यजुर्वेद भित्ति (दीवार) है और अन्य ऋग्वेद एवं सामवेद चित्र है । इसलिए यजुर्वेद सबसे मुख्य है । यज्ञ को आधार बनाकर ही ऋचाओं का पाठ और सामगान होता है ।
“भित्तिस्थानीयो यजुर्वेदः, चित्रस्थानावितरौ । तस्मात् कर्मसु यजुर्वेदस्यैव प्राधान्यम् ।” (तै.सं. भू.)
यजुर्वेद का दार्शनिक रूपः-
ब्राह्मण-ग्रन्थों में यजुर्वेद का दार्शनिक रूप प्रस्तुत किया गया है । यजुर्वेद विष्णु का स्वरूप है,
अर्थात् इसमें विष्णु (परमात्मा) के स्वरूप का वर्णन है ।
“यजूंषि विष्णुः।” शतपथ-ब्राह्मण—4.6.7.3) )
यजुर्वेद प्राणतत्त्व और मनस्तत्त्व का वर्णन करता है , अतः वह प्राण है, मन हैः—“प्राणो वै यजुः।” (शतपथ-ब्राह्मण–14.8.14.2) । “मनो यजुः।” (शतपथ-ब्राह्मण—14.4.3.12)
यजुर्वेद में वायु और अन्तरिक्ष का वर्णन है, अतः वह अन्तरिक्ष का प्रतिनिधि है ।
“अन्तरिक्षलोको यजुर्वेदः ।” (षड्विंश-ब्राह्मण–1.5 )
यजुर्वेद तेजस्विता का उपदेश देता है ,
अतः वह महः (तेज) है । “यजुर्वेदः एव महः ।” (गोपथ-ब्राह्मण–5.15) ।
यजुर्वेद क्षात्रधर्म और कर्मठता की शिक्षा देता है. अतः वह क्षत्रियों का वेद है ।
“यजुर्वेदं क्षत्रियस्याहुर्योनिम् ।” (तैत्तिरीय-ब्राह्मण–3.12.9.2) इस वेद में अधिकांशतः यज्ञों और हवनों के नियम और विधान हैं, अतःयह ग्रन्थ कर्मकाण्ड प्रधान है।
यजुर्वेद की संहिताएं लगभग अंतिम रची गई संहिताएं थीं, जो ईसा पूर्व द्वितीय सहस्राब्दि से प्रथम सहस्राब्दी के आरंभिक सदियों में लिखी गईं थी। इस ग्रन्थ से आर्यों के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है।
यजुर्वेद संहिता में वैदिक काल के धर्म के कर्मकाण्ड आयोजन हेतु यज्ञ करने के लिये मंत्रों का संग्रह है।
इनमे कर्मकाण्ड के कई यज्ञों का विवरण हैः-
अग्निहोत्र अश्वमेध वाजपेय सोमयज्ञ राजसूय अग्निचयन ऋग्वेद के लगभग ६६३ मंत्र यथावत् यजुर्वेद में मिलते हैं। यजुर्वेद वेद का एक ऐसा प्रभाग है, जो आज भी जन-जीवन में अपना स्थान किसी न किसी रूप में बनाये हुऐ है संस्कारों एवं यज्ञीय कर्मकाण्डों के अधिकांश मन्त्र यजुर्वेद के ही हैं।
Related Posts
0 Comments
Comments are not available.