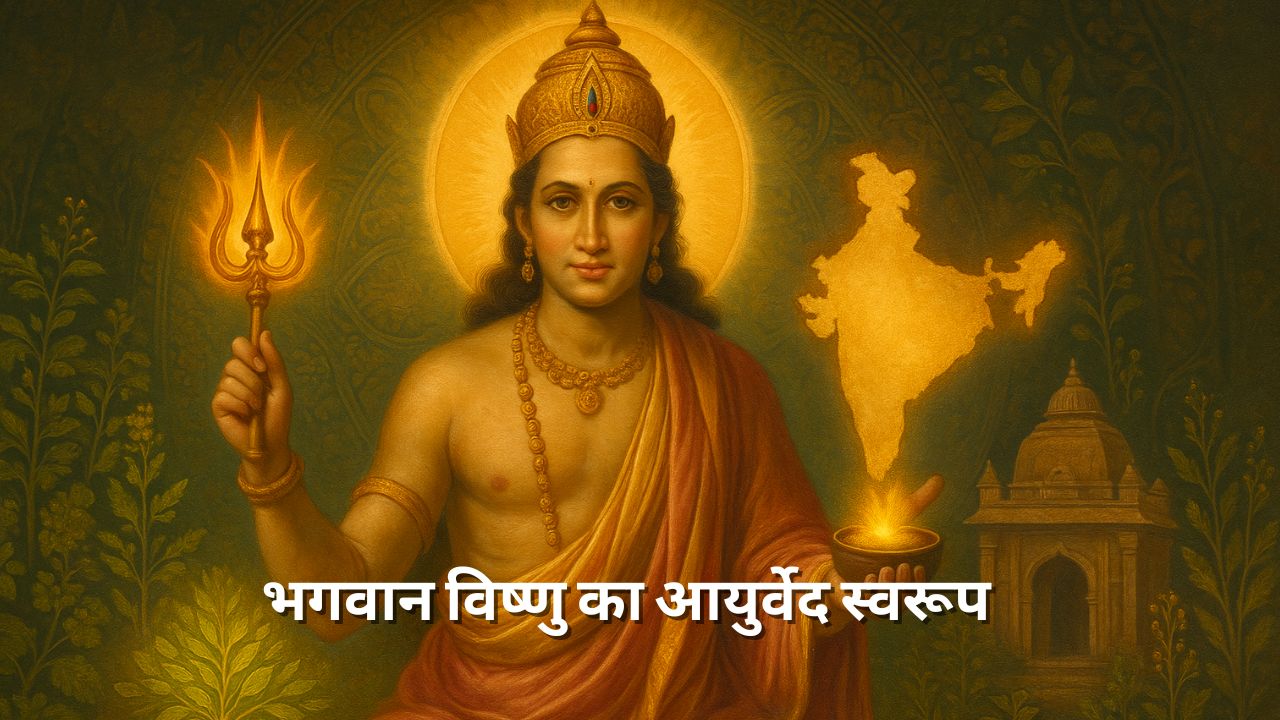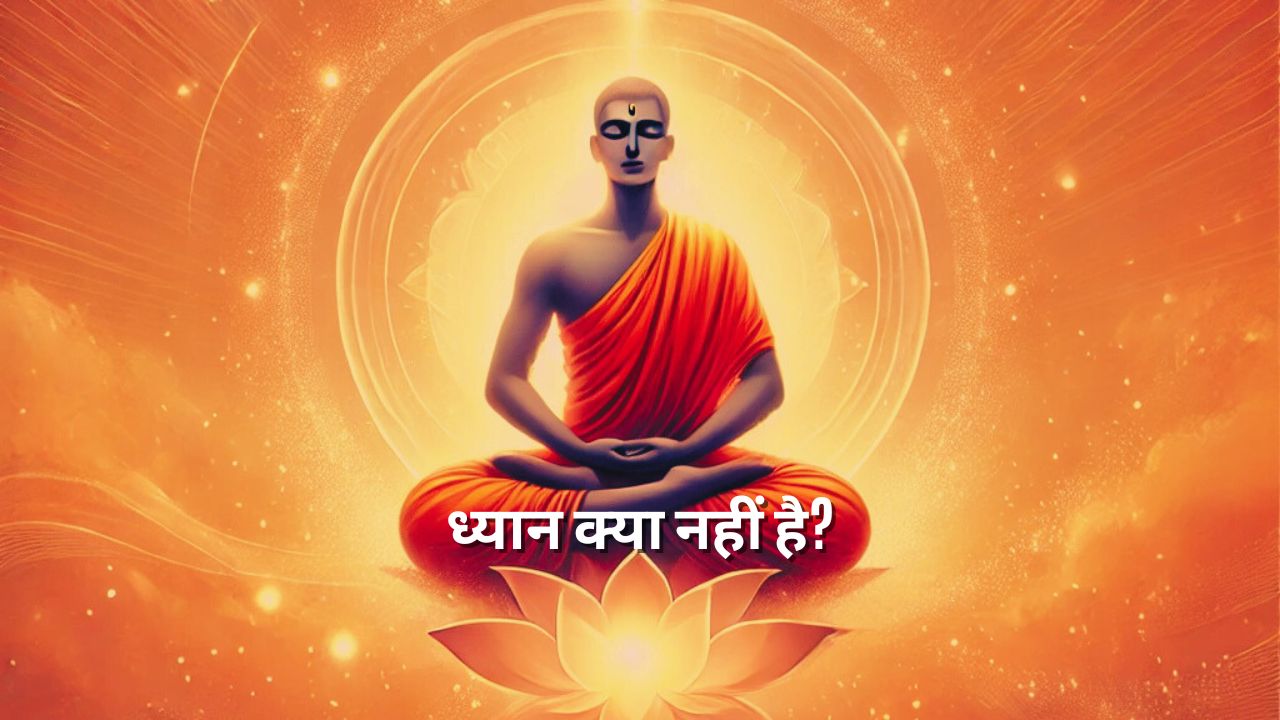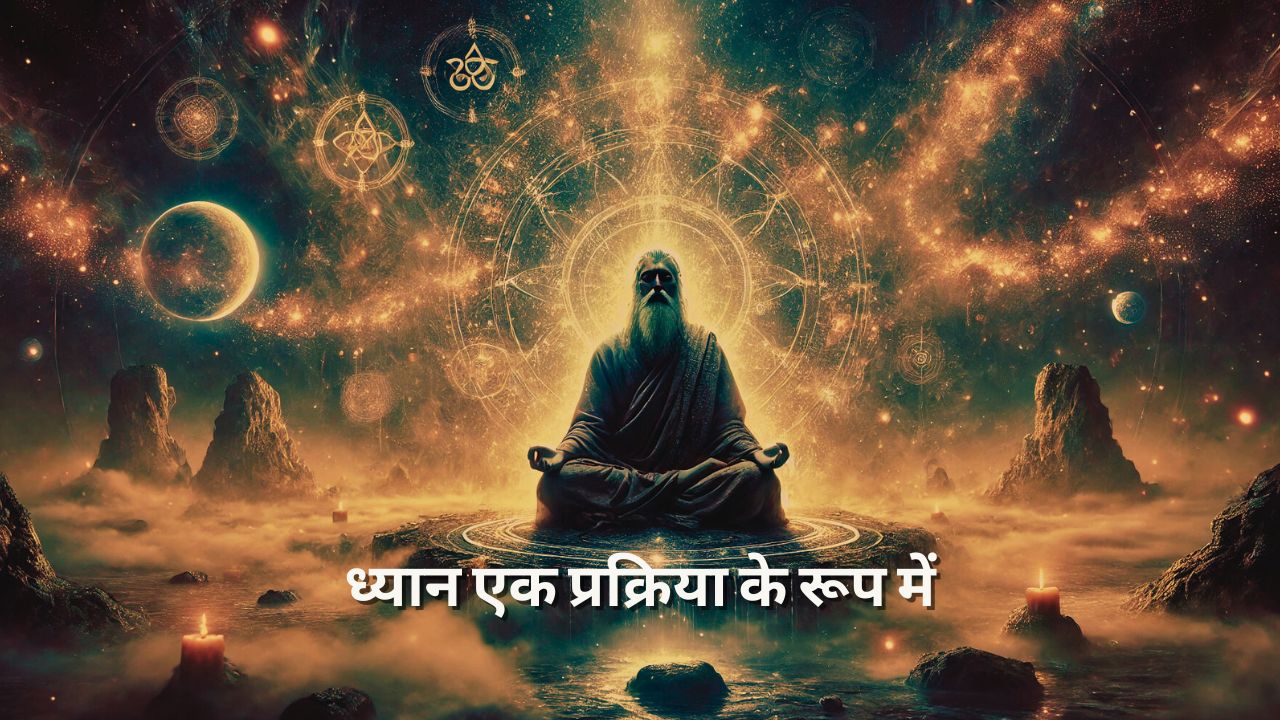- आयुष
- |
- 26 May 2025
- |
- 0 Comments
प्रत्येक ईश्वरवादी ईश्वर को सत् मानता है अर्थात् ईश्वर का अस्तित्व उसके लिये सदा बना रहता है। प्राणियों की तरह ईश्वर मरा नहीं करता। इसी तरह ईश्वर को वह 'प्रेमानन्द' रूप मानता है, अर्थात् प्राणियों की तरह ईश्वर में सुख-दुःख नहीं होता। इसी तरह ईश्वर को चित्स्वरूप भी माना जाता है। चित्का अर्थ होता है ज्ञान अर्थात् ईश्वर पूर्ण ज्ञानमय होता है। ईश्वर नित्य ज्ञान रूप होता है। इसमें कभी अज्ञता नहीं होती। इसी ज्ञान को वेद कहा जाता है। ज्ञान में सदा शब्द का अनुवेध रहता है। अतः वेद के शब्द, अर्थ और सम्बन्ध - ये तीनों ही नित्य होते हैं।
शंकराचार्यजी ने लिखा है-
'नियतरचनावतो विद्यमानस्यैव वेद' (बृहदा० उप० शा०भा० २।४।१०)।
इस तरह वेद ईश्वरके स्वरूप भूत हो गया। अतः भगवान् विष्णु को हम वेद-स्वरूप कहते हैं। यहाँ विष्णु को आयुर्वेद-स्वरूप कहा गया है, वह इसलिये कि आयुर्वेद वेद का ही उपाङ्ग है। इसी से आयुर्वेद की महत्ता प्रकट हो जाती है, अर्थात् आयुर्वेद भगवान् श्री विष्णु का रूप ही है।
ऊपर भगवान् विष्णु को हम सत्, चित् और आनन्द कह आये हैं, अर्थात् सत्-चित्-आनन्द ही व भगवान् होता है। आनन्द का ही उल्लसित रूप होता है -प्रेम। इसलिये वेद ने भगवान् विष्णु को प्रेमानन्द-रूप कहा है। प्रेम का स्वभाव होता है कि वह अपने प्रेमास्पद के साथ कोई-न-कोई खेल खेलता ही रहता है। अतः भगवान् यह खेल हम प्रेमास्पदों के साथ खेलते ही रहते हैं। जाग्रत्-अवस्था और स्वप्रावस्था में हम भगवान् के साथ प्रेम का खेल खेलते हुए थक जाते हैं, तब वह महान् चिकित्सक हमें संज्ञा-हरण का इंजेक्शन दे देता है और सुषुप्ति-अवस्था में पहुँचा देता है। इस अवस्था में न तो हमें प्राकृतिक सुख की प्रतीति होती है और न प्राकृतिक दुःख का थपेड़ा ही सहना पड़ता है। भगवान् अपने आनन्दरूप में हमको लीन कर देते हैं। इनके आनन्दांश को पाकर हम चिर प्रफुल्लित हो उठते हैं और अच्छी तरह संज्ञा के लौट आने पर अनुभव करते हैं कि मैं सुखपूर्वक सोया- ‘सुखमहमस्वाप्सम् ।’
लीलाओं में प्रेमलीला सबसे उत्तम होती है। सच पूछिये तो हमारे साथ प्रेम की लीला करने के लिये ही भगवान् लीलास्थली बनाते हैं। हमें नाम और रूप देकर हमारे साथ प्रेम की ही लीला करते हैं। किंतु हममें से कुछ लोग भटक कर भगवान् के साथ प्रेम न करके उनकी बहिरङ्गासक्ति के फेर में पड़कर भगवान्को ठुकराकर किसी और से प्रेम करने लगते हैं। जैसे शिशुपाल और कंस भी हमारी तरह भगवान् के अंश थे। परंतु वे भगवान्से प्रेम न कर प्रकृति से प्रेम और भगवान्से ईर्ष्या-द्वेष करने लगे। यह भगवान्के हम प्रेमास्पदों की गलती है; किंतु भगवान् इतने दयालु और प्रेमातुर हैं कि वे कंस और शिशुपाल के भी स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर के साथ भी अपनी ओर से प्रेमलीला करते ही रहते हैं और फिर ऐसे प्रतिकूल लोगों को भी संज्ञा-हरण की सुई लगाकर उन्हें दुःख आदि के थपेड़ों से हुई थकान को मिटाने के लिये सुषुप्ति अवस्था में अपने में लीन कर लेते हैं।
यह स्मरण रखना चाहिये कि प्रत्येक दिन चिकित्सक की तरह प्रत्येक प्राणी को संज्ञा-हरण की सुई उसके अङ्गमें चुभोते नहीं हैं; क्योंकि वे चिकित्सकों के भी चिकित्सक हैं-आयुर्वेद के स्वरूप हैं, इसलिये संज्ञा-हरण की स्वयंचालित (Automatic) व्यवस्था करते हैं।
हम जीवों में सब लोग आण्डाल, मीरा और चैतन्य महाप्रभु की तरह न तो भगवान्से मधुर लीला कर पाते हैं और न दशरथ कौसल्या एवं यशोदा की तरह वात्सल्य-प्रेम ही। अपितु माया के चक्कर में पड़कर उनके विरुद्ध ही लीला करने लग जाते हैं। इस तरह जब हम प्रकृति के थपेड़ों से अच्छी तरह प्रताड़ित हो जाते हैं और मारे थकान के निढाल हो जाते हैं, तब वे आयुर्वेद-स्वरूप भगवान् संज्ञा-हरण की वह प्रभावक सुई लगा देते हैं, जिससे हम अरबों वर्षों तक उनमें लीन होकर आनन्द भोगी बने रहते हैं। इसी संज्ञा-हरण की सुई लगने से उत्पन्न होने वाली अवस्था को महाप्रलय कहा जाता है। अर्थात् इस अवस्था में हम, बहुत दिनों तक भगवान्में अच्छी तरह से लीन रहते हैं और लीन रहकर उनके आनन्दोश से भरपूर हो जाते हैं। किंतु यह महा संज्ञा-हरण की क्रिया उनकी स्वयंचालित (Automatic) ही होती है। यही तो भगवान् के चिकित्सक रूप की विशेषता है।
जब भगवान् देखते हैं कि हमारे प्रेमास्पदों में प्रकृति के थपेड़ों का असर समाप्त हो गया है और मेरा आनन्दांश इनमें भर गया है तो उनका मन फिर प्रेमका खेल खेलने के लिये मचल उठता है; क्योंकि प्रेम का स्वभाव ही होता है कि वह अपने प्रेमास्पद के साथ कोई-न-कोई खेल खेला करे। अकेले उनका मन लग नहीं रहा था, इसलिये 'नारमतैकः' (मैत्रा० उप०२।६।८ प्रेमका स्वभाव ही होता है कि वह प्रेमास्पदों को अपनी आँखों से देखे, उसका स्पर्श पाये। इसलिये भगवान् अपने प्रेमास्पदों को चाहने लगे 'स आत्मानमभिध्यायत्' (मैत्रा०ठप० २।६)।इस खेल के लिये प्रेमास्पदों को लिङ्गशरीर और कारण शरीर भी देना था और लीला के लिये लीलास्थली भी बनानी थी।
भगवान्ने पाद-विभूति में लीला की आयोजिका प्रकृतिपर एक दृष्टि डाली। दृष्टि पड़ते ही प्रकृति में गति आ गयी और वह महत्-तत्त्व से प्रारम्भकर पञ्चमहाभूत तक तेईस तत्त्वोंके रूप में परिणत होती चली गयी। इस तरह चौबीस तत्त्व बन तो गये, किंतु ये चौबीस तत्त्व लीलास्थली (ब्रह्माण्ड) को न बना सकें; क्योंकि ये सब-के-सब जड़ हैं और जड़ गणित नहीं कर सकता। तब महान् गणितज्ञ ने पञ्चीकरण की पद्धति से सब तत्त्वोंको परस्पर मिला दिया और एक अण्डके रूप में गोल लीलास्थली बन गयी। एक हजार दिव्य वर्षतक यह लीलास्थली (ब्रह्माण्ड) गतिहीन ही पड़ी रही, तब भगवान्ने इसमें प्रवेशकर इसे सजीव कर दिया। फिर स्वयं इसे फोड़कर विराट् पुरुषके रूपमें ब्रह्माण्डके बाहर आये। पुरुषसूक्त में इन्हीं पुरुष का वर्णन है। इनके अनन्त चरण, मुख, नेत्र तथा नाभि आदि हैं (श्रीमद्भा० २।६।४१)। इस स्फोट के कारण वे इन्हीं अनन्त नाभियोंसे अनन्त क्षुद्र ब्रह्माण्ड (लीलास्थली) बने। यही क्षुद्र ब्रह्माण्ड उनकी नाभियों से निकले कमल हैं (श्रीमद्भा० २।८।८)।
उस कमलरूपी क्षुद्र ब्रह्माण्ड की कर्णिका पर पितामह ब्रह्माजी अपने को अकेले बैठे हुए पाते हैं। इन ब्रह्मा को भगवान् इसलिये उत्पन्न करते हैं कि ये देवता, असुर, उद्भिज्ज, अण्डज और पिण्डज प्राणियों का निर्माण करके ब्रह्माण्ड को सजा सकें। उत्पन्न होने के साथ ही पितामह ब्रह्मा में सृष्टि करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तब भगवान् उनसे तपस्या कराते हैं फिर दर्शन देकर समझाते हैं कि इन सबका निर्माण वेद के शब्दों से होगा और उस वेद को तुम तपस्या करके ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिये फिर तपस्या करो। पितामह ब्रह्मा ने घोर तप प्रारम्भ कर दिया। जब तपस्या पूर्णता पर पहुँचने लगी, तब उनको पहले पुराण याद आ गये। पुराण नित्य-वेद के नित्य-अंश हैं। अतः आयुर्वेद भी याद आ गया। इस पुराण को पितामह ब्रह्मा ने एक लाख श्लोकों में ग्रथित किया, उसी तरह आयुर्वेद को भी एक लाख श्लोकों में ग्रधित कर लिया।
आयुर्वेद और पुराण-ये दोनों शाश्वत वेद के अर्थ हैं, अतः दोनों ही शाश्वत हैं।
इसी अभिप्राय से चरकने कहां है-'ब्रह्मणा हि यथाप्रोक्तमायुर्वेदं प्रजापतिः' इस तरह ब्रह्माद्वारा स्मरण (उच्चारण) करनेके बाद उनके शब्दोंमें ग्रथित ग्रन्थ जो पुराण और आयुर्वेद हैं-सव-के सब ब्रह्माद्वारा श्रुत हैं, स्मृत नहीं। ब्रह्मा से ही हमें दोनों एक-एक लाख श्लोक वाले ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं और ब्रह्मा के द्वारा ही हमें वेद प्राप्त हुआ है।
फिर भी दोनों में भेद इसलिये है कि स्मृत ग्रन्थ के शब्द नित्य नहीं हैं; क्योंकि ब्रह्माद्वारा निर्मित नहीं हैं, अतः अपौरुषेय हैं और वेदमें ब्रह्माका किसी प्रकारका कृतित्व नहीं है, न वेदका उच्चारण उनका कृत है, न अर्थ-कृत है, न शब्द-कृत है। इस प्रकार वेद ब्रह्मरूप ठहरता है और वेदाङ्ग आयुर्वेद भी भगवान् श्रीविष्णुका स्वरूप ही है।
दौर्भाग्यसे पाश्चात्त्य विद्वानोंके मस्तिष्कमें वेदकी इस अपौरुषेयताका तथ्य उतर नहीं पाया। एक साधारण दृष्टान्तसे हम इस तथ्यको बुद्धिमें उतार सकते हैं। जैसे किसी श्रुतधर व्यक्तिने रेडियो सुना। उससे किसी गानेका प्रसारण हो रहा था।
श्रुतधर व्यक्तिने उस गाने के शब्द और अर्थ के साथ-साथ उसके उच्चारण को भी व याद कर लिया और गा-गाकर सुनाने लगा। यहाँ विचारणीय यह है कि श्रुतधर जिस ध्वनि को सुना रहा है, वह उसके द्वारा निर्मित है क्या? इसी प्रकार उस गाने के शब्दों को जो सुना रहा है, वे शब्द उसके द्वारा 'निर्मित हैं क्या? तथा उस गाने के जो अर्थ हैं, वे भी उसके द्वारा निर्मित हैं क्या? इस प्रश्न के उत्तर में सभी लीग एकमत से कहेंगे कि उस सुने हुए गाने में उस श्रुतधर व्यक्ति का कोई कृतित्व नहीं है; क्योंकि गाने के शब्द-अर्थ आदि सभी वस्तुओं को रेडियो से सुनकर वह सुना रहा है, इसमें उसका कोई कृतित्व नहीं है। इसी तरह इस श्रुतधर की भाँति ब्रह्मा ने अपने मुख से उच्चरित शब्दों को सुना। अर्थ और उच्चारण भी सुनकर ही उन्होंने विश्व को वेद प्रदान किया। इसलिये श्रुतधर व्यक्ति की तरह ब्रह्माका भी वेद के शब्दउच्चारण में कोई कृतित्व नहीं है। ईश्वर नित्य है और उसका स्वरूपभूत वेद भी नित्य है, वह सदा उच्चरित हो ही रहा है। भले ही हमारे कान उसे न सुन सकते हों। ब्रह्माने बहुत तपस्या करनेके बाद उसे सुना। बहुतसे ऋषियोंने तपस्या करके ब्रह्माकी तरह वेदको में सुना है। इस तरह वेद शाश्वत है और ईश्वरका स्वरूप र है। वेद आयुर्वेद है, इसलिये आयुर्वेद भी शाश्वत है। इसीलिये आचार्य चरकने ईश्वरकी तरह अपौरुषेय होनेके कारण आयुर्वेदको शाश्वत कहा है-
सोऽयमायुर्वेदः शाश्वतो निर्दिश्यते, अनादित्वात्, का स्वभावसंसिद्धलक्षणत्वात्, भावस्वभावनित्यत्वाच्च ।
(चरक० सूत्र० ३०।२७)
पाश्चात्त्य विपश्चितों ने वेदों में श्रम किया है, किंतु वे वेद के अपौरुषेय-स्वरूप को समझ नहीं सके। इसीलिये जब आयुर्वेद को शाश्वत कहा जाता है तो शाश्वत शब्द और नित्य शब्द में अन्तर समझने लगते हैं और समझते हैं कि मनुष्य में जब बुद्धि का विकास हुआ से तब आयुर्वेद बना। सच पूछा जाय तो शास्त्र ने शाश्वत और नित्य को पर्यायवाची माना है।"
भगवान् विष्णु इस प्रकार वेद या आयुर्वेदस्वरूप ठहरते हैं।
डॉ. मदन मोहन पाठक (धर्मज्ञ)
Related Posts
0 Comments
Comments are not available.