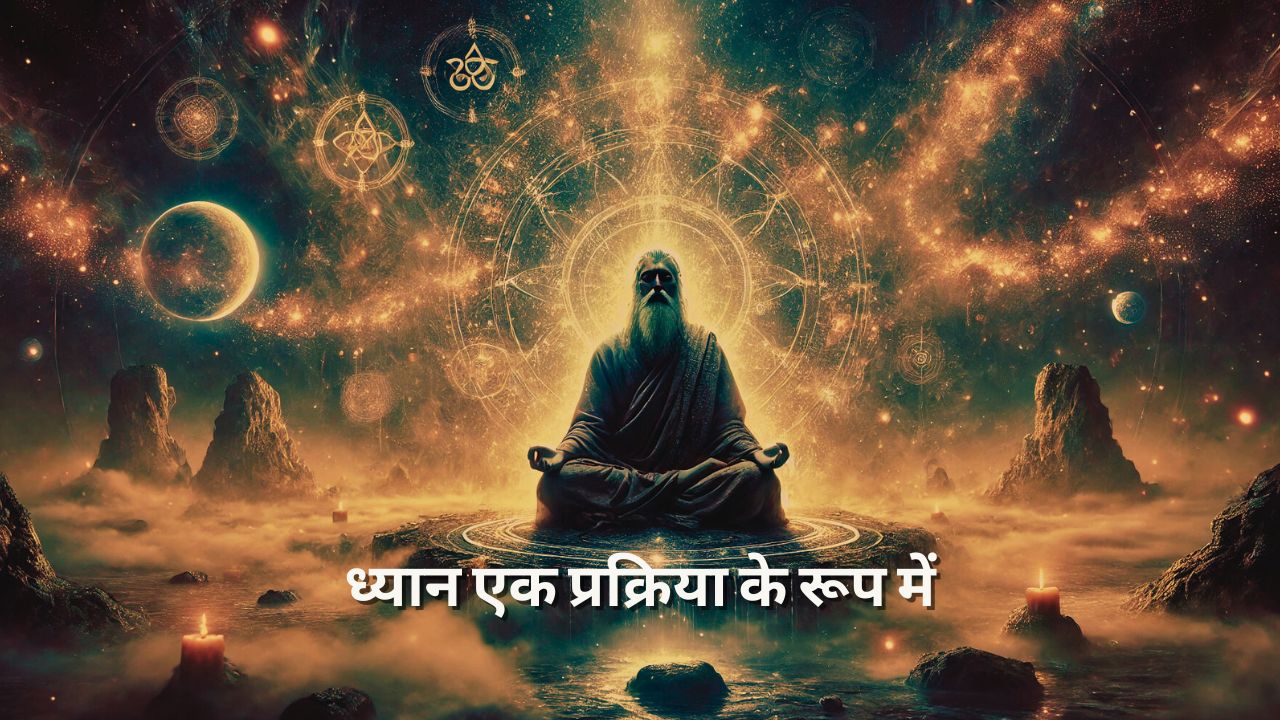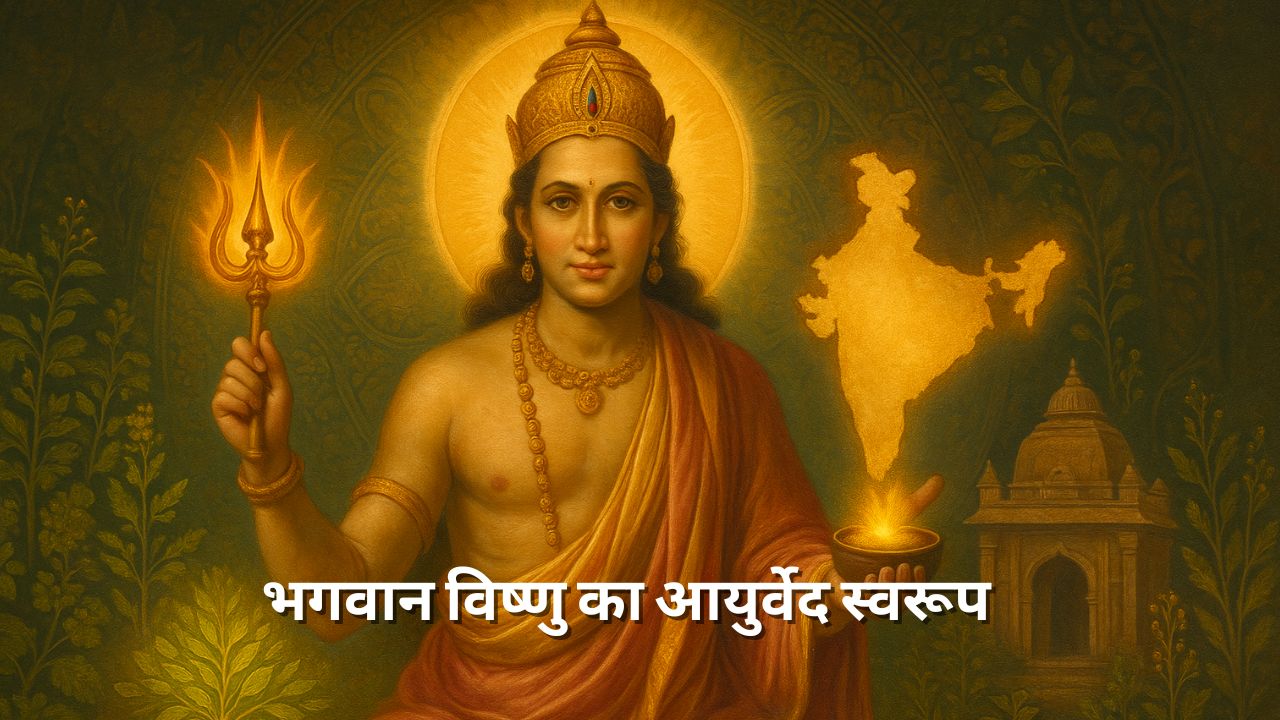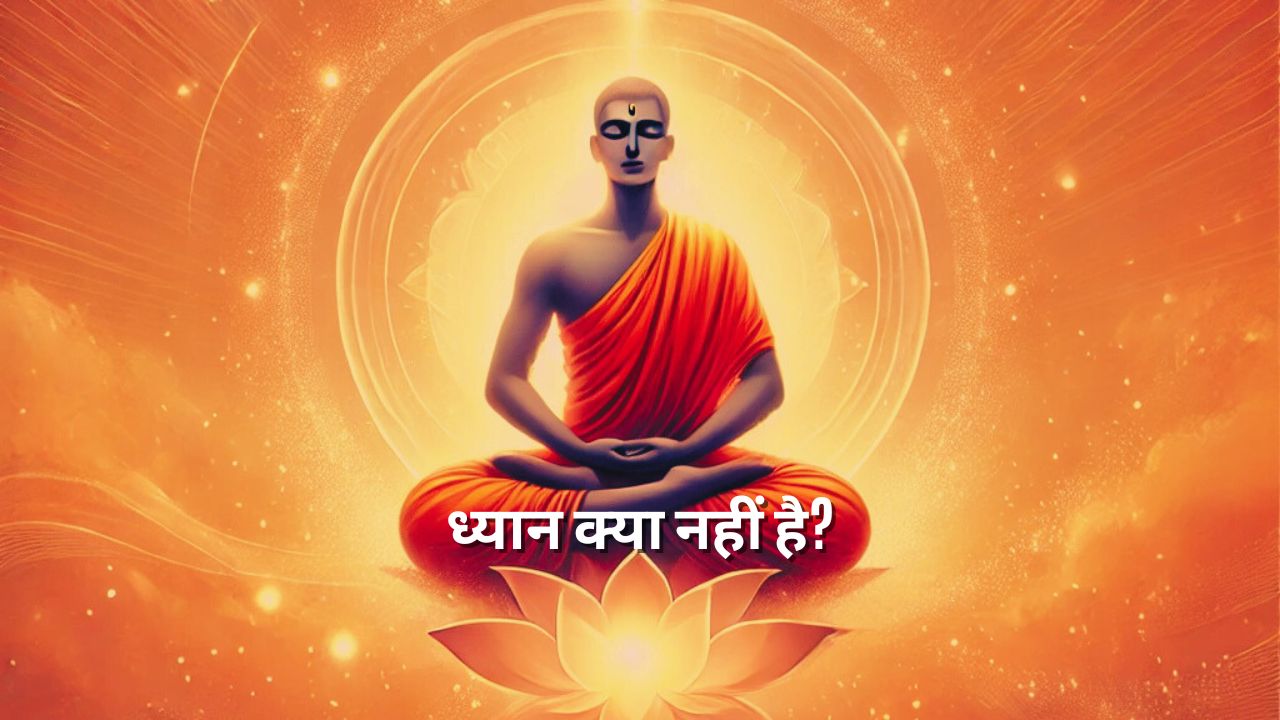- आयुष
- |
- 03 February 2025
- |
- 0 Comments
श्री स्वामी राम-
ध्यान की प्रक्रिया में, हम मन से कहते हैं कि वह चिंतन, विश्लेषण, स्मरण, समस्याओं के समाधान, तथा पिछली घटनाओं पर केंद्रित होने तथा भविष्य से जुड़ी अपेक्षाओं की प्रवृत्तियों का त्याग कर दे। हम मन की सहायता करते हैं कि वह अपने विचारों तथा भावनाओं की तीव्र गति को कम कर दे और उस मानसिक गतिविधि को आंतरिक सजगता व ध्यानाकर्षण के साथ बदलने की चेष्टा करे। इस प्रकार समस्याओं के चिंतन या समाधान के विश्लेषण को ध्यान नहीं कहते। यह किसी तरह की कल्पना या दिवास्वप्न नहीं है और न ही मन की व्यर्थ भटकन है। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि हम अपने साथ आंतरिक संवाद या बहस करते रहें या चिंतन प्रक्रिया को और भी गहन कर दें। ध्यान सजगता व मनोयोग का एक शांत व प्रयत्नरहित एकाग्रता बिंदु है।
ध्यान में, हम अनेक मानसिक बाधाओं, धारणाओं तथा जागृत अवस्था के अनेक विचारों व संबंधों से परे जाने की चेष्टा करते हैं। ऐसा करने के लिए हम मन को रिक्त नहीं करते, जिसे करना लगभग असंभव ही है। हम मन को किसी एक सूक्ष्म तत्व या वस्तु पर केंद्रित कर देते हैं, जिससे आंतरिक रूप से ध्यान को साधना सरल हो जाता है। जब हम स्वयं को पूरे मनोयोग से एक आंतरिक केंद्र बिंदु देते हैं, तो मन को अन्य तनावपूर्ण मानसिक प्रक्रियाओं को रोकने में सहायता मिलती है जैसे चिंता करना, नियोजन करना, सोचना व तर्क देना।
ध्यान के साधक को, मन को एकाग्र करने के लिए कोई आंतरिक साधन दिया जा सकता है। प्रायः इसके लिए किसी ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, वैसे कई बार बाहरी छवि पर भी ध्यान लगाने का सुझाव दिया जाता है। ध्वनि या छवि बाहरी या सूक्ष्म हो सकती है, जो कि साधक के मन की अवस्था पर निर्भर करता है। ध्यान के दौरान, जिन ध्वनियों पर मन को एकाग्र किया जाता है, उन्हें मंत्र कहते हैं। मंत्र मानसिक स्तर पर बहुत शक्तिशाली प्रभाव रखते हैं।
कोई मंत्र एक शब्द, वाक्य, ध्वनियों का समूह या कोई एक वर्ण भी हो सकता है। किसी मंत्र पर एकाग्र होने से छात्रों को अन्य अनुपयोगी, मन को भटकाने वाली प्रक्रियाओं से छुटकारा मिलता है और वे अपने भीतर गहराई तक उतर पाते हैं। पूरे संसार में विविध प्रकार के मंत्रों का प्रयोग होता है, जिनमें ओम्, आमीन या शेलोम जैसे मंत्र शामिल हैं, इनका लक्ष्य यही होता है कि मन को आंतरिक रूप से एकाग्र किया जा सके। इस पुस्तक में हम आपके अभ्यास के लिए एक आधारभूत मंत्र देंगे। नियमित रूप से उस मंत्र का अभ्यास आपके लिए लाभदायक होगा।
संसार की सभी महान प्राचीन व आधुनिक आध्यात्मिक परंपराओं में, किसी वर्ण, ध्वनि या शब्दों के समूह के उच्चारण का एक तरीक़ा है जो मंत्र की तरह काम करता है। यह एक महान और गहन विज्ञान है, और जो गुरु इस आंतरिक विज्ञान में सक्षम होते हैं, वे साधकों का इस पथ पर मार्गदर्शन कर सकते हैं। साधकों द्वारा किए जाने वाले प्रारंभिक अभ्यास सरल हैं और इन्हें किसी गुरु के मार्गदर्शन के अभाव में भी किया जा सकता है, परंतु जब साधक को अपने मन के साथ साधना करनी हो तो उस समय मंत्र का अभ्यास करना अनिवार्य है। किसी गुरु द्वारा दिया गया मंत्र, उपयोगी तथा शक्तिशाली परिणाम दे सकता है।
ध्यान का परिचय देने वाले ग्रंथों तथा पुस्तकों में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है। योग विद्या के जनक पतंजलि का कहना है कि मंत्र चेतना के आंतरिक स्त्रोत का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार, यह जीवन के मूर्त तथा अमूर्त पक्षों के बीच एक सेतु बनाता है। जब शरीर, श्वास तथा सजग मन, मृत्यु के समय अवचेतन मन तथा व्यक्तिगत आत्मा से अलग होते है, तो साधक निरंतर जिस मंत्र का जाप करता आया हो, यह अवचेतन में अपनी छाप बनाए रखता है। ये संस्कार शक्तिशाली प्रेरकों के रूप में, साधक की अंतरण की इस प्रक्रिया के दौरान सहायक होते हैं। मंत्रों की सहायता से, किसी भी व्यक्ति के लिए उन अनजान यात्रा पर निकलना सरल हो जाता है।
मंत्र किसी मन को दिया जाने वाला केंद्र बिंदु तथा सहयोग है। गुरु, शिष्य की मानसिक अवस्था तथा उसके द्वारा आंतरिक सत्य को जानने की इच्छा के अनुसार ही मन्त्र प्रदान करते हैं।
जिस प्रकार किसी एक पर्वत पर जाने के लिए अनेक मार्ग हो सकते हैं, उसी प्रकार ध्यान के अभ्यास के लिए विविध प्रकार की तकनीकें व विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। यद्यपि उन सबका लक्ष्य एक ही होता है आंतरिक एकाग्रता, प्रशांति व सहज भाव। जो भी अभ्यास आपको यह सब पाने में मदद कर सके, वह आपके लिए लाभदायक है। अनेक तकनीकें अस्तित्व में हैं इसलिए किसी एक प्रकार की प्रामाणिक विधि तथा दूसरी विधि में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, जब तक वे आपको आंतरिक सहजता, प्रशांति व केंद्र पाने के लक्ष्य को पूरा करती हैं।
कई बार लोग ध्यान की विधियों की तुलना में उलझ जाते हैं और यह बहस करने लगते हैं कि कौन से गुरु या परंपरा बेहतर है। अच्छे गुरु ध्यान की सार्वभौमिकता के भाव को पहचानते हैं व उसे मान देते हैं और उनकी तकनीकों के विषय में किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक विरोधी बैर या शंका नहीं पालते। ध्यान, आंतरिक आयामों के अन्वेषण तथा जीवन के सभी स्तरों का अनुमान लगाने का लाभदायक व सार्थक उपाय है। जब तक गुरु अहंकारी न हो तो यह सकारात्मक व मूल्यवान हैं। गुरु की ओर से यह दावा नहीं होना चाहिए कि कोई ध्यान विधि निजी रूप से उसकी है या उसे इस बात पर भी बल नहीं देना चाहिए कि उसकी विधि अन्य ध्यान विधियों की तुलना में श्रेष्ठ है।
प्रारंभ में, साधक के पास मन की इतनी स्पष्टता नहीं होती कि वह ध्यान के उचित उपाय को तलाश सके, उसे समझ सके और हो सकता है कि वह उन गुरुओं के प्रभाव में आ जाए, जो अपने ही प्रकार के ध्यान का प्रचार करते हैं। कितने खेद की बात है, इनमें से कुछ गुरु कपटी होते हैं और वे स्वयं वास्तव में ध्यान की साधना तक नहीं करते। ध्यान के अनेक आकांक्षी साधक किसी प्रामाणिक ध्यान साधना को पाने के लिए एक से दूसरे गुरु के पास जा कर अपना अमूल्य समय तथा ऊजां व्यर्थ करते रहते हैं। इसी जिज्ञासा में अपना बहुत सा समय, धन व ऊर्जा लगाने के बाद वे निराश हो जाते हैं और कुंठित हो कर, किसी भी तरह का गंभीर प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। हिमालयन परपरा में, हम प्रायः कहते हैं कि इस संसार में यदि पाप नामक कोई वस्तु है, तो वहकिसी गुरु द्वारा गंभीर शिष्यों को दिग्भ्रमित करना या उनका अनुचित मार्गदर्शन करना ही है।
यदि हम जीवन का स्पष्ट रूप से निरीक्षण करें, तो हम यह अनुभव कर सकते हैं कि हमारे बाल्यकाल से ही, हमें केवल बाहरी जगत की वस्तुओं के निरीक्षण व जांच-पड़ताल की ही शिक्षा दी गई है और किसी ने भी हमें सही मायनों में यह नहीं सिखाया कि अपने भीतर कैसे झाँके, अपने भीतर क्या खोंजे और अपने ही भीतर कैसे पुष्टि करें। इस प्रकार, हम अपने-आप से ही अजनबी बने रहते हैं, और दूसरों को जानने की कोशिश में लगे रहते हैं। अपने-आप को न समझ पाने के कारण ही हमारे संबंध सही तरह से काम नहीं करते और हमारे जीवन में हर ओर भ्रम तथा निराशा का साम्राज्य रहता है।
हमारी औपचारिक शिक्षा, मन के बहुत थोड़े से हिस्से को विकसित करती है। मन का जो हिस्सा सोता है व सपने देखता है, अवचेतन का यह विस्तृत क्षेत्र, जो सभी अनुभवों का भंडार है, वह अज्ञात तथा अनुशासनहीन ही बना रहता है; वह किसी भी प्रकार से वश में नहीं आता। यह सच है कि पूरी देह मन में सम्मिलित है परंतु संपूर्ण मन, इस देह में शामिल नहीं है। ध्यान के अभ्यास के अतिरिक्त ऐसा कोई भी अभ्यास नहीं है, जो मन की संपूर्णता को सही मायनों में अपने वश में कर सके।
हमें सिखाया जाता है कि बाहरी जगत में लोगों से कैसे भेंट करनी है या कैसे व्यवहार करना है, परंतु हमें स्थिर भाव से यह देखना कभी नहीं सिखाया जाता कि हमारे भीतर क्या है। इसके साथ ही, शांत व स्थिर होने की शिक्षा को किसी धार्मिक अनुष्ठान या समारोह से भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए; यह तो मानव के शरीर की सार्वभौमिक आवश्यकता हैं। जब हम स्थिर भाव से बैठना सीखते हैं, तो हमें ऐसे आनंद की अनुभूति होती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक मनुष्य के जीवन में आनंद के जितने भी उच्चतम शिखर तक जाया जा सकता है, उसकी प्राप्ति ध्यान के माध्यम से हो सकती है। संसार में अन्य सभी आनंद क्षणिक हैं परंतु ध्यान का आनंद विशाल व अनंत काल तक बना रहने वाला है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है; यह ऋषियों की महान परंपरा द्वारा अनुभूत किया गया सत्य है, जिनमें दोनों प्रकार के संत शामिल हैं, एक थे, जिन्होंने संसार को त्याग कर सत्य को पाया और दूसरे वे, जो संसार में रहते हुए भी, इससे अविचलित हैं। मन की प्रवृत्ति ही ऐसी है जो बार-बार आदतों के पुराने ढाँचे की ओर भागता है, ऐसे अनुभवों की कल्पना करता रहता। है, जो भविष्य में हो सकते हैं। मन वास्तव में नहीं जानता कि उसे आज ओर अभी के साथ कैसे जीना चाहिए। केवल ध्यान ही हमें, वर्तमान क्षण का संपूर्ण अनुभव लेना सिखाता है, जो कि बाहरी जगत से हमारा संबंध है। जब ध्यान की तकनीकों के माध्यम से मन की एकाग्र करके साथ लिया जाता है, तो यहहमारे अस्तित्व के गहन स्तरों तक जाने की शक्ति भी प्राप्त कर लेता है। फिर हमारा मन बाधित या विचलित नहीं होता, और एकाग्रता का संपूर्ण लाभ पाते हुए चलता है, जो कि ध्यान के अभ्यास के लिए अनिवार्य है। वे लोग धन्य हैं जो इस तथ्य के प्रति सजग हो कर ध्यान की साधना आरंभ कर चुके हैं। उनसे भी सौभाग्यशाली वे हैं, जो ध्यान करते हैं और उनसे भी अधिक सौभाग्यशाली उन्हें जानें, जिन्होंने ध्यान को ही अपने जीवन की उच्च प्राथमिकता मान लिया है और नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं।
इस पथ पर चलने के लिए, स्पष्ट रूप से समझना होगा कि ध्यान क्या है, अपने लिए ऐसे अभ्यास का चुनाव करें, जो आरामदायक हो और कुछ समय तक इसे निरंतर जारी रखें, यदि हो सके तो प्रतिदिन, एक ही समय पर, ध्यान का अभ्यास करें। आधुनिक जगत में, हालाँकि, साधक बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं और एक अभ्यास को कुछ ही समय तक करने के बाद छोड़ देते हैं, वे यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि उन तकनीकों का कोई मूल्य या प्रामाणिकता नहीं है। यह तो मानो उसी बालक की तरह हुआ, जो एक ट्यूलिप बल्ब रोपता है और यह सोच कर कुंठित हो जाता है कि उसे एक सप्ताह में ही फूल क्यों नहीं दिखा। यदि आप नियमित रूप से ध्यान की साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्रगति का अनुभव होगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास कर रहे हों और आपको प्रगति का अनुभव न हो।
हो सकता है कि आप तत्काल शारीरिक विश्रांति व भावात्मक प्रशांति के रूप में प्रगति का अनुभव करें। बाद में आप अन्य सूक्ष्म लक्षणों को भी जान सकते हैं। ध्यान के साधकों को समय के साथ-साथ ध्यान के कुछ ऐसे लाभ का परिचय मिलता है, जो बहुत प्रभावशाली नहीं होते या जिन्हें आसानी से देखा नहीं जा सकता। अपनी ध्यान साधना बनाए रखें और आपको प्रगति का अनुभव होगा। आने वाले अध्यायों में हम चर्चा करेंगे कि आप अपनी प्रगति का अनुमान कैसे लगा सकते हैं और आपको अगले चरण तक कब जाना है।
इससे पूर्व कि हम इस परिचर्चा का निष्कर्ष निकालें, हम कुछ अन्य मानसिक प्रक्रियाओं के बीच अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, जिन्हें प्रायः ध्यान का अभ्यास ही मान लिया जाता है।
Related Posts
0 Comments
Comments are not available.