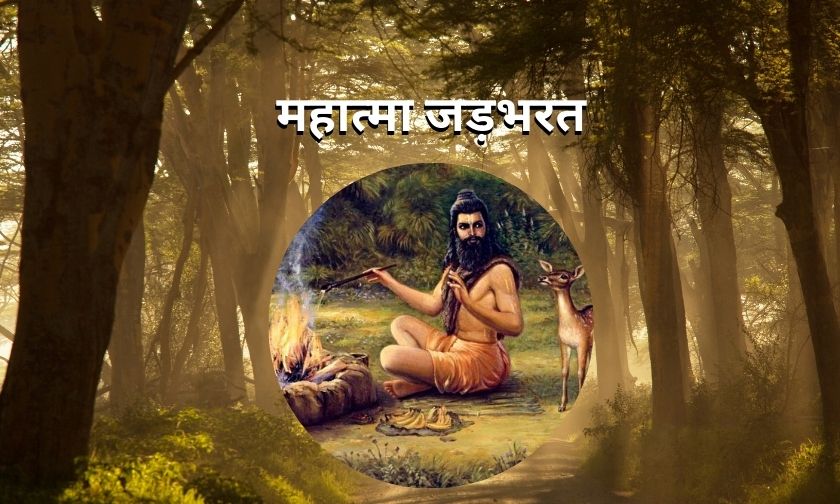- NA
- |
- 31 October 2024
- |
- 0 Comments
Mystic Power-(स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज)
तपसा प्राप्यते सत्त्वं सत्त्वात् सम्प्राप्यते मनः ।
मनसा प्राप्यते ह्यात्मा ह्यात्मापत्त्या निवर्तते ॥
' अन्तःकरण-की, सत्त्व से मन (विचार-शक्ति के विकास) की और मन से आत्मा (आत्मज्ञान) की प्राप्ति होती है तथा आत्मज्ञान से अज्ञानरूपी आवरण निवृत्त हो जाता है।'
मन और इन्द्रियों के संयम रूप तप से सत्त्व शुद्ध प्राणि मात्र में चित्त का निवास है, कार्य-भेद से उसके मन और बुद्धि ये दो विभाग हो जाते हैं। संकल्प- विकल्पात्मिका वृत्ति को मन और निश्चयात्मि का वृत्ति को 'बुद्धि' संज्ञा दी गयी है। बुद्धि को मति, विचार-शक्ति, ज्ञानग्राहिणी वृत्ति तथा क्रिया-भेद से स्मृति, मेधा आदि नाम भी दिये जाते हैं। मन और बुद्धि का शरीर के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है, ऐसा प्रत्येक मनुष्य को अनुभव होता है। जितनी भी शारीरिक क्रियाएँ होती हैं, उन सब के शुभाशुभ (संस्कार वासना) चित्त पर जम जाते हैं। इसी प्रकार दूसरी ओर मन-बुद्धि के कार्य का प्रभाव शरीर पर पड़ता रहता है। जैसे मानसिक प्रसन्नता होने पर मुख प्रफुल्लित और तेजस्वी प्रतीत होता है, चिन्ताग्रस्त होने पर शरीर निस्तेज और निर्बल हो जाता है; क्रोध की उत्पत्ति होने पर रक्त विषमय बन जाता है, हिताहित का विचार विस्मृत हो जाता है और लोभ का उदय होने पर धर्म-अधर्म का विवेक दूर हो जाता है।
 शुभ संस्कारों से शुभ कर्म में और अशुभ संस्कारों से अशुभ क्रिया में रति होने लगती है। सांसारिक वासनाओं से मनुष्य संसार में प्रवृत्त होता है और भगवद्भक्तिजनित संस्कारों से धर्म में अनुराग होकर अधर्म की ओर से उपराम वृत्ति होने लगती है। फिर परिणाम में शुभाशुभ संस्कारों अथवा मन-बुद्धि की उन्नति-अवनति के अनुरूप मनुष्य का जीवन सुखी-दुःखी या सफल निष्फल बनता है।चित्त की प्रेरणा के पश्चात् ही शारीरिक क्रियाएँ होती हैं। शिशु का हाथ-पैर हिलाना, रोना या हँसना- ये सब कार्य उसके चित्त की प्रेरणा के अनुसार ही होते हैं। मन की आज्ञा मिले बिना शारीरिक चेष्टा नहीं होती। मन भी अपनी शक्तियों द्वारा विचार, संवेदन और इच्छा- ये तीन मानस- व्यापार कर लेने के बाद ही किसी शारीरिक क्रिया के लिये आदेश देता है, ऐसा निरीक्षण करने पर अवगत हो जाता है। जैसे किसी को एक मच्छर काट रहा है, उस समय उसके मन में सबसे पहले संकल्प का स्फुरण होकर विचार का उदय होता है, फिर वात वहा नाडियों क केन्द्र स्थान मस्तिष्क देश में मच्छर के दंशजनित प्रतिकूल वेदना की प्रतीति होती है और तब उस वेदना के निवारणार्थ मन में इच्छा का उद्भव होता है। इस प्रकार इन तीन क्रियाों कि हो जाने पर मच्छर को उड़ाने के लिये हस्तेन्द्रिय प्रेरित होती है, तदनन्तर बाह्य क्रिया होती है। अतः इस उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो गयी कि शरीर के शुभाशुभ या सामान्य चेष्टारूप समस्त कर्मों का प्रारम्भ तभी होता है जब विचार, संवेदन और इच्छा (प्रेरणा)- ये तीनों मानस व्यापार हो लेते हैं। इन तीनों मानसिक शक्तियों के विपरीत किसी भी कर्म में मनुष्य को प्रवृत्ति अथवा उससे निवृत्ति नहीं हो सकती।
शुभ संस्कारों से शुभ कर्म में और अशुभ संस्कारों से अशुभ क्रिया में रति होने लगती है। सांसारिक वासनाओं से मनुष्य संसार में प्रवृत्त होता है और भगवद्भक्तिजनित संस्कारों से धर्म में अनुराग होकर अधर्म की ओर से उपराम वृत्ति होने लगती है। फिर परिणाम में शुभाशुभ संस्कारों अथवा मन-बुद्धि की उन्नति-अवनति के अनुरूप मनुष्य का जीवन सुखी-दुःखी या सफल निष्फल बनता है।चित्त की प्रेरणा के पश्चात् ही शारीरिक क्रियाएँ होती हैं। शिशु का हाथ-पैर हिलाना, रोना या हँसना- ये सब कार्य उसके चित्त की प्रेरणा के अनुसार ही होते हैं। मन की आज्ञा मिले बिना शारीरिक चेष्टा नहीं होती। मन भी अपनी शक्तियों द्वारा विचार, संवेदन और इच्छा- ये तीन मानस- व्यापार कर लेने के बाद ही किसी शारीरिक क्रिया के लिये आदेश देता है, ऐसा निरीक्षण करने पर अवगत हो जाता है। जैसे किसी को एक मच्छर काट रहा है, उस समय उसके मन में सबसे पहले संकल्प का स्फुरण होकर विचार का उदय होता है, फिर वात वहा नाडियों क केन्द्र स्थान मस्तिष्क देश में मच्छर के दंशजनित प्रतिकूल वेदना की प्रतीति होती है और तब उस वेदना के निवारणार्थ मन में इच्छा का उद्भव होता है। इस प्रकार इन तीन क्रियाों कि हो जाने पर मच्छर को उड़ाने के लिये हस्तेन्द्रिय प्रेरित होती है, तदनन्तर बाह्य क्रिया होती है। अतः इस उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो गयी कि शरीर के शुभाशुभ या सामान्य चेष्टारूप समस्त कर्मों का प्रारम्भ तभी होता है जब विचार, संवेदन और इच्छा (प्रेरणा)- ये तीनों मानस व्यापार हो लेते हैं। इन तीनों मानसिक शक्तियों के विपरीत किसी भी कर्म में मनुष्य को प्रवृत्ति अथवा उससे निवृत्ति नहीं हो सकती।
 यदि मनुष्य इन तीनों मानसवृत्तियों का सामंजस्य रखकर मनोवृत्तिरूप साधन के यथोचित विकास के लिये प्रयत्न करे, तो वह इच्छानुसार सांसारिक उन्नति या परब्रह्म को प्राप्ति कर सकता है। जितने अंश में इन त्रिविध शक्तियों का विकास कम होगा अथवा इनमें से केवल एक या दो शक्तियों का विकास करके इनके सामंजस्य को भंग किया जायगा, उतने ही अंश में सुख की प्राप्ति कम हो जायगी या जीवन दुःखमय बन जायगा। इसलिये आस्तिक या नास्तिक-सभी मनुष्यों को इन तीनों वृत्तियों का समन्वय करके ही मानसिक प्रगति करनी चाहिये।
इन तीनों वृत्तियों की' मूल शक्ति सृष्टि में विलसित मूलतत्त्व (ब्रह्मचैतन्य) में अवस्थित है। सृष्टि के बाहर भीतर ऐसा एक भी पदार्थ नहीं है, जो इस मूलतत्त्व से पृथक् हो। यह बात वेदों के निम्नलिखित मन्त्रों से प्रकट होती है-
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, तद् विजिज्ञासस्व, तद् ब्रह्मेति। (वैति०)
सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति । (छान्दोग्य०)
इन मन्त्रों का सोपपत्तिक विचार भगवान् बादरायण- रचित ब्रह्मसूत्र के 'जन्माद्यस्य यतः' (१।१।२) इस सूत्र में किया गया है। जिनको इस विषय की विशेष जिज्ञासा हो, उन्हें उक्त सूत्र का भाष्य देखना चाहिये।
इस ब्रह्मतत्त्व में सत्, चित, आनन्द, ज्ञान, बल, क्रिया आदि अनेक शक्तियाँ विद्यमान हैं। वे ही सृष्टिकाल में मलिन-सी होकर मन के भीतर प्रतीत होती हैं। क्योंकि यह अविचल नियम है कि 'कारणगुणाः कार्य सङ्क्रामन्ति' अर्थात् कारण में रहने वाले गुण-धर्म या शक्तिकार्य में सहज ही उतर आते हैं। पर ब्रह्म की शक्तियों का मन और तन में प्रवेश हो ही जाता है-इस बात को भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र ने भी गीता के 'इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना' इस वचन के द्वारा स्पष्ट कर दिया है। अस्तु, मन की जो शान्त साम्यावस्था है, वह परब्रह्म की सामान्यावस्था (सत्- शक्ति) के साथ सम्बन्ध रखने वाली है। मन में रहने वाली विचार-शक्ति और ब्रह्म के चिदंश (चेतना-शक्ति) में प्रकाशकत्वरूप गुण समान होनेके कारण दोनों की एकता जानी जाती है। अतः मनुष्य की विचार-शक्ति का विकास चिदंश के साथ एकता के द्वारा ही हो सकता है। मन की संवेदना-शक्ति और ब्रह्म के आनन्द-अंश का घनिष्ठ सम्बन्ध भी अनुभव में आता रहता है। इसी प्रकार मन की कर्तृत्वशक्ति (इच्छा और प्रेरणावृत्ति) तथा ब्रह्म की बल-शक्ति एवं शरीर को क्रिया और ब्रह्म में रहने वाली क्रियाशक्ति भी तत्त्वतः एक ही हैं। मतलब यह कि मानसिक शक्तियाँ परब्रह्म की सत् चित्, आनन्द आदि शक्तियों से पृथक् नहीं हैं। अतः मनुष्य जितने अंश में परब्रह्म के साथ सहयोग रखेगा, उतने ही अंश में अपने अन्तरकी शक्तियों को उन्नत कर सकेगा। इस निबन्ध में केवल विचारशक्तिरूप प्राथमिक साधन का ही मुख्यतया विवेचन किया जायगा। शेष दो साधनों (संवेदन और कर्तृत्वशक्ति) तथा शारीरिक शक्तिके सम्बन्धमें यदि कभी अवसर मिला, तो अलग-अलग लेख लिखकर पाठकों की सेवामें समर्पित किये जायेंगे।
विचार-शक्ति प्राणिमात्र के जीवन का दीपक है। जैसे चित्-शक्ति विश्व को प्रकाशित करती है, वैसे ही विचार- शक्ति जीवोंके कर्तव्य-पथ को निश्चित करती है। किसी प्रश्न के सत्यासत्य का निर्णय करना अथवा हित-अहित, सज्जन-दुर्जन, मित्र-शत्रु, गुण-दोष, लाभ-हानि, कर्तव्य अकर्तव्य और तन-मन-धन की योग्यता-अयोग्यता आदि का विचार करना तथा जीवन के ध्येय और उसके सहायक साधनों का निश्चय करना- ये सब कार्य विचार-शक्ति के द्वारा ही होते हैं। अत:एव इसकी जितनी अधिक प्रगति को जाय, उतनी ही अधिक मात्रा में परीक्षण का बल बढ़ता है। यहाँ तक कि सृष्टि के मूल निमित्तोपादान कारण परब्रह्म और धर्म के स्वरूप का निर्णय भी विचार-शक्ति के द्वारा ही होता है।
धर्म का प्रधान लक्ष्य तत्त्वज्ञान की प्राप्ति द्वारा कैवल्य मुक्ति पाना ही है। यह कार्य विचार-शक्ति का विकास किये बिना कदापि नहीं हो सकता। यदि विचार-शक्ति का उपयोग इसके विपरीत दिशा में अर्थात् भौतिक विद्याओं की प्रगति के लिये किया जाय, तो उस विषय के ही ज्ञान को वृद्धि होती है। किन्तु नैसर्गिक नियमों का अनादर करके भौतिक ज्ञान की उन्नति की जायगी, तो वह कदापि समुचित कल्याणकारी नहीं हो सकती। जिस प्रकार अग्नि में घृत डालने पर वह अधिक प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार केवल भौतिक ज्ञान से विषय-भोग की वासनाएँ अधिकाधिक उद्दीप्त होती हैं, जिनसे मन में सदा अशान्ति बनी रहती है तथा स्वार्थवश संसार को हानि पहुँचाने की प्रवृत्ति होती है। जो मनुष्य इस हानिकर पथपर चलता है, उसकी संवेदना शक्ति के विकास में प्रतिबन्ध उपस्थित हो जाता है; फिर मन की तीनों शक्तियों का समन्वय नहीं रह पाता, जिससे वह भावी सुखसे वंचित हो जाता है। अस्तु, विचार-शक्ति का यथोचित विकास धर्म-शास्त्र के अनुग्रह से ही होता है।
जब तक धर्मशास्त्र के तात्पर्य को हृदयगंम नहीं किया जायगा एवं नैसर्गिक नियमों का यथावत् पालन नहीं होगा, तब तक सच्चेविचार-शक्ति का सम्यकू विकास होनेपर विदित होता है कि ब्रहा ही इस सृष्टिरूपी रंग-भूमि पर विलास कर रहा है। वहीं नट-नटी समूह और द्रष्टा बना हुआ है। उसके अतिरिक्त इस ब्रह्माण्ड में कुछ है ही नहीं। सारा संसार उसी का रूप है। इस भूमण्डल पर अनादि काल से चतुर्विध योनियों और चौरासी लाख प्रकार के अनन्त प्राणियों की जीवन रक्षा, आनन्द प्राप्ति, वंशवृद्धि आदि के निमित्त उद्योग, सामाजिक क्रान्ति, देशकाल-परिवर्तन, स्वार्थवश दूसरों के देश, जीवन और सम्पत्ति का नाश तथा विभिन्न गुण-धर्म, प्रकृति और आकृतिवाली विविध प्रकार की अनन्त वस्तुओं का रूपान्तर होते रहना आदि नाटक युगारम्भ से ही निरन्तर हो रहा है। परन्तु इन सब विविधताओं में भी ब्रह्मतत्त्व सदा सम अवस्था में ही बना रहता है। समस्त भौतिक पदार्थों के बनते बिगड़ते रहने पर भी इस मूल उपादान कारण के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। विचार-शक्ति का विकास होने पर यह रहस्य स्पष्ट हो जाता है।
इसी प्रकार भूगोल के अनुसार खगोल के पदार्थों का निश्चय भी विचार शक्ति कर लेती है। आकाश में ऊर्ध्वदृष्टि डालने पर सूर्य, चन्द्र, ग्रह, उपग्रह, अनन्तकोटि तेज:पुंज, तारागण, नक्षत्रमाला और धूमकेतु आदि के अविभ्रान्त सतत परिभ्रमण का बोध होता है। इस दृश्य को देखने पर जिज्ञासु- जनों के अन्तःकरण में यह जिज्ञासा सहज ही उत्पन्न हो जाती है कि 'ये सब क्या हैं? ये नित्य हैं या अनित्य ? यदि अनित्य हैं तो इनका उद्गमस्थान कहाँ है ? इन सब अस्थिर, चल पदार्थों का कोई-न-कोई स्थिर आधार होना ही चाहिये; यह स्थिर आधार कौन, कहाँ और कैसा है ?' इन जिज्ञासाओं की उत्पत्ति होने पर विचार-शक्ति विवेक करने लगती है कि ये सब सृष्टि के अन्तर्गत ही हैं। सृष्टि साकार और कार्यरूपा है। साकार पदार्थ अनादि नहीं होता। उत्पत्तिमान् होने से वह सदा रह भी नहीं सकता। उत्पन्न होने वाला कार्य का रूपान्तर होता है, अत:एव उसका नाश भी अवश्यम्भावी है। इन अस्थिर पदार्थों को नियम में बाँध रखने वाले पर ब्रह्मतत्त्व है। वही एक अविनश्वर, चिन्मात्र तत्त्व है। वही इस विनश्वर विश्व का मूलाधार है। वही इस सृष्टि का निमित्त एवं उपादान-कारण है। वही विवर्तरूप परिवर्तन के द्वारा सृष्टिरूप बन गया है। यह सृष्टिरूप कार्य सच्चा रूपान्तर नहीं है। यदि सच्चा रूपान्तर होता तो मूलतत्त्व विकारी हो जाता, फलतः संसार अद्यावधि टिक नहीं पाता।
इस मूलतत्त्व के परिमाण में कदापि न्यूनता न होने के कारण वह अव्यय है। सब प्रकार के विकारों से रहित होने के कारण अविकारी है। नाश न होने के कारण अविनाशी है। उत्पत्तिरहित होने के कारण अनादि और अन्तरहित होने के कारण अनन्त है। जो अनादि अनन्त होगा, वही त्रिकाल में समभाव से स्थित रह सकता है। इसीलिये इस तत्त्व को नित्य और सनातन कहा गया है। इस विश्व में उससे पृथक् कोई पदार्थ न होने के कारण वह अद्वैत है। जो अद्वैत है, वही निर्भय होता है; द्वैत में नीति, भेदभाव और राग- द्वेष उत्पन्न होते रहते हैं। इस प्रकार विचार-शक्ति यह निर्णय करती है कि इस सृष्टि के मूल में एक से अधिक तत्त्व नहीं हैं यह तत्त्व सर्वदा सम अवस्था में रहता है, इसलिये सत् है; प्राणिमात्र और जड सृष्टि को प्रकाश देता है, इस हेतु से उसे चित्-चेतन कहते हैं; उसी से समस्त ब्रह्माण्डों में रहने वाले जीव-समुदायों को आनन्द की प्राप्ति होती है, इसलिये वह आनन्दरूप कहलाता है। यह तत्त्व सृष्टि के बाहर भीतर सर्वत्र अवस्थित है; कोई ऐसा स्थान नहीं, जहाँ उसका प्रवेश न हो।
अत:एव वह विभु और सर्वव्यापक कहलाता है। यह ब्रह्मतत्त्व संग से रहित होने के कारण असंग, कर्तापन के अभिमान से शून्य होने के कारण अकर्ता तथा किसी भी प्रमाण (जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि) के द्वारा अवगत न होने के कारण अप्रमेय है। वह प्राणिमात्र के अन्तःकरण में अवस्थित होने के कारण अन्तरात्मा एवं सृष्टि का नियमन करने तथा सब प्रकार की शक्तियों से युक्त होने के कारण ईश्वर और परमेश्वर कहलाता है। ऐसा जो सृष्टि का मूल उपादान कारण है, उसे श्रुति भगवती ने पूर्ण कहा है-
पूर्णमदःपूर्णस्य पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।।
यह सृष्टि जिस निरुपाधिक मूल तत्त्व के एक क्षुद्र देश में अवस्थित है, वह तत्त्व पूर्ण है। इस सृष्टि के अन्तर में रहने वाला सोपाधिक तत्त्व भी पूर्ण है, क्योंकि उसका उद्भव पूर्ण तत्व से ही हुआ है। इस विश्वान्तर तत्त्व की पूर्णता को लेकर विश्वातीत तत्त्व पूर्ण ही अवशिष्ट रहता है। अस्तु, यह ब्रह्म ही जीवात्मारूप से भासमान हो रहा है, समस्त संसार ब्रह्मरूप है और अन्तःकरण में स्थित आत्मा भी ब्रह्मरूप ही है-इस असन्दिग्ध ज्ञान का उदय विचार-शक्ति के द्वारा ही होता है। जब यह संशयरहित और दृढ़ हो जाता है, तब जीव जीवन्मुक्त होकर विचरता है और अन्त में उसी तत्त्व में लीन हो जाता है। वह फिर संसार-चक्र में नहीं फँसता। इस सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः एतद्ब्रहौतमितः प्रेत्याभिसंभवितास्मीति यस्य स्यादद्धा न विचिकित्सास्तीति ह स्माह शाण्डिल्यः शाण्डिल्यः(छा० ४० ३।१४।४)
इस प्रकार विचार-शक्तिरूप साधन के द्वारा सृष्टि के मूल उपादान-कारण का आकलन होता है। इस ज्ञान को सुदृढ़ बनाने में संवेदना शक्ति के विकास को भी आवश्यकता रहती है। उसका विकास किये बिना अहंता-ममता, राग-द्वेष, आसक्ति आदि दोषों की निवृत्ति नहीं होती। इसी तरह कर्तृत्वशक्ति का विकास किये बिना निर्विघ्न और सम्यक्रूप से प्रगति नहीं हो पाती। अतः विचार- शक्तिके साथ-साथ इन दोनों शक्तियों को भी विकसित करके शास्त्रजन्य ज्ञान के साथ अनुभवरूप विज्ञानकी भी प्राप्ति कर लेनी चाहिये।
नास्तिक लोग इस विचार शक्ति का उपयोग भौतिक ज्ञान की वृद्धि के लिये करते हैं, फलतः उनसे संसार का अहित होता है। मूर्ख आस्तिक भी, जो ईश्वर और धर्म के स्वरूप को विपरीत मान लेते हैं, ईश्वर और धर्म के नाम पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर भूतकालीन क्रिश्चियन और इस्लामधर्म के उपदेशकों के विपरीत उपदेशों द्वारा अनेकों बार भयंकर नर-संहार हुआ और वर्तमान में भी हो रहा है। इसी विपरीत भावना के कारण शैव, शाक्त और वैष्णव आदि सम्प्रदायों में भी परस्पर झगड़े हुए तथा अब भी कहीं- कहीं हो जाते हैं। इन सब विरोधों का मूल कारण विचार-शक्ति के यथोचित विकास का अभाव है। जब तक अन्तःकरण मंलिन रहेगा, तब तक सदाचार या धर्म के बोध का प्रभाव नहीं पड़ सकता। अतः विवेकी सज्जनों को चाहिये कि वे अपने अन्तःकरण को निष्काम कर्म और भगवद्भक्ति द्वारा विशुद्ध बनाने के साथ-साथ परब्रह्म को प्राप्ति के लिये विचार-शक्ति का विकास करें और उसके द्वारा सच्चे सुख की प्राप्ति करें।
यदि मनुष्य इन तीनों मानसवृत्तियों का सामंजस्य रखकर मनोवृत्तिरूप साधन के यथोचित विकास के लिये प्रयत्न करे, तो वह इच्छानुसार सांसारिक उन्नति या परब्रह्म को प्राप्ति कर सकता है। जितने अंश में इन त्रिविध शक्तियों का विकास कम होगा अथवा इनमें से केवल एक या दो शक्तियों का विकास करके इनके सामंजस्य को भंग किया जायगा, उतने ही अंश में सुख की प्राप्ति कम हो जायगी या जीवन दुःखमय बन जायगा। इसलिये आस्तिक या नास्तिक-सभी मनुष्यों को इन तीनों वृत्तियों का समन्वय करके ही मानसिक प्रगति करनी चाहिये।
इन तीनों वृत्तियों की' मूल शक्ति सृष्टि में विलसित मूलतत्त्व (ब्रह्मचैतन्य) में अवस्थित है। सृष्टि के बाहर भीतर ऐसा एक भी पदार्थ नहीं है, जो इस मूलतत्त्व से पृथक् हो। यह बात वेदों के निम्नलिखित मन्त्रों से प्रकट होती है-
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, तद् विजिज्ञासस्व, तद् ब्रह्मेति। (वैति०)
सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति । (छान्दोग्य०)
इन मन्त्रों का सोपपत्तिक विचार भगवान् बादरायण- रचित ब्रह्मसूत्र के 'जन्माद्यस्य यतः' (१।१।२) इस सूत्र में किया गया है। जिनको इस विषय की विशेष जिज्ञासा हो, उन्हें उक्त सूत्र का भाष्य देखना चाहिये।
इस ब्रह्मतत्त्व में सत्, चित, आनन्द, ज्ञान, बल, क्रिया आदि अनेक शक्तियाँ विद्यमान हैं। वे ही सृष्टिकाल में मलिन-सी होकर मन के भीतर प्रतीत होती हैं। क्योंकि यह अविचल नियम है कि 'कारणगुणाः कार्य सङ्क्रामन्ति' अर्थात् कारण में रहने वाले गुण-धर्म या शक्तिकार्य में सहज ही उतर आते हैं। पर ब्रह्म की शक्तियों का मन और तन में प्रवेश हो ही जाता है-इस बात को भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र ने भी गीता के 'इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना' इस वचन के द्वारा स्पष्ट कर दिया है। अस्तु, मन की जो शान्त साम्यावस्था है, वह परब्रह्म की सामान्यावस्था (सत्- शक्ति) के साथ सम्बन्ध रखने वाली है। मन में रहने वाली विचार-शक्ति और ब्रह्म के चिदंश (चेतना-शक्ति) में प्रकाशकत्वरूप गुण समान होनेके कारण दोनों की एकता जानी जाती है। अतः मनुष्य की विचार-शक्ति का विकास चिदंश के साथ एकता के द्वारा ही हो सकता है। मन की संवेदना-शक्ति और ब्रह्म के आनन्द-अंश का घनिष्ठ सम्बन्ध भी अनुभव में आता रहता है। इसी प्रकार मन की कर्तृत्वशक्ति (इच्छा और प्रेरणावृत्ति) तथा ब्रह्म की बल-शक्ति एवं शरीर को क्रिया और ब्रह्म में रहने वाली क्रियाशक्ति भी तत्त्वतः एक ही हैं। मतलब यह कि मानसिक शक्तियाँ परब्रह्म की सत् चित्, आनन्द आदि शक्तियों से पृथक् नहीं हैं। अतः मनुष्य जितने अंश में परब्रह्म के साथ सहयोग रखेगा, उतने ही अंश में अपने अन्तरकी शक्तियों को उन्नत कर सकेगा। इस निबन्ध में केवल विचारशक्तिरूप प्राथमिक साधन का ही मुख्यतया विवेचन किया जायगा। शेष दो साधनों (संवेदन और कर्तृत्वशक्ति) तथा शारीरिक शक्तिके सम्बन्धमें यदि कभी अवसर मिला, तो अलग-अलग लेख लिखकर पाठकों की सेवामें समर्पित किये जायेंगे।
विचार-शक्ति प्राणिमात्र के जीवन का दीपक है। जैसे चित्-शक्ति विश्व को प्रकाशित करती है, वैसे ही विचार- शक्ति जीवोंके कर्तव्य-पथ को निश्चित करती है। किसी प्रश्न के सत्यासत्य का निर्णय करना अथवा हित-अहित, सज्जन-दुर्जन, मित्र-शत्रु, गुण-दोष, लाभ-हानि, कर्तव्य अकर्तव्य और तन-मन-धन की योग्यता-अयोग्यता आदि का विचार करना तथा जीवन के ध्येय और उसके सहायक साधनों का निश्चय करना- ये सब कार्य विचार-शक्ति के द्वारा ही होते हैं। अत:एव इसकी जितनी अधिक प्रगति को जाय, उतनी ही अधिक मात्रा में परीक्षण का बल बढ़ता है। यहाँ तक कि सृष्टि के मूल निमित्तोपादान कारण परब्रह्म और धर्म के स्वरूप का निर्णय भी विचार-शक्ति के द्वारा ही होता है।
धर्म का प्रधान लक्ष्य तत्त्वज्ञान की प्राप्ति द्वारा कैवल्य मुक्ति पाना ही है। यह कार्य विचार-शक्ति का विकास किये बिना कदापि नहीं हो सकता। यदि विचार-शक्ति का उपयोग इसके विपरीत दिशा में अर्थात् भौतिक विद्याओं की प्रगति के लिये किया जाय, तो उस विषय के ही ज्ञान को वृद्धि होती है। किन्तु नैसर्गिक नियमों का अनादर करके भौतिक ज्ञान की उन्नति की जायगी, तो वह कदापि समुचित कल्याणकारी नहीं हो सकती। जिस प्रकार अग्नि में घृत डालने पर वह अधिक प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार केवल भौतिक ज्ञान से विषय-भोग की वासनाएँ अधिकाधिक उद्दीप्त होती हैं, जिनसे मन में सदा अशान्ति बनी रहती है तथा स्वार्थवश संसार को हानि पहुँचाने की प्रवृत्ति होती है। जो मनुष्य इस हानिकर पथपर चलता है, उसकी संवेदना शक्ति के विकास में प्रतिबन्ध उपस्थित हो जाता है; फिर मन की तीनों शक्तियों का समन्वय नहीं रह पाता, जिससे वह भावी सुखसे वंचित हो जाता है। अस्तु, विचार-शक्ति का यथोचित विकास धर्म-शास्त्र के अनुग्रह से ही होता है।
जब तक धर्मशास्त्र के तात्पर्य को हृदयगंम नहीं किया जायगा एवं नैसर्गिक नियमों का यथावत् पालन नहीं होगा, तब तक सच्चेविचार-शक्ति का सम्यकू विकास होनेपर विदित होता है कि ब्रहा ही इस सृष्टिरूपी रंग-भूमि पर विलास कर रहा है। वहीं नट-नटी समूह और द्रष्टा बना हुआ है। उसके अतिरिक्त इस ब्रह्माण्ड में कुछ है ही नहीं। सारा संसार उसी का रूप है। इस भूमण्डल पर अनादि काल से चतुर्विध योनियों और चौरासी लाख प्रकार के अनन्त प्राणियों की जीवन रक्षा, आनन्द प्राप्ति, वंशवृद्धि आदि के निमित्त उद्योग, सामाजिक क्रान्ति, देशकाल-परिवर्तन, स्वार्थवश दूसरों के देश, जीवन और सम्पत्ति का नाश तथा विभिन्न गुण-धर्म, प्रकृति और आकृतिवाली विविध प्रकार की अनन्त वस्तुओं का रूपान्तर होते रहना आदि नाटक युगारम्भ से ही निरन्तर हो रहा है। परन्तु इन सब विविधताओं में भी ब्रह्मतत्त्व सदा सम अवस्था में ही बना रहता है। समस्त भौतिक पदार्थों के बनते बिगड़ते रहने पर भी इस मूल उपादान कारण के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। विचार-शक्ति का विकास होने पर यह रहस्य स्पष्ट हो जाता है।
इसी प्रकार भूगोल के अनुसार खगोल के पदार्थों का निश्चय भी विचार शक्ति कर लेती है। आकाश में ऊर्ध्वदृष्टि डालने पर सूर्य, चन्द्र, ग्रह, उपग्रह, अनन्तकोटि तेज:पुंज, तारागण, नक्षत्रमाला और धूमकेतु आदि के अविभ्रान्त सतत परिभ्रमण का बोध होता है। इस दृश्य को देखने पर जिज्ञासु- जनों के अन्तःकरण में यह जिज्ञासा सहज ही उत्पन्न हो जाती है कि 'ये सब क्या हैं? ये नित्य हैं या अनित्य ? यदि अनित्य हैं तो इनका उद्गमस्थान कहाँ है ? इन सब अस्थिर, चल पदार्थों का कोई-न-कोई स्थिर आधार होना ही चाहिये; यह स्थिर आधार कौन, कहाँ और कैसा है ?' इन जिज्ञासाओं की उत्पत्ति होने पर विचार-शक्ति विवेक करने लगती है कि ये सब सृष्टि के अन्तर्गत ही हैं। सृष्टि साकार और कार्यरूपा है। साकार पदार्थ अनादि नहीं होता। उत्पत्तिमान् होने से वह सदा रह भी नहीं सकता। उत्पन्न होने वाला कार्य का रूपान्तर होता है, अत:एव उसका नाश भी अवश्यम्भावी है। इन अस्थिर पदार्थों को नियम में बाँध रखने वाले पर ब्रह्मतत्त्व है। वही एक अविनश्वर, चिन्मात्र तत्त्व है। वही इस विनश्वर विश्व का मूलाधार है। वही इस सृष्टि का निमित्त एवं उपादान-कारण है। वही विवर्तरूप परिवर्तन के द्वारा सृष्टिरूप बन गया है। यह सृष्टिरूप कार्य सच्चा रूपान्तर नहीं है। यदि सच्चा रूपान्तर होता तो मूलतत्त्व विकारी हो जाता, फलतः संसार अद्यावधि टिक नहीं पाता।
इस मूलतत्त्व के परिमाण में कदापि न्यूनता न होने के कारण वह अव्यय है। सब प्रकार के विकारों से रहित होने के कारण अविकारी है। नाश न होने के कारण अविनाशी है। उत्पत्तिरहित होने के कारण अनादि और अन्तरहित होने के कारण अनन्त है। जो अनादि अनन्त होगा, वही त्रिकाल में समभाव से स्थित रह सकता है। इसीलिये इस तत्त्व को नित्य और सनातन कहा गया है। इस विश्व में उससे पृथक् कोई पदार्थ न होने के कारण वह अद्वैत है। जो अद्वैत है, वही निर्भय होता है; द्वैत में नीति, भेदभाव और राग- द्वेष उत्पन्न होते रहते हैं। इस प्रकार विचार-शक्ति यह निर्णय करती है कि इस सृष्टि के मूल में एक से अधिक तत्त्व नहीं हैं यह तत्त्व सर्वदा सम अवस्था में रहता है, इसलिये सत् है; प्राणिमात्र और जड सृष्टि को प्रकाश देता है, इस हेतु से उसे चित्-चेतन कहते हैं; उसी से समस्त ब्रह्माण्डों में रहने वाले जीव-समुदायों को आनन्द की प्राप्ति होती है, इसलिये वह आनन्दरूप कहलाता है। यह तत्त्व सृष्टि के बाहर भीतर सर्वत्र अवस्थित है; कोई ऐसा स्थान नहीं, जहाँ उसका प्रवेश न हो।
अत:एव वह विभु और सर्वव्यापक कहलाता है। यह ब्रह्मतत्त्व संग से रहित होने के कारण असंग, कर्तापन के अभिमान से शून्य होने के कारण अकर्ता तथा किसी भी प्रमाण (जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि) के द्वारा अवगत न होने के कारण अप्रमेय है। वह प्राणिमात्र के अन्तःकरण में अवस्थित होने के कारण अन्तरात्मा एवं सृष्टि का नियमन करने तथा सब प्रकार की शक्तियों से युक्त होने के कारण ईश्वर और परमेश्वर कहलाता है। ऐसा जो सृष्टि का मूल उपादान कारण है, उसे श्रुति भगवती ने पूर्ण कहा है-
पूर्णमदःपूर्णस्य पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।।
यह सृष्टि जिस निरुपाधिक मूल तत्त्व के एक क्षुद्र देश में अवस्थित है, वह तत्त्व पूर्ण है। इस सृष्टि के अन्तर में रहने वाला सोपाधिक तत्त्व भी पूर्ण है, क्योंकि उसका उद्भव पूर्ण तत्व से ही हुआ है। इस विश्वान्तर तत्त्व की पूर्णता को लेकर विश्वातीत तत्त्व पूर्ण ही अवशिष्ट रहता है। अस्तु, यह ब्रह्म ही जीवात्मारूप से भासमान हो रहा है, समस्त संसार ब्रह्मरूप है और अन्तःकरण में स्थित आत्मा भी ब्रह्मरूप ही है-इस असन्दिग्ध ज्ञान का उदय विचार-शक्ति के द्वारा ही होता है। जब यह संशयरहित और दृढ़ हो जाता है, तब जीव जीवन्मुक्त होकर विचरता है और अन्त में उसी तत्त्व में लीन हो जाता है। वह फिर संसार-चक्र में नहीं फँसता। इस सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः एतद्ब्रहौतमितः प्रेत्याभिसंभवितास्मीति यस्य स्यादद्धा न विचिकित्सास्तीति ह स्माह शाण्डिल्यः शाण्डिल्यः(छा० ४० ३।१४।४)
इस प्रकार विचार-शक्तिरूप साधन के द्वारा सृष्टि के मूल उपादान-कारण का आकलन होता है। इस ज्ञान को सुदृढ़ बनाने में संवेदना शक्ति के विकास को भी आवश्यकता रहती है। उसका विकास किये बिना अहंता-ममता, राग-द्वेष, आसक्ति आदि दोषों की निवृत्ति नहीं होती। इसी तरह कर्तृत्वशक्ति का विकास किये बिना निर्विघ्न और सम्यक्रूप से प्रगति नहीं हो पाती। अतः विचार- शक्तिके साथ-साथ इन दोनों शक्तियों को भी विकसित करके शास्त्रजन्य ज्ञान के साथ अनुभवरूप विज्ञानकी भी प्राप्ति कर लेनी चाहिये।
नास्तिक लोग इस विचार शक्ति का उपयोग भौतिक ज्ञान की वृद्धि के लिये करते हैं, फलतः उनसे संसार का अहित होता है। मूर्ख आस्तिक भी, जो ईश्वर और धर्म के स्वरूप को विपरीत मान लेते हैं, ईश्वर और धर्म के नाम पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर भूतकालीन क्रिश्चियन और इस्लामधर्म के उपदेशकों के विपरीत उपदेशों द्वारा अनेकों बार भयंकर नर-संहार हुआ और वर्तमान में भी हो रहा है। इसी विपरीत भावना के कारण शैव, शाक्त और वैष्णव आदि सम्प्रदायों में भी परस्पर झगड़े हुए तथा अब भी कहीं- कहीं हो जाते हैं। इन सब विरोधों का मूल कारण विचार-शक्ति के यथोचित विकास का अभाव है। जब तक अन्तःकरण मंलिन रहेगा, तब तक सदाचार या धर्म के बोध का प्रभाव नहीं पड़ सकता। अतः विवेकी सज्जनों को चाहिये कि वे अपने अन्तःकरण को निष्काम कर्म और भगवद्भक्ति द्वारा विशुद्ध बनाने के साथ-साथ परब्रह्म को प्राप्ति के लिये विचार-शक्ति का विकास करें और उसके द्वारा सच्चे सुख की प्राप्ति करें।
Related Posts
0 Comments
Comments are not available.