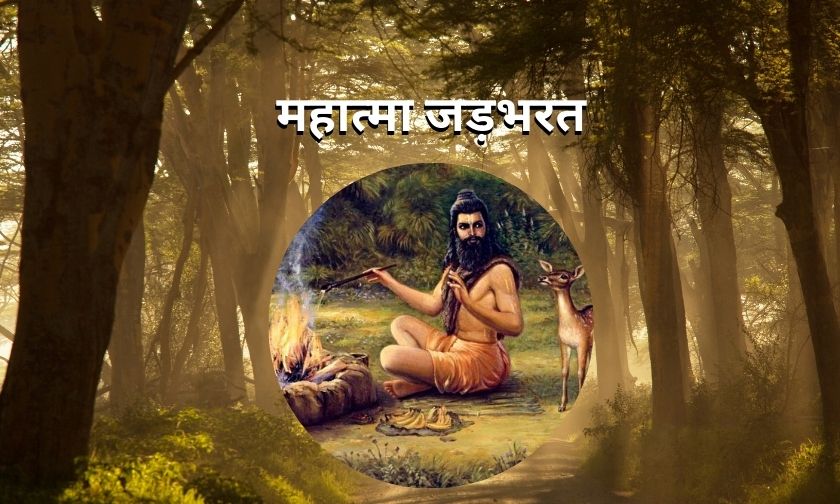- NA
- |
- 31 October 2024
- |
- 0 Comments
( श्री 'श्रोज्योतिजी')
Mystic power- साधना का अर्थ है मन को किसी विषय में एकनिष्ठ भाव से संयुक्त करना। यह जिस प्रकार किसी उत्कृष्ट विषय में किया जा सकता है, उसी प्रकार उसके विपरीत निकृष्ट विषय में भी हो सकता है। परन्तु हम यहाँ जिस साधना के विषय में कहने को प्रस्तुत हुए हैं, वह तो विश्व-ब्रह्माण्ड की सृष्टि आदि के कारण अवाङ्मनसगोचर परम तत्त्व की प्राप्ति का उपाय है। उसे व्यक्त करने के लिये जिस भाषा की आवश्यकता होती है, वह भी अव्यक्त है। मनुष्य तो अपनी भाषा के द्वारा उसे निरूपण करने का केवल प्रयत्न मात्र करता है।
'साधना' भी उस मानवी भाषा का ही एक शब्द है। इसलिये उस अव्यक्त तत्त्व का इससे भी ठीक-ठीक दिग्दर्शन नहीं हो सकता। इस साधना में प्रवृत्त होने के लिये नीति, वैराग्य एवं ज्ञानादि कुछ विशिष्ट गुणों की आवश्यकता होती है। इसका मुख्य यन्त्र मन है। अज्ञातरूप से मन सर्वदा इसी के लिये उत्सुक रहता है। समय-समय पर हम ईश्वर के लिये व्याकुल हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? कारण यही है कि मन अव्यक्तरूप से प्रभु के ही पास है, किन्तु अज्ञानवश उनसे विमुख हो रहा है। कभी-कभी कारणवश जब उस संस्कार का उद्दीपन होता है तो वह उनसे मिलने के लिये व्याकुल हो जाता है; परन्तु वह त्याग, वह वैराग्य और वह आन्तरिक व्याकुलता इस समय कहाँ है?
 संसारचक्र में पड़कर यह निरन्तर उसी में छटपटा रहा है। साधना के लिये मन की ध्यानावस्था होनी चाहिये, क्योंकि ध्यान ही साधना का प्रधान अंग है। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि ध्यान कहाँ करना चाहिये। जिसे कुछ भी पता नहीं है, उसे यह कौन बतावेगा कि किस स्थान में ध्यान करना होगा? कहते हैं कि ध्यान के लिये स्थान हृदय है। इसो को और भी स्पष्ट रूप से ऐसा कहा जा सकता है कि गुरुदेव के उपदेश के अनुसार हृदय में शब्द, ज्योति और रूप-इन तीन वस्तुओं का अनुभव करने का प्रयत्न करे। शब्द-साधन करनेसे अन्तमें एक ऐसे शब्द का अपरोक्ष अनुभव होता है, जो जीव के हृदय से लेकर प्रत्येक अणु-परमाणु में निरन्तर व्याप्त है। इस प्रकार शब्द को सिद्धि हो जाने पर शब्द में ही डूबने से एक अद्भुत ज्योतिका अनुभव होता है। वह भी उसी प्रकार सर्वव्यापक जान पड़ती है। शब्द और ज्योति-इन दोनों की उपलब्धि ध्यान से ही होती है, परन्तु इनकी एक नित्य अवस्था भी है, जो स्वयं पूर्ण ब्रह्मस्वरूपा ही है, जिसे शब्दब्रह्म और ज्योतिब्रह्म कहा जाता है। उसमें रूप नाम की कोई वस्तु नहीं है। साधक को शब्द अथवा ज्योति के ही भीतर मग्न रहना पड़ता है। यह एकमात्र चैतन्यस्वरूप अथवा शुद्ध अहंबोधस्वरूप है, परन्तु इन दोनों में एक साथ कोई भी डूबकर नहीं रह सकता। इनमें से किसी एक में ही डूबना होगा। उसमें डूबने से ब्रह्मस्वरूप में स्थिति होती है। शब्द और ज्योति का ध्यान यथार्थ भगवत्साधना का केवल रास्ता ही है। तीसरी वस्तु रूप है। शब्द और ज्योति से साधक के मन को कल्पना के अनुसार रूप की सृष्टि होती है। जिसकी जिस वस्तु या मूर्ति में निष्ठा है, उसके लिये उसी रूप या वस्तु की रचना होती है। साधारणतः जिस वस्तु की रचना शब्दब्रह्म से होती है, वह निम्न स्तर की होती है- जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी एवं लता आदि। तथा जिस वस्तु को रचना मन ज्योतिर्मय ब्रह्म से करता है, वह उच्च स्तर की होती है- जैसे ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव आदि सम्पूर्ण देववर्ग। जिस समय साधक साधना के द्वारा पूर्णत्व प्राप्त करता है, उस समय उसका इन सब सृष्टियों में अधिकार होता है। यही साधन की पूर्ण अवस्था है और यही जीव के लिये वाञ्छनीय है।
संसारचक्र में पड़कर यह निरन्तर उसी में छटपटा रहा है। साधना के लिये मन की ध्यानावस्था होनी चाहिये, क्योंकि ध्यान ही साधना का प्रधान अंग है। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि ध्यान कहाँ करना चाहिये। जिसे कुछ भी पता नहीं है, उसे यह कौन बतावेगा कि किस स्थान में ध्यान करना होगा? कहते हैं कि ध्यान के लिये स्थान हृदय है। इसो को और भी स्पष्ट रूप से ऐसा कहा जा सकता है कि गुरुदेव के उपदेश के अनुसार हृदय में शब्द, ज्योति और रूप-इन तीन वस्तुओं का अनुभव करने का प्रयत्न करे। शब्द-साधन करनेसे अन्तमें एक ऐसे शब्द का अपरोक्ष अनुभव होता है, जो जीव के हृदय से लेकर प्रत्येक अणु-परमाणु में निरन्तर व्याप्त है। इस प्रकार शब्द को सिद्धि हो जाने पर शब्द में ही डूबने से एक अद्भुत ज्योतिका अनुभव होता है। वह भी उसी प्रकार सर्वव्यापक जान पड़ती है। शब्द और ज्योति-इन दोनों की उपलब्धि ध्यान से ही होती है, परन्तु इनकी एक नित्य अवस्था भी है, जो स्वयं पूर्ण ब्रह्मस्वरूपा ही है, जिसे शब्दब्रह्म और ज्योतिब्रह्म कहा जाता है। उसमें रूप नाम की कोई वस्तु नहीं है। साधक को शब्द अथवा ज्योति के ही भीतर मग्न रहना पड़ता है। यह एकमात्र चैतन्यस्वरूप अथवा शुद्ध अहंबोधस्वरूप है, परन्तु इन दोनों में एक साथ कोई भी डूबकर नहीं रह सकता। इनमें से किसी एक में ही डूबना होगा। उसमें डूबने से ब्रह्मस्वरूप में स्थिति होती है। शब्द और ज्योति का ध्यान यथार्थ भगवत्साधना का केवल रास्ता ही है। तीसरी वस्तु रूप है। शब्द और ज्योति से साधक के मन को कल्पना के अनुसार रूप की सृष्टि होती है। जिसकी जिस वस्तु या मूर्ति में निष्ठा है, उसके लिये उसी रूप या वस्तु की रचना होती है। साधारणतः जिस वस्तु की रचना शब्दब्रह्म से होती है, वह निम्न स्तर की होती है- जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी एवं लता आदि। तथा जिस वस्तु को रचना मन ज्योतिर्मय ब्रह्म से करता है, वह उच्च स्तर की होती है- जैसे ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव आदि सम्पूर्ण देववर्ग। जिस समय साधक साधना के द्वारा पूर्णत्व प्राप्त करता है, उस समय उसका इन सब सृष्टियों में अधिकार होता है। यही साधन की पूर्ण अवस्था है और यही जीव के लिये वाञ्छनीय है।
 किसी भी प्रकार साधन के द्वारा इन तीनों (शब्द, ज्योति, रूप) में से किसी भी एक को स्वायत्त करना ही चाहिये। चाहे गुरु के उपदेश से हो, चाहे नैतिक जीवन के उत्कर्ष से-इन तीनों में से किसी एक को स्वायत्त करके उसी में डूबने से क्रमशः सत्य का मार्ग पाने की आशा की जा सकती है। हम जिस समय बालक थे, उस समय एक महापुरुष के अनुग्रह से हमने यह सब देखा था। इस सम्बन्ध में एक घटना का उल्लेख करते हैं। बहुत लोगों को यह बात विदित नहीं होगी कि महात्मागण काल्पनिक जगत् रचकर आवश्यकता होने पर अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दिखा सकते हैं। हमें भी इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ था मैंने यह प्रत्यक्ष देखा कि मैं ध्रुवलोक में पहुँच गया हूँ और वहाँ ध्रुव यह उपदेश कर रहे हैं कि उन्होंने किस प्रकार बाल्यावस्था में तपस्या करके पद्मपलाशलोचन श्रीभगवान्का साक्षात्कार किया था। मैंने देखा कि वे व्याकुल होकर कभी वन-जंगल में घूमते-घूमते और कभी एकाग्र चित्त से बैठकर भगवान्को पुकार रहे हैं। वे प्रत्येक वस्तु में चैतन्यमय श्रीहरि का अनुभव करते हुए अपने को भूल जाते हैं। यहाँ तक कि हिंसक पशुओं को देखते हैं तो उनके कण्ठ में लिपटकर भी यही कहते हैं कि क्या तुम्हीं हमारे पद्मलोचन हरि हो। जिन लोगों ने जीवन में कभी ऐसा अनुभव नहीं किया, उन्हें भाषा के द्वारा समझाया नहीं जा सकता कि यह व्याकुलता-यह छटपटाहट कैसी थी। इस प्रकार ध्रुव को प्रत्येक वस्तु में श्रीहरि का अनुभव होने पर भी स्थूल रूप में उनका दर्शन नहीं होता था। जब तक पूर्ण प्रेम का उदय नहीं होता, तब तक मूर्ति का आविर्भाव नहीं होता। अन्त में मैंने देखा कि शब्द और ज्योति को स्वायत्त करके ध्रुव उनमें डूबे हुए हैं। तब कमललोचन श्रीहरि को देखने की इच्छा होते ही ज्योति से तत्क्षण उनकी मूर्ति का विकास हो गया। उस समय ध्रुव खुले हृदय से अपने प्रियतम का दर्शन करने लगे। साथ ही मुझको भी उपदेश करते हुए कहने लगे कि जब तुम्हें ऐसी व्याकुलता और प्रीति होगी,तभी तुम उन्हें पा सकोगे। मैंने यह सब देखा तो सही, परन्तु अपने आसपास के आवरण का विचार कर निराश हो गया। उसी निराशा के साथ अभी तक अपने जीवन के क्षण बिता रहा हूँ। अतः मेरी तो ऐसी धारणा है कि महापुरुष जो सांसारिक वातावरण को छोड़कर वन-पर्वतों में चले जाते हैं, वहाँ के वातावरण का उन पर बड़ा ही अद्भुत प्रभाव पड़ता है। वहाँ शब्द में कृत्रिमता नहीं है। प्राण का स्पन्दन गम्भीर भाव से शब्द का आलोडन करता है तथा मन एकाग्र होकर इष्टसाधन में नियुक्त हो जाता है। वहाँ हिंसा की स्मृति भी नहीं होती, पूर्ण अहिंसा का भाव रहता है तथा नैतिक जीवनका विकास होने लगता है
अतः वहाँ सन प्रकार साधनायें उन्नति होनेकी सामग्री विद्यमान रहती है।
साधना की धारा पृथक् पृथक् होने पर भी अन्त में सभी को एक ही स्थान पर पहुंचना होगा। एक बात और कहनी रह गयी। भगवत्साधना में सिद्धि होने से भक्त को उनका साक्षात्कार होता है तथा उनसे मिलन हो जाता है। कोई-कोई इसी को निर्वाण या मुक्ति भी कहते हैं। यह साधन की सिद्धावस्था होनेपर भी इसमें एक ऐसी वस्तु है, जिसका कारण ढूँढ़ने पर भी नहीं मिलता। उसका नाम 'कृपा' है। ऊपर यह कहा जा चुका है कि साधना का विषय उत्कृष्ट भी हो सकता है और निकृष्ट भी। इसी प्रकार कृपा भी उत्कृष्ट और निकृष्ट दोनों ही प्रकार के पुरुषों पर हो सकती है। बहुत बार यह देखा जाता है कि जिन्हें हम घृणा की दृष्टि से देखते हैं और बहुत पतित समझते हैं, वे भी साधना में अग्रसर होकर भविष्य में उन्नति के मार्गपर चलने लगते हैं। इसी को हम 'कृपा' कहते हैं। बहुत ढूँढ़नेपर भी इसका कोई कारण नहीं मिलता। इसलिये इस विषय में कृपा के ऊपर ही निर्भर करना पड़ता है।
अन्त में कहना यह है कि ये आत्मतत्त्व या साधना-सम्बन्धी बातें लिखने का साहस करना हमारी अनधिकार चेष्टा ही है। यह विषय सदा से ही अप्रकाश्य रहा है और रहेगा भी। इसका रहस्य कभी कोई प्रकाशित कर सकेगा-ऐसी सम्भावना नहीं है, क्योंकि वह गुरुगम्य विषय है। तब भी मनुष्य का कर्तव्य है कि नीति और अहिंसा का आश्रय लेकर उनकी कृपाकी प्रतीक्षा करता रहे। यही साधना का प्रथम स्तर है। ऐसा करते-करते द्वितीय स्तर अर्थात् योगावस्था का उदय होता है। बहुत लोग अहिंसा की बात समझने पर भी नीतिका ठीक-ठीक रहस्य नहीं समझते। इसलिये यहाँ उसका कुछ उल्लेख किया जाता है। सेवा-शुश्रूषा, पिता-माता के प्रति प्रेम और ईश्वर की आज्ञा समझकर कर्तव्य का पालन-यही नीति का स्वरूप है। योगावस्था सिद्ध हो जाने पर जिस अवस्था का उदय होता है, उसका यहाँ वर्णन करने की हमारी इच्छा नहीं है। वह साधक की अपनी चीज है। तब भी इतना कह सकते हैं- 'अवाङ्मनसगोचर श्रीहरि, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो।
किसी भी प्रकार साधन के द्वारा इन तीनों (शब्द, ज्योति, रूप) में से किसी भी एक को स्वायत्त करना ही चाहिये। चाहे गुरु के उपदेश से हो, चाहे नैतिक जीवन के उत्कर्ष से-इन तीनों में से किसी एक को स्वायत्त करके उसी में डूबने से क्रमशः सत्य का मार्ग पाने की आशा की जा सकती है। हम जिस समय बालक थे, उस समय एक महापुरुष के अनुग्रह से हमने यह सब देखा था। इस सम्बन्ध में एक घटना का उल्लेख करते हैं। बहुत लोगों को यह बात विदित नहीं होगी कि महात्मागण काल्पनिक जगत् रचकर आवश्यकता होने पर अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दिखा सकते हैं। हमें भी इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ था मैंने यह प्रत्यक्ष देखा कि मैं ध्रुवलोक में पहुँच गया हूँ और वहाँ ध्रुव यह उपदेश कर रहे हैं कि उन्होंने किस प्रकार बाल्यावस्था में तपस्या करके पद्मपलाशलोचन श्रीभगवान्का साक्षात्कार किया था। मैंने देखा कि वे व्याकुल होकर कभी वन-जंगल में घूमते-घूमते और कभी एकाग्र चित्त से बैठकर भगवान्को पुकार रहे हैं। वे प्रत्येक वस्तु में चैतन्यमय श्रीहरि का अनुभव करते हुए अपने को भूल जाते हैं। यहाँ तक कि हिंसक पशुओं को देखते हैं तो उनके कण्ठ में लिपटकर भी यही कहते हैं कि क्या तुम्हीं हमारे पद्मलोचन हरि हो। जिन लोगों ने जीवन में कभी ऐसा अनुभव नहीं किया, उन्हें भाषा के द्वारा समझाया नहीं जा सकता कि यह व्याकुलता-यह छटपटाहट कैसी थी। इस प्रकार ध्रुव को प्रत्येक वस्तु में श्रीहरि का अनुभव होने पर भी स्थूल रूप में उनका दर्शन नहीं होता था। जब तक पूर्ण प्रेम का उदय नहीं होता, तब तक मूर्ति का आविर्भाव नहीं होता। अन्त में मैंने देखा कि शब्द और ज्योति को स्वायत्त करके ध्रुव उनमें डूबे हुए हैं। तब कमललोचन श्रीहरि को देखने की इच्छा होते ही ज्योति से तत्क्षण उनकी मूर्ति का विकास हो गया। उस समय ध्रुव खुले हृदय से अपने प्रियतम का दर्शन करने लगे। साथ ही मुझको भी उपदेश करते हुए कहने लगे कि जब तुम्हें ऐसी व्याकुलता और प्रीति होगी,तभी तुम उन्हें पा सकोगे। मैंने यह सब देखा तो सही, परन्तु अपने आसपास के आवरण का विचार कर निराश हो गया। उसी निराशा के साथ अभी तक अपने जीवन के क्षण बिता रहा हूँ। अतः मेरी तो ऐसी धारणा है कि महापुरुष जो सांसारिक वातावरण को छोड़कर वन-पर्वतों में चले जाते हैं, वहाँ के वातावरण का उन पर बड़ा ही अद्भुत प्रभाव पड़ता है। वहाँ शब्द में कृत्रिमता नहीं है। प्राण का स्पन्दन गम्भीर भाव से शब्द का आलोडन करता है तथा मन एकाग्र होकर इष्टसाधन में नियुक्त हो जाता है। वहाँ हिंसा की स्मृति भी नहीं होती, पूर्ण अहिंसा का भाव रहता है तथा नैतिक जीवनका विकास होने लगता है
अतः वहाँ सन प्रकार साधनायें उन्नति होनेकी सामग्री विद्यमान रहती है।
साधना की धारा पृथक् पृथक् होने पर भी अन्त में सभी को एक ही स्थान पर पहुंचना होगा। एक बात और कहनी रह गयी। भगवत्साधना में सिद्धि होने से भक्त को उनका साक्षात्कार होता है तथा उनसे मिलन हो जाता है। कोई-कोई इसी को निर्वाण या मुक्ति भी कहते हैं। यह साधन की सिद्धावस्था होनेपर भी इसमें एक ऐसी वस्तु है, जिसका कारण ढूँढ़ने पर भी नहीं मिलता। उसका नाम 'कृपा' है। ऊपर यह कहा जा चुका है कि साधना का विषय उत्कृष्ट भी हो सकता है और निकृष्ट भी। इसी प्रकार कृपा भी उत्कृष्ट और निकृष्ट दोनों ही प्रकार के पुरुषों पर हो सकती है। बहुत बार यह देखा जाता है कि जिन्हें हम घृणा की दृष्टि से देखते हैं और बहुत पतित समझते हैं, वे भी साधना में अग्रसर होकर भविष्य में उन्नति के मार्गपर चलने लगते हैं। इसी को हम 'कृपा' कहते हैं। बहुत ढूँढ़नेपर भी इसका कोई कारण नहीं मिलता। इसलिये इस विषय में कृपा के ऊपर ही निर्भर करना पड़ता है।
अन्त में कहना यह है कि ये आत्मतत्त्व या साधना-सम्बन्धी बातें लिखने का साहस करना हमारी अनधिकार चेष्टा ही है। यह विषय सदा से ही अप्रकाश्य रहा है और रहेगा भी। इसका रहस्य कभी कोई प्रकाशित कर सकेगा-ऐसी सम्भावना नहीं है, क्योंकि वह गुरुगम्य विषय है। तब भी मनुष्य का कर्तव्य है कि नीति और अहिंसा का आश्रय लेकर उनकी कृपाकी प्रतीक्षा करता रहे। यही साधना का प्रथम स्तर है। ऐसा करते-करते द्वितीय स्तर अर्थात् योगावस्था का उदय होता है। बहुत लोग अहिंसा की बात समझने पर भी नीतिका ठीक-ठीक रहस्य नहीं समझते। इसलिये यहाँ उसका कुछ उल्लेख किया जाता है। सेवा-शुश्रूषा, पिता-माता के प्रति प्रेम और ईश्वर की आज्ञा समझकर कर्तव्य का पालन-यही नीति का स्वरूप है। योगावस्था सिद्ध हो जाने पर जिस अवस्था का उदय होता है, उसका यहाँ वर्णन करने की हमारी इच्छा नहीं है। वह साधक की अपनी चीज है। तब भी इतना कह सकते हैं- 'अवाङ्मनसगोचर श्रीहरि, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो।
Related Posts
0 Comments
Comments are not available.