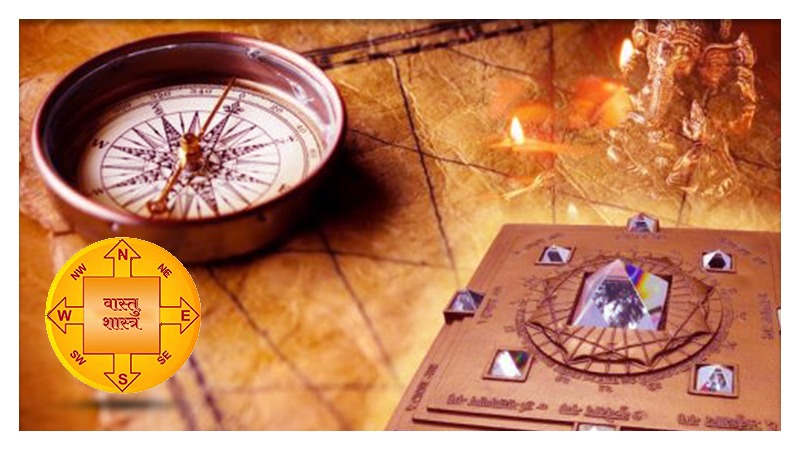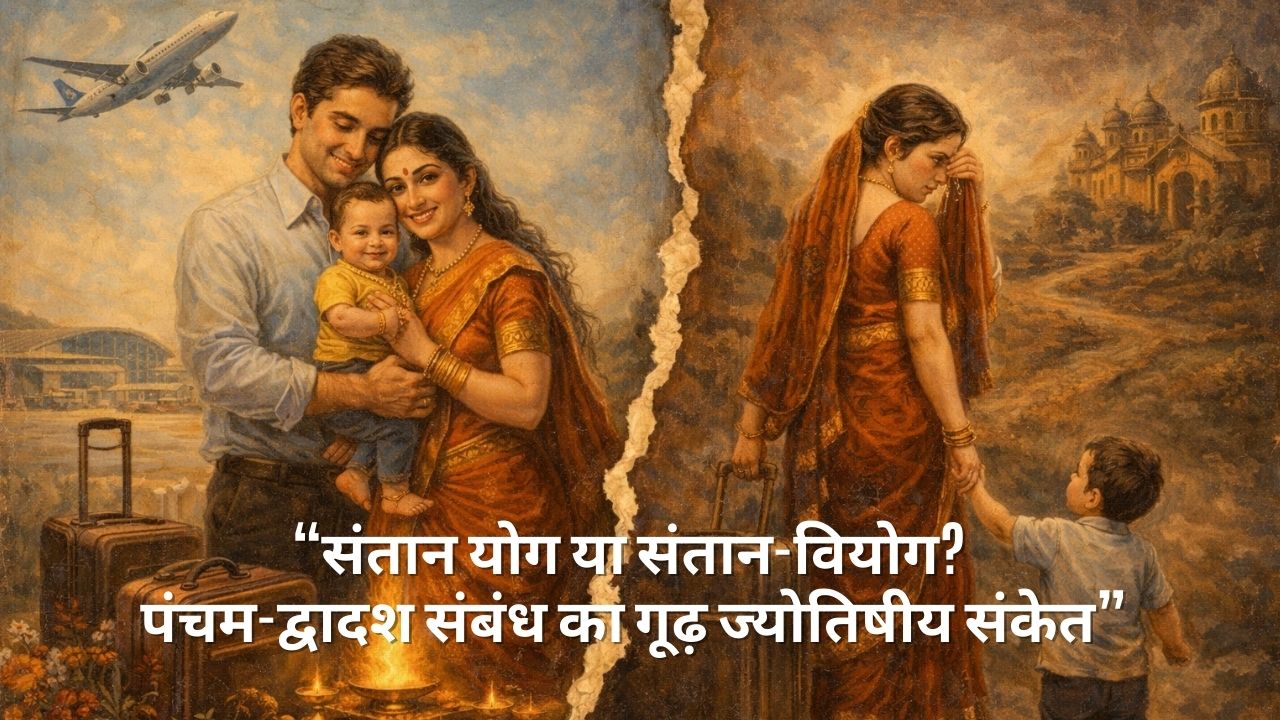- ज्योतिष विज्ञान
- |
- 31 October 2024
- |
- 0 Comments
 शिल्प और स्थापत्य के प्रवर्तक के रूप में भगवान् विश्वकर्मा का संदर्भ बहुत पुराने समय से भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञेय और प्रेय ध्येय रहा है। विश्वकर्मा को ग्रंथकर्ता मान कर अनेकानेक शिल्पकारों ने समय-समय पर अनेक ग्रंथों को लिखा और स्वयं कोई श्रेय नहीं लिया। सारा ही श्रेय सृष्टि के सौंदर्य और उपयोगी स्वरूप के रचयिता विश्वकर्मा को दिया।
उत्तरबौद्धकाल से ही शिल्पकारों के लिए वर्धकी या वढ़्ढी संज्ञा का प्रयोग होता आया है।’मिलिन्दपन्हो’ में वर्णित शिल्पों में वढ़ढ़की के योगदान और कामकाज की सुंदर चर्चा आई है जो नक्शा बना कर नगर नियोजन का कार्य करते थे।यह बहुत प्रामाणिक संदर्भ है,इसी के आसपास सौंदरानंद, हरिवंशआदि में भी अष्टाष्टपद यानी चौंसठ पद वास्तु पूर्वक कपिलवस्तु और द्वारका के न्यास का संदर्भ आया है। हरिवंश में वास्तु के देवता के रूप में विश्वकर्मा का स्मरण किया गया है।
प्रभास के देववर्धकी विश्वकर्मा यानी सोमनाथ के शिल्पिकारों का संदर्भ मत्स्य,विष्णु आदि पुराणों में आया है जिनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनकी परंपरा का स्मरण किया गया किंतु शिल्पग्रंथों में विश्वकर्मा को कभी शिव तो कभी विधाता का अंशीभूत कहा गया है। कहीं-कहीं समस्त सृष्टिरचना को ही विश्वकर्मीय कहा गया।
शिल्प और स्थापत्य के प्रवर्तक के रूप में भगवान् विश्वकर्मा का संदर्भ बहुत पुराने समय से भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञेय और प्रेय ध्येय रहा है। विश्वकर्मा को ग्रंथकर्ता मान कर अनेकानेक शिल्पकारों ने समय-समय पर अनेक ग्रंथों को लिखा और स्वयं कोई श्रेय नहीं लिया। सारा ही श्रेय सृष्टि के सौंदर्य और उपयोगी स्वरूप के रचयिता विश्वकर्मा को दिया।
उत्तरबौद्धकाल से ही शिल्पकारों के लिए वर्धकी या वढ़्ढी संज्ञा का प्रयोग होता आया है।’मिलिन्दपन्हो’ में वर्णित शिल्पों में वढ़ढ़की के योगदान और कामकाज की सुंदर चर्चा आई है जो नक्शा बना कर नगर नियोजन का कार्य करते थे।यह बहुत प्रामाणिक संदर्भ है,इसी के आसपास सौंदरानंद, हरिवंशआदि में भी अष्टाष्टपद यानी चौंसठ पद वास्तु पूर्वक कपिलवस्तु और द्वारका के न्यास का संदर्भ आया है। हरिवंश में वास्तु के देवता के रूप में विश्वकर्मा का स्मरण किया गया है।
प्रभास के देववर्धकी विश्वकर्मा यानी सोमनाथ के शिल्पिकारों का संदर्भ मत्स्य,विष्णु आदि पुराणों में आया है जिनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनकी परंपरा का स्मरण किया गया किंतु शिल्पग्रंथों में विश्वकर्मा को कभी शिव तो कभी विधाता का अंशीभूत कहा गया है। कहीं-कहीं समस्त सृष्टिरचना को ही विश्वकर्मीय कहा गया।
 विश्वकर्मावतार, विश्वकर्मशास्त्र, विश्वकर्मसंहिता, विश्वकर्माप्रकाश, विश्वकर्मवास्तुशास्त्र, विश्वकर्म शिल्पशास्त्रम्, विश्वकर्मीयम् आदि कई ग्रंथ है जिनमें विश्वकर्मीय परंपरा के शिल्पों और शिल्पियों के लिए आवश्यक सूत्रों का गणितीय रूप में सम्यक परिपाक हुआ है। इनमें कुछ का प्रकाशन हुआ है।समरांगण सूत्रधार, अपराजितपृच्छा आदि ग्रंथों के प्रवक्ता विश्वकर्मा ही हैं। ये ग्रंथ भारतीय आवश्यकता के अनुसार ही रचे गए हैं।
इन ग्रंथों का परिमाण और विस्तार इतना अधिक है कि यदि उनके पठन-पाठन की परंपरा शुरू की जाए तो बरस हो जाए। अनेक पाठ्यक्रम लागू किए जा सकते हैं। इसके बाद हमें पाश्चात्य पाठ्यक्रम के पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। यह ज्ञातव्य है कि यदि यह सामान्य विषय होता तो भारत के पास सैकड़ों की संख्या में शिल्प ग्रंथ नहीं होते।तंत्रों,यामलों व आगमों में सर्वाधिक विषय ही स्थापत्य शास्त्र के रूप में मिलता है। इस तरह से लाखों श्लोक मिलते हैं। मगर, उनको पढ़ा कितना गया। भवन की बढ़ती आवश्यकता के चलते कुकुरमुत्ते की तरह वास्तु के नाम पर किताबें बाजार में उतार दी गईं मगर मूल ग्रंथों की ओर ध्यान ही नहीं गया। इस पर लगभग सौ ग्रंथों का संपादन और अनुवाद हुआ है
भारत में गृह निर्माण के बारे में जितना नहीं लिखा,उससे कहीं ज्यादा देवालयों के निर्माण के विधान और नियमों के बारे में लिखा गया।वराहमिहिर (587 ई.) ने अपने स्तर पर देवालयों के भेदों का नामकरण किया और फिर हजारों रूप, स्वरूप, भेद, उपभेद, शैली, उपशैली में मन्दिर बने।इस कला का बहुत तेजी से विस्तार क्यों और कैसे हुआ?
अनेक ग्रंथ लिखे गए।अखंड भारत ही नहीं,तिब्बत,चीन,बर्मा, सिलोन,थाईलैण्ड,कंबोडिया,बाली तक ग्रंथ और उनके प्रयोगकर्ता सूत्रधार पहुंचे और धरातल से ऊपर अथवा धरातल से नीचे भी देवालय बनाए।
मंदिरों के निर्माण का अपना वैशिष्ट्य रहा है। युगानुसार भी और क्षेत्रानुसार भी उनका निर्माण होता रहा है। वे तल या अधिष्ठान से लेकर शिखर या स्तूपी तक अपना आकार मानव के शरीर के रचना की तरह ही अपना स्वरूप रखते हैं। उनकी सज्जा या अलंकरण का अपना खास विधान रहा है और इसके लिए शिल्पियों ने अपने कौशल को दिखाने में प्रतिस्पर्द्धा सी की है।
प्रासादों के स्वरूप के निर्णय के लिए हमें हमारे शिल्प ग्रंथों को जरूर देखना चाहिए जिनमें उनके रचनाकाल से पूर्व की परंपराओं काे लिखा गया है। मयमतं हो या मानसार या फिर शैवागमअथवा वैष्णवागम हों,उनमें प्रासादों की रचना के लिए पर्याप्त विवरण मिलता है।दक्षिण के नारायण नंबूदिरीपाद ने ‘देवालय चंद्रिका’ में प्रासादों के शिल्प के लिए निर्देश किए हैं तो सूत्रधार मंडन ने ‘प्रासादमण्डनम्’ में प्रासादों के संबंध में समग्र योजना और कार्यविधि को लिखा है।
शिल्परत्नम पर काम कर था, ग्रंथ की रचना16वीं सदी की हैं। इसमें कहा गया है 1. नागर, 2. द्राविड और 3. वेसर शैलियों के मंदिर भारत में बनते आए हैं, मगर सबका अपना अपना स्वरूप रहा है। लाख प्रयासों के बावजूद शिल्पियों ने अपने ढंग से ही मंदिरों की रचना की है।
मानव की तरह ही उनके रूप रंग में कुछ न कुछ भेद मिलता ही है। यही कारण है कि समरांगण सूत्रधार में मंदिरों के संबंध में जो विवरण है, उनको यदि नमूने के तौर पर भी बनाया जाए तो एक भारत कम पड़ जाए।ऐसा ही विस्तृत विवरण ईशान शिवगुरुदेव पद्धति में मिलता है जिसके उत्तरार्ध का क्रिया- पाद अधिकांशत: देवालयों से संबंध रखता है।
शिल्परत्नकार श्रीकुमार का मत है कि हिमालय से लेकर विंध्याचल तक सात्विक गुणों के नागर, विंध्याचल से लेकर कृष्णा तक राजस गुणों के द्रविड़ और कृष्णा से लेकर कन्यान्त तक तामस गुणों वाले वेसर शैली के प्रासादों के निर्माण की परंपरा रही है –
नागरं सात्विके देशे राजसे द्राविडं भवेत्।
वेसरं तामसे देशे क्रमेण परिर्कीतिता:।।
इसी प्रकार की मान्यताएं 8वीं सदी के ग्रंथ ‘लक्षण सार समुच्चय’ में आई हैं।
विश्वकर्मावतार, विश्वकर्मशास्त्र, विश्वकर्मसंहिता, विश्वकर्माप्रकाश, विश्वकर्मवास्तुशास्त्र, विश्वकर्म शिल्पशास्त्रम्, विश्वकर्मीयम् आदि कई ग्रंथ है जिनमें विश्वकर्मीय परंपरा के शिल्पों और शिल्पियों के लिए आवश्यक सूत्रों का गणितीय रूप में सम्यक परिपाक हुआ है। इनमें कुछ का प्रकाशन हुआ है।समरांगण सूत्रधार, अपराजितपृच्छा आदि ग्रंथों के प्रवक्ता विश्वकर्मा ही हैं। ये ग्रंथ भारतीय आवश्यकता के अनुसार ही रचे गए हैं।
इन ग्रंथों का परिमाण और विस्तार इतना अधिक है कि यदि उनके पठन-पाठन की परंपरा शुरू की जाए तो बरस हो जाए। अनेक पाठ्यक्रम लागू किए जा सकते हैं। इसके बाद हमें पाश्चात्य पाठ्यक्रम के पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। यह ज्ञातव्य है कि यदि यह सामान्य विषय होता तो भारत के पास सैकड़ों की संख्या में शिल्प ग्रंथ नहीं होते।तंत्रों,यामलों व आगमों में सर्वाधिक विषय ही स्थापत्य शास्त्र के रूप में मिलता है। इस तरह से लाखों श्लोक मिलते हैं। मगर, उनको पढ़ा कितना गया। भवन की बढ़ती आवश्यकता के चलते कुकुरमुत्ते की तरह वास्तु के नाम पर किताबें बाजार में उतार दी गईं मगर मूल ग्रंथों की ओर ध्यान ही नहीं गया। इस पर लगभग सौ ग्रंथों का संपादन और अनुवाद हुआ है
भारत में गृह निर्माण के बारे में जितना नहीं लिखा,उससे कहीं ज्यादा देवालयों के निर्माण के विधान और नियमों के बारे में लिखा गया।वराहमिहिर (587 ई.) ने अपने स्तर पर देवालयों के भेदों का नामकरण किया और फिर हजारों रूप, स्वरूप, भेद, उपभेद, शैली, उपशैली में मन्दिर बने।इस कला का बहुत तेजी से विस्तार क्यों और कैसे हुआ?
अनेक ग्रंथ लिखे गए।अखंड भारत ही नहीं,तिब्बत,चीन,बर्मा, सिलोन,थाईलैण्ड,कंबोडिया,बाली तक ग्रंथ और उनके प्रयोगकर्ता सूत्रधार पहुंचे और धरातल से ऊपर अथवा धरातल से नीचे भी देवालय बनाए।
मंदिरों के निर्माण का अपना वैशिष्ट्य रहा है। युगानुसार भी और क्षेत्रानुसार भी उनका निर्माण होता रहा है। वे तल या अधिष्ठान से लेकर शिखर या स्तूपी तक अपना आकार मानव के शरीर के रचना की तरह ही अपना स्वरूप रखते हैं। उनकी सज्जा या अलंकरण का अपना खास विधान रहा है और इसके लिए शिल्पियों ने अपने कौशल को दिखाने में प्रतिस्पर्द्धा सी की है।
प्रासादों के स्वरूप के निर्णय के लिए हमें हमारे शिल्प ग्रंथों को जरूर देखना चाहिए जिनमें उनके रचनाकाल से पूर्व की परंपराओं काे लिखा गया है। मयमतं हो या मानसार या फिर शैवागमअथवा वैष्णवागम हों,उनमें प्रासादों की रचना के लिए पर्याप्त विवरण मिलता है।दक्षिण के नारायण नंबूदिरीपाद ने ‘देवालय चंद्रिका’ में प्रासादों के शिल्प के लिए निर्देश किए हैं तो सूत्रधार मंडन ने ‘प्रासादमण्डनम्’ में प्रासादों के संबंध में समग्र योजना और कार्यविधि को लिखा है।
शिल्परत्नम पर काम कर था, ग्रंथ की रचना16वीं सदी की हैं। इसमें कहा गया है 1. नागर, 2. द्राविड और 3. वेसर शैलियों के मंदिर भारत में बनते आए हैं, मगर सबका अपना अपना स्वरूप रहा है। लाख प्रयासों के बावजूद शिल्पियों ने अपने ढंग से ही मंदिरों की रचना की है।
मानव की तरह ही उनके रूप रंग में कुछ न कुछ भेद मिलता ही है। यही कारण है कि समरांगण सूत्रधार में मंदिरों के संबंध में जो विवरण है, उनको यदि नमूने के तौर पर भी बनाया जाए तो एक भारत कम पड़ जाए।ऐसा ही विस्तृत विवरण ईशान शिवगुरुदेव पद्धति में मिलता है जिसके उत्तरार्ध का क्रिया- पाद अधिकांशत: देवालयों से संबंध रखता है।
शिल्परत्नकार श्रीकुमार का मत है कि हिमालय से लेकर विंध्याचल तक सात्विक गुणों के नागर, विंध्याचल से लेकर कृष्णा तक राजस गुणों के द्रविड़ और कृष्णा से लेकर कन्यान्त तक तामस गुणों वाले वेसर शैली के प्रासादों के निर्माण की परंपरा रही है –
नागरं सात्विके देशे राजसे द्राविडं भवेत्।
वेसरं तामसे देशे क्रमेण परिर्कीतिता:।।
इसी प्रकार की मान्यताएं 8वीं सदी के ग्रंथ ‘लक्षण सार समुच्चय’ में आई हैं।
Related Posts
- ज्योतिष विज्ञान
- |
- 18 February 2026
“संतान योग या संतान-वियोग? पंचम-द्वादश संबंध का गूढ़ ज्योतिषीय संकेत”
0 Comments
Comments are not available.