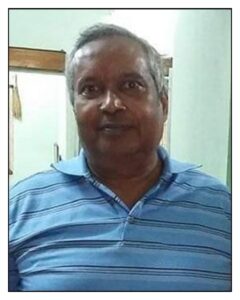- धर्म-पथ
- |
-
31 October 2024
- |
- 0 Comments
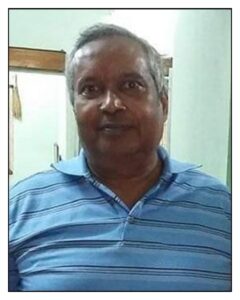
अरुण कुमार उपाध्याय (धर्मज्ञ)
१. निःश्वसित वेद-
एवं वा अरेऽस्य महतोभूतस्य निःश्वसितं एतत् यत् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ऽथर्वाङ्गिरस इतिहास पुराण विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राणि अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि अस्यैव एतानि निःश्वसितानि।
(
बृहदारण्यक उपनिषद्, २/४/१०)
जाकी सहज स्वास श्रुति चारी। सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी॥
(रामचरितमानस, बालकाण्ड, २०३/४)
स्पष्टतः यह उस वेद के बारे में नहीं है जिसकी १५ संहिता तथा अनेक ब्राह्मण ग्रन्थ उपलब्ध हैं। उपनिषद् में संहिता-ब्राह्मण सहित इतिहास, पुराण, विद्या, सूत्र, व्याख्यान आदि को भी परब्रह्म का निःश्वास कहा है। ये जीवित व्यक्ति नहीं हैं, जो श्वास लें।
वेद विश्व को जानने का साधन है। इस प्रकार यह वाक्-अर्थ प्रतिपत्ति है।
यावद् ब्रह्म विष्ठति तावती वाक्
(ऋक्, १०/११४/८, अथर्व, १/३/८/८)
अस्माकमग्रे मघवत्सु दीदिह्यध श्वसीवान् वृषभो समूनाः।
अवास्या शिशुमतीरदीदेर्वर्मेव युत्सु पर्जर्भुराणः॥
(ऋक्, १/१४०/१०)
द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परं च यत् ।
शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परंब्रह्माधिगच्छति ॥
(मैत्रायणी उपनिषद् ६/२२)
इयं या परमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्म संशिता।
(अथर्व १९/९/३)
वाचीमा विश्वा भुवनानि अर्पिता
(तैत्तिरीय ब्राह्मण, २/८/८/४)
वागिति पृथिवी, वागित्यन्तरिक्षं, वागिति द्यौः।
(जैमिनीय ब्राह्मण उपनिषद्, ४/२२/११)
विश्व रूप में वेद पुरुष कहा है, वाक् रूप में स्त्री या देवी-
शब्दात्मिकां सुविमलर्ग्यजुषां निधानमुद्गीथ रम्य पद-पाठवतां च साम्नाम्।
देवी त्रयी भगवती भव भावनाय वार्ता च सर्व जगतां परमार्ति हन्त्री॥
(दुर्गा सप्तशती, ४/१०)
अर्थ (जगत्) और वाक् (शब्द) में प्रतिपत्ति (सामञ्जस्य) को विश्व-वेद या जातवेद (जिसका जन्म हुआ) कहा है-
अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं निरञ्जनम्। विवर्त्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥
(वाक्यपदीय, ब्रह्मकाण्ड, १)
जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेदः।
(महानारायण उपनिषद् ६/२, ऋक् १/९९/१)
त्वं सोम क्रतुभिः सुक्रतुर्भूस्त्वं दक्षैः सुदक्षो विश्ववेदाः।
(ऋक् १/९१/२)
विश्वा अपश्यद् बहुधा ते अग्ने जातवेदस्तन्वो देव एक।
(ऋक् १०/५१/१)
२. श्वास-
मनुष्य या अन्य जीवों का श्वास एक चक्रीय क्रिया है जिसमें वायु ग्रहण कर उसके उपयोगी भाग से शरीर में भोजन के पाचन आदि क्रिया कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और काम करते हैं। जलचर जीव जल से ही विलीन वायु ग्रहण कर काम करते हैं। इस प्रकार चक्रीय क्रम में उत्पादन होता है, जिसे गीता में यज्ञ कहा है।
गीता, अध्याय ८ में विश्व का ३ प्रकार से वर्णन है-
(१) ब्रह्म-जो कुछ भी सृष्टि में है वह ब्रह्म है-निर्माता + निर्माण। सर्वं खलु इदं ब्रह्म (छान्दोग्य उपनिषद्, ३/१४/१)
(२) कर्म-जो भी गति है, अर्थात् कणों पिण्डों का स्थान परिवर्तन, वह कर्म है। आन्तरिक गति दीखती नहीं है, वह कृष्ण गति है, बाह्य गति शुक्ल है। मृत्यु के बाद प्रेत पृथ्वी सीमा में रह जाता है वह कृष्ण गति है, बाह्य लोकों में गति शुक्ल है। इस परिवर्तन के आभास से काल का अनुभव होता है।
(३) यज्ञ-चक्रीय क्रम में उपयोगी वस्तु का निर्माण यज्ञ है।
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। अनेन प्रसविध्यष्वमेषवोऽस्त्विष्टकामधुक्॥ (गीता ३/१०)
एवं प्रवर्तितं चक्रं … (गीता ३/१६)
इस चक्र की पूर्ति से काल की माप होती है, जैसे प्राकृतिक कालमान हैं-दिन, मास, वर्ष।
सृष्टि के विभिन्न चक्रीय क्रियाओं का ज्ञान निःश्वसित वेद है।
३. वेद तथा विभाग-
वेद का अर्थ ज्ञान है, अर्थात् किसी वस्तु का अनुभव, या उसके कारण परिवर्तन का ज्ञान। हर विन्दु का कुछ गुण है। विन्दु आकाश चित् है। उसमें सर्वव्यापी मूल रस या आनन्द है। उसका कुछ भाग अनुभव योग्य है, वह सत् है। यह सच्चिदानद (सत् + चित् + आनन्द) स्वरूप ब्रह्म है। जैसा ब्रह्म वैसा वेद है, यह अनन्त तथा मुख्यतः अज्ञेय है। ज्ञेय भाग सत् है। ज्ञेय भाग का भी तभी ज्ञान होगा यदि उसकी महिमा (प्रभाव, गुरुत्व बल, विकिरण, ताप आदि) द्रष्टा तक पहुंचे। इस ज्ञेय का भी पूर्ण ज्ञान सम्भव नहीं है। कुछ हमारे निरीक्षण की सीमा है, यन्त्र द्वारा या बिना यन्त्र के। कुछ पद्धति या निष्कर्ष की भूल है। वस्तु में कुछ परिवर्तन हमारे निरीक्षण द्वारा भी हो रहा है। अतः पूर्ण ज्ञान के बदले परिज्ञान होगा। यह ज्ञान प्राप्ति का कर्म है जिसके ३ स्तर गीता में कहे हैं-
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना (गीता, १८/१८)
हर विन्दु या कण की स्थिति ऋक् है, उसकी गति या परिवर्तन यजु है। मूल स्थिति में परिवर्तन का क्रम इतिहास है, उसका कारण या परिवर्तन का यज्ञ समझना पुराण है (पुरा + नवति = पुराना नया कैसे हो रहा है-निरुक्त, ३/१९)। वस्तु की महिमा साम है। इनका आधार या सन्दर्भ सनातन ब्रह्म या विश्व है जो अथर्व है। थर्व = थरथराना, अथर्व = स्थिर, सनातन।
ऋग्भ्यो जातां सर्वशो मूर्त्तिमाहुः, सर्वा गतिर्याजुषी हैव शश्वत्।
सर्वं तेजं सामरूप्यं ह शश्वत्, सर्वं हेदं ब्रह्मणा हैव सृष्टम्॥ (तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३/१२/८/१)
ऋच सामानि छन्दांसि पुराण यजुषा सह।
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रिता॥ (अथर्व, ११/७/२५)
ब्रह्म का मूल क्रियात्मक रूप पुराण है-
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् (गीता, ११/३८)
४. शब्द वेद का श्वास-
वेद के सिद्धान्त सनातन हैं- सृष्टि के आरम्भ से वर्तमान और भविष्य काल तक। किन्तु उनका शब्द रूप में वर्णन सनातन नहीं है। सृष्टि कई प्रकार की है, अव्यक्त से व्यक्त, ब्रह्माण्ड निर्माण, तारा, ग्रह उत्पत्ति, वनस्पति, जीव, मनुष्य, सभ्यता तथा लिपि भाषा का विकास। भाषा स्थिर तथा सर्व सम्मत होने पर ही शब्दरूप वेद सम्भव है। सभ्यता के हर विकास का क्रम एक कल्प है। प्रत्येक कल्प में मुनियों द्वारा वेद सृष्टि होती है जैसा पूर्व उद्धृत अथर्व (११/७/२५) में कहा है-पुराने कल्प के उच्छिष्ट से वर्तमान कल्प में देव तथा सभी वेद हुए। यही बात पुराणों तथा वेद में कही है-
प्रतिमन्वन्तरं चैव श्रुतिरन्या विधीयते। ऋचो यजूंषि सामानि यथावत् प्रतिदैवतम्॥५८॥
विधिहोत्रं तथा स्तोत्रं पूर्ववत् सम्प्रवर्तते। द्रव्यस्तोत्रं गुणस्तोत्रं कर्मस्तोत्रं तथैव च॥५९॥
तथैवाभिजनस्तोत्रं स्तोत्रमेवं चतुर्विधम्। मन्वन्तरेषु सर्वेषु यथाभेदा भवन्ति हि॥६०॥
प्रवर्तयन्ति तेषां वै ब्रह्मस्तोत्रं पुनः पुनः। एवं मन्त्रगुणानां तु समुत्पत्तिश्चतुर्विधम्॥६१॥
अथर्व-ऋग्-यजुःसाम्नां वेदेष्विह पृथक् पृथक्। ऋषीणां तपुयतां तेषां तपः परमदुष्चरम्॥६२॥
मन्त्रः प्रादुर्भवन्त्यादौ पूर्वमन्वन्तरस्य ह। असन्तोषाद् भयाद् दुःखान्मोहाच्छोकाच्च पञ्चधा॥६३॥
(मत्स्य पुराण, अध्याय १४५)
पुराणं सर्व शास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्। अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः॥३॥
(मत्स्य पुराण, अध्याय ५३)
पुराने, मध्यम और नये सूक्त-
यज्ञेनेन्द्रमवसा चक्रे अर्वागेन सुम्नाय नव्यसे ववृत्याम्।
यः स्तोमेभिर्वावृधे पूर्व्येभिर्यो मध्यमेभिरुत नूतनेभिः॥ (ऋक्, ३/३२/१३)
इयं ते पूषन्नाघृणे सुष्टुतिर्देव नव्यसी। अस्माभिस्तुभ्यं शस्यते॥ (ऋक्, ३/६२/७)
नृ नव्यसे नवीयसे सूक्ताय साधया पथः। प्रत्नवद्रोचया रुचः॥ (ऋक्, ९/९/८)-
ऋषे मन्त्रकृतां स्तोमैः कश्यपोद्वर्धयन् गिरः।
सोमं नमस्य राजानं यो यज्ञे वीरुधां पतिः इन्द्रायेन्द्रो परि स्रव॥ (ऋक्, ९/११४/२)
५. मनुष्य श्वास-
चार वेदों की तरह मनुष्य श्वास के ४ भाग हैं-पूरक, अन्तः कुम्भक, रेचक, बाह्य कुम्भक। यह आन्तरिक यज्ञ है, अतः इस रूप में यजुर्वेद प्रथम है। इसका कुम्भक ऋक् है। रेचक बाह्य प्रभाव करता है, वह साम है। शरीर या वक्ष अथर्व है जिसमें श्वास क्रिया हो रही है।
विद्याश्च वा अविद्याश्च यच्चान्यदुपदेश्यम्।
शरीरं ब्रह्म प्राविशत् ऋचः सामाथो यजुः। (अथर्व, ११/८/२३)
श्वास सम्बन्धित कई यज्ञ गीता में कहे हैं-
दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति॥२५॥
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति॥२६॥
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते॥२७॥
द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे। स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः॥२८॥
अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे। प्राणापानगती रुद्ध्वा प्रणायामपरायणाः॥२९॥
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्वति। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः॥३०॥
(गीता, अध्याय, ४)
(१) ब्रह्म यज्ञ- सभी आधार, निर्माण, निर्माता आदिको ब्रह्म समझना। इस आशय का मन्त्र भोजन के समय पढ़ते हैं-
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् । ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना॥ (गीता, ४/२४)
(२) दैव यज्ञ-ऊर्जा का जो भाग निर्माण करता है, वह देव है-
ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देव दानवाः।
देवेभ्यश्च जगत् सर्वं चरं स्थाण्वनुपूर्वशः॥ (मनु स्मृति, ३/२०१)
आन्तरिक और बाह्य देवों का परस्पर पोषण दैव यज्ञ है-
देवान् भावयतानेनं ते देवा भावयन्तु वः ।
परस्परं भावयन्तः श्रेयं परमवाप्स्यथ ॥ (गीता, ३/११)
(३) ब्रह्माग्नि यज्ञ-एक यज्ञ से दूसरे का पोषण। सभी यज्ञ परस्पर की सहायता करेंगे तो पूरे विश्व की उन्नति होगी-
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ।
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ (पुरुष-सूक्त, यजुर्वेद ३१/१६)
(४) संयम यज्ञ-विषयों से आकर्षित होकर मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है। बेकार कामों से अपनी शक्ति हटाना प्रत्याहार है। उसे मुख्य कार्य में लगाना धारणा है। धारणा लगातार बनाये रखना ध्यान है। मस्तिष्क को शान्त रखना समाधि है। इन तीनों-धारणा, ध्यान, समाधि-का संयोग कर कार्य करना संयम है।
(५) इन्द्रिय यज्ञ-यह संयम यज्ञ से सम्बन्धित है। उसका एक साधन होने पर भी यह अपने आप में यज्ञ है जिससे शरीर स्वस्थ, कार्यक्षम बनता है तथा सभी प्रकार के यज्ञ पूरे किये जा सकते हैं। इसके लिये ज्ञानेन्द्रियों के ५ गुणों को अपने विषयों से दूर करते हैं- शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध।
(६) प्राण-कर्म यज्ञ-५ प्राण और ५ उप-प्राण हैं, जो शरीर अंगों की क्रियाओं से सम्बन्धित हैं। प्राणों का कर्म जानने पर उनको आत्म-संयम की अग्नि में जलाते हैं। इन्द्रियों और उनके प्राणों में समन्वय रख कर उनका अधिकतम उपयोग हो सकता है।
(७) तपो यज्ञ- साधना के लिये परिश्रम और कष्ट सहना, नियमित रूप से कार्य।
(८) योग यज्ञ-योग का अर्थ है जोड़ना। शरीर में श्वास और क्रिया को जोड़ना योग है। इसके ८ स्तरों के बाद अन्ततः आत्मा और परमात्मा का योग होता है-(१) यम, (२) नियम, (३) आसन, (४) प्राणायाम, (५) प्रत्याहार, (६) धारणा, (७) ध्यान, (८) समाधि।
(९) स्वाध्याय यज्ञ-नियमित अध्ययन, चिन्तन और ध्यान द्वारा अपनी मानसिक शक्ति का विकास और ज्ञान पाना स्वाध्याय यज्ञ है।
(१०) ज्ञान यज्ञ-समाज में शिक्षा व्यवस्था, ज्ञान परम्परा को चलाना और विकास ज्ञान यज्ञ है। यह गुरु-शिष्य परम्परा से आगे बढ़ता है। स्वाध्याय व्यक्ति के लिये है, यह समाज के लिये।
(११) प्राणायाम यज्ञ-श्वास नियन्त्रण के रूप में यह योग यज्ञ का चतुर्थ अंग है। यहां इसका अर्थ है कि कम से कम साधन द्वारा शरीर को शक्तिशाली और उपयोगी बनाया जाय। शरीर में शक्ति के लिये भोजन लेना और उसका पाचन जरूरी है। यह प्राण का अपान में हवन है। अपान वायु से पाचन होकर मल निष्कासन होता है। किन्तु शरीर में भोजन सञ्चित करने से ही कोई लाभ नहीं है। जैसे नियमित भोजन जरूरी है, नियमित रूप से कुछ शक्ति खर्च कर काम करना भी जरूरी है। यह अपान का प्राण में हवन है।
(१२) प्राण यज्ञ- यह प्राण का अपान में तथा अपान का प्राण में हवन है तथा नियत आहार द्वारा प्राण का प्राण में हवन है-
अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे। प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः॥
अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। (गीता, ४/२९-३०)
६. मनुष्य का जन्म मृत्यु चक्र-
सायण ने ऋक् सूक्त (१/१४०) को पुनर्जन्म विषयक सूक्त माना है। अन्य कई स्थानों पर पुनर्जन्म के वर्णन हैं।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने ‘सत्यार्थ प्रकाश’ के नवम समुल्लास में आवागमनीय पुनर्जन्म की धारणा का प्रतिपादन करते हुए लिखा है-पूर्व जन्म के पुण्य-पाप के अनुसार वर्तमान जन्म और वर्तमान तथा पूर्व जन्म के कर्मानुसार भविष्यत् जन्म होते हैं। (९/७३)। इसी समुल्लास में कर्म के अनुसार मरणोपरान्त गति का भी वर्णन है।
अपनी पुस्तक ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के पुनर्जन्म अध्याय में कई वेद मन्त्रों को पुनर्जन्म सिद्धान्त के समर्थन में उद्धृत किया है-
ऋग्वेद, (१०/५९/६, ७, १/१२१/१-२), यजुर्वेद (४/१५, १९/४७), अथर्ववेद (७/६/६७/१, ५/१/१/२, १०/८/२७-२८, ११/८/३३)
अन्य प्रवचनों में उन्होंने न्याय, योग दर्शन, गीता द्वारा पुनर्जन्म की व्याख्या की है।
न्याय, वैशेषिक, वेदान्त दर्शनों में तर्क द्वारा पुनर्जन्म का समर्थन किया है। पर इसका प्रायोगिक प्रमाण नहीं है। कई लोगों को पूर्व जन्म की कुछ स्मृति रहती है। पतञ्जलि के योग सूत्र में पूर्व जन्म की स्मृति के लिए विधि कही है कि संस्कार पर संयम करने से जाति-स्मरण होता है (योग सूत्र, ३/१८)। इसमें कई सन्देह हैं जिनको जानने की कोई प्रायोगिक विधि नहीं है। मृत्यु के बाद क्या शेष रहता है, वह कहां जाता है, पुनर्जन्म में संस्कार तथा स्मृति कैसे अगले जीवन में जाते हैं।
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने पुनर्जन्म माना है, ३ प्रकार की लोकोत्तर गति भी कही है, किन्तु पितर और उनका श्राद्ध नहीं मानते हैं
बौद्ध लोग आत्मा का अस्तित्व नहीं मानते पर १०० जन्मों तक सिद्धार्थ बुद्ध की क्रमशः उन्नति के लिए जातक कथायें लिखीं। यदि आत्मा या पितर नहीं हैं तो किसका पुनर्जन्म हो रहा है।
एक धारणा है कि १०० जन्मों तक मनुष्य के संस्कार या कर्म फल जा सकते हैं, जैसा भीष्म पितामह ने कहा था कि उनको १०० जन्मों की स्मृति है किन्तु शरशय्या के पाप का स्मरण नहीं है। यजुर्वेद की १०१ शाखा मानी जाती हैं या हृदय से १०१ नाड़ियों का उद्गम मानते हैं जिनमें एक ब्रह्म रन्ध्र से मुक्ति होती है, अन्य से पुनर्जन्म (कठोपनिषद्, ६/१६)।
७. सृष्टि चक्र-
ज्योतिष में गणना के लिए ९ कालमान हैं, जो सृष्टि के विभिन्न स्तरों के निर्माण चक्र हैं। हमारी गणना ब्रह्माण्ड या गैलेक्सी तक ही सीमित है। यह सबसे बड़ी ईंट होने के कारण परमेष्ठी मण्डल है। ब्रह्माण्ड की परिक्रमा करने में पृथ्वी को अपनी मध्यम कक्षा गति से जितना समय लगेगा, उसे ब्रह्मा का दिन कहते हैं, जो १००० युग = ४३२ करोड़ वर्ष है। इतने ही समय की रात्रि होगी। ब्रह्मा के दिन-रात (८६४ कोटि वर्ष) में प्रकाश जितनी दूर जाता है, वह तपः लोक है। यहां तक का प्रकाश हम तक पहुंच सकता है। आधुनिक विज्ञान में इसे दृश्य जगत् कहते हैं। इसके बाहर क्या है, यह जानना सम्भव नहीं है। ब्रह्मा के दिन में सृष्टि होती है, रात्रि में पुनः अव्यक्त में लय होता है। पूरी सृष्टि कभी समाप्त नहीं होती। सदा १/४ भाग सृष्टि बनी रहती है, बाकी ३/४ भाग अव्यक्त रस रूप विश्व स्थिर है। सभी ४ पाद मिलाकर पूरुष (दीर्घ पू) कहा गया है।
एतावानस्य महिमा अतो ज्यायाँश्च पूरुषः।
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥ (पुरुष सूक्त, वाज यजु, ३१/३)
भास्कराचार्य ने कहा है कि ब्रह्मा के दिन या कल्प में पृथ्वी हर दिशा में १ योजन बढ़ जाती है। यहां पृथ्वी तथा योजन का अर्थ सन्दिग्ध है।
वृद्धिर्विधेरह्नि भुवः समन्तात् स्याद्योजनं भूभवभूतपूर्वैः।
ब्राह्मे लये योजनमात्र वृद्धॆर्नाशो भुवः प्राकृतिकेऽखिलायाः॥
(सिद्धान्त शिरोमणि, गोलाध्याय, भुवनकोष, ६२)
वेद तथा पुराण में ३ पृथ्वी और ३ आकाश कहा गया है जिनको ३ माता तथा ३ पिता कहा है।
तिस्रो भूमीर्धारयन् त्रीरुत द्यून्त्रीणि व्रता विदथे अन्तरेषाम् ।
ऋतेनादित्या महि वो महित्वं तदर्यमन् वरुण मित्र चारु ॥ (ऋग्वेद, २/२७/८)
रवि चन्द्रमसोर्यावन्मयूखैरवभास्यते। स समुद्र सरिच्छैला पृथिवी तावती स्मृता॥
यावत्प्रमाणा पृथिवी विस्तार परिमण्डलात्।
नभस्तावत्प्रमाणं वै व्यास मण्डलतो द्विज॥
(विष्णु पुराण, २/७/३-४)
पहली पृथ्वी हमारा ग्रह है जो सूर्य-चन्द्र दोनों से प्रकाशित है। दूसरी पृथ्वी सूर्य प्रकाश का क्षेत्र है जहां तक उसका प्रकाश ब्रह्माण्ड से अधिक है। सबसे बड़ी पृथ्वी ब्रह्माण्ड है जिसकी सीमा तक सूर्य विन्दु रूप में दीख सकता है। सम्पूर्ण पृथ्वी ही आकाश के लिए मापदण्ड है, अतः ब्रह्मा के दिन में इसका विस्तार २ गुणा हो जाता है, रात्रि में वापस अपने मूल आकार में आ जाता है। ८६४ कोटि वर्ष का विस्तार और संकोच ही महत भूत का निःश्वास है। विष्णु के २४ अवतारों में एक ऋषभदेव के विषय में ऐसी ही गणना की गयी। भगवती सूत्र के अनुसार उन्होंने ५३ पूर्वा या वर्ष शासन किया था। उनकी १ श्वास (४ सेकण्ड) को ब्रह्म श्वास ८६४ कोटि वर्ष मानें तो ५३ वर्ष का राज्य काल १०० कोटि x कोटि (कोड़ा-कोड़ी) वर्ष होगा, जो विश्व की आयु का १०,००० गुणा हो जाता है।
किसी भी चक्र के इन विपरीत भागों को चान्द्र मास की तरह दर्श-पूर्ण मास, निकट-दूर गति के कारण अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी, संकोच-प्रसार के अर्थ में उद्ग्राभ-निग्राभ कहा गया है।
उत्सर्पिणी युगार्धं पश्चादपसरिणी युगार्धं च। मध्ये युगस्य सुषमाऽऽदावन्ते दुष्षमेन्दूच्चात्॥ (आर्यभटीय, कालक्रियापाद २/९)
तद्यदेना उरसि (इन्द्रः) न्यग्रहीत तस्मान्निग्राभ्या नाम।
(शतपथ ब्राह्मण ३/९/४/१५)
उद्ग्राभेणोदग्रभीत् (वाज.यजु.१७/६३, तैत्तिरीय संहिता १/१/१३/१, ६/४/२, ४/६/३/४, मैत्रायणी संहिता १/१/१३, ८/१३, ३/३/८, ४१/९, काण्व संहिता १/१२, १८/३, २१/८, शतपथ ब्राह्मण ९/२/३/२१)
एष वै पूर्णिमाः। य एष (सूर्यः) तपत्यहरहर्ह्येवैश पूर्णोऽथैष एव दर्शो यच्चन्द्रमा ददृश इव ह्येषः। अथोऽइतरथाहुः। एष एव पूर्णमा यच्चन्द्रमा एतस्य ह्यनु पूरणं पौर्णमासीत्याचक्षते ऽथैष एष दर्षो य एष (सूर्यः) तपति ददृश इव ह्येषः। (शतपथ ब्राह्मण ११/२/४/१-२) सवृत (= चक्रीय) यज्ञो वा एष यद्दर्शपूर्णमासौ।
(गोपथ उत्तर २/२४)
दर्शपूर्णमासौ वा अश्वस्य मेध्यस्य पदे।
(तैत्तिरीय ब्राह्मण ३/९/२३/१)
सभी पृथ्वी-द्यौ में वेद यज्ञ चल रहा है-
सामाहमस्मि ऋक् त्वं द्यौरहं पृथिई त्वम्।
ताविह सम्भवाव प्रजामा जनयावहै॥ (अथर्व, १४/२/७१)
८. ब्रह्माण्ड यज्ञ-
ब्रह्माण्ड तथा सौर मण्डल में आकर्षण (भृगु) तथा विकिरण (अङ्गिरा या अङ्गारा) से सृष्टि हो रही है।
आपो भृग्वङ्गिरो रूपमापो भृग्वङ्गिरोमयम्।
सर्वमापोमयं भूतं सर्वं भृग्वङ्गिरोमयम्।
अन्तरैते त्रयो वेदा भृगूनङ्गिरसोऽनुगाः॥
(गोपथ ब्राह्मण, पूर्व, २/३९)
सौर मण्डल के भीतर भी त्रयी विद्या से सृष्टि हो रही है-
यदेतन्मण्डलं तपति-तत् महदुक्थं, ता ऋचः, स ऋचां लोकः। अथ यदेतत् अर्चिः दीप्यते-तत् महाव्रतं, तानि सामानि, स साम्नां लोकः। अथ य एव एतस्मिन् मण्डले पुरुषः- सो अग्निः; तानि यजूंषि, स यजुषां लोकः। सैषा त्रय्येव विद्या तपति।
(शतपथ ब्राह्मण, १०/५/२/१-२)
सूर्य का मण्डल ऋक् ह, उसका तेज प्रसार साम है, चेतन पुरुष क्रिया यजु है।